समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषतायें | समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार | सिद्धांत एवं अनुसंधान में संबंध व परस्पर निर्भरता
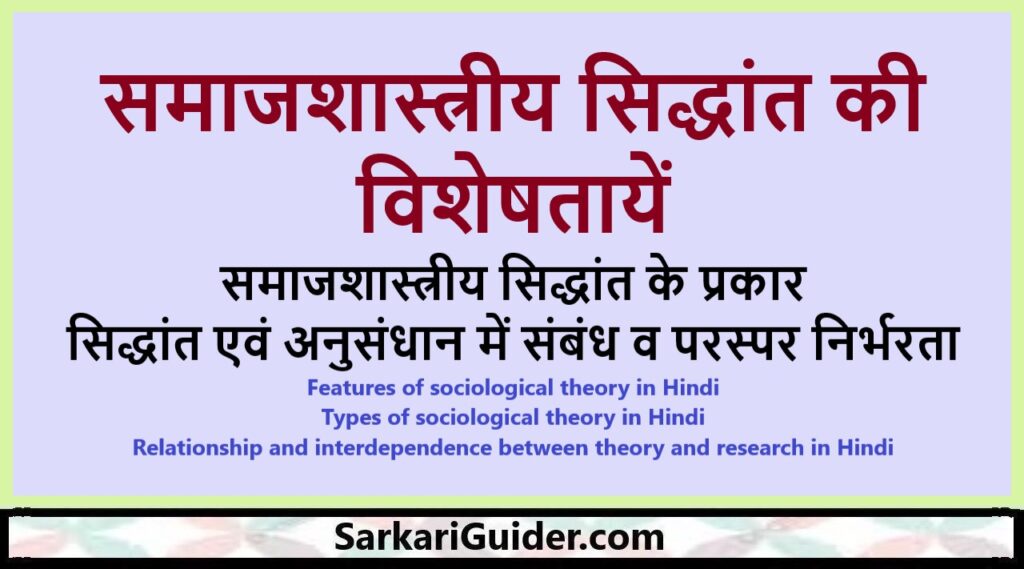
समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषतायें | समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार | सिद्धांत एवं अनुसंधान में संबंध व परस्पर निर्भरता | Features of sociological theory in Hindi | Types of sociological theory in Hindi | Relationship and interdependence between theory and research in Hindi
समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषतायें
(Characteristics of Sociological Theory)
समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है-
- वैज्ञानिक आधार- अन्य सिद्धांतों की तरह समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माणक तत्व भी सामाजिक तथ्य होते हैं। इसीलिये इनका वैज्ञानिक आधार होता है। ये वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही आधारित होते हैं।
- अनुभवसिद्ध- समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक अनुसंधान का आधार है, जिससे उपकल्पनाओं का परीक्षण एवं निरीक्षण किया जाता है।
- अर्मूत– अन्य सिद्धांतों की तरह समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी अमूर्त होते हैं। इनमें प्रयुक्त अवधारणायें सुस्पष्ट होती है तथा प्रस्तावनायें परस्पर संबंधित होती है।
- यथार्थता की व्याख्या के साधन- समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का उद्देश्य समाज, सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं को समझकर इनकी व्याख्या करना है। अतः ये साधन हैं, साध्य नहीं।
- सार्वभौमिक- समाजशास्त्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक प्राकृति के होते हैं अर्थात इन पर स्थान काल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरणार्थ- कार्लमार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत कहा जाता है।
- तार्किक- समाजशास्त्रीय सिद्धांत आनुभविक तथ्यों की एक तार्किक या बौद्धिक व्यवस्था है। जब एक विषय से संबंधित विभिन्न तथ्य एकत्रित कर लिये जाते हैं तो उनको तार्किक रूप से परस्पर संबंधित करके सिद्धांत का निर्माण किया जाता है।
- मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ- समाजशास्त्रीय सिद्धांत मूल्यों से मुक्त होते हैं क्योंकि ये अच्छे या बुरे का वर्णन नहीं करते। इनका उद्देश्य तो मात्र सामाजिक यथार्थता को समझना एवं इनकी व्याख्या करना है।
समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकार
प्रो. डॉन मार्टिनण्डेल ने अपनी ‘वाद’ के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है-
(1) प्रत्यक्षात्मक सावयवीवाद- इस श्रेणी के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा गया है जिनमें समाज या सामाजिक घटना की विवेचना या व्याख्या किसी न किसी रूप में उससे हटकर की गई है। इसके अंतर्गत कॉम्ट, हरबर्ट, स्पेंसर, लेस्टर वार्ड, टॉनिज, दुर्खीम आदि द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। इस श्रेणी में परेटो, फ्रायड आदि के सिद्धांतों को भी रखा गया है।
(2) समाजशास्त्रीय सिद्धांत का स्वरूपात्मक संप्रदाय– इसमें उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तकों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन विषय ‘मानवीय संबंधों का स्वरूप’, ‘समाजीकरण का स्वरूप है।
(3) सामाजिक व्यवहारवाद- इसके अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं, जो सामाजिक व्यवहार या सामाजिक क्रिया से संबंधित है। टार्ड द्वारा प्रस्तुत अनुकरण का सिद्धांत अथवा लीबों द्वारा भीड़ में मानव-व्यवहार से संबंधित सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत ही है। इस श्रेणी के अंतर्गत चार्ल्स कूले, विलियम थॉमस, जार्ज मीड आदि के सिद्धांतों को भी सम्मिलित किया गया है, जिनमें सामाजिक व्यवहार को प्रतीकात्मक अंतःक्रियाओं के आधार पर विश्लेषित किया गया है। साथ ही, इस श्रेणी के अंतर्गत मैक्स वेवर, वेब्लन, पारसन्स आदि के सामाजिक क्रिया सिद्धांत भी सम्मिलित हैं।
(4) समाजशास्त्रीय प्रकार्यात्मवाद- इस श्रेणी के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जिनका प्रतिपादन समाज के निर्माणक अंगों या इकाइयों के प्रकार्यों के संबंध में किया गया है। स्पेंसर, दुखम, परेटो, मैलिनाव्सकी, रेडक्लिफ ब्राउन आदि द्वारा प्रस्तुत प्रकार्यात्मक सिद्धान्त इसी प्रकार के सिद्धांत हैं।
(5) संघर्ष सिद्धांत- इस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जो मानव-जीवन या समाज में संघर्ष की स्थिति से संबंधित हैं। इस प्रकार के सिद्धांत की आधारशिला के रूप में बोडिन, हॉब्स, ह्यूम आदि के सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है।
वाल्टर वालैस ने अपनी पुस्तक “Sociological Theory” में समाशास्त्रीय सिद्धांतों के निम्न प्रकारों का उल्लेख किया है-
(1) विनिमय संरचनात्मवाद- सामाजिक जीवन में सक्रिय दो या अधिक इकाइयों के व्यवहारों के विनिमय के फलस्वरूप संरचना का निर्माण- इस उप-कल्पना को प्रमाणित करने वाले सिद्धांत इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी संदर्भ में दुर्खीम के सिद्धांत के अनुसार इसमें संदेह नहीं है कि सामाजिक तथा वैयक्तिक तथ्य मस्तिष्क के विद्यमान रहता है फिर भी कोई सामाजिक तथ्य तब तक नहीं पनपता जब तक ये व्यक्ति एक-दूसरे के साहचर्य में नहीं आते।
(2) परिस्थितिवाद- इस श्रेणी के अंतर्गत ये सिद्धात आते हैं जो मानवीय परिस्थिति से संबंधित है अर्थात इन सिद्धांतों में मानव और उसके गैर-मानवीय पर्यावरण या परिस्थितियों के बीच आंतरिक संबंधों की व्याख्या होती है, जैसे लीप्ले, डब्ल्यू. ई. मूर आदि के सिद्धांत ।
(3) जनांकिकीबाद- इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जो जनांकिकीय या मानवीय पर्यावरणों से संबंधित होते हैं, एव उसी से संबंधित किसी प्रवृत्ति की व्याख्या करते हैं जैसे-माल्थस, सैंडलर आदि का जनसंख्या सिद्धांत।
(4) प्रकार्यात्मक संरचनात्मक- इस श्रेणी के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण वाले सिद्धांत आते हैं, जैसे लीवी, मर्टन आदि का सिद्धान्त।
(5) प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद- इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जिनमें सामाजिक अतःक्रियाओं की व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार संबंधों में विवेचना की जाती है। चार्ल्स कूले, विलियम थॉमस, जार्ज हर्बर्ट मीड आदि के सिद्धांत इसी प्रकार के हैं।
(6) संघर्ष संरचनात्मकवाद- इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जिनके अनुसार सामाजिक जीवन में भाग लेने वाले दो या अधिक इकाइयों के व्यवहारों के विनिमय के फलस्वरूप संरचना का निर्माण नहीं, विघटन भी हो सकता है। इस प्रकार के सिद्धांत, सामाजिक संरचना के अंतर्गत दो या अधिक तत्वों के बीच होने वाले संघर्ष के स्वरूप और परिणामों को दर्शाते हैं। जैसे- कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत समाज के दो महान वर्गों के बीच होने वाले वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।
(7) मनोवैज्ञानिकवाद- इन सिद्धांतों में सामाजिक जीवन या मानवीय व्यवहारों की मनोवैज्ञानिक आधार पर व्याख्या प्रस्तुत की जाती है।
(8) प्रौद्योगिकवाद- इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनमें औद्योगिकी या प्रौद्योगिकी को सामाजिक घटनाओं का आधार या निर्णायक कारक माना जाता है।
(9) सामाजिक क्रियावाद- इस श्रेणी के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जिनमें सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार संबंधों के संदर्भ में विवेचना की जाती है। मैक्स वेवर, पारसंस आदि के सिद्धांत इसी प्रकार के हैं।
(10) भौतिकवाद- सामाजिक जीवन या सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक आधार पर करने वाले सिद्धांत इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
सिद्धांत एवं अनुसंधान में संबंध व परस्पर निर्भरता
(Relation or Interdependency of Theory and Research)
सिद्धांत एवं अनुसंधान के संबंध व परस्पर निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं (Points) को प्रस्तुत किया जा सकता है।
(1) समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सिद्धांत और अनुसंधान में ठीक प्रकार से सामंजस्य नहीं हो पाया है। सामाजिक वास्तविकता का पता लगाने के लिये सैद्धांतिक प्रतिस्थापना तथा तथ्यात्मक खोज दोनों ही आवश्यक हैं। कुछ समाजवादी तो अनुभवसिद्ध तथ्यों की खोज के बिना ही समाजशास्त्रीय नियमों का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी ओर कुछ विद्वान केवल तथ्यों के अवलोकन और संकलन मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। मर्टन के विचार से सिद्धांतवादी महत्वपूर्ण पक्ष को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं चाहे वह वास्तविक हो या न हो, और अनुभववादी या तथ्यवादी वास्तविक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं चाहे वह महत्वपूर्ण हो या न हो, यह धारणा गलत है।
(2) सिद्धांत और अनुसंधान एक-दूसरे से पृथक नहीं किये जा सकते हैं। इन दोनों को अलग-अलग करने से सिद्धांत और अनुसंधान दोनों को हानि हुई है। तथ्यात्मक खोज सैद्धांतिक मार्गदर्शन के अभाव में एक निरंतर श्रृंखला नहीं बन पाई और तथ्यात्मक तथा अनुभवसिद्ध प्रमाणों के अभाव में व्यवस्थित सैद्धांतीकरण नहीं हो पाया। स्थापित सिद्धांत से प्राप्त उपकल्पनाओं के आधार पर क्रमबद्ध अनुसंधान बहुत कम हुआ है। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों पर बिना किसी केंद्रीय सैद्धांतिक उन्मेष के संगतिहीन तथ्यात्मक अनुसंधान होता रहा है। परस्पर संबंधित उपकल्पनाओं की व्यवस्थाओं से पृथक सामान्य अवधारणात्मक विश्लेषणों की ओर अधिक झुकाव होने के कारण तथ्यात्मक अनुसंधान और सैद्धांतिक कार्य एक-दूसरे से अलग हो गये हैं। समाजशास्त्रीय ज्ञान की निरंतरता के लिये यह आवश्यक है कि तथ्यात्मक अध्ययन सिद्धांतोन्मुख हों और सिद्धांत अनुसंधान में प्रमाणित और अनुमोदित हों।
(3) सिद्धांत अनुसंधान का आधार है व सामाजिक सिद्धांत अनुसंधान को प्रेरित करता है। संपूर्ण सिद्धांत या इसका कोई अंश तथ्यात्मक अनुसंधान का आधार बन सकता है। सिद्धांत के द्वारा उन समस्याओं और मानवीय क्षेत्रों का ज्ञान होता है जिन पर अधिक उपयोगी खोज की जा सकती है। सिद्धांत ऐसी घटनाओं और स्थितियों की ओर संकेत करता है जिनमें सार्थक संबंध पाये जाते हैं। सिद्धांत उपकल्पनाओं को जन्म देता है। वह प्रत्येक अध्ययन को निरंतरता तथा शृंखलाबद्ध स्वरूप प्रदान करता है। सिद्धांत के आधार पर विश्वासपूर्वक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करना आसान होता है। इसी प्रकार सिद्धांत की सहायता से अध्ययन प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सकता है तथा ज्ञान के विकास में संगठित योगदान किया जा सकता है। मार्टन ने सिद्धांत के विभिन्न तत्वों का अनुसंधान पर प्रभाव दर्शाया है।
(4) सैद्धांतिक प्रस्थापनायें अनुसंधान की पद्धति और प्रणालियों को प्रभावित करती हैं। सैद्धांतिक उन्मेष अनुसंधान के क्षेत्र का निश्चिय करने में सहायक होता है। अवधारणायें (Concepts) भी सिद्धांत का एक भाग हैं। इन अवधारणाओं की परिभाषा अनुसंधान की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। इनके द्वारा उन तथ्यों का निश्चय होता है जिनके बीच अनुभवसिद्ध संबंधों का अवलोकन करना आवश्यक होता है। सिद्धांत नवीन तथ्यों की खोज के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है। व्यवस्थित सिद्धांत के द्वारा सिद्धांत और अनुसंधान दोनों में वृद्धि होती है। तथ्यात्मक आवश्यकताओं का सैद्धांतिक कथनों में परिवर्तन कर देने के बाद अनुसंधान की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार अनुसंधान को विवेकपूर्ण व्यवस्था प्रदान करके सिद्धांत पूर्वानुमान के लिये मार्ग प्रशस्त करते हैं। संक्षेप में सिद्धांत और सैद्धांतिक उपकल्पनायें अनुसंधान से संबंधित व्याख्यात्मक चलों (Intepretative Variables) को निर्धारित करता है। सैद्धांतिक व्यवस्था (Dodification) उपलब्ध तथ्यात्मक निष्कर्षों को व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित और व्यवस्थित करने में सहायक होती है।
(5) अनुसंधान मी सिद्धांत का सहायक है। यदि सिद्धांत अनुसंधान को प्रेरित करता है तो अनुसंधान के नये सिद्धांतों को आधार प्रदान करता है और प्रचलित सिद्धांतों की परीक्षा करता है। अनुसंधान से ही सिद्धांत विकसित होता है। अनुसंधान सैद्धांतिक अवधारणाओं की व्याख्या करता है। अनुसंधान नवीन उपकल्पनाओं को भी जन्म दे सकता है। अनुसंधान के दौरान कुछ नये तथ्य सामने आते हैं जिनके आधार पर नये सिद्धांतों का निर्माण हो जाता है। अनुसंधान प्रणालियों के विकास से ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं जो पहले दृष्टि में न आये हों, या उपेक्षित रहे हों। ये तथ्य कई बार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि संपूर्ण सिद्धांत की दिशा को ही बदल देते हैं। सिद्धांत का परीक्षण या पुनर्परीक्षण अनुसंधान के द्वारा ही संभव होता है। इस प्रकार अनुसंधान सिद्धांत को तार्किकता प्रदान करता है तथा उसका सत्यापन करता है।
समाजशास्त्र / Sociology – महत्वपूर्ण लिंक
- नगरीय संस्कृति | नगरीकरण से उत्पन्न समस्यायें | Urban culture in Hindi | Problems arising from urbanization
- समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति | समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्राकृति के संबंध में समाजशास्त्रियों के विचार | समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति एवं उपयोगिता | समाजशास्त्रीय सिद्धान्त की प्रकृति का विश्लेषण
- समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वास्तविक प्रकृति | समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमायें | समाजशास्त्रीय सिद्धांत की उपयोगिता
- समाजशास्त्र की परिभाषा | प्राचीनकाल में समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास | आधुनिक काल में समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास
- समाजशास्त्रीय सिद्धांत | समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]

