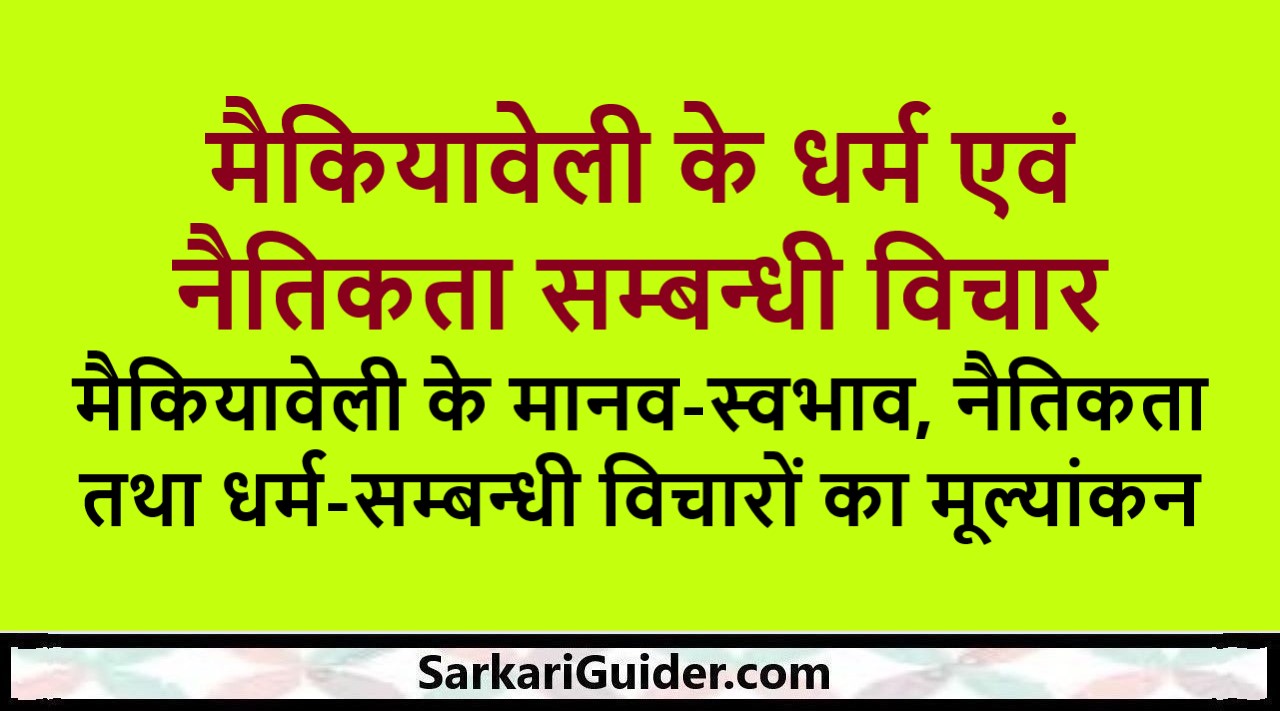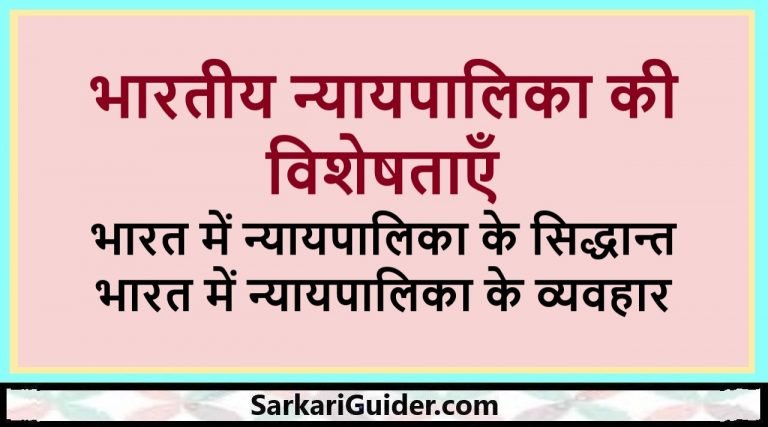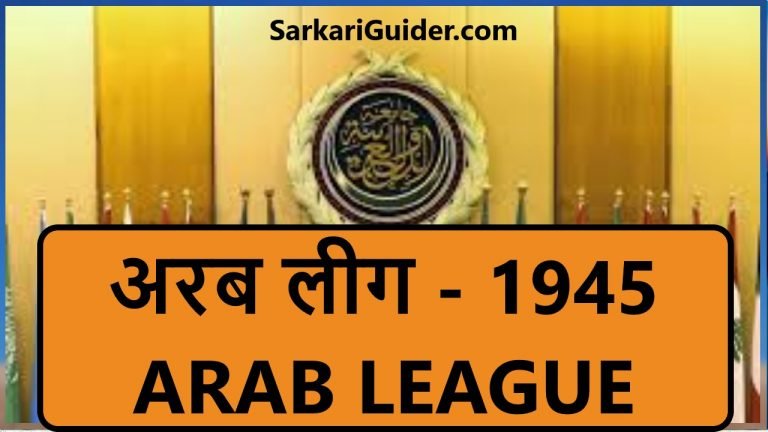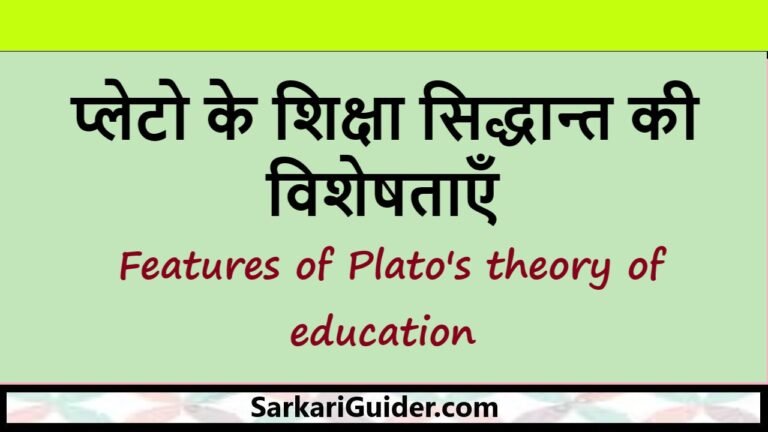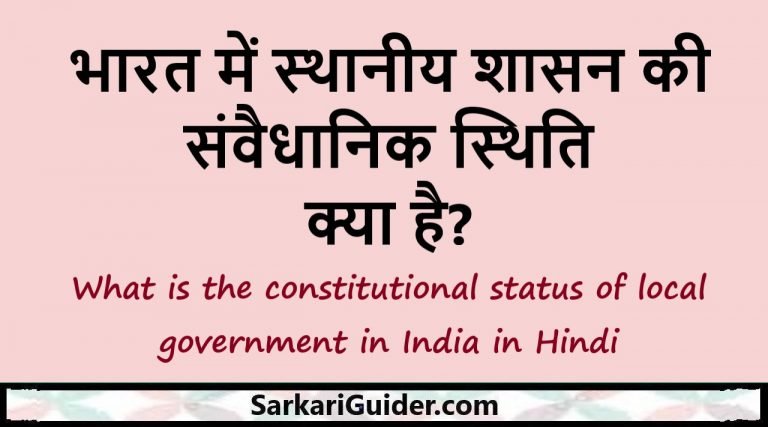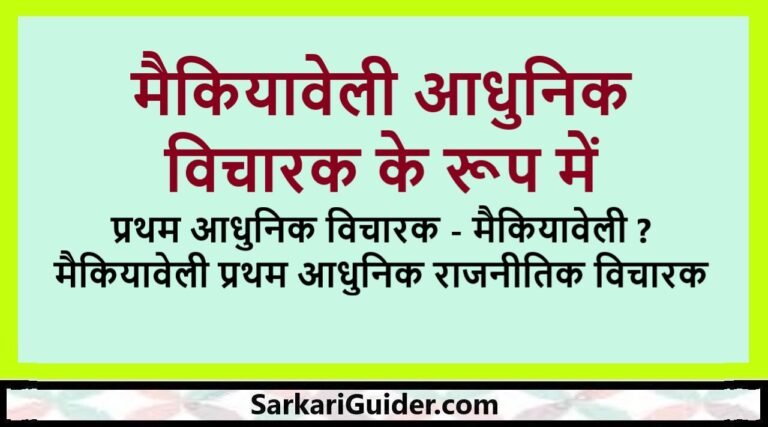मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता सम्बन्धी विचार | मैकियावेली के मानव-स्वभाव, नैतिकता तथा धर्म-सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन

मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता सम्बन्धी विचार | मैकियावेली के मानव-स्वभाव, नैतिकता तथा धर्म-सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन
मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता सम्बन्धी विचार
(Views on Religion and Morality)
(1) मानव स्वभाव-
मकियावेली ने मानव स्वभाव का जो विश्लेषण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘प्रिंस’ में किया है वह समकालीन इटली-निवासियों के आचरण पर आधारित है। मैकियावेली अनुभववादी था। उसने देखा कि इटली के लोग अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में अत्यन्त स्वार्थी हो गये थे; अत: वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी होता है। वह अनिवार्यतः सद्गुणी नहीं होता; अतः यह आवश्यक है कि उसे दबाया जाय और मनुष्य के स्वभाव को सुधारने का प्रयत्न किया जाय जिससे समाज को उत्तम बनाया जा सके। मैकियावेली का कहना है कि मनुष्य कृतघ्न, विश्वासघाती, कायर और लालची होता है। वह अच्छा बनने की तभी चेय करता है. जब ऐसा करने में उसे कोई लाभ दिखाई देता है। भय मानव स्वभाव का एक और महत्वपूर्ण तत्व है। उसका कहना था कि भय मानव जीवन को प्रेम से भी अधिक प्रभावित करता है; अतः शासक (राजा) को प्रजावत्सल नहीं, वरन् ऐसा होना चाहिये कि लोग उससे बराबर डरते रहें। जब तक वे डरेंगे तभी तक राजा की आज्ञा का पालन करेंगे। मैकियावेली का कहना था कि शासक अपने कार्यों से प्रजा को भयभीत रखे किन्तु उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे कोई वर्ग उससे घृणा करने लगे।
मानव-स्वभाव के सम्बन्ध में मैकियावेली के विचार हाब्स के विचारों से मिलते हैं। मनुष्य पापी एवं दुराचारी होता है। हाब्स ने भी मनुष्य के स्वभाव को स्वार्थी तथा अहंवादी कहा है। मैकियावेली के कथनानुसार मनुष्य भोगी, विलासी एवं आनन्दप्रिय होता है। मनुष्य सदा दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार करने का प्रयत्न करता है; अतः मनुष्य सदैव संघर्ष की स्थिति में रहता है जिससे समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। कानून के बन्धन से ही इस स्थिति पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा तभी हो सकती है जबकि सरकार सुदृढ़ हो । अत: मैकियावेली के राजनीतिक विचारों में मानव- स्वभाव के इस निरूपण का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। उसका विश्वास था कि इस परिस्थिति में राजतन्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी शासन प्रभावशाली नहीं सिद्ध होगा। मैकियावेली का भ्रष्टाचार से क्या अभिप्राय था, इसे प्रोफेसर सैबाइन, ने स्पष्ट किया है-
“साधारण रूप से भ्रष्टाचार का अर्थ है, व्यक्तिगत गुण, नागरिक गुण तथा त्याग का पतन होना जिससे कि प्रजातंत्रीय सरकार का चलना असम्भव था। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के हिंसात्मक कार्य, शक्ति और धन की असमानतायें, न्याय और शान्ति का अन्त, उथल-पुथल का उत्पन्न होना, अनैक्य, अवैधता, असम्मान और धर्म के प्रति तिरस्कार आदि बातें आती हैं।”
मैकियावेली ने मानव-स्वभाव का जो चित्रण किया है, वह वास्तविकता से दूर है। उसके द्वारा मानव-स्वभाव का चित्रण त्रुटिपूर्ण है । यह मान लेना कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि केवल इटली की जनता के स्वभाव के आधार पर ही मनुष्य स्वभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मैकियावेली के मानव-विकास सम्बन्धी अवैज्ञानिक भी हैं। उसके विचारों में विरोधाभास है।
(2) नैतिक धारणाएँ–
मैकियावेली की एक महत्त्वपूर्ण देन यह है कि उसने राजनीति को नैतिकता वे अलग किया। मैकियावेली का नैतिकता का सिद्धान्त ३ध (Dual) है। उसका कहना है कि न कोई कार्य या बात पूर्णतः अच्छी ही होती है न खराब ही। मैकियावेली प्रत्येक कार्य की अच्छाई को इस आधार पर निश्चित करता है कि उससे राज्य को कोई लाभ पहुँचता है या नहीं। यदि कोई वस्तु या काम राज्य के लिए उपयोगी है, तो वह नैतिक है, अन्यथा अनैतिक । डनिंग के अनुसार–
मैकियावेली के विचारों की एक प्रधान विशेषता यह है कि उसने राजनीतिशास्त्र को नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त, पृथक् और स्वतन्त्र कर दिया। इस दृष्टि से वह सर्वथा मौलिक विचारक था और प्राचीन एवं मध्यकालीन विचारकों से सर्वथा भिन्न था। यूनानी विचारक, सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तू नैतिक जीवन को बहुत महत्व देते थे। किन्तु मैकियावेली मध्ययुग का प्रथम विचारक है, जिसने राजनीति में नैतिकता के सिद्धान्तों को कोई महत्त्व नहीं दिया । ‘मैकियावेली’ का कहना है कि राजा के लिये नैतिकता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करना प्रशंसनीय हो सकता है किन्तु इतिहास में उसी प्रजा को अधिक सफलताएँ मिली हैं जिसने धार्मिक जीवन को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है; अतः उसे ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक, सच्चा ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती, अमानवीय, अधार्मिक और झूठा बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह राजा के लिए धोखा व दोष ओवश्यक गुण मानता है परन्तु प्रजा को सद्गुण उत्पन्न होना चाहिये | प्रजा का कर्त्तव्य है कि राजा चाहे हो वह उसकी बराबर सेवा करती. रहे। राजा की आज्ञा का पालन करना उसका कर्त्तव्य है। इसके विपरीत राजा के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी की आज्ञा का पालन करे। प्रजा के लिए यह अपेक्षित है कि उसमें सार्वजनिक सेवा का भाव हो। वह समाज के हित के लिए अपने निजी स्वार्थों का बलिदान कर दे किन्तु राजा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रजा की सेवा करे।
वास्तव में मैकियावेली समकालीन इटली की राजनीतिक एवं सामाजिक दशा के विषय में अपना विचार अभिव्यक्त कर रहा था। यही कारण है कि उसका नैतिक सिद्धांत, द्वैध, परस्पर विरोधी तथा त्रुटिपूर्ण बन गया है। इसी कारण मैकियावेली ने उसी राजा को सर्वोत्तम बताया है जिसमें शेर और लोमड़ी के स्वभाव का सुन्दर समन्वय हो। मैकियावेली का विचार है कि शासक में मानवता एवं धर्म के गुण प्रतीत हो सकते हैं परन्तु उसके मस्तिष्क में इतना अनुशासन होना चाहिए कि वह आवश्यकता पड़ने पर राज्य को बचाने के लिये कभी भी इन गुणों के विपरीत कार्य कर सकें।
राज्य को नैतिकता से श्रेष्ठतम बताने के लिये मैकियावेली ने तीन तर्क दिये-
(1) वह यह मानकर चलता है कि राज्य मनुष्य का सर्वोच्च संगठन है। यह मानव- कल्याण के लिए सबसे अनिवार्य संगठन है; अत: राज्य का स्थान सर्वोच्च होना आवश्यक है।
(2) वह एक यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर चलता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वार्थी है। इस परिस्थिति में यदि राज्य नैतिकता का समर्थन करता है तो वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
(3) मैकियावेली राज्य की सुरक्षा के हेतु सब प्रकार की नीति को उचित मानता है। राज्य के लिए कोई भी कार्य किया जा सकता है।
इस प्रकार मैकियावेली ने दोहरी नैतिकता का समर्थन किया है-एक शासक के लिए तथा दूसरी जनता के लिए। शासक को वह नैतिकता के सभी बन्धनों से मुक्त कर देता है। उसका विचार है कि शासक का कोई भी कार्य न नैतिक होता है और न अनैतिक । वस्तुतः उसके कार्यों पर इस दृष्टि से विचार करना ही उचित नहीं है। राजा का प्रत्येक कार्य उचित है क्योंकि ये कार्य राज्य की सुरक्षा एवं उन्नति के लिये अनिवार्य है। इस प्रकार यदि शासक राज्य के हित में कोई सामाजिक दृष्टि के अनैतिक कहे जाना वाला कार्य करता है तो भी उसे अनैतिक नहीं माना जायगा; अतः इस दृष्टि से शासक का प्रत्येक कार्य उचित एवं नैतिक है। दूसरी ओर जनता के अनैतिक कार्यों का मैकियावेली किसी भी आधार पर समर्थन नहीं करता । नागरिकों की नैतिकता इसी में निहित है कि वे राज्य तथा शासक के हित में कार्य करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना या समझौतों को भंग करना उनके लिए दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार जो कार्य शासक के लिए नैतिक है वे ही कार्य जनता के लिए अनैतिक हो सकते हैं। यही मैकियावेली का दोहरी नैतिकता का सिद्धान्त कहलाता है। इसके द्वारा वह निरंकुश शासन की स्थापना करता है और राजनीति को नैतिकता के सभी नियन्त्रणों से स्वतन्त्र कर देता है।
(3) धर्म-सम्बन्धी विचार-
सद्गुण एवं धर्म को मैकियावेली ने शासक का गुण नहीं माना। शासन की दृढ़ता की हेतु उसने यही आवश्यक समझा कि राजा को राज्य की सुरक्षा के लिये शान्ति की स्थापना के लिए अनैतिक कार्य करने में भी हिचक नहीं करनी चाहिये और उसके इन कार्यों को राजनैतिक दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है।
उसके लिये धर्म का कोई महत्त्व न था। परन्तु जहाँ तक धर्म द्वारा राज्य का सम्बन्ध स्थापित होता है वहीं तक मैकियावेली धर्म के महत्व को स्वीकार करता है। किन्तु उसने धर्म को कोई उच्च स्थान नहीं दिया। नैतिकता की भाँति धर्म को भी आवश्यकता पड़ने पर शासक त्याग सकता है। वह राज्य पर किसी प्रकार का धार्मिक बन्धन नहीं लगाता। राज्य की सुरक्षा के लिए अधार्मिक कार्य भी किये जा सकते हैं। राजा धर्म के बन्धनों से पूर्णतः स्वतन्त्र है। वह राज्य की रक्षा एवं उन्नति के लिए धर्म-विरोधी कार्य भी कार्य कर सकता । राज्य के लिए किए गए उसके किसी कार्य को बुरा नहीं कहा जा सकता।
परन्तु मैकियावेली अधार्मिक व अनैतिक नहीं है, वह केवल राजनीति में धार्मिकता व नैतिकता का विरोधी है। वह राज्य की सुरक्षा व उन्नति के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। इसी कारण उसने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। मैकियावेली ने आचारशास्त्र और राजनीति को पूर्णत: अलग कर दिया है। वह राजनीति में धर्म या आचार सम्बन्धी विचारों को कोई स्थान नहीं देता। उसने राजनीति में नैतिकता के सिद्धान्त को उपयोगिता की दृष्टि से निश्चय किया। यदि किसी कार्य से राज्य को लाभ होता है तो राजनीति में उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि धर्म और आचार किसी बात का सिद्धान्तत: विरोध करते हैं और शासक यह अनुभव करता है कि उस कार्य को करने से राज्य का लाभ होगां तो राजा को वह कार्य कर डालना चाहिये। ऐसा करना राजनीति की दृष्टि से कोई अनुचित बात नहीं। इससे स्पष्ट है कि मैकियावेली राजनीति को धार्मिकता और नैतिकता को बन्धनों से मुक्त रखना चाहता था। व्यक्ति और राजा के आचरण के मापदण्डों को सर्वथा भिन्न करने का श्रेय मैकियावेली को ही प्राप्त है। प्रो० डनिंग ने लिखा है कि-
“On the whole… Machiavelli’s attitude towards morality and religion was scientifically justifiable, and contributed greatly to the classification of the problems of Politics.” -Dunning.
राजनीतिक शास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य युग के राजनीतिक चिन्तन की सामान्य विशेषतायें | General characteristics of political thinking of the Middle Ages in Hindi
- जीन बोदों का संप्रभुत्ता का सिद्धान्त | Gene Bodo’s theory of sovereignty in Hindi
- राजनीतिक दर्शन के इतिहास में बोदोँ का महत्त्व | Bodo’s importance in the history of political philosophy in Hindi
- राज्य की उत्पत्ति पर हॉब्स के विचार | Hobbes’s views on the origin of the state in Hindi
- हॉब्स का प्रभुसत्ता सिद्धान्त | Hobbes Theory of Sovereignty in Hindi
- टामस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धान्त | Thomas Hobbes’ Social Compromise Theory in Hindi
- टामस हॉब्स की व्यक्तिवाद विचारधारा | Thomas Hobbes’s Individualism Ideology in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]