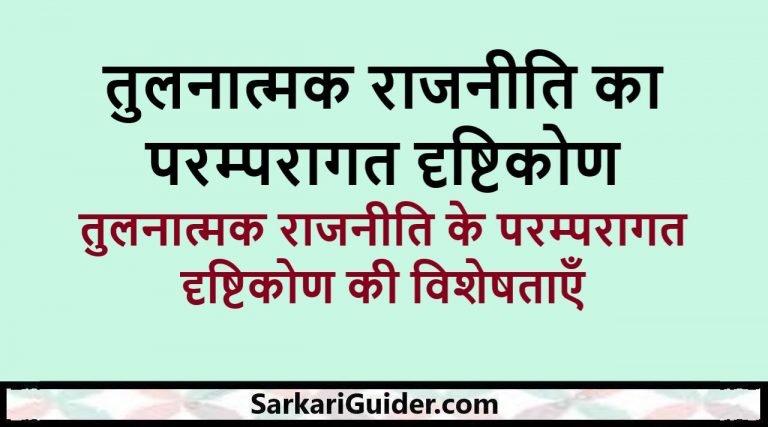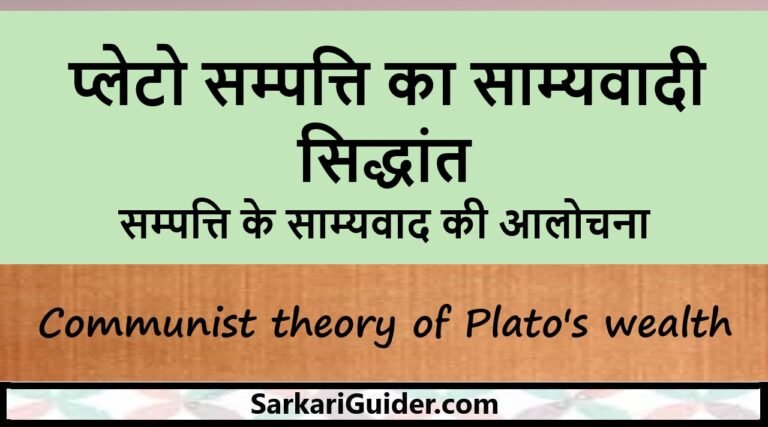दास-प्रथा पर अरस्तू के विचार | Aristotle’s Views on Slavery in Hindi

दास-प्रथा पर अरस्तू के विचार | Aristotle’s Views on Slavery in Hindi
दास-प्रथा पर अरस्तू के विचार
दासप्रथा तत्कालीन यूनान की एक प्रमुख प्रथा थी। प्लेटो ने दास प्रथा को अपने राजनीतिक चिन्तन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया क्योंकि उसका लक्ष्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। अरस्तू ने अपनी पुस्तक राजनीतिक’ में दास प्रथा का समर्थन किया है। उसके अनुसार दास अपने स्वामी की जीती-जागती सम्पत्ति है तथा उसका एक उपकरण है। स्वामी का दास पर पूर्ण अधिकार होता है। अरस्तू का दास प्रथा का सिद्धान्त दो धारणाओं पर आधारित हैं-प्रथम मनुष्य प्रकृति से असमान होते हैं तथा उनमें अलग-अलग गुण तथा कार्य क्षमताएं होती हैं। इस प्राकृतिक असमानता के कारण ही समाज में कुछ लोग दास होते हैं तथा कुछ स्वामी होते हैं, अत: द्वास बनाना उचित है। द्वितीय, अरस्तू के अनुसार यह निर्धारित करना सम्भव है कि कौन व्यक्ति गुणी है तथा कौन गुणी नहीं है।
अरस्तू ने दास प्रथा तथा स्वामी के मध्य सम्बन्धों की व्याख्या करते हुये कहा है कि स्वामी का दास के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है और दास स्वामी की पूर्ण सम्पत्ति है। दास का अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। उसकी अपनी इच्छा का कोई महत्त्व नहीं है। वह स्वामी के कार्य करने का उपकरण है। मैकलविन के शब्दों में, “यदि मनुष्य प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है तो दास एक पारिवारिक प्राणी से अधिक कुछ भी नहीं है, वह केवल चल सम्पत्ति है तथा अपने स्वामी के कार्य करने का उपकरण है।”
- अरस्तू का राजनीति शास्त्र में योगदान | Aristotle’s contribution to political science in Hindi
- अरस्तू के दासता सम्बन्धी विचारों की आलोचना | Aristotle criticized slavery ideas in Hindi
इस भाँति स्पष्ट है कि अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन ही नहीं किया वरन् इसे आवश्यक भी बताया है।
अरस्तू ने निम्नलिखित आधारों पर दास प्रथा का समर्थन किया है:
-
मनुष्यों में असमानता स्वाभाविक है-
अरस्तू का अभिमत था कि मनुष्यों में कार्य करने की क्षमताओं में प्राकृतिक रूप से असमानता पाई जाती है। प्रकृति ने मनुष्यों को भिन्न-भिन्न गुण तथा स्वभाव दिये हैं। कुछ व्यक्तियों में बौद्धिक क्षमता अधिक होती है जबकि दूसरे लोगों में बौद्धिक क्षमता कम होती है। कुछ व्यक्तियों में बुद्धि की प्रधानता होती है तो कुछ में शारीरिक शक्ति अधिक होती है। कुछ में शासक के गुण होते हैं तो कुछ में आज्ञापालन का गुण होता है; अतः कुछ स्वामी एवं दूसरे सेवक होते हैं। स्वामी बौद्धिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जबकि सेवक शारीरिक शक्ति का | इन दोनों का समन्वय पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपेक्षित है और इस प्रकार दास प्रथा प्राकृतिक असमानता के आधार पर आवश्यक है।
2. दास प्रथा प्रकृति के मूल सिद्धान्त के अनुकूल है-
अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन करते हुये प्रकृति का उदाहरण दिया है। उसका विचार है कि जिस प्रकार शरीर आत्मा के नियन्त्रण में रहता है तथा क्षुधा, विवेक् के नियन्त्रण में तथा स्त्री पुरुष के नियन्त्रण में, इसी प्रकार निकष्ट व्यक्तियों को श्रेष्ठ व्यक्तियो के नियन्त्रण में रहना चाहिये। यह प्रकृति का नियम है कि निकृष्टों को श्रेष्ठ के अधीन रहना चाहिये । अरस्तू इस प्राकृतिक नियम के आधार पर दास प्रथा का समर्थन करते हुये कहते हैं कि “यह स्पष्ट है कि शरीर के ऊपर आत्मा का तथा निम्न तत्त्वों के ऊपर विवेक तथा मस्तिष्क का शासन होता है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष स्त्री से स्वभाव में श्रेष्ठ होता है तथा स्त्री स्वभाव से ही दुर्बल होती है। इसलिये पुरुष शासन करता है। तथा स्त्री प्रासित होती है।” यह सिद्धान्त आवश्यक है तथा समस्त मानव जाति पर लागू होता है।
3. योग्य का अयोग्य पर स्वाभाविक शासन-
अरस्तू के अनुसार प्रकृति ने कुछ व्यक्तियों को अधिक योग्य बनाया है जो विवेकशील होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से शासन करने के लिये हुये हैं, जबकि कुछ कम योग्य, शासित होने के लिये। अरस्तू के शब्दों में, “प्रकृति के द्वारा जिस व्यक्ति में सोच-विचार की दूरदश्शिता अधिक है वह श्रेश्ठ तथा शासक है तथा जिस व्यक्ति में शारीरिक क्षमता अधिक है उसका जन्म सेवा करने के लिये हुआ है।”
4. कार्यों की विभिन्नता का आधार-
अरस्तू के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य के लिये भिन्न-भिन्न कार्य बनाये हैं। कोई भी कार्य बैकार नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्वामियों के लिये बनाये गये हैं। इसी प्रकार कुछ दासों के लिये हैं। अत: दासों वाले कार्यों को पूरा करने के लिये दास प्रथा आवश्यक है।
5. दूसरी प्रजाति के लोगों को दास बनाना चाहिए-
अरस्तू ने यूनान निवासियों में जाति प्रथा को लोकप्रिय बनाने के लिये इस मान्यता की स्थापना की कि दूसरी जाति के लोगों को दास बनाया जाना चाहिये क्योंकि बौद्धिक दृष्टि से यूनानी दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ है।
6. दासों के हित में-
दास प्रथा के पक्ष में अरस्तू तर्क देते हैं कि इस प्रथा के अन्तर्गत दासों को सर्वोत्तम दशाएँ प्राप्त होती हैं। उसके अपने स्वामी के साथ सम्बन्ध में उसमें श्रेष्ठता उत्पन्न होती है। दास का अपने स्वामी के नियन्त्रण में रहना उसके स्वयं के तथा उसके स्वामी दोनों के हित में है।
7. शासक के लिए उपयोगी-
शासक वर्ग को दासों की आवश्यकता होती है क्योंकि दासों के होने पर ही उसे सोचने-समझने का समय मिल सकता है, दास उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्वामी को आर्थिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह विवेक से अन्य समस्याओं की ओर ध्यान दे सकता है।
8. निम्न तथा उच्च का भेद-
दास प्रथा को अरस्तू इस आधार पर भी मान्यता देता है कि निम्न का स्वभाव है कि उच्च को मान दे। उदाहरणतः शरीर आत्मा से, क्षुधा वृत्ति विवेक से, जानवर आदमी से, स्त्री पुरुष से निम्न है।
9. सार्वभौमिक प्रथा-
अरस्तू इस प्रथा को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखता है। दास प्रथा उस समय सभी जगह प्रचलित थी। यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था एवं स्थायित्व के लिए आवश्यक मानी जाती थी। इस प्रथा की समाप्त से नगर राज्य के अस्तित्त्व संकट में थे; अंतः अरस्तू ने इस आधार पर भी इसको मान्यता दी।
अरस्तू के अनुसार दासता के दो भेद होते हैं-
(1) स्वाभाविक दासता- अरस्तू के अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से ही आज्ञा पालन एवं दासता के लिये होते हैं; अतः इस प्रकार की दासता को स्वाभाविक दासता कहा जाता है।
(2) कानूनी दासता- इसके अतिरिक्त युद्ध में पराजित होने पर बन्दी व्यक्ति भी दास बनाये जाते थे। ये कानूनी (Legal) दास कहलाते हैं।
राजनीतिक शास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- प्लेटो का न्याय सिद्धान्त | प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की विशेषताएँ | सिद्धान्त की आलोचना
- प्लेटो का आदर्श राज्य | प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धान्त
- प्लेटो का दार्शनिक राजा | प्लेटो के दार्शनिक शासक की विशेषताएँ, सीमाएँ तथा आलोचना
- प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएँ | आदर्श राज्य की समीक्षा
- प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना | Criticism of Plato’s ideal state in Hindi
- प्लेटो के शिक्षा सिद्धान्त की विशेषताएँ | Features of Plato’s theory of education in Hindi
- प्लेटो के शिक्षा-सिद्धान्त | प्लेटो के शिक्षा सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षा का पाठ्यक्म
- प्लेटो के शिक्षा सिद्धान्त की आलोचना | Criticism of Plato’s Theory of Education in Hindi
- प्लेटो सम्पत्ति का साम्यवादी सिद्धांत | सम्पत्ति के साम्यवाद की आलोचना
- प्लेटो स्त्रियों का साम्यवादी सिद्धांत | स्त्रियों के साम्यवाद की आलोचना
- प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना | समानताएँ – असमानताएँ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]