शिक्षा के विभिन्न प्रकार | शिक्षा के प्रकार या रूप | Different types of education in Hindi | Types or forms of education in Hindi

शिक्षा के विभिन्न प्रकार | शिक्षा के प्रकार या रूप | Different types of education in Hindi | Types or forms of education in Hindi
इस पोस्ट की PDF को नीचे दिये लिंक्स से download किया जा सकता है।
शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की “शिक्ष” धातु से हुई है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते है।
शिक्षा के प्रकार या रूप
शिक्षा को शिक्षक, बालक, विषय-वस्तु तथा शिक्षण विधियों के आधार पर विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है जो इस प्रकार है-
(1) औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा
शिक्षा के औपचारिक रूप के अन्तर्गत शिक्षा एक सुनियोजित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझी जाती है। इस रूप में शिक्षा जिस भी माध्यम से दी जाती है, उनका प्राथमिक उद्देश्य बालक को शिक्षित करना, उसके मानसिक स्तर में अभिवृद्धि करना व शिक्षा द्वारा उसे निश्चित ध्येय तक पहुँचाना है। इस शिक्षा में शिक्षा की योजना पूर्व निर्धारित होती है अर्थात शिक्षा देने का स्थान, समय, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय-वस्तु व समय-सारणी सभी सुनिश्चित होते हैं। इस शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य छात्र को परीक्षा पश्चात् उपाधि से अलंकृत करना भी है। औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके द्वारा बालक एवं समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं व उसे किसी व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा, शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किये गये शैक्षिक साधन है, यथा-स्कूल, पुस्तकालय आदि।
इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ बालक के जन्म से हो जाता है। व यह जीवन पर्यन्त बालक की शिक्षा को प्रभावित करते है। इन साधनों में शिक्षा देने का स्थान, समय, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय-वस्तु व समय सारिणी निश्चित नहीं होती। शिक्षा के अनौपचारिक साधन का प्राथमिक उद्देश्य न तो बालक को शिक्षा देना है और न ही उसे किसी उपाधि से अलंकृत करना है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप में हमें प्रभावित करती है व हमारे व्यवहार और आचरण को सुधारते हुए हमें भावी जीवनं हेतु तैयार करती है। यह शिक्षा सुव्यवस्थित व सुनियोजि न नहीं होती। बालक उठते-बैठते, खेलते-कूदते, खाते-पीते कुछ न कुछ सीखता है और यही सीखना शिक्षा है।
शिक्षा के दोनों ही रूप बालक के लिए परमावश्यक है व बालक के विकास में सहयोगी है। यह साधन पृथक-पृथक न होकर एक दूसरे के पूरक है चूंकि औपचारिक शिक्षा द्वारा हमारे ज्ञान का वर्धन किया जाता है व ज्ञान को व्यवस्थित करके हमें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। वही अनौपचारिक शिक्षा हमारे व्यवहार को वाछनीय निशा प्रदान करते हुए। हमें वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है। इसी कारण शिक्षा के इन दो रूपों में सामंजस्य होने पर ही बालक का विकास सुचारु रूप से किया जा सकता है।
(2) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा
शिक्षा की प्रक्रिया को प्रारम्भ से ही शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। इस कारण प्रत्यक्ष शिक्षा उसे कहते हैं। जिसमें शिक्षक और बालक एक-दूसरे के सामने बैठकर पूर्व निश्चित योजना के अनुसार विचारों का आदान-प्रदान करते है। इस शिक्षा में उद्देश्य प्राप्ति के लिए किसी निश्चित शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हुए बालक को निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है।
इसके विपरीत अप्रत्यक्ष शिक्षा उसे कहते हैं जो न किसी पूर्व योजना के अनुसार दी जाती है और न ही इसका कोई उद्देश्य होता है बल्कि यह स्वतन्त्र वातावरण में दी जाती है व शिक्षा देने के साधन अप्रत्यक्ष होते हैं। इस दिशा में शिक्षार्थी को अपनी इच्छानुकूल बढ़ने की स्वतन्त्रता होती है। यह साधन विद्यार्थी को प्रभावित करते हुए उसे परोक्ष रूप से शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा बालक पर्यावरण से ग्रहण करता है। अत: यह जरुरी है कि जिस पर्यावरण में बालक को रखा जाये, वह अच्छा हो जिससे बालक सुशिक्षा अर्जित कर सके।
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शिक्षा भी एक-दूसरे के विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक है। बालक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह दूसरों के माध्यम से ज्ञानार्जन करें साथ ही उसमें स्व-सीखने की भी रुचि होनी चाहिए। अतः दोनों प्रकार की शिक्षाएं आवश्यक है।
(3) सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा
सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा में बालक का सामान्य स्तर पर विकास करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षाशास्त्रियों का विचार है कि इस शिक्षा को मानव को अनिवार्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। चूंकि यह मनुष्य को पशुवत् व्यवहार से ऊंचा उठाने में सहयोग देती है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालक को सामान्य जीवन हेतु तैयार करना है।
विशिष्ट शिक्षा वह है जो किसी विशेष उद्दश्य हेतु संचालित की जाती है। इस शिक्षा में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा बालक की रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं के अनुकूल हो। चूंकि यह शिक्षा बालक को किसी विशेष क्षेत्र अथवा व्यवसाय हेतु तैयार करती है। इस शिक्षा के द्वारा बालक को इस प्रकार के अवसर दिये जाते हैं कि वह अपनी सृजनात्मकता का विकास कर सके और अपने जीवन लक्ष्य तक पहुँच सके। इस दिशा में इस बात का भी प्रयास किया जाता है कि बालक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग दे सके और इसके लिए उसे विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया जाता है।
शिक्षा में यह दोनों रूप भी परस्पर एक-दूसरे के पूरक है चूंकि एक ओर यह भी आवश्यक है कि बालक के सामान्य व्यक्तित्व का विकास करते हुए उसे व्यवहार कुशल बनाया जाये, साथ ही यह भी आवश्यक है कि बालक किसी एक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करते हुए समाज को उनकी मौलिक देन दे तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति करे।
(4) व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिक्षा
व्यक्तिगत शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो बालक की रुचियों, आवश्यकताओं व क्षमताओं के अनुकूल होती है। साथ ही इस शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पर भी नियन्त्रण रखा जाता है। एक समय में एक ही अध्यापक एक ही छात्र को शिक्षा देता है। इस प्रकार की शिक्षा पर बल मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है चूंकि मनोवैज्ञानिक शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता की बात पर बल देते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतन्त्र वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे उसे ज्ञान को प्राप्त करने में सुविधा होती है।
सामूहिक शिक्षा वह है जिसमें एक ही समय में एक ही अध्यापक द्वारा कई छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के इस रूप में बालकों को एक कक्षा में एकत्रित किया जाता है परन्तु बालक की व्यक्तिगत रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं की अवहेलना की जाती है।
उपरोक्त दोनों ही रूप कुछ सीमा तक अच्छे हैं चूंकि व्यक्तिगत शिक्षण व्यक्ति विशेष पर ध्यान देता है व सामूहिक शिक्षण व्यक्ति की उपेक्षा करता है। परन्तु आज के समय में व्यक्तिगत शिक्षण को क्रियान्वित कर सकना असम्भव है। अध्यापक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह सामूहिक रूप से शिक्षण कार्य करते हुए बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण करें।
(5) सकारात्मक एवं नकारात्मक शिक्षा
सकारात्मक शिक्षा में बालक ज्ञान को अध्यापक के कथनानुसार ग्रहण करता जाता है। स्वयं के अनुभव, तर्क व चिन्तन का इसमें कोई स्थान नहीं होता। ज्ञान प्रदान करने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण बालक को स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जाता। इस शिक्षण में बालक के स्वानुभवों का भी कोई स्थान नहीं।
नकारात्मक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से हैं जिसमें बालक स्वयं के अनुभवों व क्रियाओं के आधार पर ज्ञान अ्जित करता है। बालक अपने लिए स्वयं ही आदर्शों का निर्माण करता है व अध्यापक उसके लिए उचित वातावरण तैयार करके उसका मार्गदर्शन करता है।
शिक्षा के इन दोनों रूपों में भी परस्पर समन्वय होना जरुरी है। न तो हमें शिक्षा को पूर्णतया बालक के हाथ में सौंप देनी चाहिए और न ही उसे अध्यापक के पूर्ण नियन्त्रण में होना चाहिए। बालक को स्वक्रिया व स्वानुभव के आधार पर सीखने के अवसर देते हुए अध्यापक को एक नियन्त्रक के रूप में अहम भूमिका अदा करनी चाहिए।
For Download – Click Here
महत्वपूर्ण लिंक
- शिक्षा का अर्थ | शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएँ | शिक्षा की विशेषताएँ | Meaning of education in Hindi | Key definitions of education in Hindi | Characteristics of education in Hindi
- शिक्षा की अवधारणा | भारतीय शिक्षा की अवधारणा | Concept of education in Hindi | Concept of Indian education in Hindi
- शिक्षा के प्रकार | औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा | औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अन्तर
- शिक्षा के अंग अथवा घटक | Parts or components of education in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]


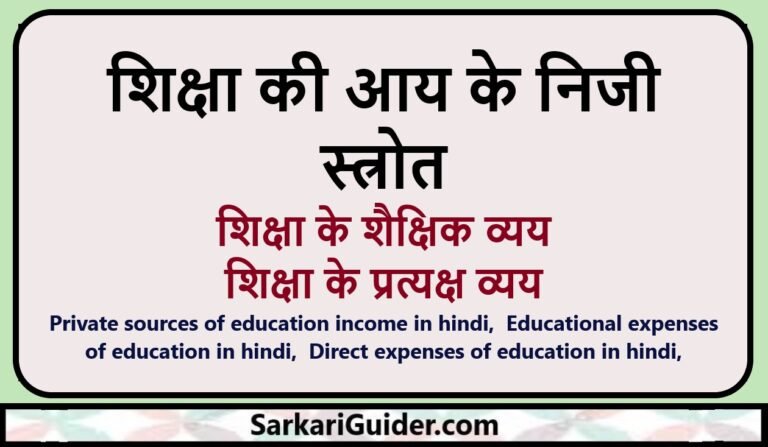



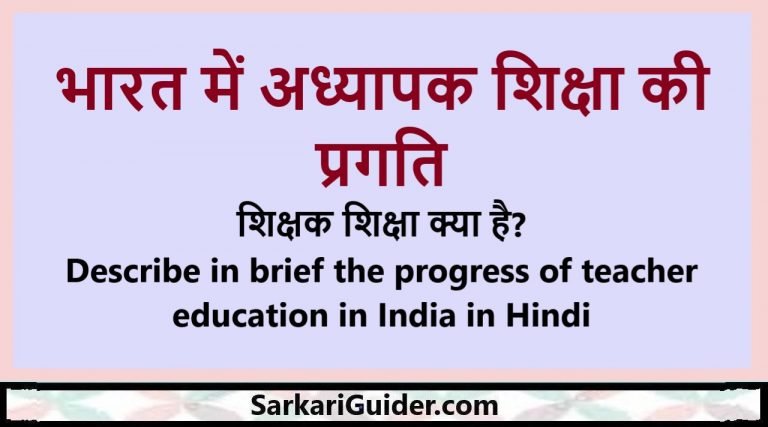

Aapko ase hi notes aor Daley bed me bohut help ho jati h