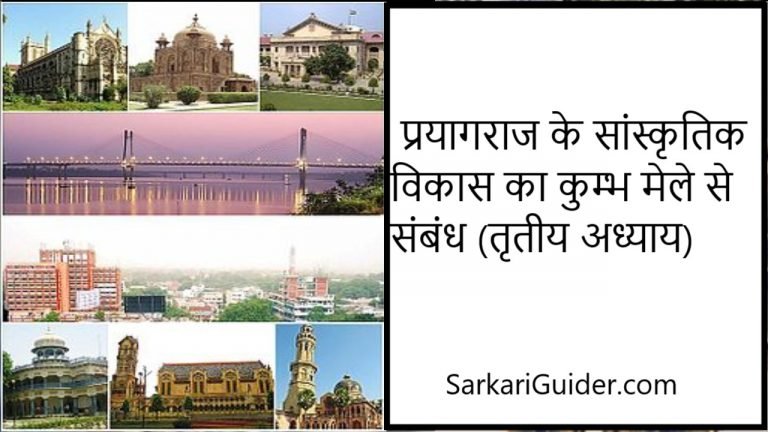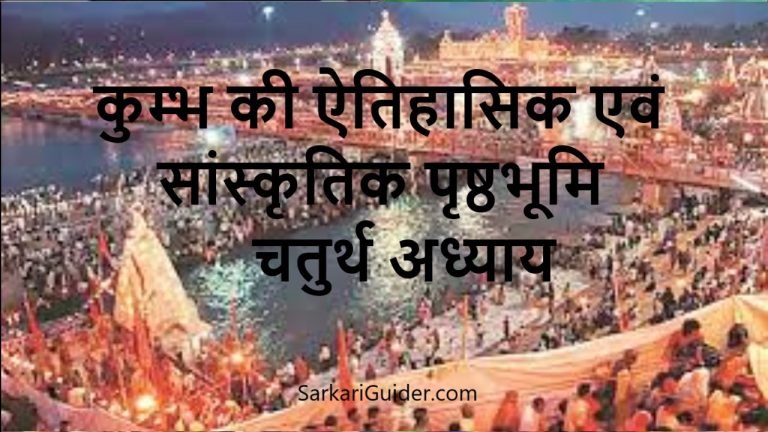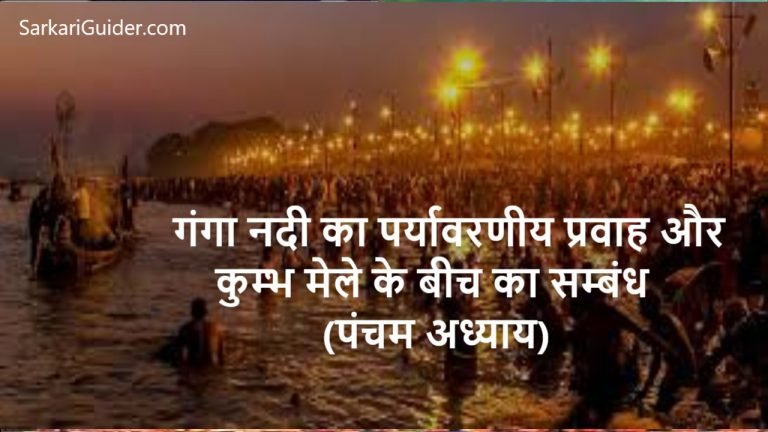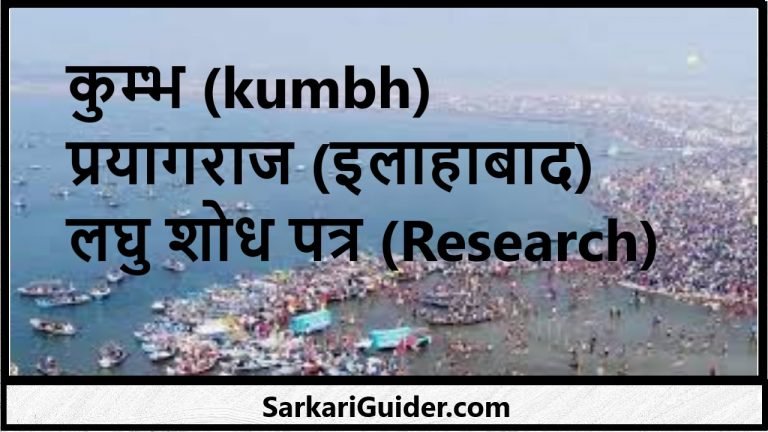कुम्भ की प्रस्तावना (प्रथम अध्याय)
प्रथम अध्याय
कुम्भ की प्रस्तावना
परिचय
कुम्भ की भव्यता जो की लगातार बढ़ती जा रही है उसकी चर्चा इस लघु शोध के अंतर्गत की गयी है | प्रयागराज उन चार तीर्थ स्थानों में से एक है जहां पर कुम्भ के पर्व को मनाया जाता है | भारतीय समुदाय में हिंदुओं के पर्व कुम्भ के बीच का संबंध ज्ञात किया गया है | कुम्भ के संदर्भ में प्रयागराज जैसे क्षेत्र को विषय क्षेत्र के रुप में चुना गया है क्योकि प्रयागराज का कुम्भ चारों स्थानों (हरिद्वार, उज्जैन, नासिक तथा प्रयागराज) में सबसे भव्य रुप में संपादित किया जाता है |
प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जिसका क्षेत्र 5,482 वर्ग किमी है उसमें कुम्भ मेले का आयोजन होना तथा कुम्भ के समय विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या एकत्रित होने वाला क्षेत्र बन जाता है यह प्रयागराज कुम्भ के दौरान | कुम्भ की भव्यता दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष और अधिक बढ़ती जा रही है जिसमें की भारतीय यात्री ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लोग भी भाग ले रहे हैं| कुम्भ में विदेशी यात्रियों की बढ़ती मात्रा का कारण शायद यह भी है कि सम्पूर्ण विश्व धीरे-धीरे अपनी सांस्कृतिक क्षेत्र या पृष्ठभूमी से दूर होते जा रहे हैं तथा साथ ही साथ कुम्भ का इतना भव्य तथा विस्तृत होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है |
विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत का वर्णन 640 वर्ष के पूर्व के समय से प्राप्त होता है | कुम्भ मेले का अपना एक अलग स्वरूप है यह महीने दो महीने चलने वाला एक सांस्कृतिक पर्व है कुम्भ के अर्थ से ज्ञात होता है कि पर्व का प्रचलन किसी कुम्भ अर्थात घड़े (अमृत कलश ) के द्वारा प्रारम्भ हुआ होगा | अमृत कलश के किसी दानव के हाथों में से जाने से बचाते समय हुए युद्ध के दौरान जिन चार जगहों में ये अमृत बूंदें गिरी थी वहाँ पर कुम्भ का आयोजन किया जाता है जिसमें कि प्रयागराज एक प्रमुख स्थान रखता है |
यह दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ त्योहार, कुम्भ मेले का एक ऐतिहासिक अध्ययन है | प्रयागराज, उत्तरी भारत का एक राजनीतिक शहर है, जिसमें होने वाले विश्व के सबसे बड़े जमघट पर ध्यान केन्द्रित किया गया है | इसमें मेले के एतिहासिक महत्व तथा परिवर्तनों का पता लगाने, प्रयागराज के साथ कुम्भ का क्या सम्बंध है तथा कुम्भ से प्रयागराज के हो रहे सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालने की पूर्ण कोशिश की गयी है |
पृष्ठभूमि
कुम्भ हिन्दू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें करोड़ो श्रद्धालु कुम्भ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं | प्रत्येक स्थान पर प्रति बारहवें वर्ष और प्रयोग में दो कुम्भ पर्वों के बीच छह वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है | खगोल गणनाओं के अनुसार कुम्भ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारम्भ होता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा, विश्चिक राशि में और वृहस्पति, मेष राशि में प्रवेश करते हैं| 2013 में कुम्भ तथा 2019 में प्रयागराज में इस वर्ष अर्ध कुम्भ का आयोजन किया गया है |
‘अर्ध’ शब्द का अर्थ है आधा | इसी कारण से बारह वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाले कुम्भ के बीच अर्थात पूर्ण कुम्भ के छः वर्ष बाद अर्ध कुम्भ आयोजित होता है |
प्रयागराज का कुम्भ मेला लगभग 50 दिनों तक संगम क्षेत्र के आस-पास हजारों हेक्टेअर भूमि पर चलने के कारण यहाँ विश्व के विशालतम अस्थायी शहर का रूप ले लेता है | आदिकाल से चली आ रही इस आयोजन की एकरूपता अपने आप में ही अद्वितीय है |
कुम्भ मेले से संबन्धित स्थल तथा उनकी तिथियाँ
|
वर्ष |
प्रयाग |
नाशिक |
उज्जैन |
हरिद्वार |
|
1983 |
अर्ध कुम्भ |
– |
– |
– |
|
1989 |
पूर्ण कुम्भ |
– |
– |
– |
|
1991 |
– |
कुम्भ |
– |
– |
|
1992 |
– |
– |
कुम्भ |
अर्ध कुम्भ |
|
1995 |
अर्ध कुम्भ |
– |
– |
– |
|
1998 |
– |
– |
– |
कुम्भ |
|
2001 |
पूर्ण कुम्भ |
– |
– |
– |
|
2003 |
– |
कुम्भ |
– |
– |
|
2004 |
– |
– |
सिहस्थ |
अर्ध कुम्भ |
|
2007 |
अर्ध कुम्भ |
– |
– |
– |
|
2010 |
– |
– |
– |
कुम्भ |
|
2013 |
पूर्ण कुम्भ |
– |
– |
– |
|
2015 |
– |
कुम्भ |
– |
– |
|
2016 |
– |
– |
सि हस्थ |
अर्ध कुम्भ |
|
2019 |
अर्ध कुम्भ |
– |
– |
– |
|
2022 |
– |
– |
– |
कुम्भ |
21वीं सदी में प्रयागराज में बारह वर्षीय कुम्भ
|
दिनांक |
संवत |
मास पक्ष तिथि |
वार |
|
24 जनवरी 2001 |
2057 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
बुधवार |
|
10 फरवरी 2013 |
2069 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
रविवार |
|
29 जनवरी 2025 |
2081 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
बुधवार |
|
16 जनवरी 2037 |
2093 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
शुक्रवार |
|
2 फरवरी 2049 |
2105 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
मंगलवार |
|
2 फरवरी 2060 |
2116 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
सोमवार |
|
20 जनवरी 2072 |
2128 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
बुधवार |
|
6 फरवरी 2084 |
2140 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
रविवार |
|
25 जनवरी 2096 |
2152 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
बुधवार |
|
11 फरवरी 2108 |
2164 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
शनिवार |
|
30 जनवरी 2120 |
2176 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
मंगलवार |
टिप्पणी – प्रयागराज कुम्भ में अनेक पर्व होते है यथा – मकर संक्रांति, पौष पुर्णिमा, माघी (मौनी) अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पुर्णिमा एवं महाशिवरात्री, परंतु माघी (मौनी) अमावस्या प्रयागराज कुम्भ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व होता है, अतः इस सारणी में माघी (मौनी) अमावस्या की तिथि उल्लिखित है |
21वीं सदी में प्रयागराज में छः वर्षीय कुम्भ
|
दिनांक |
संवत |
मास पक्ष तिथि |
वार |
|
19 जनवरी 2007 |
2063 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
शुक्रवार |
|
4 फरवरी 2019 |
2075 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
सोमवार |
|
23 जनवरी 2031 |
2087 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
गुरुवार |
|
21 जनवरी 2042 |
2098 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
मंगलवार |
|
7 फरवरी 2054 |
2110 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
शनिवार |
|
25 जनवरी 2066 |
2122 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
सोमवार |
|
12 फरवरी 2078 |
2134 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
शनिवार |
|
30 जनवरी 2090 |
2146 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
सोमवार |
|
19 जनवरी 2102 |
2158 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
गुरुवार |
|
5 फरवरी 2114 |
2170 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
सोमवार |
|
23 जनवरी 2126 |
2182 |
माघ कृष्ण अमावस्या |
बुधवार |
टिप्पणी – प्रयागराज कुम्भ में अनेक पर्व होते है यथा – मकर संक्रांति, पौष पुर्णिमा, माघी (मौनी) अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पुर्णिमा एवं महाशिवरात्री, परंतु माघी (मौनी) अमावस्या प्रयागराज कुम्भ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व होता है, अतः इस सारणी में माघी (मौनी) अमावस्या की तिथि उल्लिखित है |
अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन
प्रयागराज जिला 24° 47‘ उत्तर से 25° उत्तर अक्षांश के बीच और 81° 19′ और 82° 21′ पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। इसमें 5,246 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यह जिला राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है जो भारत के विंध्य पठार के समीप और गंगा के समतल मे है। प्रयागराज जिला पूर्व मे भदोही और मिर्जापुर द्वारा घिरा हुआ है, पश्चिम में कौशाम्बी तथा बांदा द्वारा तथा उत्तर में प्रतापगढ तथा जौनपुर द्वारा और बांदा तथा मध्य प्रदेश द्वारा दक्षिण मे घिरा है। जिला मे गंगा और यमुना नदी बहती हैं| जिले में आठ तहसील शामिल हैं, जिनका नाम सदर, सोरांव, फूलपुर, हंडिया, बारा, करछना, कोरांव और मेजा है | प्रयागराज जिले मे मेजा तहसील क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी आबादी वाली तहसील है और सदर तहसील जिले की सबसे बड़ी तहसील है। प्रयागराज जिले मे 20 विकास खंड, 2715 गांव और 10 कस्बे हैं ।
प्रयागराज, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थिर एक नगर एवं इलाहाबाद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है | इसका प्राचीन नाम प्रयाग है | प्रयागराज को तीर्थराज ( तीर्थों का राजा ) भी कहते हैं | ऐसा कहा जाता है कि उत्कृष्ट यज्ञ और दान दक्षिणा आदि से सम्पन्न स्थल देखकर भगवान विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं ने इसका नाम प्रयागराज रख दिया, इसका उल्लेख पुराणों द्वरा प्राप्त होता है | तीर्थराज प्रयागराज एक ऐसा पावन स्थल है, जिसकी महिमा हमारे सभी धर्मग्रंथों में वर्णित है | प्रयागराज को शोध कार्य हेतु चुनने का मुख्य कारण है कि चार स्थान ( हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक ) जहां पर कुम्भ की भव्यता प्राप्त कि जाती है वहाँ प्रयागराज एक अलग ही स्थान रखता है | प्रयागराज का संगम जो की तीन नदियों द्वारा मिल के बनता है गंगा, यनुना और सरस्वती प्रयागराज की अलग से शान बढ़ाता है |
अध्ययन का उद्देश्य
– कुंभ मेले के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना।
– कुंभ मेला और प्रयागराज जिले के सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को समझाने के लिए।
– कुम्भ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को समझना |
– कुंभ की घटना के दौरान मानव- संस्कृति संबंध का अध्ययन करना।
– कुंभ के दौरान लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए गंगा नदी के प्रवाह को समझना।
अनुसंधान विधि
वर्तमान शोध निबंध कार्य गुणात्मक दृष्टिकोणों पर आधारित है। शोध निबंध में प्राथमिक तथा द्वितीयक आकड़ों दोनों का उपयोग किया गया है |
निम्नलिखित चरणों का अवलोकन करके गुणात्मक विश्लेषण किया गया है।
पुस्तकालय सलाहकार – इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, वसंत महिला महाविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविध्यालय भूगोल के विभागीय पुस्तकालय से साहित्य की समीक्षा तैयार करने और इलाहाबाद और कुंभ की उत्पत्ति तथा बाकी की कथावस्तु के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए परामर्श लिया गया है। रिमोट सेंसिंग और जी.आई.एस. – क्षेत्र की काल्पनिकता को मानचित्र की व्याख्या के लिए रिमोट सेंसिंग और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। फील्ड वर्क – समग्र जानकारी के संबंध में डेटा एकत्र करने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में एक गहन क्षेत्र कार्य किया गया था। इसके द्वारा प्राथमिक अकड़ों को एकत्रित करने में सहायता प्राप्त हुई है | डेटा स्रोत / संग्रह – शोध कार्य का विश्लेषण और अंतर्संबंध प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आंकड़ों पर आधारित है। कुंभ मेला क्षेत्र में संचालन कार्य द्वारा प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया है। इलाहाबाद जिले के बारे में सामाजिक-आर्थिक डेटा को माध्यमिक डेटा से एकत्र किया गया है।
महत्वपूर्ण माध्यमिक डेटा स्रोत जिला गजेटियर, सांख्यिकीय रूपरेखा, जिला खनिज सर्वेक्षण रिपोर्ट इलाहाबाद और वन विभाग, पर्यटन विभाग की रिपोर्ट और इलाहाबाद नगर निगम के रिकॉर्ड द्वारा प्राप्त किया गया है।
संस्कृति
संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का समग्र नाम हैं, जो की उस समाज की सोचने, विचार करने, कार्य करने आदि से संबन्धित होती है | संस्कृति शब्द का अर्थ है- उत्तम या सुधरी हुई स्थिति | मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है | वह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों तरफ की प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है | प्रत्येक जीवन-पद्धति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार, तथा सभ्य बनता है, सभ्यता और संस्कृति का ही अंग है | सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति की सूचना मिलती है जबकि संस्कृति से मनुष्य की मानसिक क्षेत्र की प्रगति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है | मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं | सौंदर्य की खोज करते हुये वह संगीत, साहित्य, मूर्त, चित्र और वस्तु आदि अनेक कलाओं को उन्नात करता है |
भूगोल और संस्कृति
संस्कृति, जीवन का कुल तरीका जो लोगों के एक समूह की विशेषता है, भूगोल का अध्ययन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों ( वस्तु ) में से एक है। पृथ्वी पर वस्तुतः हजारों संस्कृतियां हैं। संस्कृति में कई सांस्कृतिक घटक होते हैं, ये घटक केवल मानव तक ही सीमित नहीं होते हैं। पृथ्वी के कई स्थानों तथा रुप में अच्छी तरह से चिह्नित हो जाते हैं लोगों की संस्कृति के अनुसार। मुख्य रूप से लोग उनकी संस्कृति के माध्यम से है जो की लोग पृथ्वी की सतह के साथ संबंध स्थापित करते हैं और उसे संशोधित करते हैं। असंख्य सांस्कृतिक अंतरों के कारण, जो लोगों की अपनी अलग-अलग विशेषता रखते हैं और दुनिया भर में भूमि या भू क्षेत्र का निर्माण करते हैं, भूगोल का एक पूरा उप क्षेत्र है, जो संस्कृति-संबंधी सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन के लिए समर्पित है।
भूगोल सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल का शाब्दिक अर्थ है ‘पृथ्वी का वर्णन’। यह हमारी ग्रह सतह की विशेषता वाली घटनाओं के वितरण का वर्णन और व्याख्या करती है। ऐसा करते हुए भूगोल में शामिल प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।
– चीजें कहां स्थित हैं?
– वो लोग वहाँ क्यों हैं?
– उनका क्या महत्व है?
– विशेष स्थान या क्षेत्र क्या है?
– कैसे और क्यों पृथ्वी पर कुछ स्थान एक जैसे या दूसरे से अलग हैं?
इन सभी विशेषताओं की एक अद्भुत विविधता हमारे ग्रह की विशेषता है। इनमें जलवायु, भूमि रूप और प्राकृतिक वनस्पति जैसी भौतिक विशेषताएं भी शामिल हैं जो की सांस्कृतिक रुप को प्रभावित करती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से। उनमें मनुष्य, उनकी विशेषताएं और उनके कार्य भी शामिल हैं-जैसे शहर, कृषि, परिवहन प्रणाली और उद्योग आदि।
सांस्कृतिक भूगोल किसी दिए गए संस्कृति के पर्यावरण विशेषता विशेषताओं की पहचान करने के लिए और यदि संभव हो तो भौगोलिक विशेषता बनाने और बनाए रखने में मानव क्रिया की भूमिका की खोज करने के लिए, पृथ्वी की सतह के वितरण के साथ सांस्कृतिक क्षेत्र के बदलते वितरण की तुलना करें।
सांस्कृतिक भूगोल
सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल के भीतर एक उप-क्षेत्र है | पर्यावरणीय वर्गीकरणों के आधार पर पूर्व-निर्धारित क्षेत्रों का अध्ययन करने के बजाय, सांस्कृतिक भूगोल सांस्कृतिक परिदृश्य में रुचि रखता है। यह कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में “कार्ल ओ0 सॉवर” (जिसे सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है) का नेतृत्व किया गया था। परिणामस्वरूप, अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं पर सांस्कृतिक भूगोल लंबे समय तक हावी रहा। प्राकृतिक परिदृश्य और मनुष्यों के बीच यह संपर्क सांस्कृतिक परिदृश्य बनाता है। यह समझ सांस्कृतिक भूगोल की एक नींव है, लेकिन पिछले 40 वर्षों में संस्कृति की अधिक बारीकियों और जटिल अवधारणाओं के साथ संवर्धित किया गया है | संस्कृतियाँ और समाज दोनों ही अपने परिदृश्य से विकसित होते हैं, तथा उन्हें आकार भी देते हैं। प्राकृतिक परिदृश्य और मनुष्यों के बीच यह संपर्क सांस्कृतिक परिदृश्य बनाता है |
सांस्कृतिक प्रसार
सांस्कृतिक प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सांस्कृतिक लक्षण एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं। सांस्कृतिक का भूगोल लगातार बदलता रहा है। आम तौर पर, संस्कृति के लक्षण एक विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और अंततः बाहरी क्षेत्र के बड़े हिस्से को चिह्नित करने के लिए बाहर की ओर फैलते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र सांस्कृतिक लक्षणों के स्थान का वर्णन करते हैं, सांस्कृतिक प्रसार यह समझाने में मदद करता है कि वे वहां कैसे पहुंचे। सांस्कृतिक प्रसार विभिन्न तरीकों से होता है। प्रवासन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब लोग चलते हैं, तो वे अपने साथ “सांस्कृतिक सामान” ले जाते हैं। इस प्रकार का एक बेहिसाब उदाहरण है, अतीत और वर्तमान जिसमें प्रवासियों के आगमन के परिणामस्वरूप संस्कृति लक्षण उस क्षेत्र में दिखाई देते हैं जहां वे पहले मौजूद नहीं था |
साहित्य की समीक्षा
साहित्य की समीक्षा अध्ययन के अंतर्गत वर्तमान विषय के संबंध में किए गए पर्यायवाची कार्य से संबंधित है। इस अध्ययन में, प्रत्येक अध्याय में संबंधित अध्ययनों के संदर्भ प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बावजूद, मेलों और त्यौहारों में भौगोलिक अनुसंधान की प्रवृत्ति को समझने के लिए प्रमुख कार्यों की एक संक्षिप्त समीक्षा दी गई है। इस विषय पर कुछ प्रयास इस प्रकार से किए गए हैं:
भारद्वाज, सिंदर मोहन (1977) ने अपने लेख andप्रयाग और इसके कुंभ मेले में इस विषय पर स्मारकीय कार्य किया।
- डी.पी. दुबे (2001) द्वारा अपने लेख में कुंभ मेले की साइट: ‘इन टेम्पोरल एंड ट्रेडिशनल स्पेस’ में कुंभ मेला और इसकी पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय सामने लाने का प्रयास किया गया है |
- हेबरमैन, डेविड एल0 (2006) द्वारा अपनी थीसिस में ‘लव रिवर ऑफ लव इन पॉल्यूशन: द गंगा एंड यमुना नदी ऑफ नॉर्दन इंडिया’ में हिंदू धर्म की संरचना, विकास और कार्य पर नदी के प्रभाव की जांच की है।
- रत्नदीप, सिंह (1996) द्वारा अपनी पुस्तक इनफ़्रास्ट्रक्चर ऑफ़ टूरिज़्म इन इंडिया के माध्यम से भारतीय पर्यटन के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में अपने विचार को विस्तार रूप से दिया है तथा अपनी पुस्तक में, उन्होंने पर्यटन के बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति विकास पर ध्यान केंद्रित किया है |
प्रयागराज की भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति कुम्भ के संदर्भ में (द्वितीय अध्याय)
प्रयागराज के सांस्कृतिक विकास का कुम्भ मेले से संबंध (तृतीय अध्याय)
INTRODUCTION TO COMMERCIAL ORGANISATIONS
| संज्ञानात्मक नक्शा, मानसिक नक्शा या मानसिक मॉडल Cognitive Map |
गतिक संतुलन संकल्पना Dynamic Equilibrium concept
भूमण्डलीय ऊष्मन( Global Warming)|भूमंडलीय ऊष्मन द्वारा उत्पन्न समस्याएँ|भूमंडलीय ऊष्मन के कारक
प्राचीन भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएँ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है | हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है| यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- sarkariguider@gmail.com