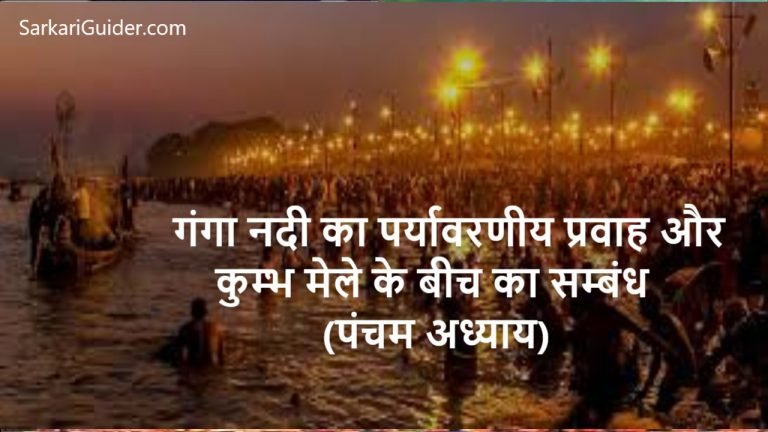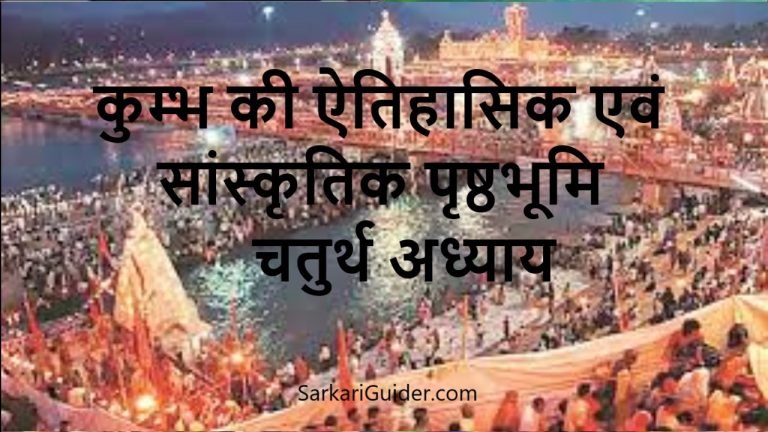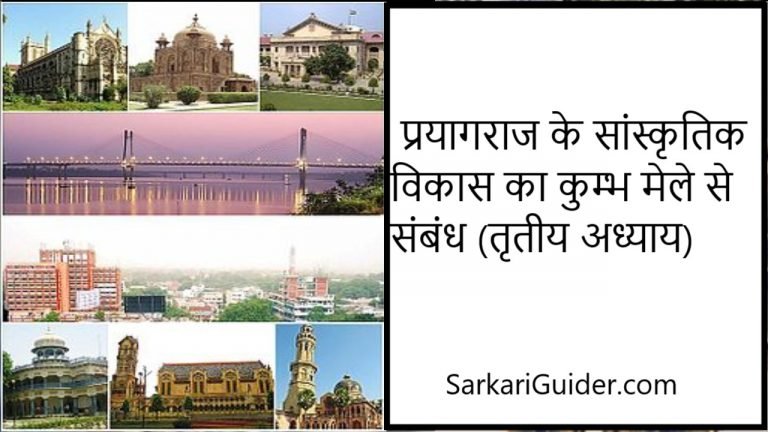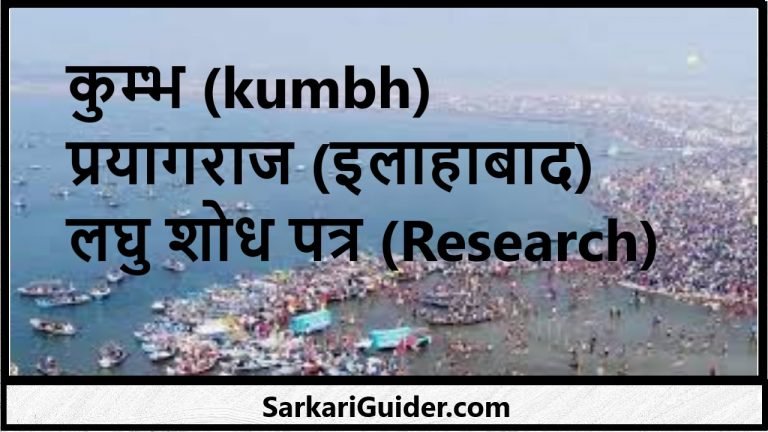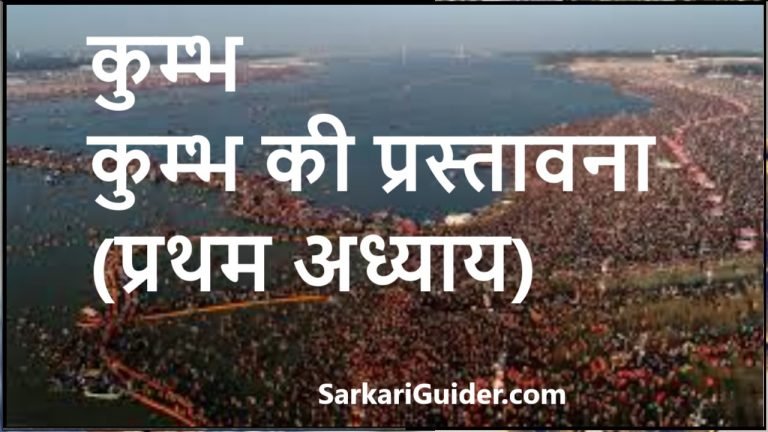प्रयागराज की भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति कुम्भ के संदर्भ में (द्वितीय अध्याय)
प्रयागराज की भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति कुम्भ के संदर्भ में (द्वितीय अध्याय)
परिचय
प्रयागराज जिला 24° 47‘ उत्तर से 25° उत्तर अक्षांश के बीच और 81° 19′ और 82° 21′ पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। इसमें 5,246 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यह जिला राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है जो भारत के विंध्य पठार के समीप और गंगा के समतल मे है। प्रयागराज जिला पूर्व मे भदोही और मिर्जापुर द्वारा घिरा हुआ है, पश्चिम में कौशाम्बी तथा बांदा द्वारा तथा उत्तर में प्रतापगढ तथा जौनपुर द्वारा और बांदा तथा मध्य प्रदेश द्वारा दक्षिण मे घिरा है। जिला मे गंगा और यमुना नदी बहती हैं| जिले में आठ तहसील शामिल हैं, जिनका नाम सदर, सोरांव, फूलपुर, हंडिया, बारा, करछना, कोरांव और मेजा है | प्रयागराज जिले मे मेजा तहसील क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी आबादी वाली तहसील है और सदर तहसील जिले की सबसे बड़ी तहसील है। प्रयागराज जिले मे 20 विकास खंड, 2715 गांव और 10 कस्बे हैं ।
‘प्रयागराज जिले को इलाहाबाद और कौशाम्बी में 1997 में विभाजित किया गया था । द्विविभाजन से पहले इसके द्वारा 7,261 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया गया था तब 9 तहसील और 28 सीडी ब्लॉक थे। दोआब क्षेत्र 2,015 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है तीन तहसील के साथ, और 8 सीडी ब्लॉक कौशाम्बी के रूप में बनाए गए थे।
जिला क्षेत्र जलोढ़, साथ ही कठोर चट्टानों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जिला यमुना नदी और विंध्य पहाड़ियों द्वारा द्विभाजित है। प्रकृतिक एवं भूगोल संबंधी जिले की विशेषता गंगा और यमुना का मैदान तथा विंध्य पठार है | इसे तीन प्राकृतिक उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है-
i) सक्रिय बाढ़ मैदान
ii) पुराने जलोढ़ मैदान और चट्टान की सतह
iii) अनाच्छादित पर्वत
सक्रिय जलोढ़ मैदान मिट्टी, कंकर, रेत और बजरी के मोटे जमाव की विशेषता है। पुराना जलोढ़ मैदान गंगा नदी के किनारे स्थित है। ट्रांस यमुना क्षेत्र में इसका उच्चारण कम है। ट्रांस यमुना क्षेत्र में और विशेष रूप से शंकरगढ़, कोरांव, मेजा और मांडा में अनाच्छादित पहाडि़यां काफी प्रसिद्ध हैं।
जिले का सामान्य प्रतिरुप
प्रयागराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (पेंशन) पीसीडीए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) कार्यालय के साथ एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर है, जो कि एक प्रमुख संस्थान है।
प्रयागराज शहर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है और तीन नदियों- गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। बैठक बिंदु त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से यह स्थान हिंदुओं के लिए एक पवित्र भूमि है। आर्यों की पहले की बस्तियाँ इस शहर में स्थापित की गई थीं, जिसे “प्रयाग” के नाम से जाना जाता था। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है है कि , “प्रयागस्य प्रवाशेषु पापम् नाशवती तत्क्षणम्“ (सभी पापों को प्रयाग में प्रवेश मात्र से साफ किया जाता है)। यह शहर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दिल भी था।
जिले की भौगोलिक रूपरेखा
जिला प्रयागराज की भौगोलिक रूपरेखा निम्नलिखित पहलुओं में है:
जलवायु दशा
प्रयागराज जिले की जलवायु लंबी और तेज गर्मी, काफी सुखद मानसून और ठंड के मौसम की विशेषता के साथ है। आमतौर पर सर्दियों का विस्तार मध्य नवंबर से फरवरी तक होता है और इसके बाद गर्मी आती है जो जून के मध्य तक जारी रहती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून बरसात के मौसम में प्रवेश करता है, जो सितंबर, अक्टूबर के अंत तक रहता है और नवंबर की पहली छमाही में मानसून के बाद का मौसम बनता है। प्रयागराज जिले की वर्षा आम तौर पर दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम तक घटती चली जाती है | वार्षिक वर्षा का लगभग 88 प्रतिशत मानसून के मौसम के दौरान प्राप्त होता है। जुलाई और अगस्त अधिकतम वर्षा के महीने हैं। जिले में सामान्य वर्षा 975.4 मिमी की है। (38.40 “) लेकिन साल-दर-साल भिन्नता औसतन सराहनीय है, साल में लगभग 48 बारिश के दिन होते हैं, जिले के विभिन्न हिस्सों में नगण्य होने की भी भिन्नता है।
नवंबर के मध्य से, तापमान तेजी से गिरना शुरू हो जाता है और जनवरी में (सबसे ठंडा महीना) औसत दैनिक अधिकतम 23.7 ° C (74.7 ° F) होता है। पूर्व की ओर से गुजरने वाली पश्चिमी विक्षोभ के मद्देनजर शीत लहरों के साथ, न्यूनतम तापमान पानी के हिमांक से दो डिग्री ऊपर एक डिग्री तक नीचे जा सकता है और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फरवरी के बाद तापमान तेजी से बढ़ता है। गर्मी के मौसम में-विशेष रूप से मई में और जून के शुरुआती दिनों में गर्मी तीव्र होती है। आमतौर पर औसत दैनिक तापमान 41.8 ° C (107.2 ° F) और औसत दैनिक न्यूनतम 26.8 ° C (80.2 ° F) के साथ वर्ष का सबसे गर्म महीना हो सकता है।
गर्म शुष्क और अक्सर धूल भरी हवाएं (स्थानीय रूप से ‘लू’ के रूप में जानी जाती हैं) दिन के समय विशेष रूप से ट्रांस-यमुना पथ में विकिरण के कारण विकिरण के प्रकोप से विकिरण को और अधिक तीव्र कर देती हैं जिससे गर्मी और अधिक बढ़ जाती है।
जलवायु में उच्च सापेक्ष आर्द्रता 70 से 80 प्रतिशत यानी मानसून के दौरान और आर्द्रता में प्रगतिशील कमी (ग्रीष्मकाल के दौरान आर्द्रता बहुत कम है यानी केवल 15 से 20 प्रतिशत)। मानसून के मौसम के दौरान आसमान पर भारी बादल छाए रहते हैं लेकिन बाकी के साल के दौरान ठंड के मौसम में एक या दो दिन के छोटे-छोटे छींटों को छोड़कर साफ या हल्के बादल छाए रहते हैं, जब ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो उस के साथ मिलकर बादल बन जाते हैं।
स्थलाकृति और स्थल
जिले को तीन अलग-अलग भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, ट्रांस-गंगा या गंगापार मैदान, दोआब और ट्रांस-यमुना या यमुनापार पथ जो गंगा और उसकी सहायक नदी, यमुना द्वारा निर्मित होते हैं, बाद में ये पूर्व में शामिल ( मिल ) हो जाते हैं। प्रयागराज, संगम के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस गंगा ट्रैक्ट में घाटियां रेतीली मिट्टी (कंकर से भरी) शामिल हैं, जिसे “ऊसर” के रूप में भी जाना जाता है जो कि तहसील हंडिया में है , पानी का स्तर ऊचा है और पानी अधिक मात्रा में है, जो कई झीलों में एकत्रित है, जो विशेष रूप से क्षेत्र की सबसे अधिक ध्यान देने योग्य विशेषता बनाती है। ट्रांस यमुना पथ बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है। जिले में मुख्य रूप से गंगा, यमुना जलोढ़ मैदान और विंध्य पठार की विशेषता है। जी.एस .आई . (2001) ने निम्नलिखित भू-आकृति संबंधी विशेषताओं की पहचान की है।
1. सक्रिय बाढ़ का मैदान: यह काफी स्थानीयकृत है और केवल नदी प्रणाली तक ही सीमित है।
2. पुराने जलोढ़ मैदान: यह सक्रिय मैदान के साथ पैच में पाए जाने वाले अपक्षय और अपरिपक्व छतों की विशेषता है।
3. रॉकी सतह (डेन्यूडेशनल हिल्स): ये ट्रांस यमुना क्षेत्र में प्रमुख हैं जो मुख्य रूप से क्वार्ट्जिटिक प्रकृति के हैं। ट्रांस गंगा का मुख्य ढलान पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसका रुख 89.30 से लेकर 93.57 तक है। जिले की नदियाँ यमुना, टोंस, साई और वरुण; गंगा की मुख्य जल निकासी प्रणाली से संबंधित हैं। वृछ के समान ड्रेनेज पैटर्न जिले में सबसे आम विशेषताएं हैं जो संरचनात्मक रूप से नियंत्रित होती हैं। पाँचवे क्रम तक की धाराएँ जिले में मिलती हैं।
जल और जल विज्ञान
गंगा नदी में जल के स्रोत वर्षा का जल, उपसतह प्रवाह और हिमखंड का पिघलना हैं। गंगा के सतही जल संसाधनों का मूल्यांकन 525 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पर किया गया है। इसकी 17 मुख्य सहायक नदियों में से यमुना, सोन, घाघरा और कोसी गंगा की वार्षिक जल उपज का आधा हिस्सा हैं। ये सहायक नदियाँ प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं और आगे की ओर बहती हैं। हरिद्वार-प्रयागराज खंड के बीच नदी के बहाव मे समस्या होती है। दिसंबर से मई तक गंगा में जल का स्तर कम होने का महीना हैं। गंगा बेसिन के प्रत्येक वर्ग किमी पर औसतन एक मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पानी वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। इसका 30% वाष्पीकरण के रूप में खो जाता है, 20% भूमीगत जल के लिए रिसता है और शेष 50% सतह अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है।
उच्च नदी तट द्वारा बंधी नदी का गहरा चैनल भूजल के प्रवाह को आधार प्रवाह के रूप में पारित करने की सुविधा प्रदान करता है। वार्षिक बाढ़ गंगा बेसिन में सभी नदियों की विशेषता है। मानसून के दौरान गंगा उठती है लेकिन उच्च नदी तट बाढ़ के पानी को फैलने से रोकते हैं। बाढ़ का मैदान आमतौर पर 0.5 से 2 किमी चौड़ा होता है। इस सक्रिय बाढ़ के मैदान में हर साल बाढ़ आती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन पर विद्यमान संरचनाएं भी इसके निर्वहन को प्रभावित करती हैं। जिले की नदियाँ गंगा की मुख्य प्रणाली से संबंधित हैं और इनमें कई उप प्रणालियाँ शामिल हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं यमुना और टोंस, वरुणा और सई की छोटी प्रणालियों सहित अन्य नदियां।
भूजल विकास
इस क्षेत्र में भूजल का विस्तार जलोढ़ के साथ-साथ सैंडस्टोन में भी पाया जाता है। जलोढ़ में यह घटक अनाज के छिद्र स्थानों में से होता है। बलुआ पत्थर में यह रेत के दानों के चौराहों पर होता है जहां वे बहुत सघन नहीं होते हैं अन्यथा, यह बलुआ पत्थर में दरारें, संयुक्त विभाजन, आदि जैसी कमजोर स्तनों के द्वारा होता है | क्षेत्र के भूजल मे सैंडर वाटर टेबल की स्थिति होती है, लेकिन गहरे जलभृत सीमित होते हैं, क्योंकि क्षेत्र में मिट्टी के बेड मौजूद होते हैं।
अफवाह प्रणाली
यमुना नदी के उत्तर का क्षेत्र लगभग एक सपाट है, जबकि दक्षिणी भाग थोड़ा सा बहाव रखता है। क्षेत्र में प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई 90.22 मीटर (196 फीट) है और गंगा और यमुना नदियों के संगम के पास 187.45 मीटर (615 फीट) बंगला में (25 ° 14’9 “: 81 ° 36’44”), क्रमशः समुद्र तल से ऊपर।
क्षेत्र की औसत स्थलाकृतिक ढलान पश्चिम उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में है। गंगा और यमुना क्षेत्र की मुख्य जल निकासी प्रणाली टोंस और बेलन नदियों के साथ मिलकर है। इसके अलावा ससुर खदेरी नदी और किल्नाही नदी दोआब के मध्य भाग से बहते पानी को इकट्ठा करती है, और इसे यमुना में ले जाती है। दक्षिणी भाग में, झगबरिया नदी यमुना तक अपवाह जल ले जाती है; लोनी और लाप्री नदी टोंस नदी तक जल ले के जाती हैं।
प्रयागराज की अपवाह प्रणाली कुछ मुख्य विशेषताओं के साथ
| क्रम संख्या | नदी का नाम | विस्तृत क्षेत्र ( वर्ग किमी) | % विस्तृत क्षेत्र |
| 1 | गंगा | 105.3 वर्ग किलोमीटर | 1.9% |
| 2 | यमुना | 63.75 वर्ग किलोमीटर | 1.17% |
| 3 | टोंस | 55.3 वर्ग किलोमीटर | 1.01% |
| 4 | बेलन | 5.85 वर्ग किलोमीटर | 0.11% |
प्रयागराज की नदियों की विस्तृत क्षेत्र को प्रतिशत मे दिखाया गया है |
प्रयागराज की नदियों की कुछ मुख्य विशेषताएँ
| क्रम संख्या | नदी का नाम | जिले के अंदर नदियों की लंबाई (किलोमीटर में ) | उदभाव स्थल | उदभाव स्थल पर की उचाई ( मी ) |
| 1 | गंगा | 117 | गंगोत्री | 4100 |
| 2 | यमुना | 51 | यमुनोत्री | 6387 |
| 3 | टोंस | 79 | सतना (म0 प्र0) | 90 |
| 4 | बेलन | 39 | सोनभद्र (उ0 प्र0) | 6316 |
इसके पूर्व और दक्षिण पश्चिम में बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में अवध क्षेत्र है और इसके पश्चिम में दोआब का निचला हिस्सा है। यह यमुना नदी का अंतिम बिंदु है और भारतीय पश्चिम का अंतिम सीमा क्षेत्र है। जिले में भूजल जलोढ़ और बलुआ पत्थर दोनों क्षेत्रों में होता है, जो कठोर चट्टानों द्वारा रेखांकित होते हैं। मानसून से पहले की अवधि के दौरान पानी की गहराई 2 से 20 मीटर के बीच होती है, जबकि मानसून के बाद की अवधि में यह 1 से 18.00 मीटर के बीच रहता है। प्रयागराज की प्रमुख नदियों में बहने वाली छोटी धाराओं के कारण जिले की जल निकासी बहुत घनी हो गई है।
प्रयागराज की प्रकृतिक अपवाह सूची
| क्रम संख्या | जल अंग का नाम | किस नदी में मिलती हैं | ||||
| 1 | गांधी नाला | |||||
| 2 | जमुदाहा नाला | |||||
| 3 | मुरधना नदी | |||||
| 4 | बंधाई नाला | बेलन नदी | ||||
| 5 | भस्मी नाला | गंगा नदी | ||||
| 6 | लपरि नाला | |||||
| 7 | लोहांदा नाला | |||||
| 8 | नादोह नाला | |||||
| 9 | करिया नाला | |||||
| 10 | सीरिजा नाला | |||||
| 11 | टुड़ियारी नदी | |||||
| 12 | नैना नदी | |||||
| 13 | लपरि नदी | |||||
| 14 | करमहा नाला | |||||
| 15 | पटपरी नाला | |||||
| 16 | काइथा नाला | टोंस नदी | ||||
| 17 | जुञ्झुरिया नाला | |||||
| 18 | करछू नाला | |||||
| 19 | घोगमा नाला | |||||
| 20 | असरवाल नाला | |||||
| 21 | गरुआ नाला | गंगा नदी | ||||
| 22 | बरखा बाहर नाला | |||||
| 23 | झगर बेरिया नाला | |||||
| 24 | गहेरा नाला | यमुना नदी | ||||
| 25 | मलरूया नाला | |||||
| 26 | सरौली नाला | |||||
| 27 | मानसना नाला | |||||
| 28 | औघर नाला | |||||
| 29 | संगरा नाला | |||||
| 30 | औंडु नाला | |||||
| 31 | गोंदरी नाला | |||||
| 32 | बैरागीय नाला | |||||
भूमि का रूप ( भूकम्प )
प्रयागराज जिला भूकंपीय क्षेत्र द्वितीय में आता है, और कुछ उत्तरी भाग जोन तृतीय के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र निम्न से मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र में है। पिछले 200 वर्षों के दौरान जिले में कोई बड़ा भूकंप नहीं देखा गया है। जिले में कई बार भूकम्प के दौरान मामूली झटके महसूस किए गए हैं।
मृदा
इलाहाबाद में मुख्य रूप से 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है:
1. काली और मोटे भूरे रंग की मिट्टी जो (यमुनापार), शंकरगढ़, कोरांव, मांडा, मेजा ब्लॉकों में जिले के 48% भूमि क्षेत्र में है।
2. यमुना खद्दर और जलोढ़ (यमुनापार) मिट्टी लोम और सैंडी लोम में समृद्ध है और जिले के 10% क्षेत्र विशेषकर जसरा, करछना, चाका, कौंधियारा में पायी जाती है।
3. गंगा काँप भूमि और गंगापार मिट्टी रेतीली दोमट मिट्टी में समृद्ध है और इसमें प्रतापपुर, हंडिया, फूलपुर नाम के ब्लॉक शामिल हैं।
4. गंगा के मैदान (गंगापार) क्षेत्र में रेतीले और दोमट मिट्टी प्रमुख हैं और जिले के 27% हिस्से में पायी जाती हैं अर्थात् ब्लॉक फूलपुर, सैदाबाद, सोरांव इसके अंतर्गत आते हैं |
वर्षा और आर्द्रता
प्रयागराज जिले की जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय है जो पूरे उत्तर-मध्य भारत द्वारा अनुभव की जाती है। प्रयागराज में विभिन्न मौसमों का अनुभव होता है जो अत्यधिक गर्म से लेकर अत्यधिक ठंड तक होते हैं। इसके तीन मौसम होते हैं: गर्म (शुष्क गर्मी), गर्म आर्द्र मानसून और ठंडी (शुष्क सर्दी)। सर्दियों का मौसम आमतौर पर नवंबर के मध्य से फरवरी तक होता है और इसके बाद गर्मी आती है जो जून के मध्य तक जारी रहती है। प्रयागराज जनवरी में घने कोहरे का अनुभव होता है जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर यातायात और यात्रा में देरी देखने को मिलती है। गर्मी का मौसम लंबा और गर्म होता है, जिसमें अधिकतम तापमान 40 डिग्री C (104 डिग्री F) से लेकर 45 डिग्री C (113 डिग्री F) तक होता है, जिसके साथ गर्म स्थानीय हवाएँ “लू” जिनहे कहा जाता है वो चलती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून बरसात कर के गर्मी के मौसम में राहत देता है जो सितंबर के अंत तक रहता है तथा वर्षा करता है। अक्टूबर के महीने और नवंबर की पहली छमाही में मानसून के बाद का मौसम होता है। प्रयागराज जिले की वर्षा आम तौर पर दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम में घटती जाती है। मानसून का मौसम जून के मध्य से सितंबर तक शुरू रहता है। वार्षिक वर्षा का लगभग 88 प्रतिशत मानसून के मौसम के दौरान जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा करता है। जिले में सामान्य वर्षा 975.4 मिमी है। (38.40 इंच) लेकिन साल-दर-साल भिन्नता देखने को प्राप्त होती है |
वन
जिले में राज्य के वन विभाग के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र 19,839 हेक्टेयर का है, जिसमें लगभग 98 प्रतिशत ट्रांस-यमुना में मुख्य रूप से दो उप-विभाजनों मेजा 14,832 और बारा 4,806 हेक्टेयर में हैं। जिले के अंदर फूलपुर और करछना में कोई वन क्षेत्र नहीं है।इस जिले के अन्तर्गत 10 प्रकार के वन आते है |
प्रयागराज के वनो के नाम
| क्रम संख्या | वनों के नाम ( आरक्षित वन ) |
| 1 | कोहदार |
| 2 | सराइया |
| 3 | सराइया कलान |
| 4 | सिंघपुर खुर्द |
| 5 | कोएहला |
| 6 | गोदरिया |
| 7 | बदिहा |
| 8 | बाजूड्डी ( आरक्षित वन ) |
| 9 | ओस ( आरक्षित वन ) |
| 10 | लाखानपुर |
जिले का भौतिकी भौगोलिक रूप
इस क्षेत्र को इस प्रकार उपविभाजित किया जाता है-
- पृथक पहाड़ी पथ 75 मी ऊचई की जिले के मध्य और दक्षिणी छोर में है |
- एक कम नोकदार ढलान के साथ उत्तरी सतह है।
- निचले स्तर की सतह दर्शाती है की बाढ़ के मैदान से केन नदी का मैदान भी मिला हुआ है।
- वर्तमान समय में केन नदी और नदियों के सहायक नेटवर्क की सीमा वाले बैडलैंड्स ट्रैक्ट भी हैं।
यह क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली बारहमासी केन नदी से निकाला जाता है, जहाँ यह यमुना नदी से मिलती है। सामान्य तौर पर, इलाके की उत्तरी दिशा की ओर ढलान है और यमुना नदी के पास एक जलोढ़ आवरण 200 मीटर की मोटाई है। यह भूभौतिकीय अध्ययनों के अनुरूप है, जो बताता है कि बुंदेलखंड ग्रेनाइट के खदानों, जलोढ़ दोहन के तहत, उत्तरी दिशा में प्रति किलोमीटर 2 मीटर की औसत ढलान प्रदर्शित करता है।
भूविज्ञान
इस क्षेत्र में भूगर्भीय सैंडस्टोन और क्वाटरनरी जलोढ़ के साथ मिले भूगर्भीय संरचनाएँ हैं। बलुआ पत्थर जिले के दक्षिणी भाग में ही पाया जाता है। इन सैंडस्टोन की सामान्य स्ट्राइक दिशा ऊतर पश्चिम – दक्षिण पूर्व से पूर्व-पश्चिम में है। चूँकि वे आम तौर पर सतह पर बहुत ही असपष्ट होते हैं, इसलिए उनके वास्तविक झुकाव का पता लगाना संभव नहीं था। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वे ज्यादातर मामलों में दक्षिण की ओर झुके हुए हैं। जब भी इन सैंडस्टोन की सीमेंट सामग्री को बाहर निकाला जाता होता है, तो वे बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले रेत को जन्म देते हैं, जिसे “शंकरगढ़ रेत” के रूप में जाना जाता है। इस रेत का उपयोग सिरेमिक उद्योग में किया जाता है।
उत्तर, पूर्व और पश्चिम में शेष क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी द्वारा कवर किया गया है। क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी में कभी-कभी कंकर, मोटे दानेदार रेत और दोमट मिट्टी भी होती है। उत्तर की ओर दानेदार सामग्री की बढ़ती मोटाई और उत्तर-पूर्व के क्षेत्र में कई गोखुर झीलों की उपस्थिति, प्राचीन काल में इन भागों के माध्यम से कुछ बड़ी नदी के बहने की संभावना का सुझाव देती है। यह धारा संभवतः गंगा ही हो सकती है। दक्षिण के जी.टी. सड़क ( ग्रांड ट्रंक रोड ) पर दानेदार सामग्री की बढ़ती मोटाई को धारा के वर्तमान प्रवाह द्वारा जमा किए जाने का सुझाव दिया जाता है। भूवैज्ञानिक रूप से जिले में जलोढ़ और विंध्यन पठार की विशेषता है। इन संरचनाओं की आयु प्रोटेरोज़ोइक काल से लेकर हाल तक है। ट्रांस गंगा और ट्रांस यमुना क्षेत्र में सतह का लिथोलॉजिकल व्यवहार काफी भिन्न है। वर्गीकरण युवा और पुराने जलोढ़ के रूप में जाना जाता है। पुराने जलोढ़ को फिर से दो उपखंडों में वर्गीकृत किया गया है-
i) बांदा का पुराना जलोढ़
ii) वाराणसी का पुराना जलोढ़
भौगोलिक रूप से यह जिला यूपी के किसी भी अन्य जिले की तुलना में अधिक जटिल है। संपूर्ण ट्रांस- गंगा पथ, दोआब का बड़ा भाग गंगा के जलोढ़ से बना है। दोआब के दक्षिणी भाग में विंध्यवासियों का जलोढ़ अवशेष के रूप में पाया जाता है। जलोढ़ की मोटाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। आम तौर पर जिले में पाए जाने वाले खनिज उत्पाद काँच के रेत, पत्थर, कंकर, ईंट आदि हैं। शंकरगढ़ (तहसील बारा) के पड़ोस में ग्लास सैंड डिपॉजिट पाए जाते हैं और उत्तर भारत में ग्लास फैक्ट्रियों की ज्यादातर जरूरतें इन डिपॉजिट्स से पूर्ण होती हैं। भवन निर्माण के पत्थर बलुआ पत्थर को नष्ट करके निकाला जाता है| जलोढ़ पथ में उपलब्ध मिट्टी को स्थानीय रूप से ईंटों और मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ‘रेह’ विशेष रूप से ट्रांस-गंगा पथ में भूमि में एक सफेद अतिक्रमण के रूप में पाया जाता है। सोडा ऐश, जो इससे निकाला जाता है, का उपयोग साबुन और कांच बनाने में, रंगाई उद्योग में और कठोर पानी के उपचार के लिए किया जाता है |
खनिज धन ( संसाधन )
सामाजिक-आर्थिक समृद्धि और आर्थिक आधार की दृष्टि से जिले की खनिज संपदा का बहुत महत्व है। यह आर्थिक अवसरों को प्रदान करके क्षेत्र को विकसित करने और अपने प्राकृतिक बंदोबस्त के साथ एक क्षेत्र को समृद्ध बनाने में काफी हद तक योगदान देता है। आम तौर पर जिले में पाए जाने वाले खनिज उत्पाद कांच के रेत, भवन निर्माणआ के पत्थर, कंकर, ईंट और रेह हैं।
ग्लास रेत:
शंकरगढ़ और लोहगरा (तहसील बारा दोनों) के पड़ोस में सबसे अच्छी कांच की रेत के भंडार के पत्थर पाए जाते हैं और उत्तरी भारत के अधिकांश कांच कारखानों की आवश्यकताओं को इन भंडारों से निकाला जाता है।
बिल्डिंग स्टोन:
कैमूर बलुआ पत्थर एक उत्कृष्ट इमारत पत्थर है। यह 150 मिमी मोटाई के बीच भिन्न बेड में स्थित है। ये पत्थर जिले के दक्षिणी हिस्सों में पाए जाते हैं।
जिले की सामाजिक स्थिति
जिला इलाहाबाद ऐतिहासिक अतीत के माध्यम से व्यापार, शिक्षा, राजनीति और धर्म त्योहारों का केंद्र रहा है। पवित्र नदी गंगा और तीन नदियों संगम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। अपने जीवंत अतीत और वर्तमान के कारण, जिले ने जनसांख्यिकी, कृषि गतिविधियों, परिवहन आदि में काफी परिवर्तन देखा है।
जिले का इतिहास
प्राचीन काल में शहर को प्रयाग (बहु-यज्ञ स्थल) के नाम से जाना जाता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि सृष्टि का कार्य पूर्ण होने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने यही पर प्रथम यज्ञ किया था, तथा उसके बाद यहां पर अनगिनत यज्ञ भी हुए। भारतवासियों के लिये प्रयाग एवं वर्तमान कौशाम्बी जिले के कुछ भाग यहां के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में रहे हैं। यह क्षेत्र पूर्व में मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के अंश तथा पश्चिम में कुशान साम्राज्य का अंश भी रहा है। बाद में ये कन्नौज साम्राज्य में आ मिला आया। 1526ई0 में मुगल साम्राज्य के द्वारा भारत पर पुनराक्रमण के बाद से प्रयागराज मुगलों के अधीन हो गया। अकबर ने यहां संगम के घाट पर एक वृहत दुर्ग का निर्माण करवाया था जो अभी भी शहर में स्थित है। शहर में मराठों के द्वारा आक्रमण भी होते रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों के अधिकार में शहर आ गया। 1775ई0 में प्रयागराज के किले में थल-सेना के गैरीसन दुर्ग की स्थापना की गयी थी। 1857 ई0 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रयागराज भी सक्रिय रहा है। 1904ई0 से 1949ई0 तक प्रयागराज संयुक्त प्रांतों (अब, उत्तर प्रदेश) की राजधानी भी था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन यहां पर ही दरभंगा किले के विशाल मैदान में 1888ई0 एवं पुनः 1892ई0 में किया गया था।
1931ई0 में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर स्वयं को गोली मार कर अपने न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को सत्य किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में नेहरु परिवार के पारिवारिक आवास आनन्द भवन एवं स्वराज भवन भी यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों के केन्द्र रहे हैं। यहां से हजारों सत्याग्रहियों को जेल भी भेजा गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु इलाहाबाद निवासी थे।
जिले का नामकारण
प्रयागराज शहर का पूर्व नाम अकबर द्वारा 1583 ई0 में रखा गया था। हिन्दी नाम इलाहाबाद का अर्थ अरबी शब्द इलाह (अकबर द्वारा चलाये गए नये धर्म दीन-ए-इलाही के सन्दर्भ से, अल्लाह के लिये) एवं फारसी से आबाद (अर्थात बसाया हुआ) – यानि ‘ईश्वर द्वारा बसाया गया’, या ‘ईश्वर का शहर’ है। 16 अक्टूबर 2018 मंगलवार के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम इलाहाबाद से बदल कर प्रयागराज कर दिया ।
प्रयागराज जिले की जनसांख्यिकीय स्थिति
| वास्तविक जनसंख्या | 59,59,798 | जनसंख्या वृद्धि | 20.74% |
| ( 1 ) पुरुष | 31,33,479 | प्रति वर्ग किलोमीटर | 5,482 |
| ( 2 ) स्त्री | 28,26,319 | घनत्व वर्ग किलोमीटर | 1,086 |
| साक्षारता अनुपात | 74.41 | कुल बच्चों की जनसंख्या ( 0-6 वर्ष ) | 885,355 |
| ( 1 ) पुरुष साक्षारता | 85.00 | ( 1 )लड़के ( 0-6 ) | 4,67,694 |
| ( 2 ) स्त्री साक्षारता | 62.67 | ( 2 ) लड़कियां ( 0-6 ) | 417,661 |
| साक्षरों की संख्या | 44,34,686 | लिंग अनुपात ( प्रति 1000 ) | 902 |
| ( 1 ) पुरुष | 26,63,457 | बच्चों का लिंग अनुपात ( 0-6 ) | 893 |
| ( 2 ) स्त्री | 17,71,254 | बच्चों का अनुपात | 148.7% |
साक्षरता
प्रयागराज जिले में कुल साक्षरता दर 74.41 प्रतिशत है, जो प्रयागराज मंडल में सबसे बड़ी है। पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 85.00 प्रतिशत और 62.67 प्रतिशत है। 2001 में कुल साक्षरता दर 62.1 प्रतिशत थी और पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर क्रमशः 62.8 और 46.38 प्रतिशत थी। इस प्रकार हमें कुल साक्षरता में 12.3 प्रतिशत और पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्रमश: 9.19 प्रतिशत और 16.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साक्षरता दर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में परिवर्तनशील पाई गई है |
ब्लॉक द्वारा वितरण साक्षर तथा साक्षरता अनुपात का प्रयागराज जिले में ( 2011 की जनगणना द्वारा )
| क्रम संख्या | ब्लॉक | कुल जनसंख्या | कुल साक्षर | साक्षारता अनुपात |
| 1 | कौड़िहार | 397184 | 241278 | 60.75 |
| 2 | होलागढ़ | 186337 | 141119 | 75.73 |
| 3 | मऊआइमा | 180459 | 140090 | 77.63 |
| 4 | सोराव | 203681 | 158954 | 78.04 |
| 5 | बहरिया | 274633 | 187406 | 68.24 |
| 6 | फूलपुर | 230925 | 168265 | 72.87 |
| 7 | बहादुरपुर | 298586 | 200344 | 67.10 |
| 8 | प्रतापपुर | 225779 | 164015 | 72.64 |
| 9 | सैदाबाद | 253125 | 206767 | 81.69 |
| 10 | धनूपुर | 231811 | 171796 | 74.11 |
| 11 | हँडिया | 206711 | 145767 | 70.52 |
| 12 | जसरा | 172937 | 123402 | 71.36 |
| 13 | शंकरगढ़ | 163586 | 120828 | 73.86 |
| 14 | चाका | 203890 | 169659 | 83.21 |
| 15 | करछ्ना | 238122 | 182106 | 76.48 |
| 16 | कोंधियारा | 151080 | 109839 | 72.70 |
| 17 | उरुवा | 200218 | 158268 | 79.05 |
| 18 | मेजा | 191942 | 129845 | 67.65 |
| 19 | कोराव | 300405 | 212999 | 70.90 |
| 20 | मांडा | 191370 | 137644 | 71.93 |
| कुल ग्रामीण जनसंख्या | 4502781 | 3254040 | 72.27 |
| कुल शहरीय जनसंख्या | 1457017 | 1180646 | 85.17 |
| कुल जिले की जनसंख्या | 5959798 | 4434686 | 74.41 |
स्रोत : statistical bulletin of Allahabad district ( 2001 and 2011 )
जनसंख्या की तुलना प्रयागराज, उत्तर प्रदेश तथा भारत के बीच ( 1981 से 2011 )
| स्थान | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| प्रयागराज | 2965396 | 3878146 | 4936105 | 5959391 |
| उत्तर प्रदेश | 105137400 | 132062322 | 166197921 | 199812341 |
| भारत | 683330152 | 846422729 | 1028610207 | 1210569707 |
जनसंख्या घनत्व की तुलना प्रयागराज, उत्तर प्रदेश तथा भारत के बीच (1981 से 2011)
| स्थान | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| प्रयागराज | 567 | 719 | 901 | 1086 |
| उत्तर प्रदेश | 377 | 548 | 690 | 829 |
| भारत | 216 | 267 | 325 | 382 |
लिंग अनुपात की तुलना प्रयागराज, उत्तर प्रदेश तथा भारत के बीच (1981 से 2011)
| स्थान | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| प्रयागराज | 849 | 873 | 879 | 901 |
| उत्तर प्रदेश | 882 | 876 | 898 | 912 |
| भारत | 934 | 926 | 933 | 943 |
साक्षरता दर की तुलना प्रयागराज, उत्तर प्रदेश तथा भारत के बीच (1981 से 2011)
| स्थान | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| प्रयागराज | 28.00 | 46.08 | 62.11 | 72.3 |
| उत्तर प्रदेश | 32.65 | 40.71 | 56.57 | 67.7 |
| भारत | 43.57 | 52.21 | 64.83 | 74.04 |
उत्तर प्रदेश के जिले की जनसंख्या की तुलना (प्रथम पाँच तथा एक आखरी(75) के जिले साथ)
| क्रम संख्या | जिले | उत्तर प्रदेश |
| 1 | प्रयागराज | 5959391 |
| 2 | मुरादाबाद | 4772006 |
| 3 | गाज़ियाबाद | 4681452 |
| 4 | आजमगढ़ | 4613913 |
| 5 | लखनऊ | 4589838 |
| 75 | महोबा | 875958 |
कृषि
प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि जिलों में से एक है। खेती के तहत क्षेत्र 3,29, 101 हेक्टेयर का है। इस प्रकार कुल रिपोर्ट किए गए क्षेत्र का 60.03 प्रतिशत खेती के अधीन है। जिला अच्छी मिट्टी, पर्याप्त भूजल और तीन बढ़ते मौसमों यानि रबी, खरीफ और जायद से संपन्न है। गेहूं मुख्य फसल है, इसके बाद चावल आता है। बाजरा, दालें, मटर, चना, सब्जियां, आलू, अमरूद, आम, खीरा और केला अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। प्रयागराज जिले के उत्तरी भाग को गंगापार के नाम से जाना जाता है, जो खाद्यान्न, दलहन, तेल बीज और सब्जियों की खेती के लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी से संपन्न है। प्रयागराजका दक्षिणी भाग, जिसे यमुनापार के नाम से जाना जाता है, आंशिक रूप से पहाड़ी और सांस्कृतिक रूप से गरीब है। पिछले दशकों के दौरान कृषि का स्तर बढ़ा है। दूसरी हरित क्रांति के बाद, प्रयागराज जिले में भी कृषि प्रथाओं में बदलाव देखा गया है। अभी भी जिले में प्रचलित खेती के पैटर्न, कृषि उत्पादन, कृषि विपणन और बदलते कृषि प्रथाओं का गहन अध्ययन करके जिले की पूर्ण कृषि क्षमता का एहसास करने की आवश्यकता है। प्रयागराज में 2011 के दौरान एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 1,77,722 हेक्टेयर बताया गया है। जलवायु, मिट्टी, फसल के पैटर्न, कृषि-बाजारों और मांगों में बदलाव से कुल (शुद्ध) बुआई क्षेत्र में भिन्नता होती है।
जिले मे ब्लॉक के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में कुल बोया गया क्षेत्र (2011)
| क्रम संख्या | ब्लॉक | सम्पूर्ण क्षेत्र(हेक्टेयर में) | कुल बोया क्षेत्र (हे 0) | कुल बोयाक्षेत्र (%) | फसलईंटेंसिटी |
| 1 | कौड़िहार | 42057 | 16154 | 38.41 | 157.02 |
| 2 | होलागढ़ | 14846 | 10138 | 68.29 | 184.10 |
| 3 | मऊआइमा | 15080 | 10165 | 67.41 | 190.01 |
| 4 | सोराव | 13495 | 9167 | 76.41 | 192.41 |
| 5 | बहरिया | 24885 | 19023 | 76.44 | 163.92 |
| 6 | फूलपुर | 22579 | 14871 | 65.86 | 171.50 |
| 7 | बहादुरपुर | 26518 | 18476 | 69.67 | 141.23 |
| 8 | प्रतापपुर | 21153 | 14347 | 67.82 | 162.10 |
| 9 | सैदाबाद | 19182 | 14082 | 73.41 | 141.39 |
| 10 | धनुपुर | 17352 | 12678 | 73.06 | 146.04 |
| 11 | हँडिया | 16107 | 11554 | 71.73 | 146.64 |
| 12 | जसरा | 26988 | 18215 | 67.49 | 121.64 |
| 13 | शंकरगढ़ | 46978 | 17153 | 36.51 | 114.79 |
| 14 | चाका | 15399 | 8809 | 57.21 | 107.04 |
| 15 | करछ्ना | 23282 | 16958 | 72.84 | 134.66 |
| 16 | कोंधियारा | 20086 | 15150 | 75.43 | 135.49 |
| 17 | उरुवा | 16940 | 11422 | 67.43 | 142.17 |
| 18 | मेजा | 44350 | 18848 | 42.50 | 169.98 |
| 19 | कोराव | 722710 | 40574 | 55.80 | 151.94 |
| 20 | मांडा | 34742 | 15623 | 44.97 | 170.15 |
| कुल ग्रामीण | 534729 | 313407 | 61.61 | 155.29 |
| कुल शहरीय | 22285 | 2933 | 13.16 | 123.32 |
| कुल जिले का | 557014 | 316340 | 60.063 | 154.00 |
स्त्रोत : statistical bulletin of Allahabad district (2011)
प्रयागराज का फसल प्रारूप
| क्रम संख्या | फसल | क्षेत्र ( ,000 हे 0 ) |
| 1 | गेहूं | 156.091 |
| 2 | चना | 60.83 |
| 3 | मटर | 44.782 |
| 4 | दाले | 23.873 |
| 5 | सरसों | 7.78 |
| 6 | लिन बीज | 1.309 |
| 7 | मक्का | 1.219 |
| 8 | ज्वार | 1.5599 |
| 9 | उरद | 49.821 |
| 10 | मूंग | 5.854 |
| 11 | तिल | 106.791 |
| 12 | मूँगफली | 22.107 |
| 13 | चावल | 10.042 |
| 14 | सोयाबीन | 1.395 |
प्रयागराज का फसल प्रारूपप्रयागराज जिले का भूमि उपयोग प्रतिरूप
| क्रम संख्या | भूमि का विशेष रूप | प्रयागराज |
| 1 | कुल भौगोलिक क्षेत्र (000 हे 0 ) | 542.012 |
| 2 | वन (000 हे 0 ) | 21.454 |
| 3 | खेती योग्य क्षेत्र (000 हे 0 ) | 13.335 |
| 4 | गैर कृषि उपयोग भूमि (000 हे 0 ) | 78.094 |
| 5 | स्थायी चरागाह (000 हे 0 ) | 1.638 |
| 6 | खेती योग्य बंजर भूमि (000 हे 0 ) | 13.335 |
| 7 | दुरुपयोग के तहत भूमि ( हे 0 ) | 9.656 |
| 8 | बंजर और अनुपजाऊ भूमि ( हे 0 ) | 16.585 |
| 9 | करंट फोलोवर्स ( हे 0) | 76.585 |
| 10 | अन्य परती भूमि ( हे 0 ) | 25.347 |
| 11 | शुद्ध रूप से बोया गया कुल क्षेत्र | 314.356 |
| 12 | एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र | 184.356 |
| 13 | सकल फसली क्षेत्र | 499.018 |
| 14 | फसल की ईंटेंसिटी | 158.3 |
भूमि उपयोग पैटर्न काफी हद तक उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं से प्रभावित होता है, जो अंततः क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
परिवहन नेटवर्क
प्रयागराज खासतौर से कुंभ मेले के समय से ही हिंदुओं के लिए तीर्थस्थल रहा है। इस प्रकार, सड़कों का एक बहुत विस्तृत नेटवर्क पुराने समय से विकसित हुआ है। मुगल काल के दौरान शहर कालीन उद्योग का केंद्र बन गया था । इसने दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, आगरा, नागपुर, बॉम्बे और कोकुट्टा शहरों के व्यापार मार्गों के विकास को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान सड़कों को और बेहतर बनाया गया था। 1883 में, जिले को दरियागंज में गंगा को पार करने के लिए 4 धात्विक सड़कों तथा ग्रांड ट्रंक रोड द्वारा सेवा दी गई थी।
सड़के
वर्तमान में, प्रयागराज जिले में 6,331 किलोमीटर की सड़कें हैं जो जिले के प्रमुख हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। नई दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 (NH-2) द्वारा प्रयागराज की सेवा की जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवहन लाइनें क्रमशः NH 96 और NH 27 हैं जो प्रयागराज को फैजाबाद और मध्य प्रदेश से जोड़ती हैं। शहर को राज्य के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले कई राज्य राजमार्ग हैं। गंगा और यमुना नदियों पर कई पुल हैं जो शहर को जिला, राज्य और राष्ट्र के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। प्रयागराज शहर के विभिन्न हिस्सों में तीन बड़े बस अड्डे हैं। स्थानीय परिवहन मुख्य रूप से रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा या सिटी बसों के माध्यम से किया जाता है। जिले 241 बस स्टॉप (193 ग्रामीण और 48 शहरी) के माध्यम से जिले के विभिन्न हिस्सों में संचालित बसों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।
रेल
प्रयागराज जिले में रेलवे के विकास का इतिहास पूर्व भारतीय रेलवे के गठन के समय 1859 का है। 1865 में, प्रयागराज यमुना पुल के माध्यम से मुगलसराय और जबलपुर के साथ जुड़ गया। वर्तमान में, प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, और सभी प्रमुख शहरों के साथ ट्रेनों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिले में 35 रेलवे स्टेशन हैं। प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज सिटी (रामबाग), दारागंज, प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयाग घाट, सूबेदार गंज, नैनी और फाफामऊ में प्रयागराज शहर की सीमा मे दस रेलवे स्टेशन हैं।
वायु मार्ग
बमरौली वायु सेना अड्डे पर स्थित प्रयागराज हवाई अड्डे से भी शहर की सेवा की जाती है। यह प्रयागराज को नई दिल्ली, लखनऊ और देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है।
जल परिवहन
राष्ट्रीय जलमार्ग – 1 की शुरुआत हल्दिया से प्रयागराज तक की गयी है। यह 1620 किमी लंबा है, जिससे यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। NW-1 को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है | आज भी NW-1 के रूप में सौंपी गई नदी के खिंचाव का उपयोग कार्गो-ज्यादातर स्थानीय उपज और पर्यटकों को लाने के लिए किया जा रहा है।
कुम्भ की प्रस्तावना (प्रथम अध्याय)
प्रयागराज के सांस्कृतिक विकास का कुम्भ मेले से संबंध (तृतीय अध्याय)
INTRODUCTION TO COMMERCIAL ORGANISATIONS
| संज्ञानात्मक नक्शा, मानसिक नक्शा या मानसिक मॉडल Cognitive Map |
गतिक संतुलन संकल्पना Dynamic Equilibrium concept
भूमण्डलीय ऊष्मन( Global Warming)|भूमंडलीय ऊष्मन द्वारा उत्पन्न समस्याएँ|भूमंडलीय ऊष्मन के कारक
प्राचीन भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएँ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है | हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है| यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- sarkariguider@gmail.com