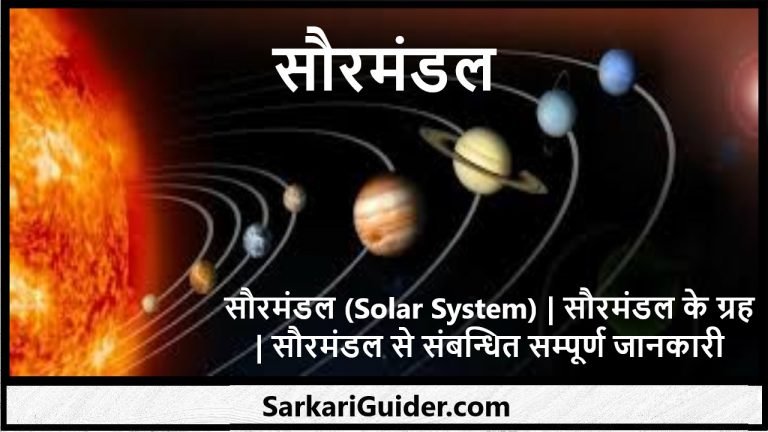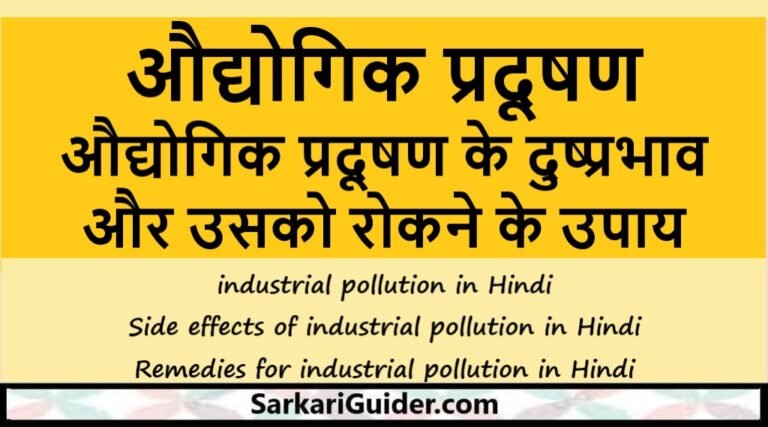भारत में लौह-इस्पात उद्योग का स्थानीकरण | लोहा एवं इस्पात उद्योग की समस्याएँ

भारत में लौह-इस्पात उद्योग का स्थानीकरण | लोहा एवं इस्पात उद्योग की समस्याएँ
भारत में लौह-इस्पात उद्योग का स्थानीकरण
लौह-इस्पात का स्थानीयकरण कच्चे मालों की ओर उन्मुख होता है। भारतीय लौह- इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में भी यही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चे मालों में लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, चूना प्रस्तर, डोलोमाइट आदि सभी भारी पदार्थ हैं जिनका बहुत दूरी तक परिवहन संभव एवं लाभदायक नहीं होता है इसीलिये अधिकांश भारतरीय लौह-इस्पात उद्योग देश के उत्तरी-पूर्वी पठारी भाग में स्थापित हैं। देश के इस भाग में देश के 10 कारखानों में से 6 ( दुर्गापुर, आसनसोल, कुल्टी, बोकारो, जमशेदपुर तथा राउरकेला) स्थित हैं। शेष चार कारखाने प्रायद्वीपीय भाग में स्थापित हैं। वस्तुतः एक टन ढलवा लोहा तैयार करने के लिए दो टन लौह अयस्क एवं तीन टन कोयले की आवश्यकता होती है। इसीलिये अधिकांश लौह-इस्पात संयंत्रों की स्थापना कोयला एवं लौह अयस्क प्राप्ति स्थलों के निकट हुई है।
लौह-इस्पात उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल-लौह अयस्क देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लौह अयस्क के भंडार बिहार, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक में, उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला बिहार एवं निम्न कोटि का कोयला मध्यप्रदेश में, चूना प्रस्तर एवं मैगनीज बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा एवं कर्नाटक आदि राज्यों में पाये जाते हैं। इसीलिए लौह- इस्पात उद्योगों की स्थापना इन्हीं राज्यों में हुई है।
उत्पादन
विगत पाँच दशकों में देश में पिग आयरन तथा इस्पात के उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि हुई है। तालिका में पिग आयरन, इस्पात पिंडों तथा तैयार इस्पात उत्पादन की प्रगति प्रदर्शित है-
तालिका- लोहा एवं इस्पात उत्पादन की उपनतियाँ (मिलियन टन)
|
वर्ष |
पिग आयरन |
इस्पात पिंड |
तैयार इस्पात |
|
1950-51 |
1.69 |
1.47 |
1.04 |
|
1960-61 |
4.31 |
3.48 |
2.39 |
|
1970-71 |
6.99 |
6.14 |
4.64 |
|
1980-81 |
9.55 |
10.33 |
6.82 |
|
1990-91 |
12.15 |
11.10 |
13.53 |
|
2000-01 |
3.39 |
– |
29.27 |
|
2001-02 |
4.08 |
– |
30.63 |
|
2002-03 |
5.28 |
– |
33.67 |
|
2003-04 |
3.76 |
– |
36.96 |
स्रात– Economics Survey, 2004-05
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत पाँच दशकों में देश में तैयार इस्पात के उत्पादन में 33 गुना वृद्धि हुई है।
भारत पर्याप्त मात्रा में पिग आयरन तथा तैयार इस्पात का निर्यात करता है। वर्ष 2003- 04 में 0.52 मिलियन टन पिग आयरन तथा 4.84 मिलियन टन तैयार इस्पात का निर्यात किया गया। भारत अपनी उत्तम इस्पात की आवश्यकता का एक भाग आयातों द्वारा पूरा करता है। तालिका 18.2 में लोहा एवं इस्पात का आयात प्रदर्शित है-
तालिका- तैयार इस्पात का आयात
|
वर्ष |
1960-61 |
1970-71 |
1980-81 |
1990-91 |
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
|
मात्रा (लाख टन) |
13.25 |
6.83 |
20.31 |
19.20 |
16.13 |
14.79 |
18.01 |
23.75 |
|
मूल्य (करोड़ रूपये) |
123 |
147 |
852 |
2,113 |
3,569 |
3,976 |
4,297 |
6,921 |
स्रोत- (Economic Survey) 2004-05 इंडिया 2005
अधिकांश आयात रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम आदि से प्राप्त होते हैं।
लोहा एवं इस्पात उद्योग की समस्याएँ
(i) देश में पूँजी की कमी है, अतः इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये गये।
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं अतः बड़ी हानियाँ उठाते रहे हैं।
(iii) अधिकांश संयंत्र अपनी स्थापित क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं। क्षमता का अपूर्ण उपयोग होने से उत्पादन लागत अधिक आती है।
(iv) रूसी तथा आसियान (ASEAN) अर्थव्यवस्थाओं के ध्वस्त होने के बाद विश्व भर में इस्पात की माँग घट गयी है। इन प्रदेशों में इस्पात उपभोग 100 मिलियन टन से घटकर 29 मिलियन टन (1999) मात्र रह गया। भारत में इस्पात उत्पादन की भरमार हो गयी है।
(v) अनेक लघु इस्पात संयंत्र निविष्टियों की कम आपूर्ति, मूल्यों में भारी वृद्धि, अपर्याप्त शक्ति आपूर्ति, कार्यशील पूँजी की कमी तथा बड़े इस्पात संयंत्रों से स्पर्द्धा आदि कारकों से रूग्ण (sick) हो गये हैं।
(vi) भारत उच्च श्रेणी के कोकिंग कोयले की कमी है। इसलिये विदेशों से उत्तम श्रेणी के कोयले के आयात की आवश्यकता पड़ती है। कोयले की आपूर्ति बाधित होने पर इस्पात संयंत्रों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
(vii) देश के अनेक संयंत्रों में इस्पात उत्पादन की पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है जो खर्चीली होने के साथ घटिया किस्म का इस्पात उत्पादन करती हैं। अतः इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने तथा उनके उत्पादों की किस्म सुधारने की आवश्यकता है।
संभावनाएँ एवं सुझाव
भारतीय इस्पात उद्योग अशुद्ध इस्पात, पिग आयरन, पिघली धातु, पिंड तथा छड़ें बनाने में पर्याप्त स्पर्द्धात्मक है। भारत को प्राथमिक इस्पात उत्पादन तथा अर्द्ध तैयार अवस्था तक उत्पादन करने में स्पर्द्धात्मक लाभ प्राप्त है जिसकी भविष्य में भी इसी प्रकार रहने की संभावना है। भारत के पास विकसित देशों तथा नव-औद्योगीकृत देशों को बड़ी मात्रा में अर्द्ध तैयार इस्पात का निर्यात करने के जबरदस्त अवसर मौजूद हैं।
भारतीय इस्पात उद्योग को अपने विकास के पूण्र्का विभव का अहसास करने तथा अपनी स्पर्द्धात्मक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिये उपयुक्त कार्ययोजना निम्नवत् है-
(i) समेकित इस्पात संयंत्रों को अपनी पिघली धातु का एक बड़ा भाग बिक्री योगय इस्पात में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिये।
(ii) अद्यतन प्राविधिकी का प्रयोग करते हुए ग्राहक-अभिमुख मूल्य वर्द्धित उत्पादों का विनिर्माण करना चाहिये।
(iii) प्राविधिकी तथा विनिर्माणी सुविधाओं के उन्नयन (upgradation) के लिये समयबद्ध योजनाएँ बनानी चाहियें।
(iv) संयंत्रों में ऊर्जा की खपत कम करने की बहुत आवश्यकता है। भारत में विद्युतीय आर्क तथा निचय भट्टियों में 570-800 इकाई ऊर्जा खर्च होती है, जबकि जापान एवं कोरिया में यह 400 इकाई मात्र है।
(v) उद्योग में प्रति व्यक्ति श्रम उत्पादकता सुधारने की आवश्यकता है जो 65 टन मात्र है। (जो विश्व की सबसे कम उत्पादकता में से है) । इस उद्योग में स्वचालन (automation) जैसे उपायों द्वारा मानव शक्ति का तर्कसंगत उपयोग करना चाहिये।
(vi) वर्तमान इकाईयों में प्रभावी द्वारा क्षमता में वृद्धि करनी चाहिये।
भूगोल – महत्वपूर्ण लिंक
- सांस्कृतिक प्रदेश | सांस्कृतिक परिक्षेत्र से तात्पर्य | विश्व के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रदेश
- एशिया में कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं | एशिया में कृषि की पद्धतियाँ
- अर्थव्यवस्था का उद्भव व विकास | विश्व में कोयला का वितरण एवं उत्पादन का वितरण
- भारतरीय मिट्टियों का वर्गीकरण | भारतवर्ष में पायी जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण | भारत की मिट्टियों की विशेषता अथवा लक्षण
- मिट्टी के कटाव का तात्पर्य | मिट्टी के अपरदन को रोकने के उपाय | मिट्टी की उर्वरता को बनाये रखने के लिए उर्वरकों के महत्व पर प्रकाश
- मानसून की उत्पत्ति | भारतीय मानसून के उद्भव की संकल्पना
- भारत में बाक्साइट का वितरण | भारत में बाक्साइट के उत्पादन का वितरण
- भारत के जलवायु प्रदेश | भारत को कृषि-जलवायु प्रदेश | भारत के कृषि-जलवायु प्रदेश की विशेषता
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]