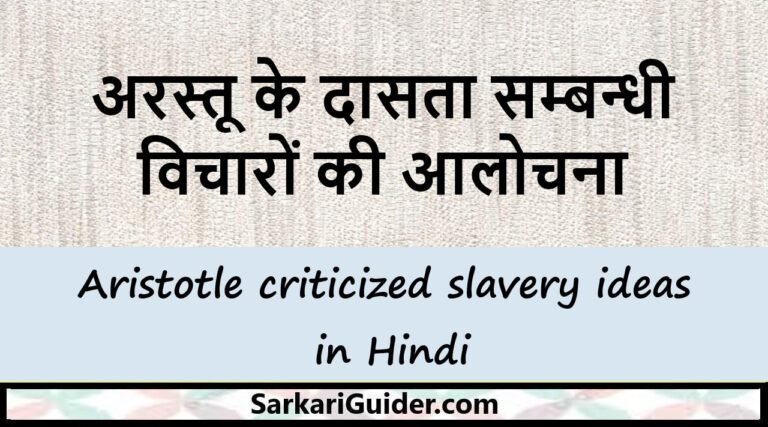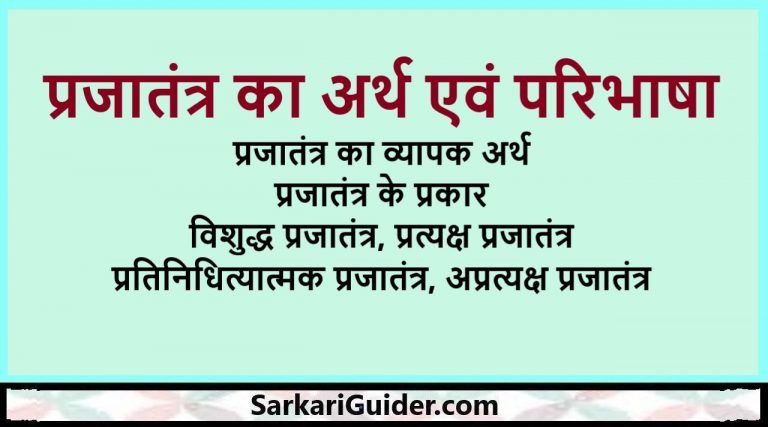मध्य युग के राजनीतिक चिन्तन की सामान्य विशेषतायें | General characteristics of political thinking of the Middle Ages in Hindi

मध्य युग के राजनीतिक चिन्तन की सामान्य विशेषतायें | General characteristics of political thinking of the Middle Ages in Hindi
मध्य युग के राजनीतिक चिन्तन की सामान्य विशेषतायें
राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मध्य युग में कुछ लेखकों द्वारा ‘अंध युग’ (Dark Age) माना जाता है। बार्कर इस युग के विचारकों को राजनीतिक चिन्तकों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं करता, क्योंकि इस युग के विचारक स्वतन्त्र मौलिक चिन्तन के बजाय पाठ्य-पुस्तकीय ज्ञान का ही प्रदर्शन करते रहे हैं। उनके चिन्तन का कोई क्रमबद्ध विषय नहीं था। कुछ चिन्तक ‘बाइबिल’ (Bible) को तो कुछ अरस्तू तथा उसकी पुस्तक ‘पॉलिटिकस (Politicus) को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उनके आधार पर अपने राजनीतिक सिद्धान्तों की रचना करते रहे। फलतः राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में किसी प्रकार की स्पष्टता नहीं थी। इस युग में स्वतंत्र मौलिक चिन्तन बहुत कम हुआ। वस्तुतः यह युग मौलिक चिन्तन का नहीं, वरन् केवल पाचन का था।
मध्य युग में विवेक के स्थान पर धर्म की प्रधानता थी, अतः इसे ‘श्रद्धा या आस्था का युग’ (Age of Faith) भी कहा जाता है। इस युग के चिन्तन और आकांक्षाओं का केन्द्र-बिन्दु धार्मिक आदर्श थे और इसमें आस्था तथा विश्वास की प्रबलता थी। रोमनों के राजनीतिक उत्तराधिकारी बर्बर जर्मनों में बाहुबल, शक्ति और उत्साह की तो प्रबलता थी, किन्तु इनमें प्राचीन यूनानियों की सी बौद्धिक प्रखरता और प्राचीन रोमनों की सी कानूनी तथा प्रशासनिक योग्यता का अभाव था। इसके अतिरिक्त, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक जर्मनों द्वारा शासित पश्चिमी यूरोप में स्थिति इतनी अनिश्चित और डावांडोल रही कि उसमें राजनीतिक अथवा दार्शनिक चिन्तन, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में कोई रचनात्मक गतिविधि हो ही नहीं सकती थी। रोम में चर्च का प्रभाव बढ़ते जाने के कारण कई शताब्दियों तक स्वतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्ष, राजनीति चिन्तन का मार्ग अवरुद्ध हो गया परिणामस्वरूप गैटिल के शब्दों में, “विवेक दासा की स्थिति में पहुँच गया, ज्ञान का विकास दब गया और राजनीतिक चिन्तन का उस समय अवसान हो जाता है, जब वह सांसारिक और धार्मिक सत्ताओं के सम्बन्ध में किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन कर चुकता है।” अतः नवीन मौलिक चिन्तन के अभाव और राजनीतिक चिन्तन पर धार्मिक चिन्तन की प्रधानता के कारण कुछ लेखकों द्वारा मध्ययुग को ‘राजनीतिक चिन्तन से शून्य’ कहा गया है। ब्राइस के अनुसार “मध्य युग मूलतः अराजनीतिक था।”
लेकिन मध्य यग को ‘राजनीतिक चिन्तन से शन्य’ या ‘मलतः अराजनीतिक’ कहना सत्य नहीं है। प्रथमतः, मध्य युग पाँचवीं सती से लेकर पन्द्रहवीं सदी के उत्तराद्द्ध तक माना जा सकता है। मध्य युग का दो भागों में विभाजन हो जाता है। इनमें प्रथम भाग तेरहवीं शताब्दी तक का है। और द्वितीय भाग चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं सदी का है। इसके केवल प्रथम भाग में ही धार्मिक चिन्तन की प्रधानता थी और द्वितीय भाग में तो राजनीतिक संस्थाओं के महत्त्व को स्पष्ट करने वाले राजनीतिक चिन्तन का प्रतिपादन हुआ। प्रथम युग में चर्च की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया| इन दोनों ही कालों में राजनीतिक चिन्तन की दृष्टि से व्यापक अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत की गयी, जिसके मुख्य विषय थे चर्च संगठन और उसके कार्य, शान्ति तथा न्याय सम्बन्धी विचार, चर्च और लौकिक सत्ता का सम्बन्ध, सामन्तवाद, सामुदायिक जीवन और स्वायत्तता की धारणा, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं का महत्त्व और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का पुनरोदय, आदि।
मध्य युग में विविध राजनीतिक विषयों पर जो व्यापक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की गयी, उसे दृष्टि में रखते हुए इसे राजनीतिक चिन्तन की दृष्टि से ‘अन्ध युग’ या ‘मूलत; अराजनीतिक युग’ नहीं कहा जा सकता। मध्य युग के राजनीतिक चिन्तन की अपनी विशेषताएँ हैं और मध्य युग के द्वारा राजनीतिक चिन्तन को महती देन दी गयी है।
मध्य युग के राजनीतिक चिन्तन की विशेषताओं और राजनीतिक चिन्तन को उसकी देन का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है।
(1) सार्वभौमिकता या सम्पूर्ण मानव समाज की एक इकाई के रूप मे कल्पना-
बार्कर ने कहा है कि “मध्य युग के चिन्तन का सार उसका सार्वभौमिकतावाद है।’ गियर्क के अनुसार, “मध्य युग की सभी शताब्दियों में ईसाई जनता को मानव जाति से अभिन्न एक सार्वभौम समाज के रूप में माना जाता रहा और यह विश्वास था कि इसकी स्थापना तथा शासन भगवान द्वारा होता है।” रोम ने इस सार्वभौमिक साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें तत्कालीन समस्त सभ्य संसार समाया हुआ था। रोमनों का विश्वास था कि उनका साम्राज्य ईश्वर-इच्छा की सृष्टि है और उनके भाग्य में शाश्वत तथा सार्वभौमिक होना लिखा है। जब ईसाई धर्म साम्राज्य का एकमात्र राजकीय धर्म हो गया, तो ईसाइयों ने भी साम्राज्य के इस विश्वास को अपना लिया। ईसाई धर्म की शिक्षा का एक सारभूत तत्व मानवीय समानेता, एकता और विश्वबन्धुत्व की धारणा थी। ईसाई धर्म प्रचारकों तथा धर्मोपदेशकों ने समस्त ईसाइयों के मध्य एकता स्थापित करने के उद्देश्य से एक ‘सार्वभौम ईसाई समाज’ की स्थापना का उद्देश्य अपनाया।
उस समय समस्त ईसाई जगत एक ईसाई राज्य समझा जाता था, जिसमें चर्च का सदस्य होना और नागरिक होना एक ही बात थी। इस समाज के दो प्रधान थे-पोप तथा सम्राट। सम्राट लौकिक विषयों का और पोप आध्यात्मिक विषयों का संरक्षक था। इस प्रकार के दो प्रधान होते हुए भी इस सार्वभौमिक समाज में धर्म की इतनी अधिक प्रधानता थी कि कोई भी व्यक्ति बिना ईसाई हुए राज्य का नागरिक नहीं हो सकता था और धर्म-बहिष्कृत व्यक्ति को कोई राजनीतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। चर्च ने जीवन के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आदि सभी क्षेत्रों में ईसाइयत के सिद्धान्त लागू कर इन्हें एक सूत्र में बाँधने का कार्य किया। विभिन्न देशों और जातियों के व्यक्तियों पर ईसाइयत ने एकसमान धार्मिक और कानूनी व्यवस्था लागू कर उन्हें एक सार्वभौम समाज का अग बनाया और एकत्व के सिद्धान्त पर बल दिया।
(2) चर्च की स्थिति और सत्ता सर्वोच्च-
मध्य यूग के राजनीतिक चिन्तन और व्यवहार में चर्च की स्थिति*और सत्ता सर्वोच्च थी। जब प्यूटन आक्रमणकारियों ने शासन सत्ता को निर्बल कर दिया तो बिशप तथा चर्च संगठन ने राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में धार्मिक सत्ता का प्रयोग सम्राटों के द्वारा किया जाता था और चर्च संगठन उनकी अधीनता में था, लेकिन कालान्तर में स्थिति बदलने लगी। सम्राटी की सत्ता निर्बल होने तथा चर्च अधिकारियों के अधिक बद्धिमान होने के परिणाम स्वरूप समाज में चर्च का प्रभाव बढ़ने लगा और चर्च अधिकारियों ने असभ्य आक्रमणकारियों पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इस प्रकार चर्च के द्वारा यह दावा किया जाने लगा कि रोम का पोप न केवल धार्मिक मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता है, वरन् उसे राजनीतिक तथा लौकिक क्षेत्र में भी राजाओं को दण्डित तथा पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है। 1075 ईo में पोप ग्रेगरी सप्तम् ने निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर चर्च की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन किया था (i) रोमन चर्च की स्थापना स्वयं ईश्वर द्वारा की गयी है। (ii) पोप की आज्ञा के बिना चर्च की कोई परिषद् नहीं बुलायी जा सकती। (iii) रोमन चर्च ने कभी कोई गलती नहीं की और वह कभी कोई गलती नहीं करेगा। (iv) विशपों को पदच्युत करने का अधिकार केवल पोप को ही है। (v) पोर को राजाओं पर नियन्त्रण रखने की शक्ति प्राप्त है और वह सम्राटों को सिंहासनच्युत कर सकता है। (vi) पोप के कार्यों पर अन्य कोई व्यक्ति विचार नहीं कर सकता, वह केवल ईश्वर के ही प्रति उत्तरदायी है।
(3) राजतन्त्र को मान्यता-
मध्य युग का सर्वप्रमुख तत्व था-सार्वभौमिकता और इस सार्वभौमिकता का सहवर्ती तत्व था-एकता का सिद्धान्त। चर्च और राज्य दोनों के ही संगठन का सर्वप्रमुख लक्ष्य एकता की प्राप्ति था और इस एकता की प्राप्ति राजतन्त्र अर्थात् एक व्यक्ति के प्रभुत्व को स्वीकार करके ही की जा सकती थी, अतः राजतन्त्र को मान्यता प्रदान की गयी। मध्य युग के एक प्रमुख विचारक दांते ने यही विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि “राजनीतिक जीवन को एक सूत्र में पिरोने वाला तत्व इच्छा है और इच्छाओं में एकता स्थापित करने के लिए एक
व्यक्ति का शासन सर्वोत्तम है। अतः राजनीतिक क्षेत्र में राजा का तथा धार्मिक क्षेत्र में पोप का शासन होना चाहिए। राजा इस पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि होकर शासन करता है।” मध्य युग में वशानुगत राजतन्त्र के साथ-साथ निर्वाचित राजतन्त्र को भी अपनाया गया था।
(4) सामन्तवाद-
मध्य युग में एकत्व के प्रतीक राजतन्त्र को अवश्य ही अपनाया गया था लेकिन इसके साथ ही सत्ता विकेन्द्रीकरण था और इस विकेन्द्रीकरण के प्रतीक के रूप में सामन्तवाद (Feudalism) को अपनाया गया था। सामन्तवाद के दो प्रकार अथवा रूपं हैं-एक, राजनीतिक और दूसरा, आर्थिक। राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही रूप में सामन्तवाद का अर्थ है ‘सत्ता का विकेन्द्रित होना’। यह एक ऐसा पदसोपानात्मक संगठन होता है जिसमें सर्वोच्च शिखर पर राजा होता है, उसके नीचे प्रमुख सामन्त, उसके नीचे उप-सामन्त, उसके नीचे और छोटे दर्जे के उप-सामन्त हो सकते हैं और संसबे नीचे के स्तर पर जनता। इसमें से प्रत्येक अपने से तुरन्त ऊपर वाले स्वामी के अधीन होता है, जो स्वयं अपने से उच्चतर स्वामियों के अधीन होते हैं। आर्थिक क्षेत्र से सामन्तवाद का अर्थ, भूमि अधिग्रहण की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें राजा से सामन्त, सामन्त से उप-सामन्त और उप-सामन्तों से वे व्यक्ति भूमि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में भूमि जोतते हैं। इस प्रकार सामन्त में ‘नागरिकता शब्द का सारा अर्थ ही समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर स्वामी तथा सेवको के सम्बन्धी का जन्म होता है। सामन्तवाद एक संक्रमणकालीन व्यवस्था ही थी और राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।
(5) राजसत्ता पर प्रतिबन्ध-
मध्य युग में यद्यपि न केवल राजतन्त्र को अपनाया गया था, वरन् राजपद में देवी सत्ता की कल्पना भी की गयी थी, लेकिन ऐसा होते हुए भी मध्य युग का राजतन्त्र निरंकुश नहीं, वरन् मर्यादित था और उस पर कुछ प्रतिबन्ध थे। प्रथम, मध्य युग में कानून का स्वरूप सामान्यतया परम्परागत था इसलिए राजा का अधिकार कानूनों का निर्माण नहीं, वरन् उनकी उद्घोषणा मात्र था। राजा के द्वारा परम्पराओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। द्वितीय, राजा के द्वारा राजपद ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाती और प्रतिज्ञाएँ की जातीं, वह उससे बँधा होता था और ये भी राजा की सत्ता पर प्रतिबन्ध थे। तृतीय, तत्कालीन सामन्तवादी व्यवस्था के कारण सविदा का प्रचलन था और प्रजा के कुछ ऐसे मॉलिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार माने जाते थे, जिसका उल्लंघन कोई भी राजकीय आदेश नहीं कर सकता था। इन सबके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था विकेन्द्रीकृत थी, राजा समस्त सत्ता का प्रतीक तो था, लेकिन इसका स्वयं ही प्रयोग करने की स्थिति में नहीं था। मध्य युग का एक विचारक जॉन ऑफ सेलिसबरी तो राजसत्ता को मर्यादित रखने की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल देता था। उनका कथन है “तलवार धारण करने वाला (बल प्रयोग और अत्याचार करने वाला) तलवार से ही (बल प्रयोग से ही) नष्ट होगा।” इन्हीं सब बातों के आधार पर मैक्वेलन ने कहा है कि “मध्यकालीन राजा यद्यपि पूर्ण सत्ता रखता था, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, फिर भी उसके अधिकार सीमित थे।”
(6) प्रतिनिध्यात्मक शासन-
जिन बर्बर प्यूटन आक्रमणकारियों के द्वारा रोमन साम्राज्य को नष्ट कर अपनी सत्ता स्थापित की गयी थी, उनमें प्रतिनिध्यात्क संस्थाओं की परम्परा प्रचलित थी और मध्य युग ने उनसे इन परम्पराओं को ग्रहण किया। इस प्रकार की प्रतिनिध्यात्मक परम्पराओं के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। प्रथम, प्रतिनिधि शासन के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए पोप के चुनाव की पद्धति को अपनाया गया था, जिसमें विभिन्न चर्चों के प्रतिनिधियों का समूह पोप का निर्वाचन करता था। द्वितीय, चर्च के संगठन और व्यवस्था में चर्च के प्रतिनिधियों की परिषद् को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। यह परिषद् विभिन्न विवादास्पद विषयों का अन्तिम निर्णय करती थी और पोप को पदच्युत भी कर सकती थी। चर्च के प्रतिनिधियों की इस परिषद में विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधि होते थे, जिन्हें उन प्रान्तों के निवासियों की संख्या तथा गुणों के आधार पर लिया जाता था। पोप की निरंकुशशाही के अन्तर्गत तो ये प्रतिनिध्यात्मक भावनाएँ कुछ दबी रहीं, लेकिन 14वीं शताब्दी में मार्सीग्लियो तथा विलियम ऑफोकम जैसे राजसत्ता के समर्थकों ने राज्य तथा चर्च दोनों के लिए ही प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया और भविष्य में यह सिद्धान्त कन्सीलिंयर आन्दोलन का प्रमुख आधार बना।
(7) लोकप्रभुसत्ता की धारणा-
मध्य युग में जहाँ एक और राजा में देवत्व का आरोपण किया जाता था, वहाँ दूसरी ओर जनता के भी कुछ दैवी अधिकार माने जाते थे, जिनके आधार पर कालान्तर में लोकप्रिय प्रभुसत्ता की धारणा का विकास हुआ। मध्य युग में इस रोमन विचार को माना जाता रहा कि प्रभुशक्ति जनता में ही विद्यमान है और जनता को शासक चुनने का अधिकार है। इस धारणा का समर्थन टामस एक्वीनास के विचारों में पाया जाता है। मार्सीग्लियो ने इस विचार को और आगे विकसित करते हुए कहा कि ‘कानून निर्माता की प्रभुसत्ता सम्पन्न होता है और कानून निर्माण का अधिकार जनता को ही है। निकोलस के द्वारा इस धारणा को और बल प्रदान किया गया। समस्त मध्य युग में इस विचार को मान्यता प्राप्त रही कि कानून का उद्देश्य समाज हित है और इसका निर्माण समस्त समाज की स्वीकृति से होना चाहिए। राजा केवल उस कानून को लागू करने वाला अभिकत्ता मात्र है और उसकी स्थिति किसी भी रूप में कानून से ऊपर नहीं है। वर्तमान युग में लोकप्रिय प्रभुसत्ता की धारणा का जो रूप है, उस पर मध्य युग के चिन्तन का पर्याप्त प्रभाव है।
(8) सामुदायिक जीवन-
मध्य युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति सामुदायिक अथवा समुदायगत जीवन व्यतीत करने की थी। मध्यकालीन परिस्थितियों में एकाकी व्यक्ति अपने आप को बहुत निर्बल समझता था, अतः उसने अनुभव किया कि किन्हीं समुदायों की सदस्यता प्राप्त कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है। अतः वह विभिन्न प्रकार के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समूहों के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार के समूहों के कुछ प्रधान रूप थे-ईसाई मठ, परिव्राजक समुदाय, आर्थिक श्रेणियाँ, कम्यून और नगर। एक्वीनास ने नगर को सामुदायिक जीवन का एक सर्वोत्तम नमूना बताया है। सामदायिक जीवन की प्रधानता के कारण मध्य युग में व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतन्त्रता उपेक्षित ही रहे। सामुदायिक जीवन की प्रधानता के कारण ही मध्य युग में नियमों के सिद्धान्त का विकास हुआ और यह माना जाने लगा कि विभिन्न सामुंदायों का अपना एक कानूनी व्यक्तित्व होता है।
राजनीतिक शास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- सन्त टामस एक्विनास की जीवनी । सन्त टामस एक्विनास की रचनायें | Biography of Saint Thomas Aquinas in Hindi | Compositions of Saint Thomas Aquinas in Hindi
- सन्त टामस एक्वीनास के राजनीतिक विचार | Political views of Saint Thomas Aquinas in Hindi
- एक्वीनास के कानून सम्बन्धी विचार | Aquinas law in Hindi
- मध्य युग के राजनीतिक चिन्तन की सामान्य विशेषतायें | General characteristics of political thinking of the Middle Ages in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]