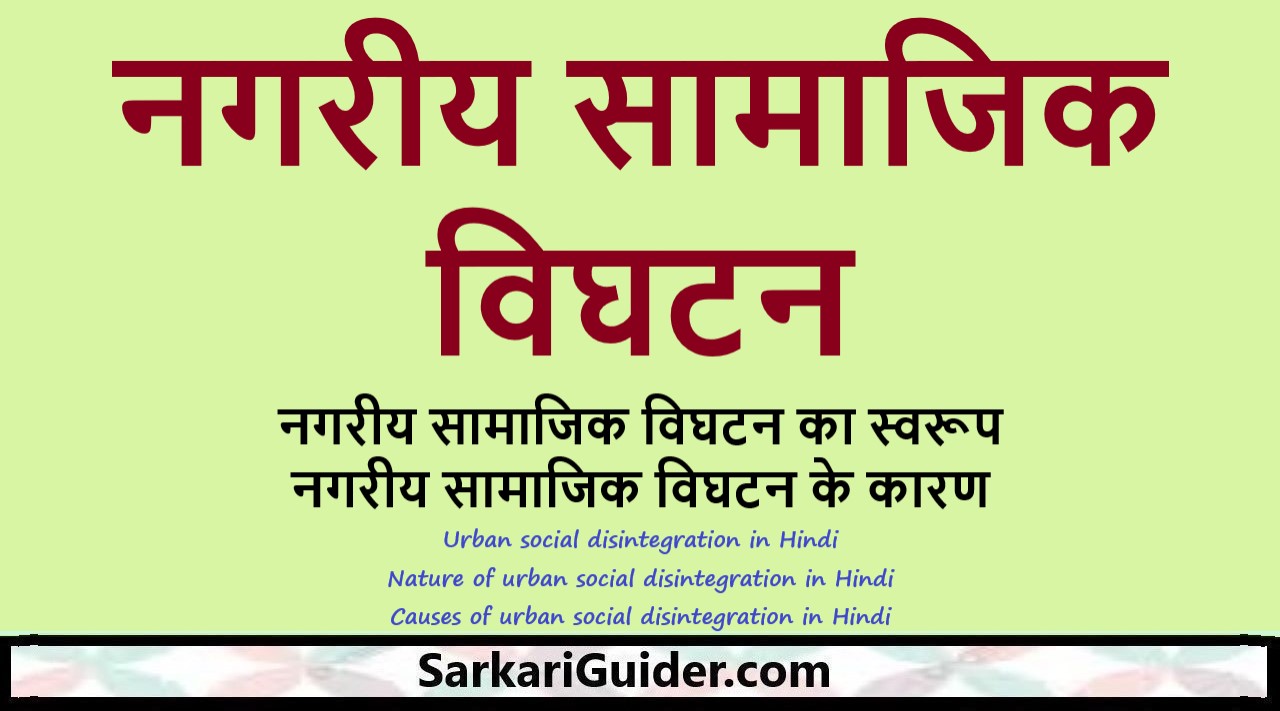नगरीय सामाजिक विघटन | नगरीय सामाजिक विघटन का स्वरूप | नगरीय सामाजिक विघटन के कारण
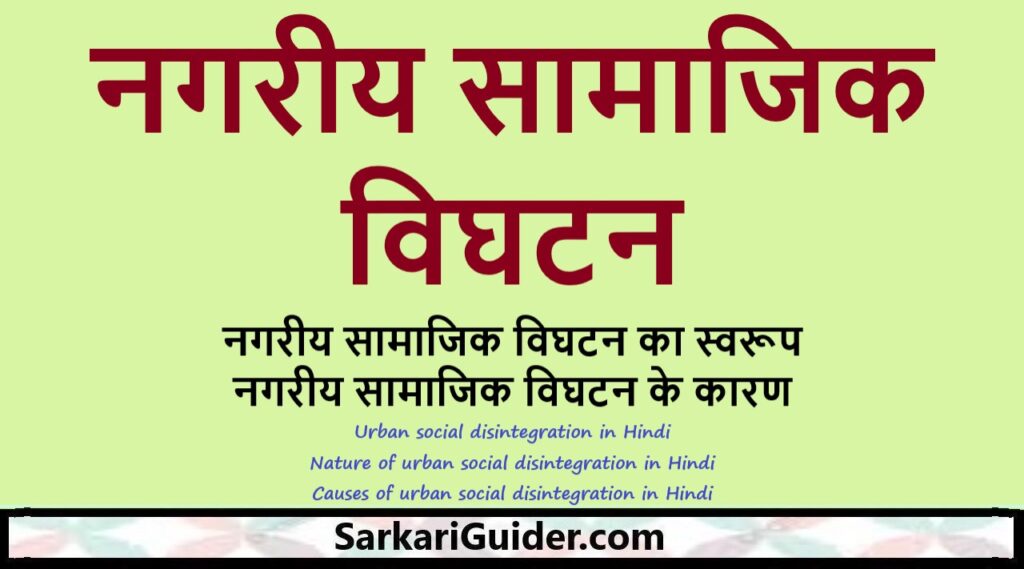
नगरीय सामाजिक विघटन | नगरीय सामाजिक विघटन का स्वरूप | नगरीय सामाजिक विघटन के कारण | Urban social disintegration in Hindi | Nature of urban social disintegration in Hindi | Causes of urban social disintegration in Hindi
नगरीय सामाजिक विघटन
विघटन की प्रक्रिया से न तो ग्रामीण समाज अछूता है और न नगरीय अन्तर केवल इतना है कि नगरीय समुदाय में विघटन की दर तीव्र होती है। इसके विपरीत ग्रामीण समाज में परिवर्तन की दर मन्द होती है। अतएव विघटन की गति भी मन्द होती है।
नगरीय सामाजिक विघटन का स्वरूप-
सामाजिक विघटन के स्वरूप होते हैं, जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विघटन होता है तो उसे वैयक्तिक विघटन कहते हैं। मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति और आत्महत्या इसकी अभिव्यक्तियाँ हैं। परिवार के क्षेत्र में इसे पारिवारिक विघटन कहते हैं। यह पारिवारिक तनाव, पृथक्करण, विवाह-विच्छेद आदि के रूप में प्रकट होता है।
नगरीय सामाजिक विघटन के कारण-
सामाजिक विघटन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। नगरीय समाज के सन्दर्भ में निम्न कारक उल्लेखनीय हैं-
- अधिक जनसंख्या- नगरों में जनसंख्या की वृद्धि भी सामाजिक विघटन का कारण है। इससे अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। विगत अनेक वर्षों से नगरीय जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या के अधिक घनत्व के कारण अवांछित परिवर्तन होता है।
भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि सामाजिक परिवर्तन को एक प्रगतिशील मोड़ देने में बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु वर्तमान समाज में जिसमें हम रह रहे हैं कल के समाज से अनेक अर्थों में भिन्न है। जब जनसं कम थी तब समाज की ऐसी दशा नहीं थी। कृषि आजीविका का प्रधान व्यवसाय था पर आज की बढ़ती आबादी वाला समाज असंख्य समस्याओं का स्रोत बन गया है।
जनसंख्या में जब किसी कारण से परिवर्तन होता है तो व्यावहारिक तथा सामाजिक जीवन के सभी पक्ष इससे प्रभावित हैं। जब जनसंख्या एक खनिज पदार्थ के स्थान पर एकत्र हो जाती है तो उस स्थल पर नगर का विकास होने लगता है और लोगों के रहन-सहन में अनेक परिवर्तन होते हैं। आज हम नगरों और गाँवों की दशा पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि नगरों में होने वाले व्यापक परिवर्तनों का बहुत बड़ा कारण जनसंख्या का जमाव है तथा गाँवों में सामाजिक परिवर्तन धीरे-धीरे होने का कारण जनसंख्या में परिवर्तन का न होना भी है। फलस्वरूप नगरीय समाजों में विघटन की मात्रा अधिक पायी जाती है।
- उद्योगों की वृद्धि- वेब्लेन तथा अन्य समाजशास्त्रियों में औद्योगिकीय कारक को सामाजिक परिवर्तन का प्रधान कारक माना है। उनका कथन है कि औद्योगिकीय कारक ही सामाजिक परितर्वन तथा विघटन के लिए उत्तरदायी हैं।
मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सभ्यता का निर्माण किया है। इस प्रकार जब वह कौशल या विधियों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है तो सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। अपनी पुरानी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के वास्ते जब हम नये साधनों का सहारा लेते हैं तो सामाजिक परिवर्तन को बल देते हैं। उदाहरणार्थ इंगलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् वहाँ के समाज में भी विकट परिवर्तन हुआ। सारे समाज के व्यवहार तथा रहन-सहन की अवस्था में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अमेरिका तथा जापान की भी यही अवस्था हो गयी है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक परिवर्तन के कारण ही नगरीकरण का प्रभाव बढ़ा और छोटे-मोटे गाँव उजड़ गये तथा उनके निवासी नगरों के आधुनिक निवासी बन गये, जिनके कारण उनके रहन-सहन में, अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा समाज विघटित होता जा रहा है और उसमें नगरीकरण के दोषों का उत्तरोत्तर समावेश हो रहा है।
- नवीन आविष्कार और नवीन विचार- मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। उसे कभी स्थिर दशा में सन्तोष नहीं होता। उसके विचारों में सदैव परिवर्तन होता है। इसी कारण समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नये विचार आते जा रहे हैं। आज का राजनीतिक क्षेत्र इस दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट दृष्टान्त के रूप में लिया जा सकता है, साम्यवादी, समाजवादी तथा पूँजीवादी विचारधाराओं के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ है।
सामाजिक ढाँचे पर आविष्कारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑगबर्न ने रेडियो के 150 प्रभाव बताये हैं। उन्होंने मोटरकार तथा रेडियों के आविष्कार के प्रभावों को लेकर निष्कर्ष निकाला है कि आविष्कार सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तन के आधार हैं। वायुयान, बेतार के तार, टेलीविजन, औषधियाँ, चिकित्सा आदि अनेक आविष्कारों ने हमारी जीवन शैली में परिवर्तन किया है।
- सामाजिक आविष्कार- अभौतिक संस्कृति में जब आविष्कार होते हैं, तो उनको सामाजिक आविष्कार कहते हैं। यह सामूहिक आविष्कार (Group Invention) होता है। इस प्रकार सामाजिक विघटन, औद्योगिक विघटन औद्योगिक आविष्कारों तक ही सीमित नहीं रहता, वरन् सामाजिक आविष्कार भी सामाजिक विघटन के कारण होते हैं। राज्य द्वारा निर्मित विभिन्न सामाजिक अधिनियम भी मानव व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हैं।
यदि उपभोक्ता वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगा दिया जाये और उत्पादन के साधन तथा आय पर, कर न लगाये जायें तो पूँजीपतियों को धन इकट्ठा करने का मौका मिलता है। फलस्वरूप सामान्य जनता में गरीबी फैलती है। निषेध कानून भी एक सामाजिक आविष्कार है और सामाजिक परिवर्तन का पोषक है। यदि एक ओर शराब पीने का निषेध किया जाये और दूसरी ओर शराब बनाने वाली फैक्टरियों की स्थापना की जाये, तो इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है और सामाजिक विघटन होता है।
- सांस्कृतिक कारक- मैक्स वेवर ने विभिन्न धर्मो और आर्थिक व्यवस्थाओं की तुलना करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि संस्कृति में परिवर्तन होने के कारण समाज में भी परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक कारक किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, इस दृष्टिकोण को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं –
(i) संस्कृति संचय करती है। नेल्सन ने सिद्ध कर दिया है कि संस्कृति संचय की एक दशा है। हमारे पूर्वज किसी समय पाषाण युग में थे। उसके बाद हम लकड़ियों के घर में रहते थे और आज गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में बिहार करते हैं। इस प्रकार समय में भी परिवर्तन हुआ है।
(ii) संस्कृति में सदैव योगदान होता रहता है, चाहे वह भौतिक संस्कृति हो अथवा अभौतिक संस्कृति पर क्रिया सदैव होती रहती है।
(क) भौतिक संस्कृति- भौतिक संस्कृति में जिस प्रकार मोटरकार, वायुयान तथा अन्य आवागमन के साधन प्रतिदिन गतिशील हैं उनसे सामाजिक परितर्वन होता है।
(ख) अभौतिक संस्कृति- अभौतिक संस्कृति में संचय की प्रतिक्रिया बहुत ही धीरे- धीरे होती रहती है जो आसानी से देखी नहीं जा सकती। पर किसी भी संस्कृति के रीति-रिवाज पर ध्यान रखें तो स्पष्ट होता है कि उसमें अनेक योग हुए हैं।
(iii) संस्कृति एकाएक अवतरित नहीं होती वरन् धीरे-धीरे विकसित होती रहती है। उसमें नित्य नये तत्वों का समावेश होता रहता है। यदि हम अभौतिक संस्कृति के आवागमन के साधनों को लें तो पता चलेगा कि सर्वप्रथम मनुष्य हजारों मील की यात्रा पैदल करता था। उसके बाद उसने घोड़े की शरण ली, नाव आदि का सहारा लिया, फिर रेल इंजन का प्रयोग हुआ। आज वह राकेट से दूसरे ग्रहों पर जा रहा है। इस प्रकार संस्कृति के क्रम में निरन्तरता पायी जाती है।
इन दशाओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते कि संस्कृति में सदैव एकीकरण, संचय, योगदान तथा निरन्तरता की अवस्था पायी जाती है, जिससे सांस्कृतिक संघर्ष आदि की भी अवस्था आ जाती है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार संस्कृति की कोई भी दिशा क्यों न हो पर सांस्कृतिक कारकों के कारण भी सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न हो जाती है।
- युद्ध- युद्ध को आगबर्न ने सामाजिक आविष्कार कहा है तथा अब समाजशास्त्रियों ने इसे सामाजिक संस्था के रूप में मान लिया है। युद्ध सामाजिक विघटन का विकृत रूप कहा गया है। युद्ध के कारण अनेक प्रकार के आविष्कार होते हैं। इसके अलावा अनेक नयी व्यवस्थायें की जाती हैं जिनके फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाती है और सामाजिक विघटन होता है। युद्ध में जनसंख्या का अधिक हास होता है, नैतिक साधन नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है। विजयी के सम्मुख पराजित की सारी इच्छाएँ झुक जाती हैं और इस प्रकार उस देश की आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था विघटित हो जाती है।
- मनोवैज्ञानिक कारक- आज के युग में निल-मालिकों तथा मजदूरों के बीच की मनोवैज्ञानिक तथा मुख्यतया औद्योगिक साधनों के प्रयोग पर बल देती है और नित्य ऐसे नवीन उपाय ढूंढ़े जाते हैं, जिससे मजदूरों को कम लगाने पड़े। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार यही मानसिक अवस्था नये विचारों को जन्म देती है जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है जो समाज को विघटन की तरफ ले जाता है।
- सामाजिक परिवर्तन- सामाजिक विघटन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। सामाजिक परिवर्तन के बिना किसी भी प्रकार का सामाजिक विघटन सम्भव नहीं। वस्तुतः सामाजिक असन्तुलन अथवा सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है और यह सामाजिक विघटन तथा सामाजिक संतुलन उसी समय होता है जब सामाजिक शक्तियों से असंतुलन और उनके सम्बन्ध में कोई परिवर्तन होता है।
समाजशास्त्र / Sociology – महत्वपूर्ण लिंक
- नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा | समाजशास्त्र का महत्त्व | नगरीय समाजशास्त्र का महत्व
- नगर की अवधारणा | नगरों के प्रकार | नगरों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन
- ग्रामीण नगरीय सातत्य | ग्रामीण नगरीय सातत्य प्रक्रिया
- नगरीय जीवन में मनोरंजन के महत्त्व | नगरीय मनोरंजन के प्रकार
- नगरीय धर्म का अर्थ | नगरीय धर्म की परिभाषा | नगरीय धर्म की विशेषताएँ
- नगरीय प्रशासन | नगरीय सरकारों की आय के साधन | भारत में नगरीय प्रशासन
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]