वाक्यों के प्रकार | वाक्यों के भेद
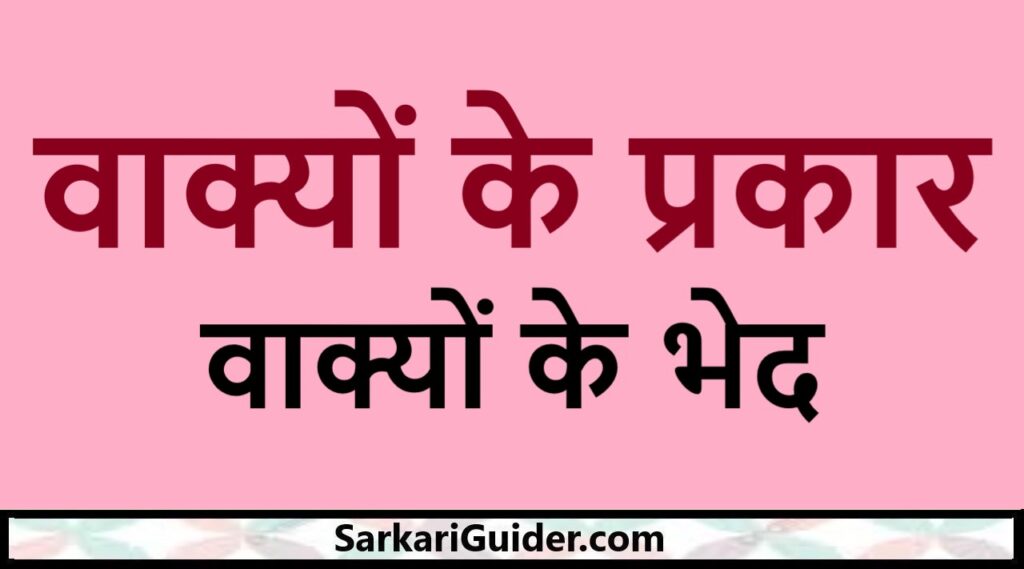
वाक्यों के प्रकार | वाक्यों के भेद
वाक्यों के प्रकार
वाक्यों के भेद के कई आधार स्वीकार किये गये हैं और वाक्यों के कई प्रकारों का उल्लेख किया गया है। डा0 कपिलदेव द्विवेदी ने प्रमुख रूप में वाक्यों के निम्न पाँच भेदों का उल्लेख किया है-
(1) आकृतिमूलक भेद। (2) रचनामूलक भेद। (3) अर्थमूलक भेद। (4) क्रियामूलक भेद। (5) शैलीमूलक भेद।
(1) आकृतिमूलक भेद-
डॉ0 द्विवेदी के अनुसार विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक भेद (Morphological Classification) किया जाता है। प्रकृति (Root) और प्रत्यय (Affix) या अर्थ-तत्त्व और सम्बंन्ध-तत्त्व किस प्रकार मिलते हैं, इसके आधार पर वाक्य भी चार प्रकार के होते हैं-
(1) अयोगात्मक (Isolating), (2) श्लिष्ट योगात्मक (Inflectional), (3) अश्लिष्ट योगात्मक (Agglutinative), (4) प्रश्लिष्ट योगात्मक (Incorporation)।
(1) अयोगात्मक वाक्य- इस प्रकार के वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय का अथवा सम्बन्ध तत्त्व और अर्थ-तत्त्व का संयोग नहीं होता। सम्बन्ध का ज्ञान वाक्य में शब्द के स्थान से होता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की भाषाओं में पदक्रम निश्चितता लिए रहता है। अंग्रेजी आज इसी प्रकार की भाषा बन गई है, जिसका पदक्रम लगभग निश्चित-सा हो गया है, जैसे-
Mohan taught Sohan.
Sohan taught Mohan.
यहाँ मोहन और सोहन पदों के स्थान परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन आ गया है। प्रथम वाक्य में मोहन कर्ता और सोहन कर्म है, परन्तु द्वितीय वाक्य में सोहन कर्ता और मोहन कर्म है। हिन्दी भी लगभग इसी प्रकार की भाषा है। यहाँ भी स्थान परिवर्तन से अर्थ-परिवर्तन हो जाता है, परन्तु उल्लेखनीय है कि कारक-चिन्हों के प्रयोग से स्थान परिवर्तन प्रायः सम्भव नहीं होता। जैसे-
राम मोहन को मारता है।
मोहन राम को मारता है।
(2) श्लिष्ट योगात्मक- डॉ. द्विवेदी के अनुसार ऐसे वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय शिलष्ट (मिले हुए या जुड़े हुए) होते हैं। इनमें प्रकृति (शब्द, धातु) और प्रत्यय को अलग-अलग करना कठिन होता है। भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाएँ संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अनेस्ता आदि इसी प्रकार की हैं। यथा-
वृक्षात् पत्रम् अपतत् (पेड़ से पत्ता गिरा)
अहं गुरुं दुष्टुम् अगच्छम् (मैं गुरु को देखने गया)
यहाँ वृक्ष + पंचमी विभक्ति एकवचन पत्र + द्वितीया विभक्ति एकवचन तथा पत् + ङ् प्रथम पुरुष एकवचन हैं। इस प्रकार के वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है।
(3) अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य- इस प्रकार के वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय अथवा अर्थ- तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व अश्लिष्ट (घनिष्ठता से मिलना) ढंग से मिले हुए होते हैं। प्रकृति और प्रत्यय जुड़े होने पर भी अलग-अलग देखे जा सकते हैं। तुर्की भाषा में इसके सुन्दर उदाहरण मिलते हैं-
एल्- इम् – डे- कि (El-um-de-ki) = मेरे हाथ में है।
(एल् = हाथ, इमू = मेरा डे = में, कि = होना)
सेव सर इब = मैं प्यार करने वाला हूँ।
(4) प्रश्लिष्ट योगात्मक- इस प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त सभी पद अपना कुछ-न-कुछ अंश छोड़कर और आपस में जुड़कर एक बड़ा शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार के उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं-
(i) भोजपुरी सुनलहतीहं (मैंने सुन लिया है)
(ii) खड़ीबोली (मेरठ) -उन्नेका (उसने कहा)
(2) रचना-मूलक भेद-
वाक्य की रचना (गठन) के आधार पर वाक्य के निम्न भेद हैं-
(क) सामान्य (सरल या साधारण) वाक्य (Simple Sentence), (ख) उपवाक्य (Clause), (ग) मिश्र-वाक्य (Complex-Sentence), (घ) संयुक्त वाक्य (Compound Sentence), (ङ) पूर्ण धाक्य (Complete Sentence), (च) अपूर्ण वाक्य (Incomplete Sentence)।
(क) सरल या सामान्य वाक्य- एक उददेश्य और एक विधेय, अथवा एक संज्ञा और एक क्रिया का वाक्य सरल वाक्य होता है। यथा-मोहन सोता है। सीता जागती है। आदि।
(ख) उपवाक्य- दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से बनने वाले वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और एक गौण होता है। यह गौण वाक्य ही उपवाक्य कहलाता है। जैसे- “वह नेता लोकप्रिय होगा जो जनता के हित की चिन्ता करेगा।” इस वाक्य में- ‘वह नेता लोकप्रिय होगा- प्रधान वाक्य है तथा ‘जो जनता के हित की चिन्ता करेगा’- गौण वाक्य है। गौण वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। यह गौण वाक्य संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया-विशेषण सम्बन्धी कुछ भी हो सकता है।
(ग) मिश्र वाक्य- जब वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हों तो वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। यथा-” वह नेता लोकप्रिय होगा जो जनता की सेवा करेगा।” इस वाक्य में- ‘जो जनता की सेवा करेगा’- उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है।
(घ) संयुक्त वाक्य- जिन वाक्यों में गौण वाक्य विद्यमान तो हों, परन्तु वे प्रधान वाक्य पर आश्रित न हों। यथा- कल रात वह आया, खाया पिया और चलता बना।
(ङ) पूर्ण वाक्य- इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के लिए आवश्यक सारे उपकरण विद्यमान रहते हैं। यथा-मोहन खाना खाएगा।
(च) अपूर्ण वाक्य- इस प्रकार के वाक्यों में कुछ उपकरणों का लोप रहता है। यथा- क्या तुम उधर जाओगे? नहीं । इसमें (मैं उधर नहीं जाऊँगा) का लोप है।
(3) अर्थमूलक अथवा भाव की दृष्टि से भेद-
अर्थ या भाव (Mood) की दृष्टि से वाक्य के निम्न भेद किये गये हैं-
(क) सकारात्मक या विधि वाक्य – वह पढ़ता है, खाता हूँ, राम काम करता है।
(ख) नकारात्मक या निषेध वाक्य- वह नहीं जाता हैं, मैं नहीं खेलता हूँ।
(ग) आदेशात्मक वाक्य या अनुज्ञा- सत्य बोलो, प्रातः काल उठो, तुम करो।
(घ) प्रश्नवाचक वाक्य- क्या तुम मेरा कहना मानोगे? क्या वह दिल्ली जाएगा ?
(ङ) संदेहात्मक- वह आ सकता है। तुम चुनाव जीत सकते हो।
(च) निश्चयात्मक- उसे तो प्रथम आया ही समझो।
(छ) अनिश्चयात्मक- तेल देखो तेल की धार देखो देखो ऊंट किस करवट बैठता है।
(ज) जिज्ञासात्मक- उसकी दशा कैसी है? इस संसार के परे क्या है?
(झ) कामनात्मक या इच्छार्थक- भगवान् तुम्हें सफलता दे। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे
(ञ) निर्णयात्मक- स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ले के रहेंगे आजादी।
(ट) संकेतार्थक वाक्य- यह उसे मिला होता तो वह अवश्य जीत जाता।
(ठ) विस्मयात्मक वाक्य- अरे तुम कैसे! अरे तुम फेल हो गए!
(4) क्रियामूलक या क्रिया के आधार पर भेद-
इस आधार पर निम्न भेद किये गये हैं-
(क) क्रिया-युक्त वाक्य- इन वाक्यों में क्रिया का स्पष्ट निर्देश रहता है, जैसे- राम जाता है, मोहन गया आदि। अधिकांश भाषाओं के अधिक वाक्य प्रायः क्रियायुक्त ही होते हैं। वाच्य के आधार पर इनके भी भेद हैं-
(1) कर्तृवाच्य- इन वाक्यों में कर्ता मुख्य होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे- रामः पुस्तकं पठति = राम पुस्तक पढ़ाता है।
(ii) कर्मवाच्य- इन वाक्यों में कर्म मुख्य होता है, अतः कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति। यथा- मया पुस्तकं पठ्यते मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है।
(iii) भाव-वाच्य – इसमें क्रिया मुख्य होती है। कर्म नहीं होता। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया में सदा प्रथम पुरुष एकवचन होता है। यथा- मया हस्यते (मेरे द्वारा हँसा जाता है), मया हसितम् (मैं हँसा) ।
(ख) क्रियाहीन वाक्य- प्रचलन के आधार पर कई भाषाओं में क्रियाहीन वाक्यों का भी प्रयोग होता है। वहाँ क्रियापद गुप्त रहता है। डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ने इसके भी उपभेदों की चर्चा की हैं –
(1) प्रचलन मूलक- प्रचलन के आधार पर संस्कृत, रूसी, बंगला आदि में सहायक क्रिया के बिना भी वाक्यों का प्रयोग होता है। क्रिया अन्तर्निहित (Understood) मानी जाती है। हिन्दी, अंग्रेजी में सामान्यतया क्रिया का होना अनिवार्य है। जैसे-
संस्कृत- इयं मम् गृहम् = यह मेरा घर है।
रूसी- एता भोय दोम = यह मेरा घर है।
बंगला- एइ आमार बाडी = यह मेरा घर है।
(ii) प्रश्न- वाक्य- इन वाक्यों में प्रश्न और उत्तर दोनों स्थलों पर या केवल उत्तर वाक्य में क्रिया नहीं होती, यथा-
प्रश्न- कस्मात त्वम् = कहाँ से?
उत्तर- प्रयागात् = प्रयाग से।
यहाँ पर पूरा प्रश्न-वाक्य होगा- तुम कहाँ से आ रहे हो ? उत्तर- मैं प्रयाग से आ रहा हूँ। प्रयत्नलाघव के कारण क्रियाहीन वाक्य का प्रयोग होता है।
भाषा विज्ञान – महत्वपूर्ण लिंक
- ‘विभाषा’ का तात्पर्य | भाषा विज्ञान की परिभाषाएँ | वर्णनात्मक भाषा विज्ञान | बोली किसे कहते हैं? | भाषा संरचना के स्तर | भाषा व्यवस्था तथा भाषा व्यवहार | भाषा और बोली में अन्तर
- भाषा की प्रकृति | भाषा के अर्थ का महत्व | भाषा विज्ञान के अध्ययन में ध्वनि विज्ञान का महत्व| ऐतिहासिक भाषा विज्ञान | भाषा के प्रकार्य | प्रयत्न लाघव
- स्वन विज्ञान | ध्वनि विज्ञान | ध्वनि विज्ञान की शाखाएँ | स्वन विज्ञान की उपयोगिता
- स्वन गुण | स्वन की सामान्य विशेषतायें
- ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारण
- ध्वनि परिवर्तन का स्वरूप और दिशा
- स्वरों का वर्गीकरण | उच्चारण प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण | घोषत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण | प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण | अनुनासिकता के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]







