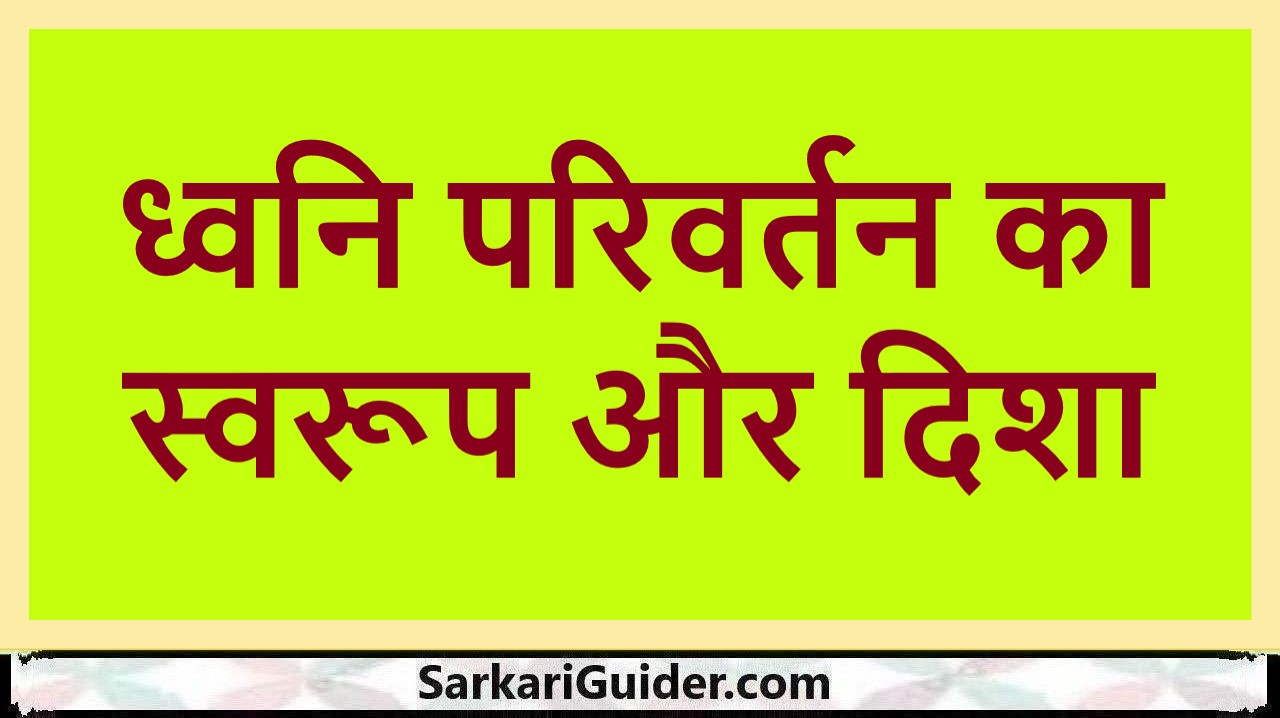ध्वनि परिवर्तन का स्वरूप और दिशा
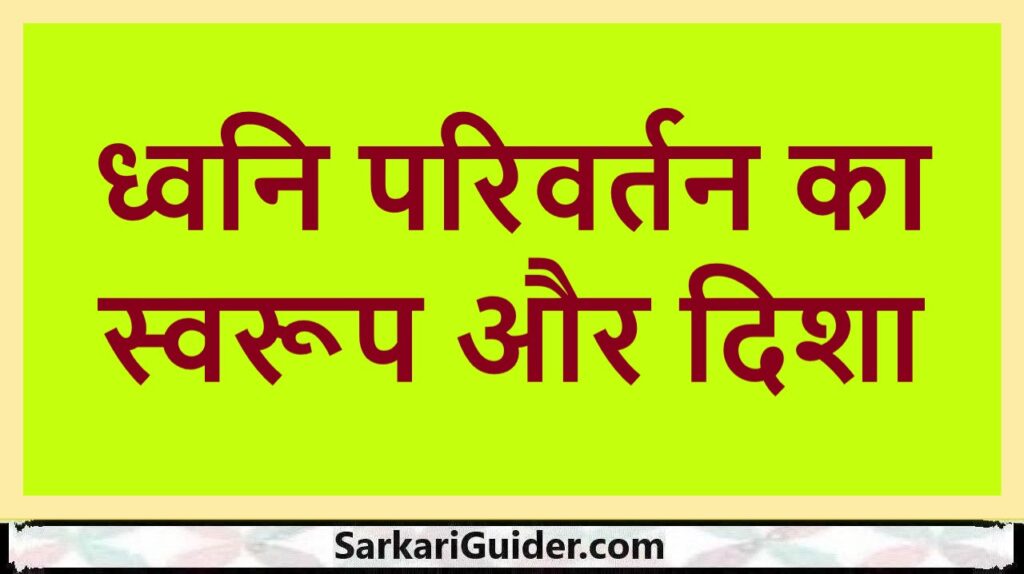
ध्वनि परिवर्तन का स्वरूप और दिशा
ध्वनि परिवर्तन का स्वरूप और दिशा
(1) समीकरण और सदृश्य, (2) विषमीकरण, (3) लोप, (4) आगमको
समीकरण और सादृश्य- कोई एक ध्वनि किसी दूसरी ध्वनि के प्रभाव से कोई तीसरा रूप ग्रहण कर ले, तो इस प्रक्रिया को समीकरण कहा जाता है। बातचीत करते समय समीपवर्ती ध्वनियाँ एक-दूसरे पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि जिनमें से एक किसी दूसरे रूप में परिणित हो जाती है। उदाहरणस्वरूप यदि ध्वनि ‘ख’ के प्रभाव से ‘ग’ ध्वनि में परिणित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को समीकरण माना जाता है। इस प्रकार से परिवर्तन संसार की सभी भाषाओं में प्रायः सभी कालों में मिलते हैं। इसके दो रूप हैं-
(1) स्थान का समीकरण, (2) प्रयत्न का समीकरण
स्थान के समीकरण में दोनों ध्वनियों के उच्चारण-स्थान समान हो जाते हैं। उदाहरणतः- संस्कृत, ‘चक्र’ प्राकृत चक्र में तथा संस्कृत ‘धर्म’, पालि धम्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार स्थान का समीकरण होता है उसी प्रकार प्रयत्न का भी होता है, अर्थात् सघोष और अघोष ध्वनियों के सान्निध्य के कारण पार्श्ववर्ती ध्वनि क्रमशः संघोष या अघोष बन जाती है।
उपर्युक्त विभिन्न विधियों से जो समीकरण होता है, उसे मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है- (1) ऐतिहासिक समीकरण, (2) सानिध्य समीकरण ।
(1) ऐतिहासिक समीकरण- युगों का परिणाम होता है। एक दो, भाषाओं में इसका उदाहरण देना संगत होगा। संस्कृत युग में व्यवहृत ‘सप्त’ तथा ‘धर्म’ शब्द पालि युग में ‘सत्त’ और ‘धम्म’ रूपों में प्राप्त होते हैं। संस्कृत ‘शर्करा’ और ‘वर्तिका’ शब्द हिन्दी में ‘शक्कर’ और ‘बत्ती’ में परिवर्तित हो गये है।
(2) सान्निध्य समीकरण- के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। हिन्दी भाषाओं में व्यवहृत ‘डाक घर’ एवं हिन्दी में व्यवहृत ‘आघ सेर’ शब्दों को, उच्चारण करते समय वक्ता ‘डाग्घर’ और ‘आस्सेर’ की भाँति बोलता है। एक ध्वनि किसी अन्य ध्वनि की समीपवर्ती न होकर भी प्रभावित कर सकती है। संस्कृत शब्द ‘आरध्यमाण’ में ‘र’ के प्रभाव से अन्तिम ‘न’ मूर्धन्य ‘ण’ में परिणित हो गया है।
एक और दृष्टि से समीकरण को दो और विभागों में बाँटा जा सकता है। पुरोगामी समीकरण और पश्चगामी समीकरण। पुरोगामी समीकरण में पूर्ववर्ती ध्वनि अपनी परवर्ती ध्वनि में स्वजातीय परिवर्तन पैदा कर देती है। पूर्ववर्ती ध्वनि के प्रभाव के प्राधान्य से इसे पुरागामी समीकरण कहते हैं।
उदाहरणार्थ- संस्कृत में
|
आस्तीर्नम् |
आस्तीर्नम |
|
मुष्नाति |
मुष्णाति |
संस्कृत में ‘रषाभ्याम् नो णः समानपदे’ जो सूत्र है। इसके अनुसार ‘आस्तीर्णम’ और ‘मुष्णाति’ शब्दों में पुरोगामा समीकरण हो गया है।
पश्चगामी समीकरण में परवर्ती ध्वनि के प्रभाव से पूर्ववर्ती ध्वनि में परवर्तित हो जाता है। परवर्ती ध्वनि के प्रभाव में प्राधान्य के कारण इसको पञ्चगामी समीकरण कहते हैं।
उदाहरणत-
|
संस्कृत |
प्राकृत |
|
सप्त |
सत्त |
|
युक्त |
जुक्त |
कुछ ध्वनिविद् इस प्रकार के समीकरण को एक मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं। जिस प्रकार
टाइप करते समय आगे वाले अक्षर को समय से पहले छाप दिया जाता है, उसी प्रकार बोलते समय अग्रिम ध्वनि को पहले से ही बोल दिया जाता है। यह प्रवृत्ति अंग्रेजी की अपेक्षा कुछ अन्य यूरोपीय भाषाओं, विशेषतः इटली में अधिकता से प्राप्त होती है।
सादृश्य एक प्रकार का समीकरण है, परन्तु उससे कुछ भित्र है। जब दो स्वनग्राम परस्पर निकट होते हैं तथा उनमें से एक अपने से पास वाले से प्रभावित होकर उसके सदृश अथवा उसके समधर्मी किसी अपने संस्वन में बदल जाता है, तब सादृश्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि ‘क’ और ‘ख’ दो स्वनग्राम परस्पर समीपवर्ती हों और ‘क’ के प्रभाव को ‘ख’ ‘क’ समगुणी किसी संस्वन में परवर्तित हो जाये, तो उसे सादृश्य या सारूप्य कहा जाता है।
विषमीकरण- यह प्रक्रिया समीकरण के विपरीत है। जिस प्रकार समीकरण में ध्वनियां परस्पर सदृश तथा सहधर्मी होने की चेष्टा करती हैं, उसी प्रकार विषमीकरण में असदृश। इसका कारण यह है कि सदृश्य ध्वनियों का बार बार उच्चारण करने से असदृश्य ध्वनियों का उच्चारण करना सहज है। एक ध्वनि के उत्पादन के लिए जो जो प्रयत्न अपेक्षित होता है, उसे एकदम वैसे ही करना कठिन होता है। एक ध्वनि के पुनः पुनः सहयोग से निर्मित वाक्य का उच्चारण करने में बच्चे जिस प्रकार जिह्वा की प्रवीणता की परीक्षा करते हैं, उसका उदाहरण सर्वज्ञात है। हिन्दी से एक रोचक उदाहरण लीजिए-
हिन्दी-सासनी की सड़क पै एक साँप, सांई सुरं निकरि गयौ।
चाँदनी चौक के चौराहे पर चाचा ने चाची को चम्मच से चाट चटाई।
जहाँ कहीं भी उक्त प्रकार की कठिनाइयाँ भाषा में मिलती है। वहां उन्हें दूर करने की चेष्टा विषमीकरण में परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त आलस्य में भी हम कुछ शब्दों का उच्चारण कुछ न कुछ कर बैठते हैं।
इस विषमीकरण की प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण बहुत सी भाषाओं में पाये जाते हैं। आसमान का नियम इस प्रक्रिया एक प्रकृष्ट उदाहरण है। विभिन्न भाषाओं में मिलने वाले कुछ उदाहरण नीचे दर्शनीय हैं-
|
संस्कृत |
प्राकृत |
|
लागंल |
नांगल (दो ल के स्थान पर एक ल, है) |
|
मध्यकालीन अंग्रेजी |
आधुनिक अंग्रेजी |
|
Marbre |
Marble (दो की जगह एक है) |
कुछ भाषाओं में समवर्ग में अन्तर्भुक्त कुछ ध्वनियों के परस्पर सत्रिकट होने के कारण उच्चारण में जो असुविधा उत्पन्न होती है, उसे दूर करने के लिए उस वर्ग में न आनेवाली किसी अन्य ध्वनि से काम लिया जाता है।
कथित भाषा में कम से कम ध्वनियों से अधिक से अधिक काम लिया जाय। अधिक ध्वनियों के स्थान पर कम ध्वनियों का प्रयोग करना लोप कहलाता है। स्वर और व्यंजन उभय ध्वनियों इस लोप प्रक्रिया के वशीभूत हैं। शब्दों के परिवर्तित रूपों को देखकर हमें इतना आश्चर्य लगता है कि समय को क्षयकारी शक्ति ने शब्दों पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है। वैदिक संस्कृत के ‘शेववृध’ तथा ‘शष्पपिंजर’ शब्द क्रमशः (प्रिय), अमूल्य तथा ‘शपिंजर’, (एक प्रकार की पीले रंग की छोटी घास) में परिणित हो गये हैं। संस्कृत के सम्बन्ध से रखने वाली प्रादेशिक भाषाओं में इस प्रकार के लोप प्रचुरता से पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, से अन्धकार उ. अन्धार, सं. बलीबद उ, बलद।
भाषा जीवित और प्रगतिशील है, इसलिए जो भाषा जितने ही बड़े क्षेत्र में और समय पर विस्तृत होती है, उसमें उतने ही अधिक परिवर्तन की प्रवृत्ति मिलती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषाओं में लोप का परिणाम कुछ मासों या वर्षों का फल नहीं अपितु शताब्दियों का फल होता है।
बलाघात प्रधान भाषाओं में जिन अक्षरों पर बलाघात का प्रयोग होता है वे तो सबल रूप में बोले जाते हैं, परन्तु समीपवर्ती जिन अक्षरों पर बलाघात नहीं होता है, उनमें पाये जाने वाले स्वर निर्बल रूप में बोले जाने के कारण कभी-कभी इतने बलहीन हो जाते हैं कि वे उदासीन स्वर में परिणित हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के उक्त सत्य सर्वाधिक स्पष्ट हैं, इसलिए किसी भी अंग्रेजी फोनेटिक रीडर में इस ध्वनि के संकेत प्रचुरता से पाये जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन तथा लोप को देखते हुए अंग्रेजी शब्दों में से कुछ को सबल और कुछ को निर्बल इन दो विभागों में विभक्त किया जाता है। प्रायः सभी भाषाओं में इस प्रकार के सबल और निर्बल रूप पाये जाते हैं।
साधारणतया सर्वनाम, क्रियाविशेषण अव्यय तथा सहायक क्रियाओं में परिवर्तन अधिक देखे जाते हैं। विशेष्य विशेषण तथा प्रधान क्रियाओं में इतना लोप नहीं होता।
आगम- भाषा में बिना स्थान रिक्त हुए भी कुछ अन्य कारणों से कई ध्वनियों का आगम हो जाता है। संस्कृत भाषा के बहुत से शब्दों के आरम्भ से संयुक्त व्यंजन स्क, स्ख, स्न, स्व आदि ध्वनियाँ पाई जाती हैं। इन शब्दों के उच्चारण में संस्कृत से सम्बन्ध रखने वाली भारतीय भाषाओं में विशेषकर अशिक्षित लोगों के उच्चारण सौकर्य के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। हिन्दी में इस प्रकार स्नान को इस्नान, स्त्री को इस्त्री तथा उड़िया में प्रताप को परताप ब्रज को बरज, रूपों में उच्चरित किया जाता है। यहाँ राम को इरामन कहते हैं।
बहुत-सी भाषाओं में स्वरागम् एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई है। परन्तु व्यंजनों का आगम अधिकांश भाषाओं में नहीं मिलता। भारतीय भाषाओं में तमिल और तेलुगु में व्यंजनागम बड़ी मात्राओं में प्राप्त होता है। इसका प्रभाव अंग्रेजी में आजकल इतना बढ़ गया है कि लोग इसे बिना स्थान के भी प्रयुक्त कर लेते हैं।
विशेष प्रकार के ध्वनि परिवर्तन- कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन भी भाषाओं में मिलते हैं। इन परिवर्तनों का अब ऐतिहासिक महत्व मात्र ही है। कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन निम्नलिखित हैं-
अपश्रुति- कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द के व्यंजन ज्यों के त्यों रहते हैं किन्तु विशेषतः आन्तरिक स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार अर्थ बदल जाता है। यह प्रवृत्ति भारोपीय, हेमेटिक तथा सेमेटिक, परिवार की भाषाओं में मिलती है। अपश्रुति में कभी-कभी कुछ अंश भी पहले या बाद में जुड़ जाता है। अपश्रुति के मात्रिक अपश्रुति और गुणीय अपश्रुती दो भेद कर सकते हैं। स्वर के यथा रूप रहने पर केवल मात्रा में परिवर्तन हो जाने को मात्रिक अपश्रुति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, संस्कृति में ‘भारद्वाज’ और ‘भारद्वाज’ या ‘वसुदेव’ और ‘वासुदेव’ को लिया जा सकता है। संस्कृत व्याकरण में इसे गुण वृद्धि कहते हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने मात्रिक अपश्रुति को सामान्य, दीर्घीींभूत, प्राहासित, निर्बलीभूत और शून्य आदि श्रेणियों में विभाजित किया है। डॉ. चटर्जी ने इसे ह्रस्वतादीर्घातात्मक अपश्रुति कहा है।
गुणीय अपश्रुती- गुणीय अपश्रुती में स्वर, मात्रा, गुण की दृष्टि से परिवर्तन होता है। डॉ. चटर्जी इसे स्थान परिवर्तनात्मक अपश्रुति मानते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के (गाना) और (गाया) तथा अरबी के किताब (पुस्तक) कुतुब (पुस्तकें और कातिब लिखने वाला आदि को लिया जा सकता है। हिन्दी में मेल, मिला, मिली, या करना, करनी, कराना, आदि भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अपश्रुति के संस्कृत के कुछ उदाहरण लीजिए-
|
सामान्य श्रेणी |
दीर्घीभूत |
शून्य श्रेणी |
|
सद्दन (सीट) |
सादयति (बैठता है) |
सेदुः (वे बैठे) |
|
सचते (सम्बन्ध करता है) |
(शतिषाच: (बदान्ता से सम्बन्ध रखने वाला) |
सस्चति (वे बैठे) |
अपश्रुति के कारण- संगीतात्मक स्वराघात तथा बलात्मक स्वराघात अपश्रुति का मुख्य कारण है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में अत्यन्त प्राचीन काल में मानिक परिवर्तन का कारण बलात्मक स्वर भात ही मा, तथा गुणीय परिवर्तन संगीतात्मक बलाघात के कारण है। अंग्रेजी, रूसी, हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में प्राय: गुणीय अपभुती है।
भाषा विज्ञान – महत्वपूर्ण लिंक
- भाषा व्यवस्था तथा भाषा व्यवहार | भाषा व्यवस्था तथा भाषा व्यवहार में अन्तर
- भाषा विज्ञान | भाषा विज्ञान के प्रमुख रूप | भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धति | भाषा विज्ञान की वर्णात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति
- ‘विभाषा’ का तात्पर्य | भाषा विज्ञान की परिभाषाएँ | वर्णनात्मक भाषा विज्ञान | बोली किसे कहते हैं? | भाषा संरचना के स्तर | भाषा व्यवस्था तथा भाषा व्यवहार | भाषा और बोली में अन्तर
- भाषा की प्रकृति | भाषा के अर्थ का महत्व | भाषा विज्ञान के अध्ययन में ध्वनि विज्ञान का महत्व| ऐतिहासिक भाषा विज्ञान | भाषा के प्रकार्य | प्रयत्न लाघव
- स्वन विज्ञान | ध्वनि विज्ञान | ध्वनि विज्ञान की शाखाएँ | स्वन विज्ञान की उपयोगिता
- स्वन गुण | स्वन की सामान्य विशेषतायें
- ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारण
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]