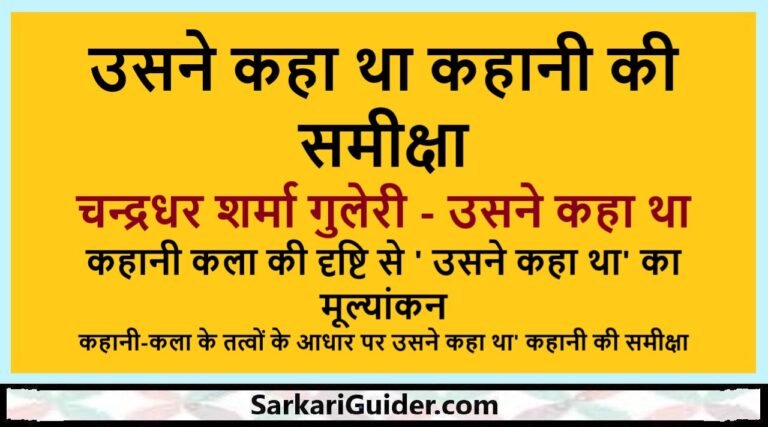भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएँ | स्वर्ण युग की विशेषताएँ

भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएँ | स्वर्ण युग की विशेषताएँ
भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएँ
हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस काल में भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता रही। इस काल की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करते हुए विद्वानों ने इसे ‘स्वर्णकाल’ की संज्ञा दी।
भक्तिकाल : स्वर्ण युग
भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएँ
भक्तिकाल की कतिपय प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है, जिनके आधार पर भक्तिकाल को हिंदी-साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है-
भक्तिकाल की विशेषताएँ-
- राज्याश्रय का त्याग
- स्वांत:सुखाय-परजन-हिताय रचना।
- भक्ति का प्राधान्य।
- समन्वय की भावना।
- भारतीय संस्कृति की रक्षा।
- श्रिंगार तथा शांत रस की प्रधानता।
- मुक्तक तथा प्रबंध काव्य।
- गुरु की महत्ता।
- सामाजिक विषमता का खंडन।
- भाषा।
- छंद।
- अलंकार।
- संगीतात्मकता।
- अमर साहित्य।
(i) राज्याश्रय का त्याग
वीरगाथा काल में सभी कवि राज्याश्रित थे, परंतु भक्तिकाल कवियों ने राज्याश्रय को स्वीकार नहीं किया। सभी कवियों ने स्वतंत्र रहकर काव्य का सृजन किया। इन कवियों ने किसी राजा की स्तुति या प्रशंसा तक नहीं की। केवल जायसी ने तत्कालीन बादशाह की स्तुति में कुछ पॉक्तियाँ लिखी हैं।
(ii) स्वान्तः सुखाय-परजनहिताय रचना
भक्तिकाल के कवियों ने जो भी रचनाएँ कीं, वे स्वांत:सुखाय (अपने अंत:करण के सुख के लिए) थीं। यद्यपि ये रचनाएँ उन्होंने अपने सुख के लिए लिखी थीं , परंतु ये दूसरों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध हुईं। उनके ग्रंथों में दिए गए धर्म उपदेश, नीति के सिद्धांत, भगवान के विविध क्रियाकलाप सभी को सदमार्ग की ओर प्रेरित करने वाले सिद्ध हुए। इसलिए ये रचनाएँ स्वांत:सुखाय होते हुए भी परजनहिताय थीं।
(iii) भक्ति का प्राधान्य
इस काल में भक्ति का प्राधान्य रहा। सभी कवियों ने परमात्मा का भक्ति संदेश दिया। इन कवियों ने भक्ति के विविध सोपानों और सिद्धांतों का अनेक प्रकार से वर्णन किया है । दास्य और सखा भाव की भक्ति के साथ-साथ नवधा भक्ति ( श्रवण, कीर्तन, नाम, जप आदि) का संकेत भी इसमें मिलता है। प्रेम, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय इस युग की देन है तुलसी कहते हैं-
ज्ञानहिं भगतहि नहिं कहु भेदा।
(iv) समन्वय की भावना
इस युग की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है। इस काल के कवियों ने सगुण-निर्गुण, कर्म-भक्ति, शैव-वैष्णव, राजा-प्रजा, निर्धन-धनी, विभिन्न संप्रदायों-मतों और विभिन्न काव्य शैलियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया है। तुलसी ने स्पष्ट कहा हैं।
अगुनहिं सगुनहिं नहिं कलु भेदा।
उभय हरहिँ भवसंभव खेंदा।।
(v) भारतीय संस्कृति की रक्षा
भक्तिकालीन कवियों ने भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की। मुसलमानों के अत्याचारों से जो भारतीय संस्कृति लुप्तप्राय हो गई थी, उसको इन कवियों ने जीवित रखा। भारतीय संस्कृति का उन्नत रूप उन्होंने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे बह श्रेष्ठ आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर सके।
(vi) शृंगार तथा शांत रस की प्रधानता
भक्तिकालीन साहित्य में मुख्यत: श्रृंगार व शांत रस का प्रयोग हुआ हैं। आत्मा-परमात्मा के विरह-मिलन, सौंदर्य-चित्रण में श्रृंगार रस हैं तो भक्ति के उपदेशों, संदेशों एवं सिद्धांतों में शांत रस। वैसे तुलसी ने अपने काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया है ।
(vii) मुक्तक तथा प्रबंधकाव्य
इस काल में प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। जायसी का ‘पद्मावत’ व तुलसी का ‘श्रीरामचरितमानस’ श्रेष्ठ प्रबंधकाव्य हैं। सूर और कबीर ने मुक्तक काव्य की रचना की। तुलसी ने भी अनेक मुक्तक काव्य लिखे।
(viii) गुरु की महत्ता
भक्तिकाल में गुरु की महत्ता सर्वोंपरि मानी गई है। गुरु को इन्होंने मार्गदर्शक मानते हुए परमात्मा से भी बढ़कर माना। यह सत्य है कि जीवन के विभिन्न संघर्षों से उद्धार पाने का मारगं गुरु ने ही बताया है और गुरु ही साधक को परमात्मा के द्वार तक पहुँचाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं-
सतगुरु की महिमा अनत अनंत किया उपगार।
लोचन अनँत उघाड़िया, अनँत दिखावणहार।
(ix) सामाजिक विषमता का खंडन
भक्तिकालीन कवियों ने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों और ऊँच-नीच के भेदभावों का खंडन किया। इन्होंने सबको एक ही परमात्मा का अंश माना और कहा कि जो भी परमात्मा का ध्यान-जप करता है। वही श्रेष्ठ है। इन कवियों ने मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा की और समाज के कुत्सित रूप को बदलने की पूर्णरूपेण चेष्टा की।
(x) भाषा
भक्तिकाल में ब्रज व अवधी भाषा का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ। संतों ने मिश्रित सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया तो जायसी ने अवधी का। तुलसी ने अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य का सृजन किया। सूर आदि ने ब्रजभाषा को स्वीकारा। इस प्रकार ब्रज और अवधी ही मुख्य भाषाएँ रहीं।
(xi) छंद
इस काल में दोहा, चौपाई, कवित्त, सबैवा, पद, सोरठा, बरवै आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया।
(xii) अलंकार
भक्तिकाल के कवियों ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया हैं। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, अर्थातरन्यास आदि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है।
(xiii) संगीतात्मकता
भक्तिकाल का संपूर्ण साहित्य संगीतात्मकता से परिपूर्ण है। दोहा चौपाई आदि तो गेय हैं ही, पदों में सबसे अधिक यही गुण विद्यमान है। अर्थात सभी पद किसी-न-किसी राग-रागिनी पर आधारित हैं।
(xiv) अमर साहित्य
भक्तिकाल का साहित्य अमर साहित्य है। अमर से अभिप्राय यह है कि इस साहित्य का महत्त्व आज भी है। इस समय की परिस्थितियों के लिए जो यह उपयोगी और कल्याणकारी था ही, आज भी यह हमें प्रभुभक्ति की पावन गंगा में अवगाहन कराता रहता है। तुलसी का ‘श्रीरामचरितमानस’ आज भी प्रातः स्मरणीय ग्रंथ है। कबीर के उपदेश आज भी हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। जावसी और सूर का काव्य आज भी पाठकों के हृदय में मधुरता का समावेश कर देता है। निश्चय ही यह अमर साहित्य है।
निष्कर्ष
इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिकालीन काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य है। भाव और शिल्प की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठतम है। परमात्मा की भक्ति का पावन संदेश देने वाला यह काव्य हिंदी-साहित्य की अमूल्य निधि है। इस काल के कवियों ने जिस साहित्य का सुजन किया बह अपनी विशेषताओं के कारण आज भी अमर है। इस काल की विभिन्न विशेषताएँ ही इसे स्वर्णयुग की संज्ञा प्रदान कराती है। डॉ श्यामसुंदर दास का कथन अक्षरश: सत्य है “जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंत:करणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सामान्वत: भक्तियुग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी-साहित्य का स्वर्णयुग था।”
- आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ- राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
- प्रमुख हिन्दी गद्य-विधाओं की परिभाषाएँ
- नाटक- परिभाषा, प्रथम नाटक, नाटक के तत्त्व, प्रमुख नाटककारों के नाम, प्रसिद्ध नाटकों के नाम
- आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ- प्रवृत्तियों की विशेषताएँ, आदिकालीन साहित्य का महत्त्व
- हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन
- कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि (Krishnbhakti Kavay Dhara Ke Pramukh Kavi)
- कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ /कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषतायें (Krishan Kavay Ki Pravritiitiyan / Krishan Kavay Ki Visheshatayen)
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]