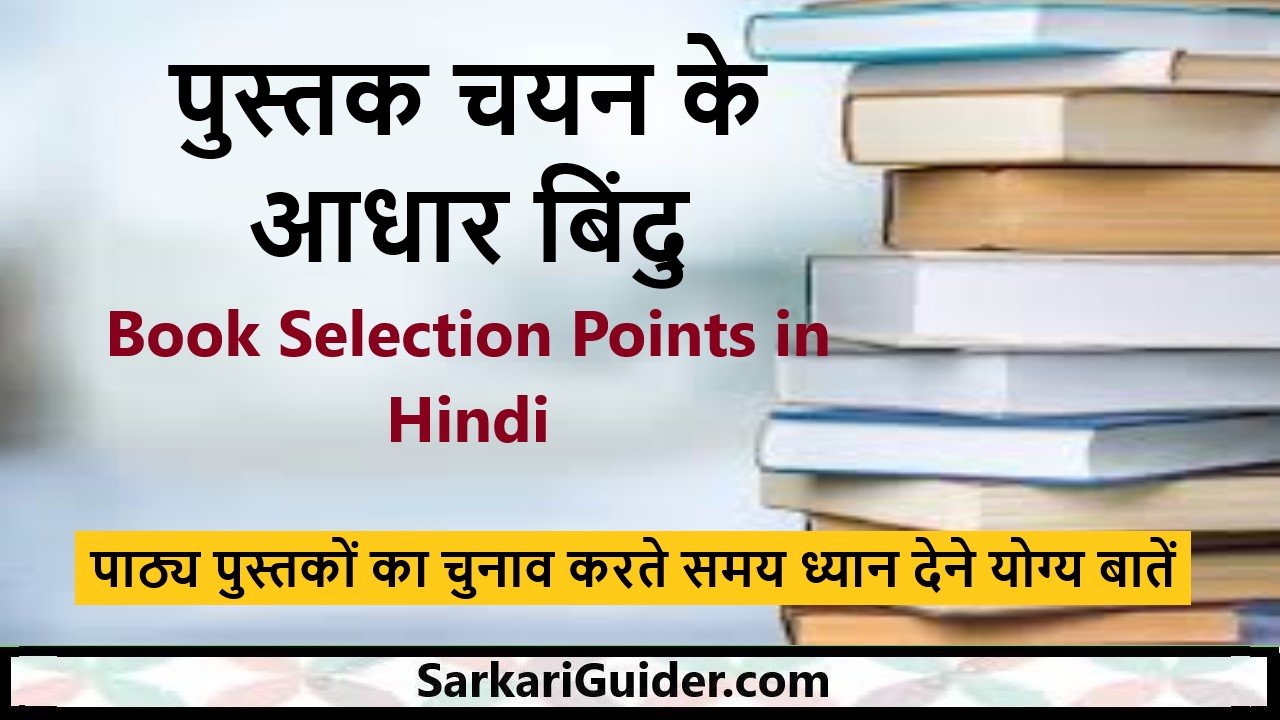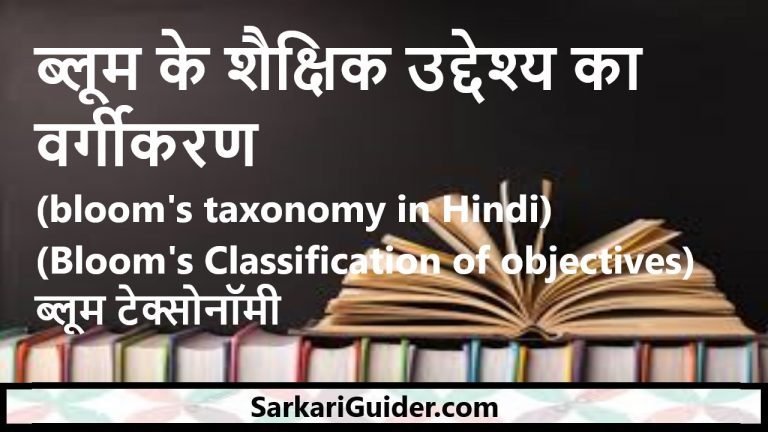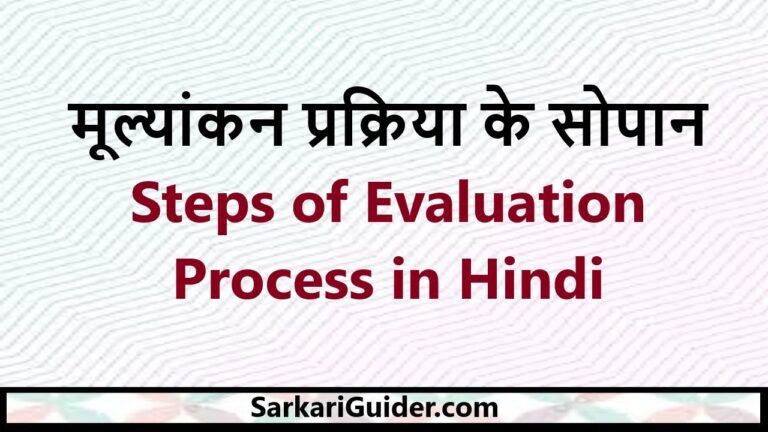पुस्तक चयन के आधार बिंदु | Book Selection Points in Hindi

पुस्तक चयन के आधार बिंदु | Book Selection Points in Hindi
पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें (पुस्तक चयन के आधार बिंदु)
- पाठ्य-पुस्तक का नाम – इसकी उपयुक्तता एवं ग्राह्यता।
- लेखक – उसकी योग्यता, अनुभव एवं प्रसिद्धि। उसके विचारों में स्पष्टवादिता, निष्पक्षता एवं मौलिकता। उसकी विषय विशेषज्ञता, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान एवं प्रगतिशील विचारधारा आदि।
- विषय-सूची – पाठ्यक्रम के अनुसार उसका महत्व एवं क्षेत्र, उसकी ग्राह्यता।
- अन्तर्वस्तु का चयन एवं संगठन
- पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप अन्तर्वस्तु का चयन।
- छात्रों की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, संवेगात्मक स्तर एवं प्रवृत्तियों से मा अन्तर्वस्तु की अनुकूलता।
- अन्तर्वस्तु की सामाजिक उपयुक्तता–सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा नागरिकों में नव–जागरण कर सकने की क्षमता।
- अन्तर्वस्तु के संगठन की मनोवैज्ञानिकता–अध्यायों का क्रम बालकों के मानसिक विकास क्रम के अनुसार।
- अन्तर्वस्तु के संगठन की शिक्षण विधियों से अनुकूलता।
- अन्तर्वस्तु के चयन में प्रजातान्त्रिक आदर्शों एवं मूल्यों का ध्यान।
- प्रस्तुतीकरण – प्रस्तुतीकरण निम्नांकित गुणों से युक्त होना चाहिए
- छात्रों में स्वतः अध्ययन करने की आदत विकसित कर सकने की क्षमता।
- छात्रों विषय के प्रति रुचि विकसित कर सकने की क्षमता।
- अन्य विषयों से अच्छा सह–सम्बन्ध।
- शिक्षण–विधियों के अनुकूल।
- शिक्षण सूत्रों के अनुरूप।
- सीखने के नियमों एवं सिद्धान्तों का अनुसरण।
- निर्देशित अध्ययन के अवसर प्रदान करने की सम्भावना।
- छात्रों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्तर के अनुकूल।
- व्यक्तिगत–भिन्नता की आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावना।
- बालकों के मानसिक विकास में सहायक।
- उपयुक्त एवं सरल भाषा–शैली।
- उदाहरण एवं चित्र आदि- शाब्दिक एवं प्रदर्शनात्मक उदाहरण।
- तालिकाओं, ग्राफ, रेखाचित्र, मानचित्र आदि की स्पष्टता, आकर्षकता एवं शुद्धता।
- आँकड़ों, उद्धरणों एवं सन्दर्भो की पर्याप्त संख्या, उनकी विश्वसनीयता एवं वैधता।
- शैक्षिक सहायक साधन – अभ्यासार्थ प्रश्न, उपयुक्त निर्देश, प्रस्तावना, परिशिष्ट आदि की यथार्थता एवं उपयुक्तता , सहायक पुस्तकों की सूची आदि का समुचित समावेश।
- पाठ्य–पुस्तक की बाह्य आकृति – पाठ्य–पुस्तकों के चयन के समय पुस्तक के आकार, पृष्ठ संख्या, कागज, मुद्रण, जिल्दसाजी, आवरण पृष्ठ की आकर्षकता आदि तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए।
- प्रकाशन- पुस्तक के प्रकाशक की विश्वसनीयता एवं प्रसिद्धि।
- प्रकाशन की तिथि।
10.मूल्य – पुस्तक का मूल्य जन-सामान्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए तथा यथा सम्भव न्यूनतम होना चाहिए।
पाठ्य-पुस्तकों का महत्व और आवश्यकता
- पाठ्य-पुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों को विद्वानों के बहुमूल्य विचारों एवं उपयोगी अनुभवों को प्रदान करती है जिससे वे इन अनुभवों का लाभ उठाने में समर्थ हो सकते हैं।
- पाठ्य-पुस्तकों से अध्ययन अध्यापन में एकरूपता आती है।
- पाठ्य-पुस्तकों में विषय के पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण रूप में व्याख्या की जाती है जिससे शिक्षक उपयुक्त अधिगम-अनुभव प्रदान कर सकता है।
- विभिन्न शिक्षा-आयोगों द्वारा भी पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया है।
- पाठ्य-पुस्तक में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है।
- पाठ्य-पुस्तकें शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है।
- पाठ्य–पुस्तकों के के द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों को यह जानकारी मिलती है कि किसी कक्षा स्तर के लिए कितनी विषय वस्तु का अध्ययन-अध्यापन करना है।
- पाठ्य-पुस्तकें छात्रों को विषय-वस्तु को संकलित करने में सहायता प्रदान करती हैं।
- इनके माध्यम से छात्रों की स्मरण एवं तर्कशक्ति का विकास होता है।
- पाठ्य-पुस्तकें मन्द बुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती है।
- ये परीक्षा के समय छात्रों की सहायक होती हैं।
- पाठ्य-पुस्तकें शिक्षक को कक्षा-स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध कराती हैं।
- पाठ्य-पुस्तक में विषय-वस्तु को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्रों के लिए विषय-वस्तु सरल एवं सुगम हो जाती है।
- पाठ्य-पुस्तक कक्षा-शिक्षण की अनेक कमियों को भी दूर करती हैं। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता है। अतः पाठ्य-पुस्तकें की सहायता से छात्र व्यक्तिगत रुचि एवं गति के साथ अध्ययन कर सकते है।
- इनके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है।
- छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊँचा नहीं होता है कि वे विद्यालय में पढ़ायी गई विषय-वस्तु को एक ही बार में आत्मसात् कर सकें। उन्हें विषय-वस्तु को होती है। कई बार पढ़ना एवं दुहराना पड़ता है। अतः पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता होती है।
- योग्य शिक्षकों का ज्ञान भी अव्यवस्थित होता है। अतः उसे व्यवस्थित करने में पाठ्य-पुस्तक सहायक होती है। इसी प्रकार छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को परिवर्धित एवं पूर्णता प्रदान करने के लिए यह सहायक होती है।
- पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को प्रेरणा प्राप्त होती है।
- पाठ्य-पुस्तक के आधार पर कक्षा-कार्य तथा मूल्यांकन सम्भव होता है।
- पाठ्य-पुस्तक के आधार पर प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक कक्षा में निश्चित पाठ्य-वस्तु का अध्यापन सम्भव होता है तथा इससे छात्रों का मूल्यांकन सामूहिक रूप से किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निष्कर्ष (स्वरूप) | National Curriculum Framework summery NCF, 2005
- शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा | शिक्षण की प्रकृति | Meaning and definition of teaching in Hindi | Nature of teaching in Hindi
- सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? | Factors affecting learning in Hindi
- बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है? | बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषतायें | What is the basic learning model in Hindi? | Characteristics of the basic learning model in hindi
- पाठ्यचर्या उपागम | Curriculum approach in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]