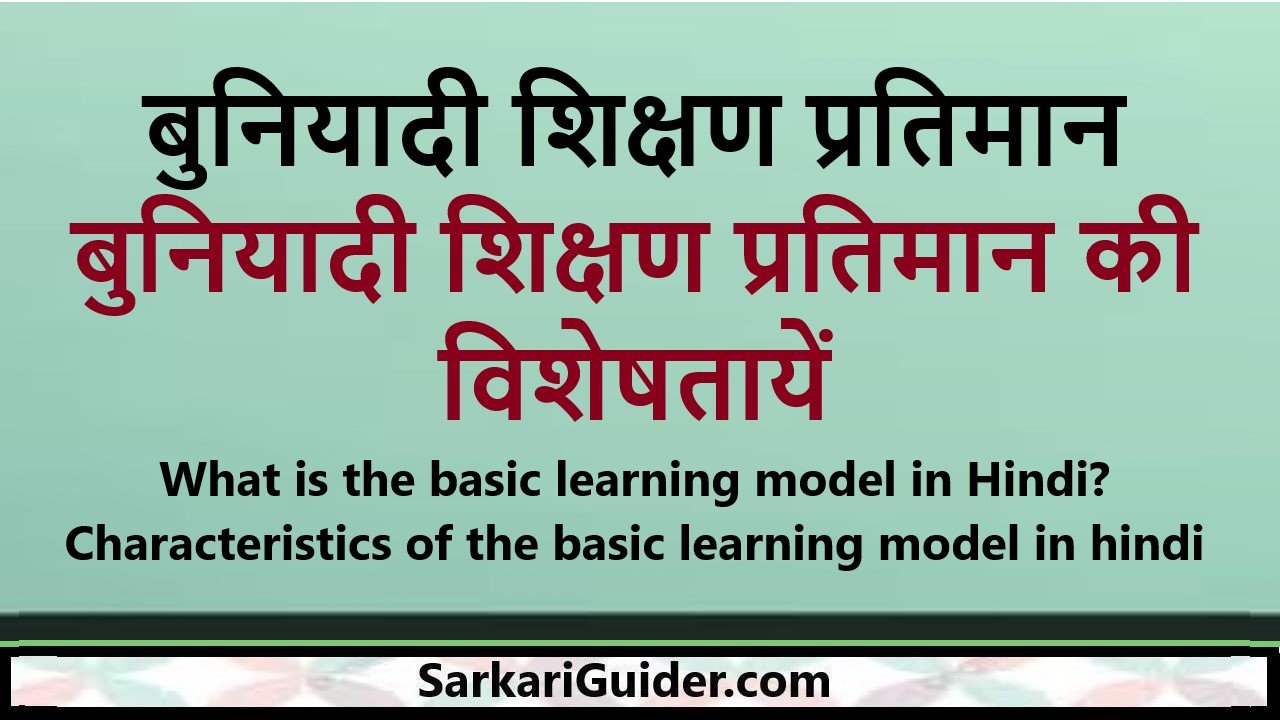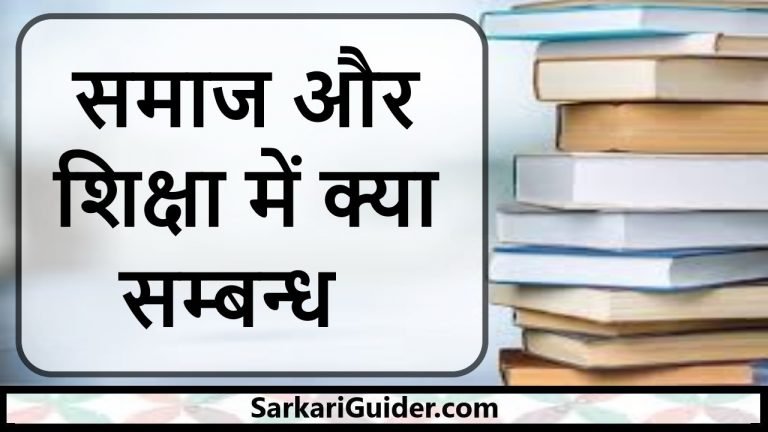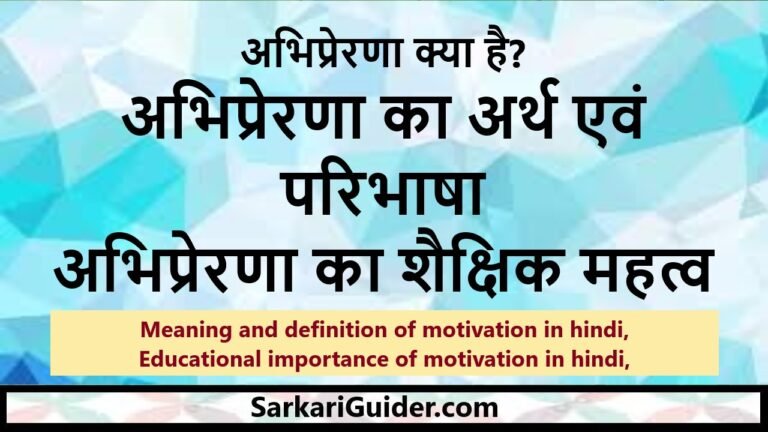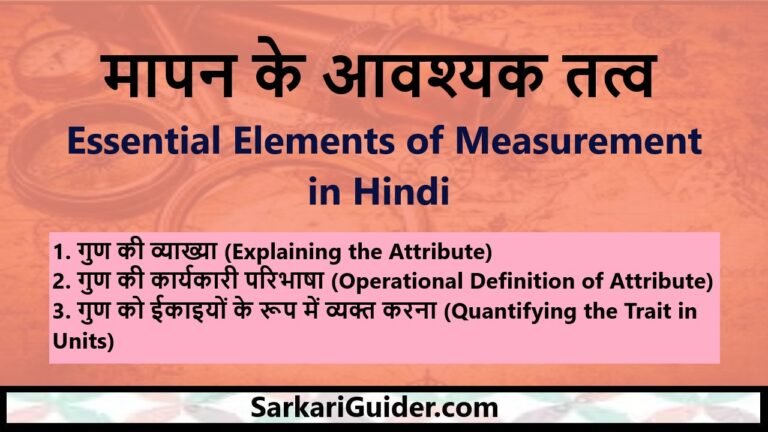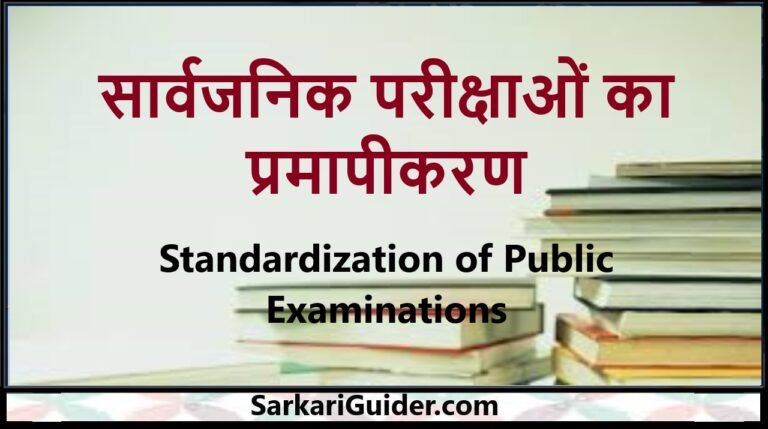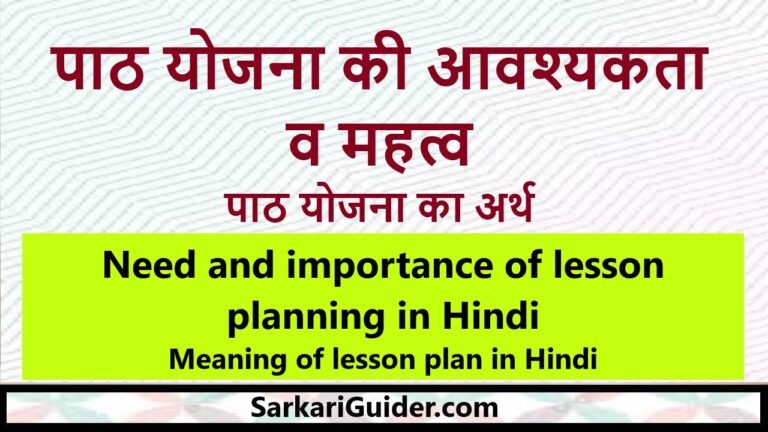बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है? | बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषतायें | What is the basic learning model in Hindi? | Characteristics of the basic learning model in hindi

बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है? | बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषतायें | What is the basic learning model in Hindi? | Characteristics of the basic learning model in hindi
राबर्ट ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान
शिक्षण के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन 1962 में राबर्ट ग्लेसर ने किया। इसी कारण इस प्रतिमान को ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। शिक्षण का यह प्रतिमान पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है। अतः इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया में अन्तर्निहित ज्ञानात्मक, तर्कसम्मत और विश्लेषणात्मक पक्षों को भली प्रकार समझने के बाद शिक्षण कार्य की व्याख्या की जाती है। जौयसी तथा वील ने इस प्रतिमान को कक्षा सभा प्रतिमान के नाम से पुकारा है। ग्लेसर महोदय ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की प्रक्रिया को 4 निम्न भागों में विभाजित किया है-
-
अनुदेशात्मक उद्देश्य (Instructional Objective)
अनुदेशात्मक उद्देश्यों का तात्पर्य उन व्यवहारों तथा क्रियाओं से है जिन्हें शिक्षण की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात अर्जित कर सकेगा। पाठ विषयवस्तु, छात्रों की योग्यता एवं परिपक्वता के आधार पर यह बदलता रहता है। जहां तक इस प्रतिमान के विस्तार का प्रश्न है इसका विस्तार बहुत विस्तृत है और विस्तार में शब्दों के याद करने से लेकर जीवन के सभी मूल्यों से सम्बन्धित शब्दों तक इसका विस्तार सम्भव है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रारम्भ करने से पूर्व अनुदेशात्मक उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है और इन्हें व्यवहारिक पदों में लिखा जाता है और इन्हीं व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण कार्य का सम्पादन किया जाता है।
-
प्रारम्भिक व्यवहार (Entering Behavior)
जॉन पी डिसिको के अनुसार, “प्रारम्भिक व्यवहार (शिक्षण) प्रारम्भ होने के पूर्व छात्र के स्तर का वर्णन करता है। यह इस बात ओर संकेत करता है कि छात्र अनुदेशन से पूर्व क्या सीख चुका है तथा छात्र की बौद्धिक योग्यता एवं विकास कितना हुआ है और छात्र में अनुदेशन से पूर्व कितनी तत्परता रुचि तथा अभिक्षमता विद्यमान है।”
स्पष्ट है यह छात्र का वह स्तर है जहां से नवीन ज्ञान या अधिगम को पुराने ज्ञान या अधिगम के साथ जोड़ा जाएगा। छात्रों का वर्तमान ज्ञान का स्तर, उसकी बौद्धिक योग्यता का विकास, उसकी अभिप्रेरणा की स्थिति और अधिगम को प्रभावित करने वाले सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्व इस प्रारम्भ स्तर के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं। शिक्षण की प्रभावकारिता पूर्व ज्ञान के साथ प्रारम्भिक व्यवहार को जोड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है।
-
अनुदेशात्मक प्रक्रिया (Instructional Procedure)
पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण के लिए की जाने वाली क्रियाओं को अनुदेशी प्रक्रिया के अन्तर्गत रखा जाता है। अनुदेशी प्रक्रिया शिक्षण व्यवस्था का वर्णन करती है। इसके अन्तर्गत अध्यापक को यह निश्चित करना होता है कि कौन-कौन सी शिक्षण विधियों को अपनाकर उसे किसी पाठ का शिक्षण प्रारम्भ करना है। शिक्षक छात्रों से किस प्रकार से प्रश्न करेगा और उसके द्वारा किन-किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा और छात्र कौन सी अनुक्रिया करेंगे। इन सभी को अनुदेशात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। संक्षेप में शिक्षक को जो कुछ भी पढ़ाना है उसका प्रस्तुतीकरण ही अनुदेशात्मक प्रक्रिया होगी।
-
निष्पादन मूल्यांकन (Evaluation)
शिक्षण प्रक्रिया यहीं पर ही सम्पन्न नहीं हो जाती। शिक्षक द्वारा विभिन्न परीक्षणों व निरीक्षणों के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप छात्रों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का मूल्यांकन भी किया जाता है। यदि मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात होता है कि छात्र शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाये हैं तो यह शिक्षण की असफलता मानी जाती है। इसके विपरीत यदि छात्रों में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं तो यह शिक्षण की सफलता है। शिक्षण की असफलता की स्थिति में उपरोक्त तीनों क्रियाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना होगा ताकि शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान का यह चौथा घटक अर्थात् निष्पादन मूल्यांकन तीनों घटकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है और उनकी प्रभाविकता को बढ़ाने में सहायक होता है।
बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विशेषतायें
बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में अनुदेशात्मक व्यवस्था के सभी अंग विद्यमान हैं। यह प्रतिमान शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में बहुत उपयोगी है। संक्षेप में इस प्रतिमान का प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार से गिनाया जा सकता है-
- यह प्रतिमान शिक्षण तथा अधिगम की लक्ष्य निर्धारित धारणा पर विशेष बल देता है जिसकी पुष्टि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रथम घटक अनुदेशात्मक उद्देश्य से हो जाती है।
- इस प्रतिमान की दूसरी विशेषता यह है कि इस प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप कुछ विशेष निर्णयों और उनके अनुकूल ही सम्पादित कार्यों और अभ्यासों के अनुसार घटित होता है न कि शिक्षक और छात्र के व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर। यही कारण है कि इस प्रतिमान में शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।
- इस प्रतिमान की सफलता के लिए शिक्षक की निपुणता बहुत महत्व रखती है। इसकी सफलता शिक्षक के व्यक्तिगत करिश्मे पर निर्भर न होकर उसकी निपुणता पर निर्भर करती है। किन्तु इस प्रतिमान में शिक्षक के व्यक्तिगत करिश्मे और निपुणता के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है।
- इस प्रतिमान में शिक्षण और पुनर्शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सीखने सम्बन्धी अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लिया जाता और इसीलिए निष्पादन मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है।
- इस प्रतिमान का मुख्य आकर्षण शैक्षिक नियोजन तथा पाठ्यों की व्यवस्था है । इसी कारण अनुदेशात्मक प्रणालियों में सुधार और उन्हें शिक्षण के साथ सम्बन्धित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।
महत्वपूर्ण लिंक
- संस्कृति और शिक्षा में सम्बन्ध(Relation Between Culture and Education in Hindi)
- शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता(Education and Social Mobility in hindi)
- शिक्षण की योजना विधि का वर्णन | शिक्षण की योजना पद्धति के आधारभूत सिद्धान्तो एवं गुण-दोषों का वर्णन
- समाज और शिक्षा में क्या सम्बन्ध(Relation between Society and Education in Hindi)
- वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष | वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष (Demerits of Present Curriculum)
- पाठ्य-पुस्तकों के प्रकार | पाठ्य-पुस्तक का अर्थ | अच्छी पाठ्य-पुस्तक की विशेषताएँ (Meaning of Text-Book in Hindi | Types of Text-Books in Hindi | Main Characteristics Of A Good Text-Book in Hindi)
- अच्छे शिक्षण की विशेषतायें | Characteristics of good teaching in Hindi
- शिक्षण के प्रमुख कार्य क्या क्या है | Major teaching tasks (works) in Hindi
- प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका | Role of Teachers in Teaching Learners in Hindi
- सीखने क्या है? | सीखने की विशेषताएं | what is learning in Hindi | characteristics of learning in Hindi
- पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता | पाठ्य पुस्तकों का महत्त्व | Need And Importance Of Text-Books in Hindi
- पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान | steps in the process of curriculum development in Hindi
- अधिगम की प्रकृति क्या है? | अधिगम की सम्पूर्ण प्रकृति का वर्णन | What is the nature of learning in Hindi? | Description of the entire nature of learning in Hindi
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निष्कर्ष (स्वरूप) | National Curriculum Framework summery NCF, 2005
- शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा | शिक्षण की प्रकृति | Meaning and definition of teaching in Hindi | Nature of teaching in Hindi
- सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? | Factors affecting learning in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]