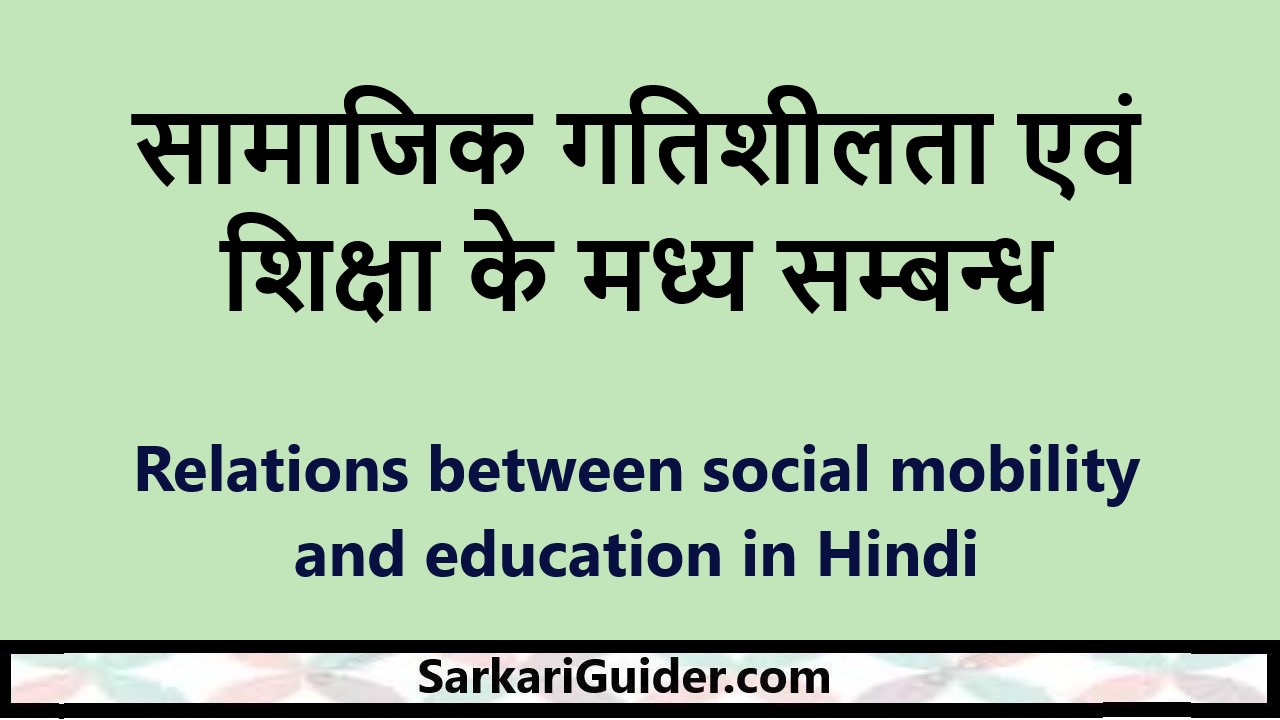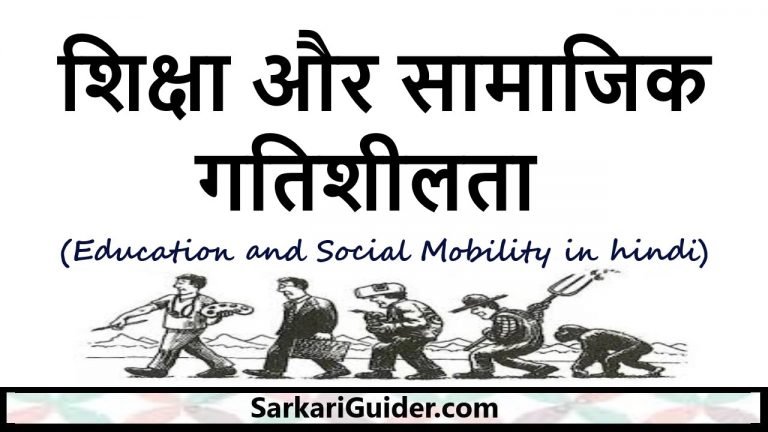सामाजिक गतिशीलता एवं शिक्षा के मध्य सम्बन्ध | Relations between social mobility and education in Hindi

सामाजिक गतिशीलता एवं शिक्षा के मध्य सम्बन्ध | Relations between social mobility and education in Hindi
इस पोस्ट की PDF को नीचे दिये लिंक्स से download किया जा सकता है।
शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत घटक और साधन है। शिक्षा के प्रसार एवं विकास ने सामाजिक गतिशीलता को बहुत प्रभावित किया है। जिन समाजों में शिक्षा की सुविधाएं जितनी अधिक मात्रा में सुलभ होती हैं उन समाजों में साभाजिक गतिशीलता उतनी ही अधिक होती है। सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण कारक है जो अन्य सभी घटकों को प्रभावित करती है। शिक्षा मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। शिक्षा भिन्न- भिन्न व्यवसायों के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है। यह मनुष्य को महत्वाकांक्षी बनाती है और उसी के द्वारा वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने योग्य बनते हैं। शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धि है। शिक्षा शीर्षात्मक गतिशीलता को उत्पन्न करती है। आधुनिक युग में शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता की प्रमुख धारा माना गया है। शिक्षा को ऐसा साधन माना गया है जो सामाजिक गतिशीलता लाती है। शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए मिलर व वूक ने कहा है कि, “औपचारिक शिक्षा सामाजिक गतिशीलता से प्रत्यक्ष तथा कारणतः सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध को सामान्यतः इस रूप में समझा जाता है शिक्षा स्वयं शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख कारक है।
उदाहरणार्थ- डाक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत आदि व्यवसायिक शिक्षा के अभाव मं व्यक्ति डॉक्टर, इन्जीनियर, या वकील नहीं बन सकता अतः शिक्षा व्यवसायिक स्थिति को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। शिक्षा द्वारा ही बालक की क्षमता और कुशलता का विकास होता है और सामाजिक गतिशीलता के लिए स्वयं को तैयार करता है।
भारतीय संविधान में शैक्षिक अवसरों की समानता की चर्चा की गई है जिसका प्रमुख कारण है कि शिक्षा के विकास द्वारा हम विभिन्न वर्गों में विद्यमान अन्तराल को दूर करना चाहते हैं। साथ ही शिक्षा के विकास द्वारा हम व्यक्ति के स्तर व रहन-सहन में सुधार लाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा जन्म पर आधारित वर्ग भेद को समाप्त करती है। समाज में विद्यमान दृढ़ संस्तरण (Rigid Stratification) को नष्ट करती है। किसी भी समाज में सामाजिक गतिशीलता की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज में सार्वभौमिक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को किस स्तर तक सुलभ कराया गया है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में कितनी विविधता है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की कैसी व्यवस्था है इस पर कितना बल दिया जा रहा है। शिक्षा समाज की मांगों की पूर्ति किस सीमा तक करती है और शिक्षा के अवसर किस सीमा तक सुलभ हैं, आदि। संक्षेप में इन सबका वर्णन इस प्रकार है।
-
सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की सीमा-
समाज में सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जितनी अधिक प्रभावी और दीर्घकालीन होगी उस समाज. की गतिशीलता उतनी ही अधिक प्रभावी होगी क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति में जागरुकता आती है। शिक्षा से ही वह अपने को सदैव आगे बढ़ाने में सफल होता है, अपने स्तर में परिवर्तन लाता है।
-
माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था-
सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में समाज के अन्तर्गत माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक होती है। इनके माध्यम से व्यक्ति समाज में ऊंचे पद पाता है। इसके अभाव में व्यक्ति उच्च सामाजिक स्तर नहीं पा सकता बल्कि उच्च सामाजिक स्तर वाले बालक भी निम्न सामाजिक स्तर पर आ सकते हैं।
-
पाठ्यक्रम में विविधता-
पाठ्यक्रम में विविधता से ही बालकों को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सामान्य पाठ्यक्रम को समाप्त कर पाठ्यक्रम में विविधता के सिद्धान्त को अपनाया जाए ताकि व्यक्तियों को अधिक अवसर प्राप्त हो सके और वे अपने सामाजिक स्तर व गतिशीलता में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सके।
उदाहरणार्थ- व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा आदि। इन शिक्षाओं द्वारा ही व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि बनकर समाज में अपने स्तर को उठा सकता है।
-
समाज की मांगों की पूर्ति-
शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में यह किहा जा सकता है कि शिक्षा समाज की मांगों की पूर्ति किस सीमा तक करती है उदाहरणार्थ यदि समाज को विकसित करने के लिए शिक्षक या बीमारियों से लड़ने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है और वहां इन्जीनियर और वकील तैयार किए जाएं तो उस समाज में बेकारी के सिवा कुछ नहीं फैलेगा। परिणामंस्वरूप उस समांज की गतिशीलता प्रभावित होगी वहां का आर्थिक स्तर भी निम्न होगा।
-
शैक्षिक अवसरों की समानता-
सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति को शैक्षिक अवसरों की समानता दी जाए। इसके अभांव में सामाजिक गतिशीलता को सर्वव्यापक नहीं बनाया जा सकता है।
शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है। परन्तु यह तब तक प्रभावी न होगी जब तक विद्यालय एवं शिक्षक दोनों ही न सचेत हों। टी. डब्ल्यू. मुसग्रेव ने विद्यालय के संदर्भ में लिखा है कि, “विद्यालय बालक में अत्यधिक आर्थिक महत्वाकांक्षा विकसित कर सकता है। इसी प्रकार वह सामाजिक गतिशीलता के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षा विकसित कर सकता है।”
विद्यालय में सभी को चाहे वे किसी जाति वर्ग के हों उन्हें शिक्षित किया जाये, विज्ञान विषय को अनिवार्य किया जाये, तकनीकी शिक्षा की सही व्यवस्था की जाये, उन्हें सामान्य अवसर उपलब्ध कराये जायें जब बालकों को ये अवसर प्राप्त होंगे तो वे समाज में अपनी योग्यतानुसार स्थान या पद प्राप्त कर सकेंगे और अपनी पदोन्नति कर सकेंगे अर्थात् सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी।
Sociology – महत्वपूर्ण लिंक
- Major Religion Of The World – Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism
- What Is Cultural Diffusion | Types Of Diffusion | Barriers In Diffusion | Elements Of Cultural Diffusion | Stages Of Diffusion
- सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है?
- सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त(Theories of Social Change in hindi)
- सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्त्व क्या क्या है? (Factors Resisting Social Change in hindi)
- सामाजिक परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? (Factors Affecting Social Change in hindi)
- सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, सामाजिक गतिशीलता के घटक
- सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार
- शैक्षिक समाजशास्त्र का महत्व स्पष्ट कीजिये | शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता
- शिक्षा का समाजशास्त्र पर प्रभाव | शिक्षा समाजशास्त्र को कैसे प्रभावित करती है?
- नव सामाजिक व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए | नव सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]