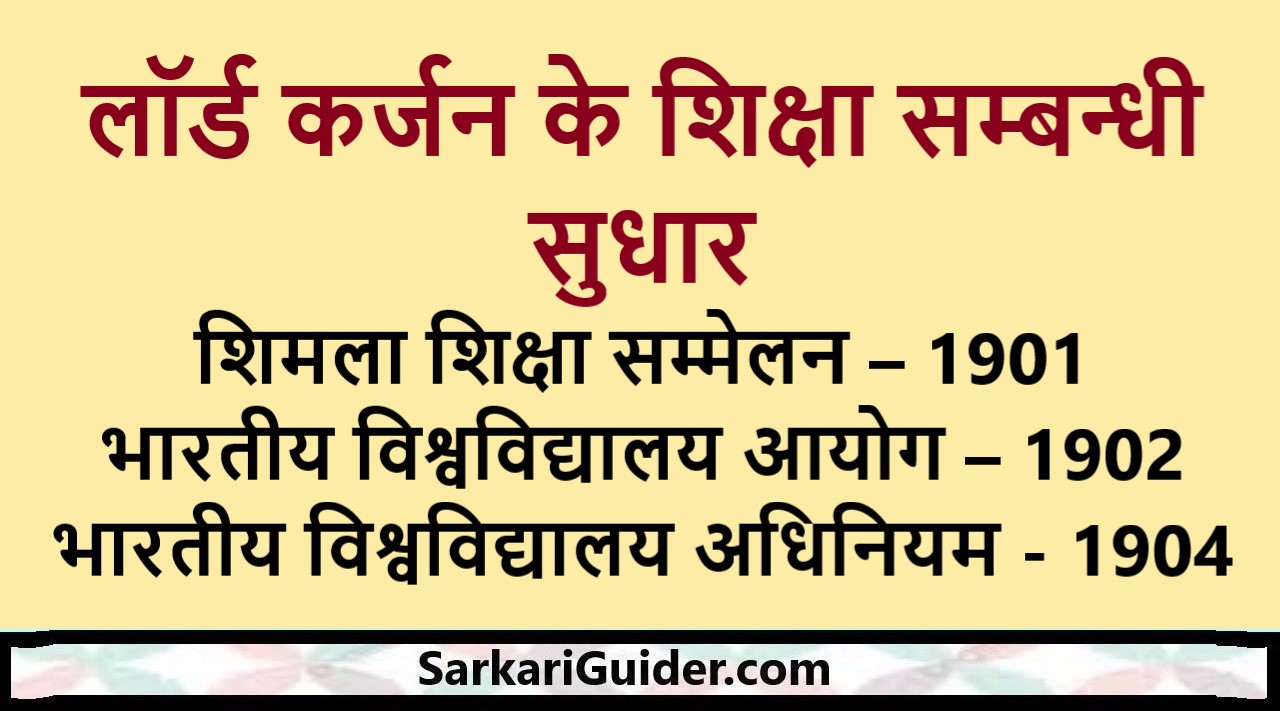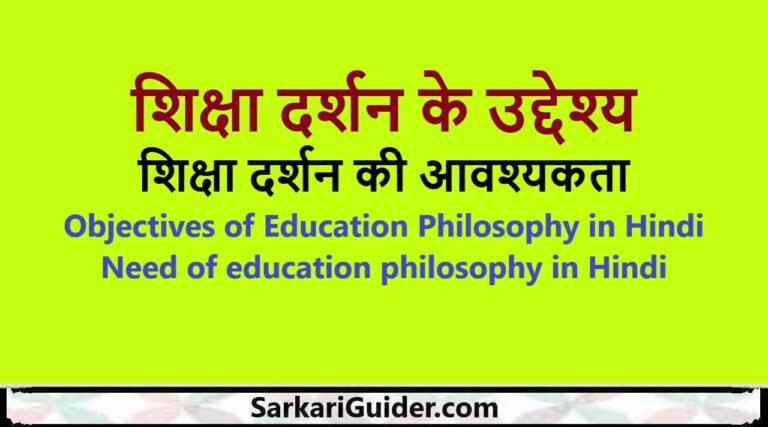लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी सुधार | शिमला शिक्षा सम्मेलन – 1901 | भारतीय विश्वविद्यालय आयोग – 1902 | भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम – 1904

लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी सुधार | शिमला शिक्षा सम्मेलन – 1901 | भारतीय विश्वविद्यालय आयोग – 1902 | भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम – 1904
लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी सुधार
(Educational Reforms of Lord Curzon)
कठोर तथा निरंकुश शासक होने के कारण कर्जन का राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोधी होना तो स्वाभाविक ही था, इसी कारण से भारतीयों द्वारा उससे घृणा करना भी स्वाभाविक था। किन्तु कर्जन की असाधारण विद्वता तथा अंग्रेजी का धुरंधर विद्वान तथा शिक्षा में उसकी अभिरुचि होने के कारण उसका भारतीय शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा।
नुरूल्ला तथा नायक के अनुसार – “कजन से श्रष्ठतर मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था।”
इस प्रकार, कर्जन में प्रशासकीय क्षमता और मानसिक योग्यता का सजीव सम्मिश्रण था। इस सम्मिश्रण के कारण कर्जन की यह धारणा थी कि शिक्षा में सुधार करके ही, प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। अपना इस धारणा के कारण उसने भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से पहले ‘शिमला-सम्मेलन’ का स्वयं सभापतित्व किया। उसके पश्चात् उसने “भारतीय विश्वविद्यालय आयोग” की नियुक्ति की, “भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम” पारित करवाया और शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किया। जिसका विवरण अग्र प्रकार है-
(1) शिमला- शिक्षा सम्मेलन, 1901
(Simla Education Conference, 1901)
जिस समय लॉर्ड कर्जन ने भारत के वाइसराय के रूप में इस देश की भूमि पर पैर रखा, उस समय यहाँ की शिक्षा अत्यन्त शोचनीय दशा में थो। विद्या और शिक्षा का प्रेमी होने के कारण, कर्जन को भारत आते ही यहाँ की शिक्षा की अप्रगतिशील स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो गया| कर्जन ने स्वयं इस सम्बन्ध में अपने विचारों को उद्घोषित करते हुए कहा-“जब मैं भारत नाया, तब शिक्षा-सम्बन्धी सुधार उन कार्यों में से मेरे समक्ष उपस्थित हुआ, जिसका प्रशासकीय पुनर्संगठन के किसी भी कार्यक्रम में प्रमुख स्थान होना उचित प्रतीत हुआ।” शिक्षा सुधार के कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लार्ड कर्जन ने सन् 1901 में “शिमला-शिक्षा-सम्मेलन” का आयोजन किया । कर्जन ने प्रान्तों के शिक्षा-संचालकों तथा मिशनरियों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। किन्तु, उसने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया। अत: भारतीयों का कर्जन के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना स्वाभाविक था।
“शिमला-शिक्षा-सम्मेलन” कर्जन के सभापतित्व में 15 दिन हुआ और उसमें शिक्षा-सम्बन्धी 150 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से निश्चित किया गया| कर्जन ने अपनी शिक्षा-नीति को इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित किया। सम्मेलन के विषय में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि उसकी कार्यवाही को आरम्भ से अन्त तक गोपनीय रखा गया था तथा उसको समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित नहीं होने दिया गया था। सम्मेलन के प्रति भारतीय पहले से ही सशंकित थे उसकी गुप्त कार्यवाही से उनको इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि उनके विरुद्ध किसी-न- किसी षड्यन्त्र की रचना अवश्य की गई थी। अत: वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे- “सम्मेलन, भारतीयों को यातना देने वाली सभा थी, जिसने उनके विरुद्ध किसी भयंकर षड्यन्त्र की रचना की थी।” “शिमला-शिक्षा-सम्मेलन में भारतीय शिक्षा से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया गया और उसी के आधार पर कर्जन ने अपनी सुधार-योजना का निर्माण किया। पर, क्योंकि भारतीय “सम्मेलन” की गुप्त कार्यवाही से अत्यधिक नाराज थे, इसलिए उन्होंने कर्जन के सुधारों को उपयोगिता की कसौटी पर परखने का प्रयास नहीं किया।
(2) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1902
(Indian Universities Commission, 1902)
(1) नियुक्ति के कारण-
“आयोग” की नियुक्ति के चार मुख्य कारण थे-
(i) विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों की संख्या में अति तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्य-भार हो गया था कि वे अपने कर्त्तव्यों का कुशलता से पालन नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप कॉलेजों का शिक्षण-स्तर निम्न हो गया था।
(ii) विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे। उनमें शिक्षण की, जो उनका मुख्य कार्य था, कोई व्यवस्था नहीं थी। इस विषय में कर्जन का मत था-” आदर्श विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए।”
(iii) पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन, लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श मान कर किया गया था लन्दन विश्वविद्यालय का सन् 1898 में पुनर्सँगठन हो गया था। अत: भारतीय विश्वविद्यालयों को उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाना आवश्यक था।
(iv) सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उनमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था।
उपर्युक्त आदर्श को प्राप्त करने और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधार करने के लिए लार्ड कर्जन में 27 जनवरी, सन् 1902 को “भारतीय विश्वविद्यालय आयोग” की नियुक्ति की।
(2) जाँच के विषय
“आयोग” को जॉँच करने के लिए तीन विषय दिए गए, यथा-
(i) विश्वविद्यालयों के विधान और उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
(ii) ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की वर्तमान दशा और उनकी भावी उन्नति की जाँच करना।
(iii) विश्वविद्यालयों के शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाने और विद्या की उन्नति करने के लिए उपयुक्त विधियों का सुझाव देना।
(3) सुझाव और सिफारिशें-
“आयोग” ने ब्रिटिश भारत के सब विश्वविद्यालयों की सूक्ष्म छानबीन करके, लगभग 6 माह के उपरान्त सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में “आयोग” ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुधार करने के निमित्त जिन सुझावों और सिफारिशों को लेखबद्ध किया, उनमें से निम्नांकित महत्त्वपूर्ण हैं-
(i) वर्तमान विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण-कार्य किया जाना चाहिए।
(ii) प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी जानी चाहिए।
(iii) सिंडीकेट (Syndicate) के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होनी चाहिए और उनका निर्वाचन सीनेट (Senate) के द्वारा किया जाना चाहिए।
(iv) कॉलेज को मान्यता देने के नियमों में कड़ाई की जानी चाहिए और द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।
(v) इण्टरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर देना चाहिए।
(vi) नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए।
(vii) स्नातक-पूर्व शिक्षण का कार्य, सम्बद्ध कॉलेजों में और स्नातकोत्तर शिक्षण-कार्य, विश्वविद्यालयों में किया जाना चाहिए।
(vii) सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जानी चाहिए और उनकी सदस्यता की अवधि पाँच वर्ष की होनी चाहिए।
(ix) प्रत्येक सम्बद्ध कॉलेज का प्रबन्ध, एक संगठित समिति के द्वारा किया जाना चाहिए।
(x) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग्य अध्यापकों को सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
(4) आयोग का मूल्यांकन-
“आयोग” के लगभग सभी सुझावों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारतीय विश्वविद्यालयों को लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित किया जाये अतः उसने भारती विश्वविद्यालय व्यवस्था के आधार भूत पुनर्सँगठन के सम्बन्ध में एक भी सुझाव नहीं दिया। उसने केवल भारत में प्रचलित विश्वविद्यालय व्यवस्था को इस देश के लिए हितकर समझकर उसको समुन्नत और शक्तिशाली बनाने के लिए ही सुझाव दिया। इस प्रसंग में डॉ० एस० एन० मुखर्जी का यह कथन अक्षरश: सत्य है- “विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में ‘आयोग’ की सिफारिशों का उद्देश्य विश्वविद्यालय-प्रणाली में किसी प्रकार का मौलिक पुनर्संगठन करना नहीं था, वरन् प्रचलित प्रणाली को केवल पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना था।”
(3) भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904
(Indian Universities Act, 1904)
लॉर्ड कर्जन की सरकार ने “भारतीय विश्वविद्यालय आयोग” के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक ने 21 मार्च, सन् 1904 को पारित होकर, “भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम” का रूप ग्रहण किया। इस “अधिनियम” द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए-
(i) सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित करके, यह निश्चित कर दिया गया कि उनकी न्यूनतम संख्या 50 एवं अधिकतम संख्या 100 होगी और वे अपने पद पर आजीवन न रहकर केवल 5 वर्ष रहेंगे।
(ii) सिंडीकेटों को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उनमे उचित प्रतिनिधित्व दिया गया।
(ii) सरकार को सीनेट द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने या स्वीकृति देने और उसके द्वारा उचित समय पर नियम न बनाये जाने पर स्वयं नियम बनाने का अधिकार मिल गया।
(iv) गवर्नर-जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं को निश्चित करने का अधिकार दिया गया।
(v) सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता विश्वविद्यालयों की सीनेटों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 एवं अन्य विश्वविद्यालयों की सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निश्चत की गई।
(vi) विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों के लिए नियम कठोर कर दिए गए और सिडीकेटों को इन कॉलेजों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया।
(vii) विश्वविद्यालयों के कार्य-क्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया। उनको परीक्षा लेने के अतिरिक्त शिक्षण और अनुसंधान-कार्य करने का भी अधिकार दिया गया।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- चार्टर एक्ट सन 1818 तथा 1833 का संक्षेप में वर्णन | सन् 1813 का चार्टर का आज्ञा पत्र | सन् 1833 का चार्टर का आज्ञा पत्र
- मैकाले का विवरण पत्र – 1835 | मैकाले का निस्यन्दन सिद्धान्त | बैंटिंक द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति – 1835
- विलियम एडम की रिपोर्ट | एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना | एडम रिपोर्ट का मूल्यांकन | एडम योजना की अस्वीकृति
- वुड का घोषणा पत्र- 1854 | वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें
- राष्ट्रीय शिक्षा की माँग | राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांत | राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांत की विशेषताएँ | राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना
- ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य | ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण | ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष
- गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक की स्वीकृति | बैंटिक की घोषणा के परिणाम
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]