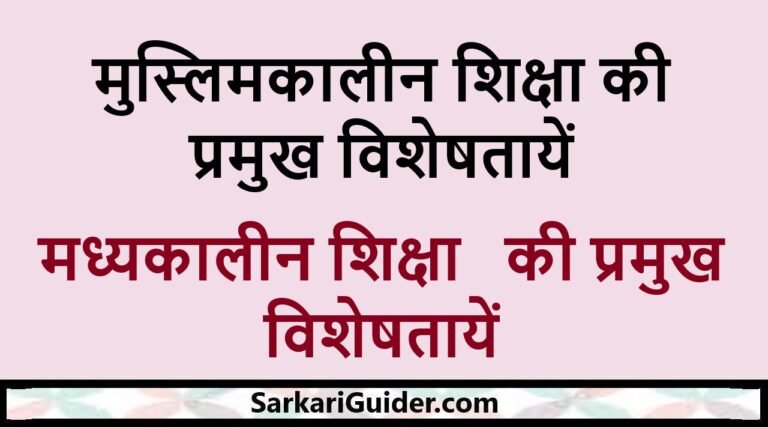प्लेटो का जीवन-वृत्त | प्लेटो की रचनाएँ | प्लेटो के दार्शनिक विचार
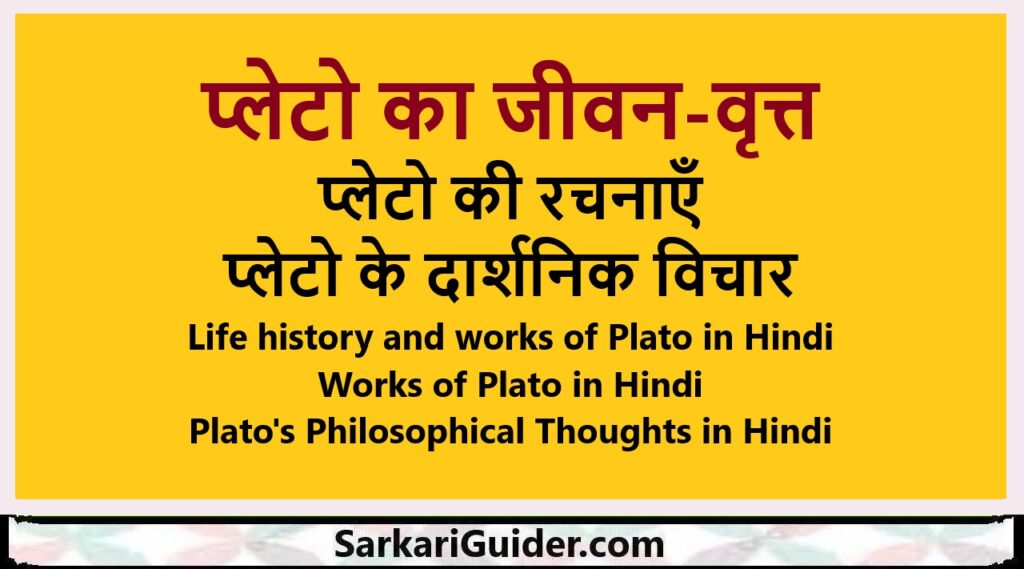
प्लेटो का जीवन-वृत्त | प्लेटो की रचनाएँ | प्लेटो के दार्शनिक विचार | Life history and works of Plato in Hindi | Works of Plato in Hindi | Plato’s Philosophical Thoughts in Hindi
प्लेटो का जीवन-वृत्त एवं रचनाएँ
प्लेटो का जन्म लगभग 427 ईसा पूर्व एथेन्स के एक कुलीन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एरिस्टनो और माता का नाम पेरिक्टोन था। प्लेटो बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। वह एक कुशल खिलाड़ी और सिपाही थे। साहित्य में भी उनकी पर्याप्त रुचि थी। उन्होंने ग्रीक साहित्य विशेषकर कविता का अध्ययन किया और स्वयं भी अनेक कविताओं की रचना की। प्लेटो की आरम्भिक शिक्षा के विषय में अधिक नहीं ज्ञात है। 20 वर्ष की अवस्था में वे सुकरात के सम्पर्क में आये और उन्हीं की देख-रेख में 28 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन करते रहे। अचानक सुकरात की दर्दनाक मृत्यु से उन्हें गहरा धक्का लगा। एथेन्स में उनको अपना जीवन भी असुरक्षित दिखलाई पड़ा; अतः उन्होंने 399 ई० पू० में एथेन्स छोड़ दिया और एक लम्बी यात्रा के लिए निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मिस्र, सिसली, मेगारा, इटली आदि देशों का भ्रमण किया और अनेक विद्वानों से परिचय प्राप्त करके बहुत कुछ सीखा। प्लेटो का यह सम्पूर्ण यात्राकाल अध्ययन, मनन, चिंतन और लेखन में ही बीता। मेगारा में रहकर प्लेटो ने आदर्शवादी सूक्ष्म दार्शनिक सिद्धान्तों का अध्ययन कियां और इटली में गणित का अध्ययन किया। अब वे सामान्य जीवन के लिए गणित और सैनिक शिक्षा को आवश्यक मानने लगे थे।
386 ई० पू० में प्लेटो इस यात्रा के बाद अपने देश एथेन्स वापस लौट आये और वहीं पर एक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों में उत्तम सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना था। इस शिक्षण संस्था में स्त्री एवं पुरुषों दोनों को समान रूप से भाषा, साहित्य, दर्शन, गणित, मानव विज्ञान आदि की शिक्षा देना आरम्भ किया। इसी संस्था में वे आजीवन अध्यापन कार्य करते रहे। यहीं पर उन्होंने अधिकांश लेखन कार्य भी किया। 347 ई० पू० में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।
प्लेटो की रचनाएँ-
प्लेटो ने अपने जीवन काल में दो प्रमुख कार्य किये। प्रथम शिक्षण- संस्था स्थापना और द्वितीय-पुस्तक लेखन। उन्होंने साहित्य, दर्शन, राजनीति, शिक्षा आदि विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं-
(1) दि रिपब्लिक (The Republic), (2) दि लॉज (The Laws). (3) एपॉलॉजी ऑफ साक्रेटीज (Apology of Socrates), (4) क्राइटो (Crito), (5) फीडो (Phaedo), (6)
सिम्पोजियम (Symposium)।
इन रचनाओं में प्रथम दो रचनाएँ ‘दि रिपब्लिक’ और ‘दि लॉज’ ही पप्लेटो के शैक्षि और राजनीतिक विचारों को प्रकट करती हैं। विशेष रचनाएँ क्रमशः सुकरात के मृत्यु-दंड, मुकदमे की सुनबाई, एथेन्स की परिषद् का निर्णय और प्रेमदर्शन आदि विषयों से सम्बन्धित है। प्लेटो की ये रचनाएँ प्रायः संवाद-ग्रन्थों के रूप में हैं जिनके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है।
प्लेटो के दार्शनिक विचार
प्लेटों के दार्शनिक विचारों पर ही उनके शैक्षिक विचार आधारित हैं। इसलिए शैक्षिक विचारों को जानने से पहले हम यहाँ पर संक्षेप में उनकी दार्शनिक विचारों का अध्ययन करेंगे-
- प्लेटो का आदर्शवाद- प्लेटो को आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा का पोषक माना जाता है। उनके अनुसार ‘विचार ही सत्य एवं अंतिम वास्तविकता’ है। प्लेटो के विचार में प्रत्यय उस वस्तु या पदार्थ से भिन्न है जिसमें यह प्रकट होता है; अतएव यह शाश्वत एवं अंतिम है तथा स्वतंत्र वास्तविकता है। ‘प्रत्यय’ मस्तिष्क में निहित अस्थायी और क्षणभंगुर विचारों से मित्र है। ये देश और काल के बन्धन से मुक्त हैं। प्लेटो ने प्रत्यय या विचार को समस्त वस्तुओं में निहित उस गुण की संज्ञा दी है जो वस्तु का सार है और समस्त वस्तुओं के साररूप विचार जगत् का निर्माण करता है। उनके अनुसार प्रत्यय या विचार शाश्वत् एवं निरपेक्ष है और इन्हीं के द्वारा वास्तविकता की दैवी व्यवस्था का निर्माण होता है। अर्थात् विचार वे स्वरूप हैं जिनके द्वारा किसी सुन्दर वस्तु की सुन्दरता का निर्माण होता है, जिनको जाना जा सकता है, सोचा जा सकता है, और प्रेम किया जा सकता है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् निरपेक्ष विचार है जिनका अस्तित्व स्वयं के लिए है; अतः स्पष्ट है कि प्लेटो का आदर्शवाद निरपेक्ष विचारों पर आधारित है।
- प्लेटो के जगत् सम्बन्धी विचार- प्लेटो की आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा की एक दूसरी विशेषता यह है कि वे दो प्रकार के जगत् में विश्वास करते हैं-(i) विचारों का जगत् और (ii) वस्तुओं का जगत्। इन दोनों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है-
(i) विचारों का जगत्- प्लेटो ने विचारों के जगत् को ही सत्य एवं वास्तविक जगत् माना है। उनके अनुसार यह जगत् स्थायी, शाश्वत्, स्थानरहित तथा अपरिवर्तित होता है। भौतिक जगत् का अस्तित्व भी विचारों पर निर्भर है। विचार-जगत् में एक प्रकार की दैवी- व्यवस्था पायी जाती है, इसलिए विचारों का जगत् ईश्वर का मन है। क्योंकि विचार या प्रत्यय शाश्वत् दैवी विचार होते हैं। इस प्रकार वे ईश्वर के विचार हैं। इन्हीं के अनुसार भौतिक जगत् की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। विचार जगत् की भौतिक वस्तुओं से पृथक् एवं स्वतंत्र अस्तित्व वाला होता है और इसके स्वरूप का निर्धारण विचारों द्वारा किया जाता है। सारांश यह कि प्लेटो ने विचार जगत् को ही सत्य, पूर्ण, स्थायी और भौतिक वस्तुओं से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला माना है।
(ii) वस्तु-जगत- प्लेटो ने वस्तु-जगत को अपूर्ण एवं जैल के समान माना है। उनके अनुसार यह जगत अस्थायी, नाशवान तथा परिवर्तनशील होता है। यह विचारों के जगत की एक छाया मात्र है। इस जगत की वस्तुएँ, देश, काल और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ स्वयं भी परिवर्तित हो जाती हैं। इस जगत का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता है। यह आध्यात्मिक जगत अथवा विचारों के जगत के अधीन होता है अर्थात् विचारों का आधार पाकर ही इस जगत की वस्तुओं का अस्तित्व होता है।
- प्लेटो के आत्मासम्बन्धी विचार- प्लेटो के अनुसार आत्मा उस परम मन का एक अंश है, जो विश्व के सम्पूर्ण अनन्त सत्यों का ज्ञान रखता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो भी आत्मा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता वरन् उसकी स्थिति पूर्ववत् बनी रहती है। इस प्रकार प्लेटो आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं। उनका मत है कि शरीर में आने से पूर्व भी आत्मा का अपना अस्तित्व रहता है और वह ज्ञानयुक्त भी होती है। यदि आत्मा को वविचारों का ज्ञान हो जाता है तो व मृत्यु के उपरांत विचारों के जगत में प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति अच्छे विचारों वाला होता है और सद्कर्मों के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी आत्मा का निवास आनन्द-लोक में होता है और वह पुनः उच्च विचारों वाले पुरुषों में अवतीर्ण होती है। इसके विपरीत दुष्ट विचारों वाले और दुष्कर्म करने वालों की आत्मा इधर-उधर भटकती रहती हैं और फिर निम्न श्रेणी के जीवों में अवतीर्ण होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटो का विश्वास पुनर्जन्म में भी था, जिसमें भारतीय दर्शन की झलक दिखलाई पड़ती है।
- आत्मा के अंग- प्लेटो ने आत्मा और शरीर में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है कि आत्मा आत्मगत और शरीर वस्तुगत होता है। उनके अनुसार मानव इस ब्रह्माण्ड का एक लघु रूप है जिसका निर्माण आत्मा और शरीर नामक दो तत्वों से हुआ है। प्लेटो के विचार में आत्मा के निम्नलिखित तीन स्वतंत्र अंग होते हैं-
(1) तृष्णा- यह आत्मा का निम्नतम् अंग है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की इच्छाएँ और कामनाएँ आदि आती हैं। तृष्णा ही मनुष्य की इच्छाओं और कामनाओं की प्रेरणा का केन्द्र है। इसकी स्थिति व्यक्ति के नाभि में मानी गई है। तृष्णा का गुण ‘संयम’ माना जाता है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति की मूल-प्रवृत्तियों अथवा प्रेरकों से है।
(2) संकल्प या इच्छा-शक्ति- यह आत्मा का दूसरा अंग है जो तृष्णा से उच्च स्तर का होता है। इसकी स्थिति व्यक्ति के हृदय में मानी गई है। संकल्प या इच्छा शक्ति का गुण ‘धैर्य, साहस, दृढता’ आदि माना जाता है। आत्मा के इन दोनों अंगों तृष्णा और संकल्प का सम्बन्ध व्यक्ति के शरीर से होता है।
(3) विवेक या तर्क- यह आत्मा का तृतीय और सर्वोच्च अंग है। इसकी स्थिति व्यक्ति के मन में मानी गई है। विवेक या तर्क का गुण ज्ञान एवं न्याय है। इसका सम्बन्ध विचार जगत से है। वस्तु-जगत से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह दैवी स्वरूप का है और शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। शरीर तो विवेक के लिए एक जेलखाने के समान होता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मन में निहित विवेक का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार विवेक का केन्द्र ‘मन’ है। मानव अपने इसी विवेक या तर्क के आधार पर समस्त कार्य करता है।
प्लेटो के विचार में जब आत्मा के उपर्युक्त तीनों अंग संगठित होकर कार्य करते हैं तो आत्मा उच्च स्थान को प्राप्त होती है और मनुष्य न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उन्नति करता है। अतः प्लेटो के अनुसार विवेकमय जीवन ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है और वह इस प्रकार का जीवन व्यतीत करके पूर्णता की दशा’ या आदर्श अवस्था का प्राप्त कर सकता है।
कुछ विद्वानों ने आत्मा के अंगों की इस विवेचना को प्लेटो का मनोविज्ञान कहा है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक तत्व प्राप्त होते हैं। कृष्णा का सम्बन्ध मूल-प्रवृत्तियों एवं प्रेरकों से है। संकल्प अथवा इच्छा-शक्ति का सम्बन्ध संवेगों तथा स्थायी भाव से तथा विवेक का सम्बन्ध बुद्धि और ज्ञान से है।
- ज्ञान का सिद्धांत- प्लेटो ने मानव प्राणी को सत्य या ज्ञान की खोज करने वाला बतलाया है। सत्य ज्ञान की खोज निरंतर होती रहती है और आत्मा जन्म के समय तथा बाद में भी ज्ञान प्राप्त करती है। ज्ञान वास्तव में आत्मा का ही एक अंश है। प्लेटो ने ज्ञान के तीन रूप बतलाये हैं-(1) इन्द्रिय ज्ञान जो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है। किन्तु यह ज्ञान सत्य नहीं होता। क्योंकि इन्द्रियाँ स्वयं ही सत्य नहीं है। (2) दूसरे प्रकार का ज्ञान वह है जो विभिन्न वस्तुओं के विषय में मतों या सम्मतियों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। प्लेटो के अनुसार किसी वस्तु के विषय में कोई मत किसी मुख्य परिस्थिति में ही सत्य हो सकता है, सभी परिस्थितियों में नहीं; अतः इस प्रकार का ज्ञान भी सत्य और नैसर्गिक नहीं होता है। (3) तीसरे प्रकार का ज्ञात तर्कयुक्त ज्ञान है। यह ज्ञान सत्य और नैसर्गिक होता है। इसका सम्बन्ध मन या बिवेक से है। अतः यह ज्ञान पूर्ण एवं सम्यक् होता है। इस प्रकार के ज्ञान अनुभव से स्वतंत्र हैं। इसके अन्तर्गत गणितीय सत्य, सामान्य प्रत्यय और निरपेक्ष विचार आदि आते हैं। निरपेक्ष विचार-सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् अनुभव द्वारा कभी प्राप्त नहीं किये जा सकते। इनकी अनुभूति तो आत्मा के द्वारा ही होती है। प्लेटो का कथन है कि आत्मा पूर्वजीवन में समस्त वस्तुओं का ज्ञान कर चुकी होती है, किन्तु जन्म के समय इन्हें भूल जाती है। जन्म के बाद वस्तुओं द्वारा एक संकेत मात्र मिलने से मन क्रियाशील हो जाता है और मन की इस प्रक्रिया से उस वस्तु का पुनः स्मरण होता है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- ज्ञानोपार्जन परीक्षण | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के उद्देश्य | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के प्रकार | निबन्धात्मक परीक्षण | निबन्धात्मक परीक्षणों में सुधार
- भारत में बुद्धि परीक्षण | intelligence test in India in Hindi
- पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन | हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना | महात्मा गांधी एवं महामना मालवीय के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन
- रवीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन-वृत्त | रवीन्द्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचार | रवीन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की समीक्षा
- डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व | डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तिगत स्वभाव का संक्षिप्त चित्रण
- आदर्श शिक्षक के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन | भारतीय संस्कृति के पोषक
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]