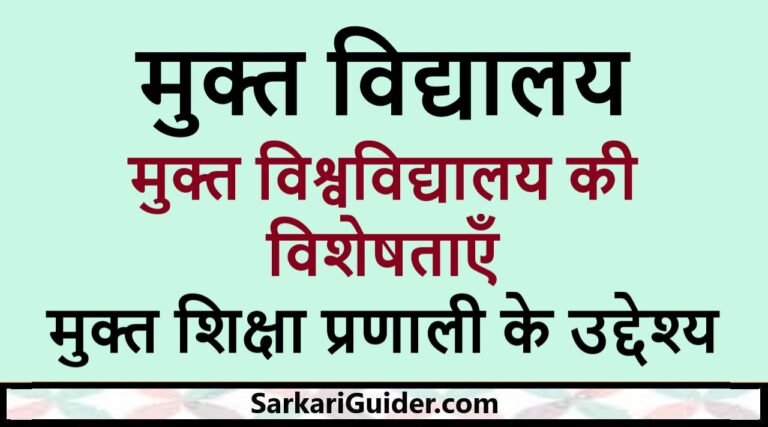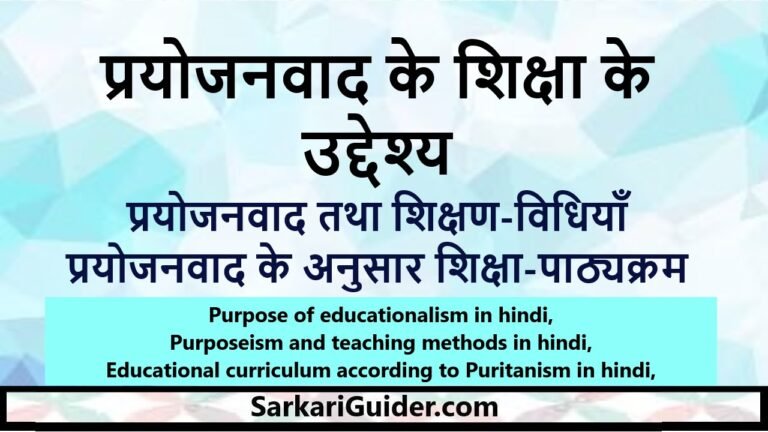प्लेटो के शैक्षिक विचार | प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य | प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षा के विभिन्न स्वरूप
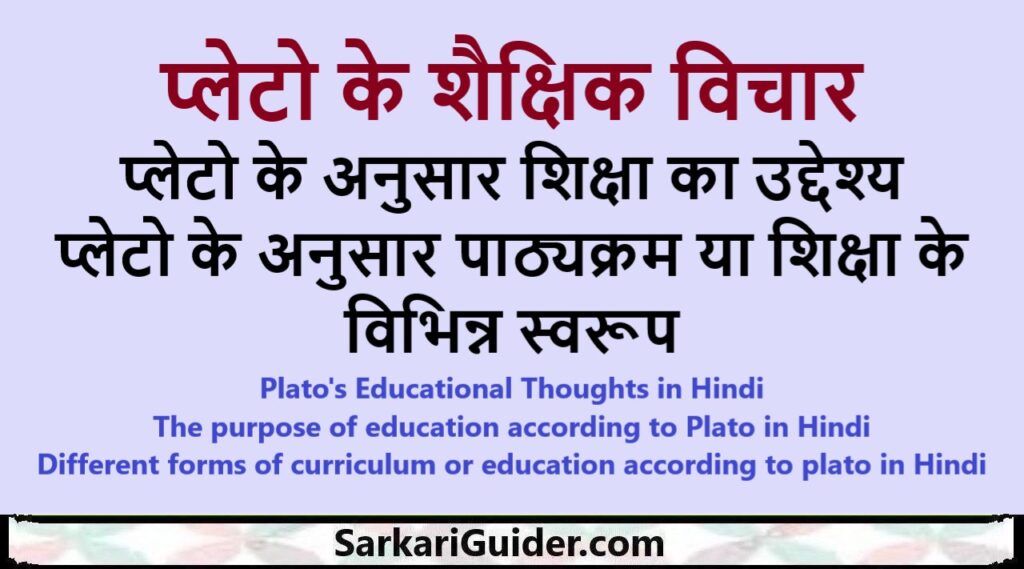
प्लेटो के शैक्षिक विचार | प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य | प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षा के विभिन्न स्वरूप | Plato’s Educational Thoughts in Hindi | The purpose of education according to Plato in Hindi | Different forms of curriculum or education according to plato in Hindi
प्लेटो के शैक्षिक विचार
प्लेटो के शैक्षिक विचार उनकी दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित हैं। ये विचार उनके दि रिपब्लिक’ और ‘दि लॉज’ नामक ग्रन्थों में मिलते हैं। प्लेटो ने शिक्षा को ‘एक महान् वस्तु माना है। उन्होंने अपने ग्रन्थ ‘दि लॉज’ में लिखा है-“शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम् वस्तु है जिसे सर्वोत्तम व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं।” प्लेटो के शिक्षा दर्शन से परिचय प्राप्त करने के लिए। हमें उनके विचारों को जानना आवश्यक है-
(1) शिक्षा का अर्थ- प्लेटो ने शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया के रूप में माना है जिसके द्वारा व्यक्ति की प्रवृत्तियों को सुधारा जा सकता है। शिक्षा छोटे बालकों की उन्नति के लिए प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रयत्न है। प्लेटो का विश्वास था कि बालकों को नैतिकता या सद्गुण सिखलाया जा सकता है। उन्होंने केवल चार सद्गुणों-बुद्धिमत्ता, संयम, साहस तथा न्याय को स्वीकार किया है। इनमें से संयम तथा साहस का विकास अभ्यास द्वारा किया जा सकता है; क्योंकि ये दोनों गुण आदतजन्य हैं। आदत और अभ्यास के आधार पर बुद्धितत्व का विकास किया जा सकता है और बुद्धितत्व के आधार पर बुद्धिमत्ता तथा न्याय जैसे सद्गुणों को विकसित किया जा सकता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा इन्हीं सद्गुणों को प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘दि लांज’ में लिखा है- “शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुणों की प्रारम्भिक मूल-प्रवृत्तियों के विकास के लिए उपयुक्त आदतों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण हमें वह योग्यता प्रदान करता है, जिससे हमें घृणा करना चाहिए और उस वस्तु से प्रेम करें जिससे वस्तुतः प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में इसी को वास्तविक शिक्षा कहा जायेगा!”
(2) संरक्षक और सैनिक वर्ग की शिक्षा पर बल- प्लेटो ने आत्मा के तीन अंगों-तृष्णा, संकल्प और विवेक के आधार पर राज्य के लोगों को तीन वर्गों में विभाजित किया है। तृष्णा की विशेषता वाला तीसरा वर्ग है। इस वर्ग के लोगों को व्यवसायी कहा जाता है। इसमें किसान, वस्त्र-निर्माता, दूकानदार, व्यापारी, उद्योगी आदि आते हैं। संकल्प की विशेषता वाला दूसरा वर्ग है। यह वर्ग सैनिकों का है। इनका कार्य राज्य की सुरक्षा-शान्ति बनाये रखना, नियमों और कानूनों की रक्षा तथा युद्ध-व्यवस्था आदि है। विवेक की विशेषता वाला प्रथम वर्ग है। इस वर्ग में दार्शनिक एवं शासक आते हैं जिनका कार्य संरक्षक के रूप में राज्य का शासन संचालन एवं सेवा करना है। प्लेटो ने इस वर्ग को अधिक महत्व दिया है। यह वर्गीकरण जाति के ऊपर निर्भर नहीं है बल्कि बुद्धि एवं ज्ञान पर है। इन तीनों वर्गों के सम्मिलित रूप से कार्य करने पर ही राज्य की समुचित उन्नति होती है। इनके प्रत्येक के कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने इनकी शिक्षा के सम्बन्ध में भी विचार प्रकट किया है। उनके अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के लोगों अर्थात् दार्शनिक, शासक और सैनिकों को शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। तृतीय वर्ग अर्थात् व्यवसायी वर्ग की शिक्षा पर प्लेटो ने अधिक ध्यान नहीं दिया है।
(3) अनिवार्य शिक्षा- प्लेटो ने व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों की प्रगति के दृष्टिकोण से समस्त नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक बतलाया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अनिवार्य शिक्षा का विचार प्रकट किया है। उन्हीं के शब्दों में-“बालक माता-पिता की इच्छा होने पर ही नहीं बल्कि उनकी इच्छा न होने पर भी विद्यालय में आयेंगे। शिक्षा अनिवार्य होगी शिक्षार्थी राज्य के समझे जायेंगे न कि अपने माता-पिता के।”
(4) स्त्री-शिक्षा- लेटो की शिक्षा योजना केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। उसमें पुरुषों के समान स्त्रियों को भी सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का विचार प्रकट किया गया है। प्लेटो के अनुसार स्त्रियाँ भी पुरुषों की भाँति दर्शन, शारीरिक शिक्षा, युद्ध-कला, संगीत एवं राजनीतिशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को राज्य के सभी प्रकार के पदों के योग्य समझा जाय और पुरुषों की ही भाँति उन्हें भी स्वीकार किया जाय। चूल्हे-चौके के संकुचित क्षेत्र से बाहर आने का अवसर दिया जाय जिससे वे भी समाज में कुछ क्रियात्मक कार्य कर सकें! इस सम्बन्ध में प्लेटो ने लिखा है-“तुम्हें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जो कुछ मैं कहता चला आ रहा हूँ वह केवल पुरुषों के लिए ही लागू होता है और स्त्रियों के लिए नहीं जहाँ तक उनके स्वभाव ग्रहण कर सकते हैं (उन पर भी लागू होता है)।”
प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य
प्लेटो ने शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों पर अपना विचार प्रकट किया है। वे शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करके उसे योग्य बनाना चाहते हैं कि वह राज्य के हित में अपना जीवन अर्पण कर दे। प्लेटो का कथन है कि “शिक्षा का अभिप्राय मैं बालकों की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को अच्छी आदतों में लगा देने में समझता हूँ जब तक कि उसे सुख-दुःख, मित्रता और घृणा के भाव का भलीभाँति ज्ञान न हो । शिक्षा के फलस्वरूप विवेक की प्राप्ति पर बालकों की आत्मा में और संसार की विभिन्न वस्तुओं में एक सामंजस्य का अनुभव करना है।” इस विचार से प्लेटो ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है-
(1) शाश्वत मूल्यों का साक्षात्कार- प्लेटो ने शाश्वत मूल्यों-सत्यम् शिवम् और सुन्दरम् का ज्ञान कराना शिक्षा का लक्ष्य माना है। उनके अनुसार ये गुण परमात्मा के गुण हैं; अतः परमात्मा से साक्षात्कार के लिए सर्वप्रथम इन गुणों का साक्षात्कार आवश्यक है। प्लेटो ने इन गुणों में से सुन्दरम् के विकास को शिक्षा का प्रारम्भिक उद्देश्य माना है। उनके अनुसार बालक की शिक्षा के आरम्भ में ही ऐसा शैक्षिक परिवेश उपस्थित करना चाहिए जिससे बालक में सुन्दरम् के प्रति अनुराग उत्पन्न हो। यही अनुराग आगे चलकर सत्यम् और शिवम् के ज्ञान में सहायक हो।
(2) शारीरिक एवं मानसिक विकास- प्लेटो ने व्यक्ति के विकास में शरीर और मन दोनों की महत्ता को स्वीकार किया है। अतः शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों- ‘शारीरिक एवं मानसिक विकास पर उन्होंने अधिक बल दिया है। उन्हीं के शब्दों में-“क्या मैं यह कहने में सही नहीं हूँ कि उत्तम शिक्षा वह है जो शरीर एवं मन को विकसित करने का सबसे अधिक प्रयास करती है।”
(3) संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण- प्लेटो के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य-संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम उसे उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों-शाश्वत मूल्यों का साक्षात्कार तथा शारीरिक और मानसिक विकास का होना आवश्यक है। प्लेटो का विचार है कि संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शाश्वत मूल्यों, शरीर तथा मन, आदतजन्य और विवेकजन्य जीवन, वैयक्तिक और सामूहिक हितों आदि में सामंजस्य होना परमावश्यक है।
(4) नागरिक कुशलता का विकास- प्लेटो ने नागरिक कुशलता का विकास करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। वे मानव-जीवन में नागरिक कुशलता के विकास को एक आवश्यक सद्गुण मानते थे। अतः उनके विचार में शिक्षा का यह परम कर्त्तव्य है कि इस सद्गुण को विकसित करने के लिए युवकों में धैर्य, साहस, उत्साह, त्याग, न्यायप्रियता, सत्य- प्रियता, क्रियाशीलता आदि जैसे गुणों का विकास करे।
(5) राज्य की एकता प्राप्त करना- प्लेटो ने राज्य को एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया है जो स्वयं में शरीर और मन के समस्त तत्वों से संयुक्त हो। उनके अनुसार राज्य एक अवयवी है और नागरिक उसके अवयव । शिक्षा का उद्देश्य राज्य का विकास करना है, जिसके लिए व्यक्ति को बलिदान करने तक से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए प्लेटो का विचार था कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य राज्य की एकता प्राप्त करना है। राज्य की एकता को स्थापित करने के लिए समस्त नागरिकों में सौहार्द्र की भावना, सेवाभाव, कर्त्तव्यपरायणता, स्वार्थहीनता आदि के गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों का विकास केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है।
(6) विवेक का विकास- प्लेटो ने विवेक को ही सामाजिक जीवन की आधारशिला माना है। उनके अनुसार यह प्रत्येक बालक में होता है किन्तु वह जागृत अवस्था में नहीं रहता। अतः शिक्षा का उद्देश्य इस विवेक को सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में लाना है। प्लेटो ने शिक्षा के इस उद्देश्य पर अधिक जोर इसलिए दिया है कि वे व्यक्ति के ऊतर विवेक का शासन स्थापित करना चाहते थे कि जिससे तृष्णा का एकाधिकार न हो सके।
(7) सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना- प्लेटो ने विद्यालय को मानवीकरण तथा समाजीकरण करने वाला साधन माना है। उनके मत नुसार विद्यालय का यह प्रमुख कार्य है कि वह बालकों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीवन बिताना सिखाये। इस दृष्टि से प्लेटो के विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘दि रिपब्लिक’ में लिखा है-“वास्तविक या सच्ची शिक्षा जो कुछ भी हो वह मनुष्यों को एक-दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों में सभ्य तथा मानवीय बनाने की प्रवृत्ति रखेगी।”
प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षा के विभिन्न स्वरूप
प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम के स्वरूप अथवा रचना पर विचार करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण में किन सिद्धान्तों को आधार माना है। प्लेटो ने पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों का सहारा लिया है-
(1) समानता का सिद्धांत,
(2) योग्यता और अभिक्षमता का सिद्धांत और
(3) आवश्यकता का सिद्धांत।
प्रथम सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों को एक जैसी शिक्षा प्रदान की जावे और स्त्री- पुरुष में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। दूसरे सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक की शक्ति, योग्यता और अभिक्षमता के अनुकूल शिक्षा दी जावे. और उसकी रुचियों और अभिरुचियों का भी ध्यान रखा जाये। तीसरे सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस सिद्धांत को मानकर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्लेटो ने सम्पूर्ण जीवन को कई भागों में बाँटा है-(1) आरम्भ से 5 वर्ष तक, (2) 6 से 13 वर्ष तक, (3) 13 से 16 वर्ष तक, (4) 16 से 20 वर्ष तक, (5) 20 ते 30 वर्ष तक, (6) 30 से 35 वर्ष तक, (7) 35 से 50 वर्ष तक, (8) 50 वर्ष से मृत्यु-पर्यन्त। इस प्रकार के विभाजन को हम सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित स्तरों में विभक्त कर सकते हैं-
(1) पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समय, (2) प्राथमिक शिक्षा का समय, (3) माध्यमिक शिक्षा का समय, (4) सैनिक शिक्षा का समय, और (5) उच्च शिक्षा तथा आगे का समय।
अब हम नीचे उक्त स्तरों के अनुकूल प्लेटो द्वारा निर्धारित पाक्रम के स्वरूप का अलग-अलग संक्षेप में वर्णन करेंगे
(1) पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समय- यह समय बालक की दशवकालीन अथवा नर्सरी शिक्षा का समय होता है। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बालक के विकास का समय होता है अतः उनके पालन-पोषण और स्वास्थ्य आदि पर विषेष ध्यान देना चाहिए। उनके समक्ष उत्तम शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का समय दृढता का समय होता है। इसमें बालकों में वीरों और महापुरुषों की जावन-कथाओं के माध्यम से तथा शिक्षक के आचरण के अनुकरण से उत्तम व्यवहार, सद्गुणों तथा अच्छी आदतों का विकास किया जाये। इस प्रकार उनमें शिवम् की भावना का विकास होगा और वे सत्यम् और सुन्दरम् की खोज कर सकेंगे।
(2) प्राथमिक शिक्षा का समय- इस अवस्था में बालक को संगीत, खेल कूद, व्यायाम, गणित, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि के विषयों को पढ़ाना चाहिए। संगीत के अन्तर्गत प्लेटो ने गायन, वादन और नृत्य त्रय-विषय और कलाओं को भी रखा है। यह शिक्षा बालक की प्रारम्भिक शिक्षा होती है।
(3) माध्यमिक शिक्षा का समय- प्लेटो के अनुसार यह अवस्था माध्यमिक शिक्षा (Secondary education) की अवस्था होती है। इसमें 10 से 13 वर्ष तक को हम लघु माध्यमिक (Middle) शिक्षा तथा 13 से 16 वर्ष तक को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कह सकते है। प्रथम स्तर पर बालकों को पढ़ना, लिखना, गणित, ज्यामिति, भाषा साहित्य, कला, संगीत और साधारण नक्षत्र-विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए और द्वितीय स्तर पर बाद्य संगीत, धार्मिक गीत, कविता, गणित तथा उच्च ज्योतिष आदि की शिक्षा प्रदान करना चाहिए।
(4) सैनिक शिक्षा का समय- इस अवस्था को ‘व्यायाम-काल की शिक्षा अथवा ‘जिमनास्टिक शिक्षा’ की अवस्था कहा जाता है। इसका उद्देश्य राज्य के लिए हष्ट-पुष्ट नागरिक एवं सैनिक तैयार करना है। अतः इसके लिए व्यायाम, खेलकूद, घुड़सवारी, युद्ध कला और अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग आदि पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए।
(5) उच्च शिक्षा तथा आगे की शिक्षा का पाठ्यक्रम- प्लेटो ने इस अवधि में शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें गणित, ज्यामिति, नक्षत्रशास्त्र आदि अध्ययन के मुख्य विषय थे। इन विषयों का अध्ययन उपयोगिता अथवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं बल्कि ज्ञानार्जन और सौन्दर्यानुभूति के लिए होता था। 30 से 35 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम योग्य पदाधिकारी बनने या शासक वर्ग में आने के लिए था। इस अवधि में अध्ययन के प्रमुख विषय दर्शनशास्त्र के साथ-साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति, न्याय एवं शिक्षाशास्त्र थे। 35 से 50 वर्ष की अवधि में शिक्षा को व्यावहारिक स्थान दिया गया। इस अवधि में नागरिक राज्य की सेवा शासक के रूप में करेंगे तथा राज्य एवं समाज के नेता होंगे। अतः उनके लिए दर्शन, न्याय, राजनीति, समाजशास्त्र आदि का विस्तृत एवं गूढ़ अध्ययन आवश्यक होगा। 50 वर्ष के बाद व्यक्ति लगभग समस्त प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था उसके आत्मज्ञान और पारलोकिक ज्ञान की अवस्था होती है; अतः इस समय इसे आध्यात्मशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि का अध्ययन करना चाहिए।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- ज्ञानोपार्जन परीक्षण | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के उद्देश्य | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के प्रकार | निबन्धात्मक परीक्षण | निबन्धात्मक परीक्षणों में सुधार
- भारत में बुद्धि परीक्षण | intelligence test in India in Hindi
- पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन | हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना | महात्मा गांधी एवं महामना मालवीय के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन
- रवीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन-वृत्त | रवीन्द्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचार | रवीन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की समीक्षा
- डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व | डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तिगत स्वभाव का संक्षिप्त चित्रण
- आदर्श शिक्षक के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन | भारतीय संस्कृति के पोषक
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]