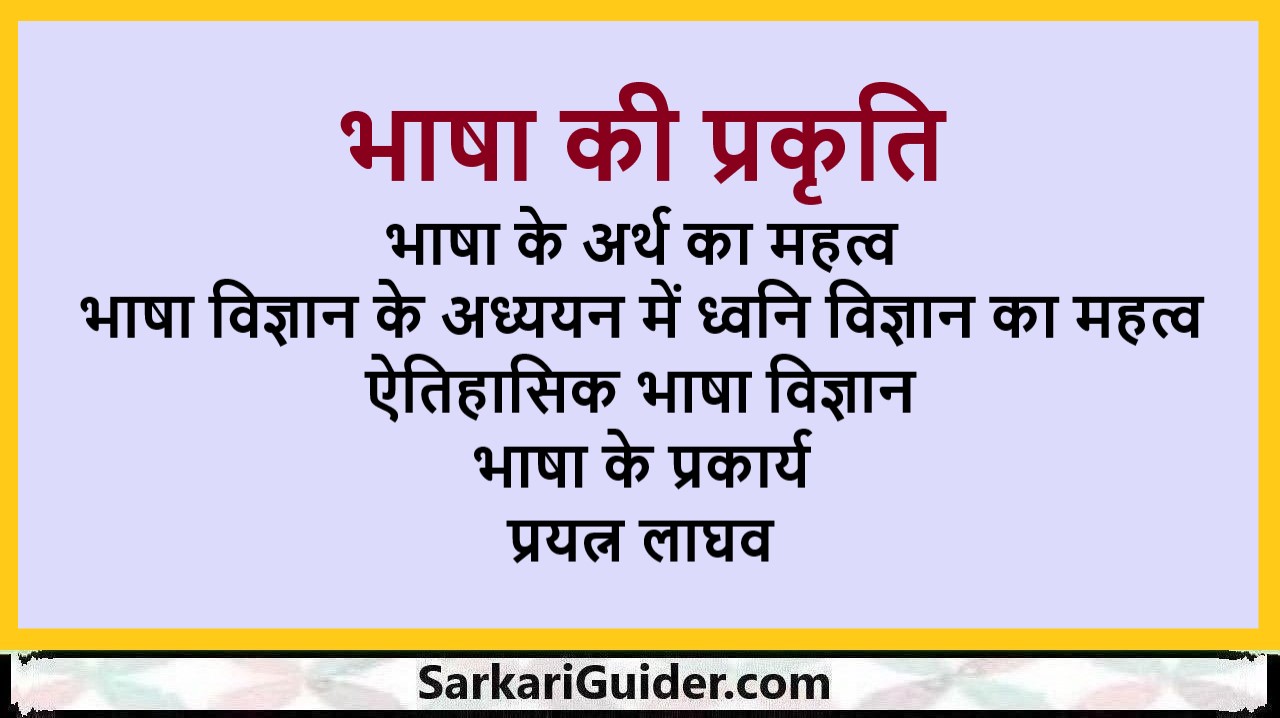भाषा की प्रकृति | भाषा के अर्थ का महत्व | भाषा विज्ञान के अध्ययन में ध्वनि विज्ञान का महत्व | ऐतिहासिक भाषा विज्ञान | भाषा के प्रकार्य | प्रयत्न लाघव
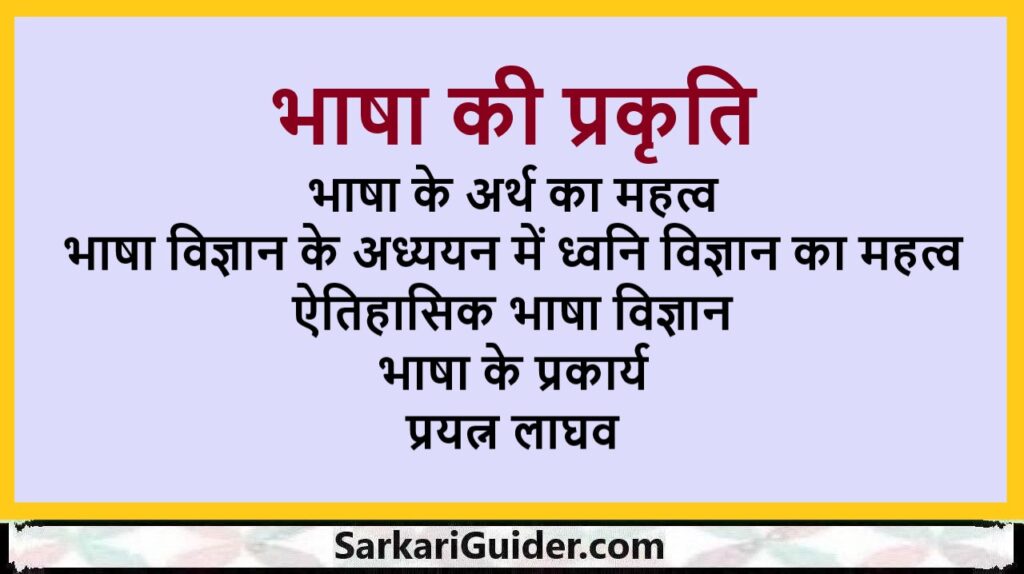
भाषा की प्रकृति | भाषा के अर्थ का महत्व | भाषा विज्ञान के अध्ययन में ध्वनि विज्ञान का महत्व | ऐतिहासिक भाषा विज्ञान | भाषा के प्रकार्य | प्रयत्न लाघव
भाषा की प्रकृति
किसी भाषा की शब्दावली के निर्माण में प्रकृति और प्रत्यय का विशेष महत्व होता है। शब्द जिन तत्वों में मिलकर बनता है। उसमें मूल अंश की प्रकृति और उनके विभिन्न रूपों को जो मूल शब्द से जुड़कर नया अर्थ देते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय स्वयं अर्थहीन होते हैं परन्तु प्रकृति से जुड़कर सार्थक बन जाते हैं। शब्दों की प्रकृति भाषा की प्रकृति भी सूक्ष्म होती है। ऊपर से ध्वनियों के योग से बने शब्द भले ही कुछ वर्णों के संयोग प्रतीत हों, उनकी आन्तरिक प्रक्रिया सर्वथा भिन्न होती है। जिस प्रकार हाथ, पैर, मुख आदि की दृष्टि से सभी मनुष्य एक प्रकार से दिखते हैं, परन्तु सबका स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है, उसी प्रकार सभी भाषाओं से ध्वनियां एक सी होती है परन्तु उनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है।
भाषा विज्ञान के अध्ययन में ध्वनि विज्ञान का महत्व
भाषाविज्ञान के क्षेत्र में ध्वनि विज्ञान का विशेष महत्व है। वस्तुतः ध्वनियाँ ही भाषा की मूलभूत लघुतम इकाई है अतः कुछ लोगों ने ध्वनि विज्ञान को भाषा विज्ञान से पृथक स्वतन्त्र विज्ञान माना लेकिन ध्वनियाँ भी अन्ततः मानव से सम्बद्ध हैं और वे मनुष्य की मानसिक स्थिति का द्योतन करती है। अतः यदि अर्थ, वाक्य और रूप भाषा विज्ञान के अंग हैं तो ध्वनि को भौतिक विज्ञानों से नहीं जोड़ा जा सकता। वस्तुतः ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का ही अंग है इसकी भाषा में बहुत उपयोगिता है। ध्वनि विज्ञान के द्वारा ही शुद्ध-शुद्ध बोलना सीखा जाता है। भाषा विज्ञान के बावजूद अशुद्ध उच्चारण अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके लिये ध्वनि के उच्चरण प्रक्रिया का अध्ययन आवश्यक है। ध्वनि विज्ञान मुख से उच्चरित ध्वनियों की उच्चारण प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि कौन ध्वनि कैसे बोली जाती है। हिन्दी में /श/ /स/, /व//ब/ के उच्चारण में अधिकांश अशुद्धियां होती हैं। ध्वनि-विज्ञान के माध्यम से हम इस उच्चारण दोष से बच सकते हैं अन्यथा सर का शर पढ़ने से अर्थ का अनर्थ ही होगा। ध्वनि विज्ञान के द्वारा दूसरी भाषाओं के सीखने में सहायता मिलती है। दूसरी भाषाओं की उच्चारण प्रक्रिया को जानकर ही उसका प्रयोग किया जा सकता है वस्तुतः भाषा मौखिक होती है और उसमें वाक्य, शब्द, पद आदि ध्वनियों के ही समूह हैं अतः किसी भाषा को मूलतः उसकी उच्चारण प्रक्रिया को समझ कर बोलना पड़ता है। वाक्य पद, शब्द ठीक होने पर भी यदि ध्वनि दोष है, तो अनर्थकारी हो जाता है। संस्कृत की यह उक्ति इस दृष्टि से प्रसिद्ध है।
भाषा के अर्थ का महत्व
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इससे उसका एक-दूसरे के सम्पर्क में आना स्वाभाविक है। सम्पर्क में आने पर विचार विनिमय अनिवार्य है। अतः जिस साधन से यह विचार विनिमय होता है उसे ही भाषा कहा जाता है। यह भाषा अर्थ से परिपूर्ण होती है। अर्थ ही भाषा को उपयोगी बनाता है। इसी के आधार पर व्यावहारिक कार्य पूर्ण होते हैं, व्यावहारिकता के साथ-साथ समाज के सभी क्षेत्रों में साहित्य में संगीत में, विज्ञान में, एवं कला में भी भाषा के अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है।
ऐतिहासिक भाषा विज्ञान
किसी एक भाषा के विभिन्न कालों के विवरण जब मिला दिये जाते हैं तब उसे ऐतिहासिक अध्ययन कहते हैं। इस प्रकार इसमें किसी भाषा के इतिहास का अध्ययन किया जाता है तथा सिद्धान्त की दृष्टि से उस भाषा के परिवर्तन सम्बन्धी सिद्धान्तों, नियमों तथा कारणों आदि का निर्धारण होता है। जहाँ वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसी भाषा का सीमित अध्ययन होता है। वहीं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में गतिशीलता होती है क्योंकि इसमें किसी भाषा का विकासात्मक अध्ययन होता है। उदाहरण के लिये यदि हम हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले ‘काम’, ‘हाथ’ शब्दों के विकास को जानना चाहें तो प्राकृत आदि में होते हुये संस्कृत भाषा के इसी ऐतिहासिक अध्ययन के सहारे इस प्रकार पहुँच सकते हैं-
|
काम हिन्दी – |
कुम्भ (प्राकृत) – |
कर्म (संस्कृत) |
|
हाथ (हिन्दी) – |
हत्थ (प्राकृत) – |
हस्त (संस्कृत) |
इस प्रकार हिन्दी के अनेक शब्दों का उद्भव एवं विकास जानने के लिये हमें संस्कृत पालि, प्राकृत, अपभ्रंश के रूपों का ध्ययन करना पड़ेगा। यह अध्ययन ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का विशेष महत्व है।
भाषा के प्रकार्यों (अभिलक्षणों)
भाषा संरचना और भाषिक प्रकार्य
समाज में रहकर मनुष्यों को अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिये निश्चित अक्षरों की शब्दावली का प्रयोग करना होता है। आदिकाल से भिन्न भिन्न शब्दावलियों का प्रयोग होता रहा है। इस असहजता को देखते हुए मनुष्य ने एक पूर्ण भाषा का निर्माण किया जिसमें भाषा की संरचना का मूल आधार ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ को विशेष महत्व दिया गया। इसके आधार पर भाषा का पूर्ण विकास किया जा सका है- (1) सांकेतिक भाषा, (2) मौखिक भाषा, (3) लिखित भाषा (4) यांत्रिक भाषा।
प्रयत्न लाघव
कठिनता से सरलता की ओर जाना मानव की स्वाभाविक वृत्ति है, सरलता की यह प्रवृत्ति उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखी जा सकती है। जब वह किसी स्थान के पीछे चलता है तो छोटा रास्ता (Short Cut) ढूँढ़ना चाहता है। यही प्रवृत्ति उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा में भी दिखलाई पड़ती है जिसे प्रयत्न लाघव अथवा मुख-सुख कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य शब्दों का उच्चारण करते समय सरलता के साथ शीघ्रता भी चाहता है। प्रयत्न लाघव की इसी प्रवृत्ति के कारण शब्द का उच्चारण करते समय उसका रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए मास्टर साहब, पण्डित जी, कृष्णचन्द्र आदि मास्साहब, पंडित जी, किशनचन्दर हो जाते हैं।
भाषा विज्ञान – महत्वपूर्ण लिंक
- भाषा की परिभाषा | भाषा के मूल तत्व या विशेषताएँ | भाषा के अभिलक्षण | भाषा की सरंचना
- भाषा व्यवस्था तथा भाषा व्यवहार | भाषा व्यवस्था तथा भाषा व्यवहार में अन्तर
- भाषा विज्ञान | भाषा विज्ञान के प्रमुख रूप | भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धति | भाषा विज्ञान की वर्णात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]