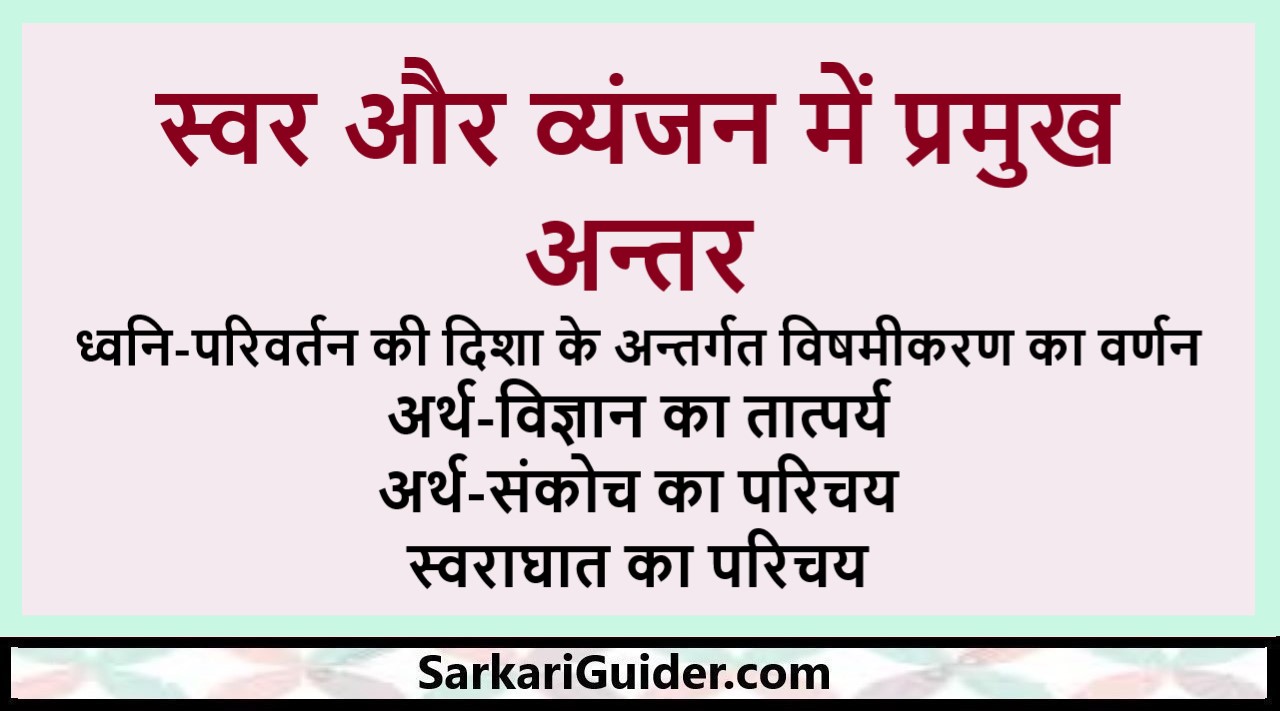स्वर और व्यंजन में प्रमुख अन्तर | ध्वनि-परिवर्तन की दिशा के अन्तर्गत विषमीकरण का वर्णन | अर्थ-विज्ञान का तात्पर्य | अर्थ-संकोच का परिचय | स्वराघात का परिचय
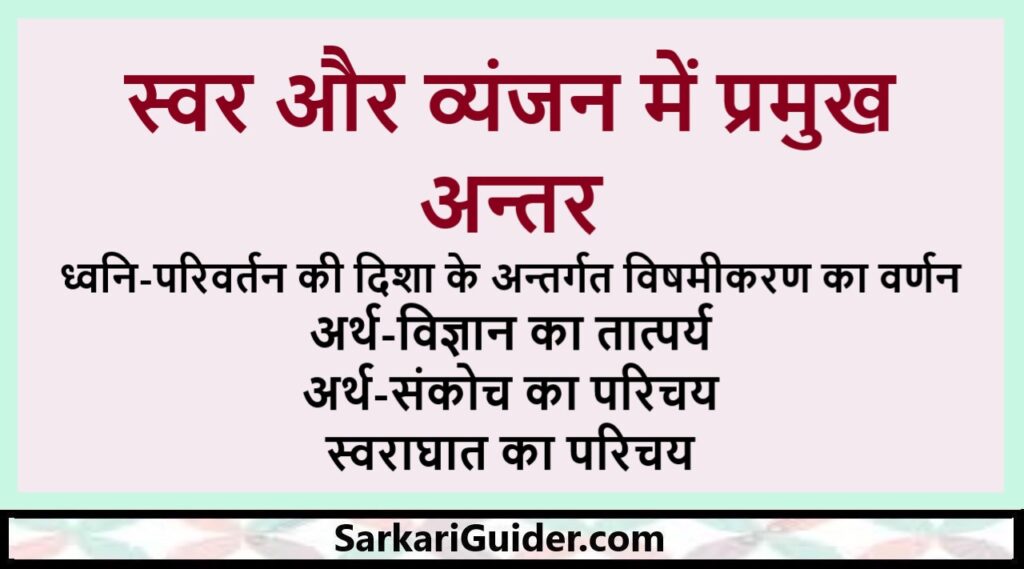
स्वर और व्यंजन में प्रमुख अन्तर | ध्वनि-परिवर्तन की दिशा के अन्तर्गत विषमीकरण का वर्णन | अर्थ-विज्ञान का तात्पर्य | अर्थ-संकोच का परिचय | स्वराघात का परिचय
स्वर और व्यंजन में प्रमुख अन्तर
स्वर और व्यंजन में निम्नलिखित प्रमुख अन्तर हैं-
(1) स्वर और व्यंजन का अन्तर श्रोता के विचार से किया जाता है। स्वर में श्रवण-गुण अथवा श्रवणीयता अधिक होती है। व्यंजन की अपेक्षा स्वर अधिक दूर भी सुना जा सकता है। ‘क्‘ की अपेक्षा ‘अ’ अधिक दूर तक तथा अधिक स्पष्ट सुनायी देता हैं यही कारण है कि साधारणतया व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना असम्भव माना जाता है।
(2) स्वर के उच्चारण में मुख-द्वारा छोटा-बड़ा तो होता है, पर वह कभी भी बिल्कुल बन्द नहीं होता। वह इतना छोटा तथा बन्द के समान भी नहीं होता जिससे कि उसके माध्यम से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर निकले। स्वरों में न किसी प्रकार का स्पर्श होता है और न घर्षण किन्तु व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा-बहुत स्पर्श अथवा घर्षण अवश्य होता है।
(3) स्वर-तन्त्र में से उत्पन्न शुद्ध नाद ‘स्वर’ ही स्वीकार किये जाते हैं। स्वर तो सभी नाद होते हैं, किन्तु व्यंजन कुछ नाद होते हैं और कुछ श्वास।
(4) स्वर की पुरानी परिभाषा थी- “स्वतन्त्र उचरत होने वाली ध्वनि को अथवा जिस ध्वनि की स्वतन्त्र अर्थात् बिना किसी की सहायता के उच्चारण होता है, उसको स्वर कहते है।” स्वर की व्युत्पत्ति है- स्वतो राजान्ते । अर्थात् जो स्वयं प्रतीत होते हैं। व्यंजन की पुरानी परिभाषा थी- “जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं।”
ध्वनि-परिवर्तन की दिशा के अन्तर्गत विषमीकरण का वर्णन
जहाँ निकटवर्ती दो समान ध्वनियाँ अपना रूप छोड़कर दूसरा रूप धारण कर लेती है, वहां विषमीकरण होता है। इसे कुछ विद्वान् असावर्ण्य भी कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं-
(1) पश्चगामी विषमीकरण- जहाँ समीपवर्ती दो समान ध्वनियों में से पूर्ववर्ती ध्वनि जैसी की जैसी बनी रहती है, किन्तु परवर्ती ध्वनि अपना रूप बदल लेती है, वहाँ पश्चगामी विषमीकरण माना जाता है। जैसे-
|
स्वर |
विषमीकरण |
व्यंजन |
विषमीकरण |
|
पुरूष |
पुलिस |
काक |
काग |
|
तित्तिर |
तीतर |
टंकण |
कंगन |
|
भित्ति |
भीतर |
पिपासा |
प्यास |
(2) पुरोगामी विषमीकरण- जहाँ समीपवर्ती दो समान ध्वनियों में से पूर्ववर्ती ध्वनि जैसी की तैसी बनी रही, किन्तु पूर्ववर्ती ध्वनि बदल जाये, वहाँ पुरोगामी विषमीकरण होता है जैसे –
|
स्वर |
विषमीकरण |
व्यंजन |
विषमीकरण |
|
नूपुर |
नेउर |
लांगल |
नांगल |
|
मुकुल |
मउल |
नवरीत |
लवली |
|
मुकुट |
मउर |
दरिद्र |
दरिद्दर |
अर्थ-विज्ञान का तात्पर्य
भाषा के अर्थ पक्ष के वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण का नाम ही अर्थ-विज्ञान है। इसी को अर्थिम भी कहा जाता है। भाषा की सफलता उसकी अर्थवत्ता में ही है। यदि किसी भाषा की ध्वनियाँ निरर्थक एवं अर्थहीन हैं तो वे न समाज के लिए उपयोगी हैं और न उनका अध्ययन भाषा- विज्ञान में किया जाता है। अतः अर्थ-विज्ञान के अन्तर्गत केवल उन्हीं सार्थक ध्वनियों द्वारा निर्मित शब्दार्थों का अध्ययन किया जाता है जो समाज के लिए उपयोगी होता है, जिनका आदिकाल से मानव-समाज में प्रचार है, जो सार्थक होने के कारण जनसाधारण में अत्यधिक प्रयुक्त होते हैं और जिनका मानव जीवन के विकास में भी अत्याधिक योग देखा जाता है। इतना ही नहीं, अर्थ-विज्ञान में शब्दार्थों का अध्ययन करते हुए यह भी देखने का प्रयत्न किया जाता है कि अर्थ का स्वरूप क्या है, शब्दार्थ का सम्बन्ध क्या है, अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, संकेत-ग्रहण क्या है, अर्थ-बोध के साधन क्या हैं, अनेकार्थी शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, अर्थ- परिवर्तन की कौन-कौन सी दिशाएँ होती हैं, बौद्धिक नियम एवं शब्दार्थ- परिवर्तन सम्बन्धी सिद्धान्त क्या हैं, आदि-आदि।
अर्थ-संकोच का परिचय
शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन की तीन दिशाएँ-अर्थ- विस्तार, अर्ध-संकोच और अर्थ-आदेश हैं। अर्थ-संकोच में शब्द के अर्थ का संकोच हो जाता है अर्थात् अर्थ की दृष्टि से शब्द दुर्बल हो जाता है। संस्कृत का गो शब्द ‘गम्’ धातु से बना है, अतः गति करने वाले अर्थात् चलने वालों के लिए भी गो की संज्ञा व्यवहृत होनी थी, किन्तु कालान्तर में इसका अर्थ केवल ‘गाय’ रह गया। मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, तीर सभी में गति है, अतः सभी के लिए ‘गो’ शब्द का प्रयोग उचित था। कोषों में गो का अर्थ इस रूप में प्राप्त होता है-वाणी, किरण, जल, चन्द्रमा, पवन, सूर्य, दृष्टि, बाण, बैल, गाय आदि। ‘वेदना’ शब्द ‘विद्’ धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ जानना है-सुख का भी दुःख का भी। आजकल केवल दुःख की अनुभूति ही वेदना है।
स्वराघात का परिचय
मूल भारतीय भाषा के संगीतात्मक स्वराघात से मान्त्रिक तथा गुणित अपश्रुतियों का विकास हुआ। इस प्रकार इस भाषा परिवार के विघटन के समय दो प्रकार का स्वराघात था-उदात्त तथा स्वरित। इधर भारत-ईरानी परिवार में अनुदात्त का विकास हो गया, जिससे वैदिक भाषा की परम्परा के रूप में तीन प्रकार के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संगीतात्मक स्वराधात प्राप्त हुए जो क्रमशः उच्चारण में उच्च, निम्न तथा मध्यम स्वर के द्योतक थे।
वैदिक भाषा में स्वराघात का अत्यधिक महत्व था। बिना स्वराघात के वैदिक ऋचाओं का उच्चारण नहीं किया जाता था और स्वर की अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता था।
इसके अतिरिक्त स्वराघात को अर्थद्योतन में भी सहायक माना गया है। वेदों के भाष्यकार वेंकट माधव के अनुसार, जिस प्रकार हाथ में दीपक लेकर चलने वाला व्यक्ति अन्धकार में ठोकर नहीं खाता, उसी प्रकार स्वराघात की सहायता से वेद-मन्त्रों के अर्थ की प्रतीति करने वाला पाठक उच्चारण आदि की दृष्टि से कभी पथ-भ्रष्ट नहीं होता।”
भाषा विज्ञान – महत्वपूर्ण लिंक
- ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारण
- ध्वनि परिवर्तन का स्वरूप और दिशा
- स्वरों का वर्गीकरण | उच्चारण प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण | घोषत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण | प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण | अनुनासिकता के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण
- वाक्यों के प्रकार | वाक्यों के भेद
- भारतीय आर्य भाषा | प्राचीन आर्य भाषा का परिचय
- प्राचीन भारतीय आर्य भाषा | वैदिक और लौकिक संस्कृत का नामकरण | वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अन्तर
- ग्रिम के ध्वनि-नियम के दोष | ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण | ध्वनि-यन्त्र का महत्व | वैदिक भाष तथा लौकिक संस्कृत को ध्वनियों का परिचय | ध्वनि-नियम और ध्वनि-प्रवृत्ति में अन्तर
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]