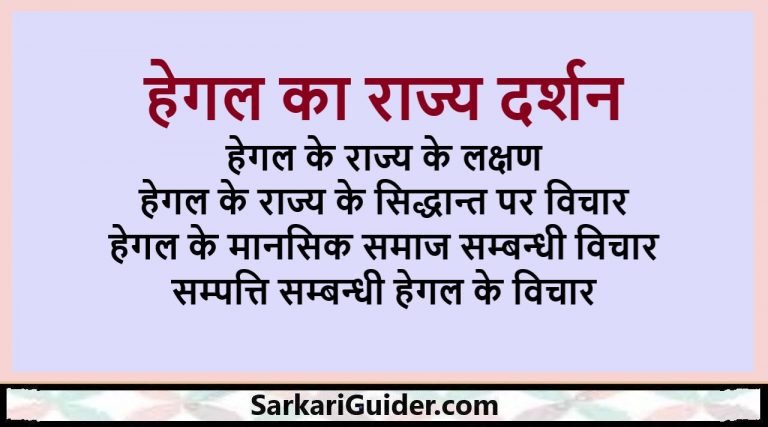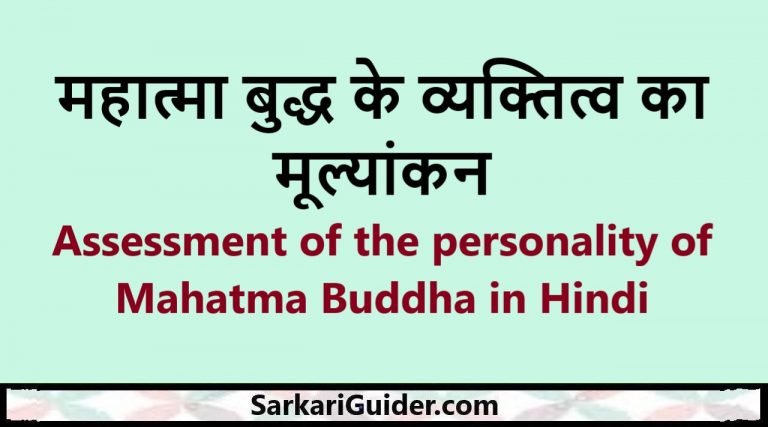उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन | उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा
उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन | उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा
उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन
प्रस्तावना- उत्तर वैदिक काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है जिसमें अन्य तीन वेदों-यजुर्वेद, सामवेद, तथा अथर्ववेद और ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई थी। यह एक दीर्घकाल था, जिसमें आर्य-सभ्यता का विस्तार व विकास हुआ तथा उसमें कुछ परिवर्तन भी हुए। वे सप्त सिन्धु प्रदेश से आगे बढ़कर समस्त उत्तरी भारत और फिर दक्षिण भारत में फैल गए। यद्यपि उनके आधारभूत सिद्धान्त बहुत-कुछ ऋग्वैदिक सभ्यता के समान हैं, तथापि आर्यों के स्वजात अनुभव, ज्ञान और विजातीय सम्पर्क ने उन्हें अधिकाधिक समृद्ध करना आरम्भ कर दिया था। अधिकांश इतिहासकारों ने इस सभ्यता की समय लगभग 1000 ई० पूर्व से 600 ई० पूर्व माना है। इस युग में आर्यों ने पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। गंगा-यमुना के दोआब का क्षेत्र आर्यों की सभ्यता का केन्द्र स्थान बन गया था। दक्षिण में विंध्याचल को पार कर गोदावरी नदी के प्रदेशों में आर्य लोग बसे हुए थे। इस प्रकार हिमालय से लेकर विन्ध्याचल तक के प्रदेशों पर आर्यों का अधिकार था।
उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा
उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा का विवेचन अग्रलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है। यथा-
-
नगरों का विकास-
ऋग्वैदिक काल में नगरीय सभ्यता से बहुत दूर थे। वे प्राकृतिक वातावरण के अधिक समीप रहते थे। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जब गंगा- यमुना के मैदान में फैल गये, तो उन्होंने बड़े नगरों को बसाया और वहाँ बस गये। राज्यों की राजधानियों में बड़े-बड़े विशाल महल बनने लगे।
-
वर्ण व्यवस्था-
पूर्व वैदिक काल में वर्ण का निश्चय व्यक्ति के व्यवसाय से होता था। किसी विशेष व्यवसाय में कुशलता अर्जित कर उस व्यवसाय को अपनाने से उस व्यक्ति का वर्ण भी उस व्यवसाय के अनुरूप हो जाता था। जातियाँ नहीं थीं और न छुआ-छूत थी। सभी वर्ण समान समझे जाते थे। अतः उनमें आपस में परिवर्तन हो जाता था। ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था ने अब जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया था। अब जन्म के आधार पर व्यक्ति का वर्ण निश्चित हो गया। वर्ण व्यवस्था में कट्टरता आ गई तथा वर्ण परिवर्तन असम्भव हो गया। अन्तर्जातीय विवाह को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा तथा शूद्रों को नीच समझा जाने लगा। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का कथन है कि “उत्तर वैदिक साहित्य में शूद्र निस्सन्देह समाज के एक पृथक अंग माने गए हैं परन्तु वास्तव में उनको अपावन समझा गया।
वे यज्ञानुष्ठानों में भाग लेने अथवा धर्म-स्तुतियों के उच्चारण के अधिकारी न समझे गए। शूद्रों के साथ आर्यों का विवाह-सम्बन्ध वर्जित कर दिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में तो एक स्थान पर कहा गया है कि “शूद्र दूसरे का सेवक है, जिसका इच्छावश निष्कासन तथा वध किया जा सकता है।’ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अधिक सम्माननीय समझा जाने लगा। व्यवसाय वंशानुगत हो गया तथा एक परिवार के लोग एक ही व्यवसाय अपनाने लगे। इससे धीरे-धीरे उपजातियों की संख्या बढ़ने लगी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टता चार वर्णों- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित हो गया था। अध्ययन-अध्यापन तथा धार्मिक अनुष्ठान कराना आदि ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य थे। क्षत्रिय युद्ध कार्यों एवं शासन में भाग लेते थे। वैश्य कृषि, पशुपालन एवं व्यवसाय द्वारा अपनी आजाविका कमाते थे। शूद्रों का कार्य उपर्युक्त तीनों वर्गों की सेवा करना था। डॉ० राजबली पाण्डेय का कथन है कि “ऋग्वेद के वर्ण गुणकर्म पर अवलम्बित थे, परन्तु इस काल का वर्ण प्रायः जन्म पर अवलम्बित होकर पैतृक हो गया था।।”
-
ब्राह्मणों का प्रभुत्व-
वेदों की भाषा अब लोगों को दुरूह व अस्पष्ट लगने लगी। सामान्य व्यक्ति के लिए वेदों को समझना कठिन हो गया। वेदों को समझने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक हो गया। अब एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जिसे प्राचीन वैदिक ग्रन्थों को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इसके फलस्वरूप एक व्यावसायिक ब्राह्मण वर्ग का उदय हुआ जो आगे चलकर शीघ्र ही एक अनम्य और स्थिर जाति बन गई। पूर्व वैदिक काल में ब्राह्मणों का कोई प्रभुत्व नहीं था। कुल का सबसे बड़ा पुरुष ही सभी धार्मिक कृत्यों को पूरा करता था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। वे राजाओं और जन साधारण के धर्म-गुरु बन गये। प्रत्येक कार्य में उनसे सलाह ली जाती थी एवं लोग ब्राह्मणों के कोप एवं श्राप से डरते थे।
-
विवाह-
विवाह अब भी एक पवित्र और धार्मिक कार्य माना जाता था। इस युग में भी बाल-विवाह प्रचलित नहीं थे। सामान्य रूप से एक स्त्री से ही विवाह किया जाता था परन्तु बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। राजवंश के व्यक्ति पुरोहित तथा धनी व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे। विधवा-विवाह प्रचलित थे। इस युग में अधिकांशतः सजातीय विवाह ही होते थे। परन्तु कहीं-कहीं अन्तर्जातीय विवाह के उल्लेख भी मिलते हैं। ऋषि च्यवन ने राजा ययाति की पुत्री सुकन्या से विवाह किया था।
-
अहिंसा का बीजारोपण–
ऋग्वैदिक काल में लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। उत्तर वैदिक काल में मांस भक्षण एवं सुरा पान हेय दृष्टि से देखे जाते थे तथा पाप समझे जाते थे। एक प्रकार से लोगों की प्रवृत्ति अहिंसा की तरफ बढ़ने लगी। जीवनमात्र पर दया की भावना की विकास हुआ।
-
मनोरंजन के साधन-
उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित थे। रथ-दौड़, घुड़-दौड़, आखेट, संगीत-नृत्य आदि आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उन्हें जुआ खेलने का भी बड़ा शौक था। वे अपने मनोरंजन के लिए शिकार भी करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही संगीत एवं नृत्य में भाग लेते थे। ये लोग वीणा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों का प्रयोग करते थे।
-
स्त्रियों की दशा-
उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। अब समाज में उन्हें वह सम्मान प्राप्त नहीं था जो पूर्व वैदिक काल में था। इस युग में बहुविवाह प्रथा ने स्त्रियों की दशा को दयनीय बना दिया था। स्त्रियों का जीवन कलहमय हो गया था। उत्तर- वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पतन की ओर थी। कन्याओं के जन्म पर लोग दुःखी होते थे। परिवार के अनेक धार्मिक कार्य स्त्रियों के स्थान पर पुरोहित करने लगे थे। जिससे स्त्रियों का महत्व कम हो गया था। परन्तु इस काल में भी स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थीं। गार्गी, मैत्रेयी आदि इस युग की महान विदुषी महिलाएं थीं। इस युग में पर्दा-प्रथा, सती प्रथा आदि बुराइयाँ समाज में प्रचलित नहीं थीं। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ऋग्वेद काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी।
-
शिक्षा को अधिक महत्व–
उत्तर वैदिक काल में यज्ञ काफी होने लगे, जिससे शिक्षा का पहले की अपेक्षा अधिक महत्व हो गया था। शिक्षा का विकास वेदों का अध्ययन ही था परन्तु वैदिक मन्त्रों के साथ-साथ विज्ञान, गणित, भाषा, युद्ध-विद्या आदि की भी शिक्षा दी जाने लगी थी। शिक्षा गुरु के आश्रम में ही दी जाती थी।
-
पारिवारिक जीवन-
इस युग में भी संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया प्रायः पिता ही होता था। उसका परिवार पर नियन्त्रण रहता था। परिवार के सभी सदस्य मुखिया की आज्ञा का पालन करते थे। पिता अपने पुत्रों को दंन्डित कर सकता था, परन्तु परिवार के सभी सदस्यों का पालन-पोषण तथा उनकी उन्नति के लिए प्रयास करना उसका कर्तव्य माना जाता था। पिता की सम्पत्ति पर सब पुत्रों का अधिकार रहता था। बहु- विवाह प्रथा के कारण परिवार में कभी-कभी परस्पर झगड़े भी हो जाया करते थे।
-
भोजन और वेशभषा-
इस युग में आर्यों का मुख्य भोजन अन्न, दूध दूध से बना अन्य पदार्थ और चावल खाते थे (चावल को दूध में पकाना), तिलौदन (तेल को दूध में पकाना) तथा अपूप (पूआ) आदि का भी प्रयोग करते थे। आर्य लोग मांस का सेवन भी करते थे। सुरा और सोम अब भी उनके पेय पदार्थ थे।
इस युग में आर्य लोग सूती, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ब्रह्मचारी और तपस्वी मृग-चर्म का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे।
-
आश्रम व्यवस्था-
उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। इस युग में मनुष्य का जीवनकाल निम्न चार आश्रमों में विभाजित था
(i) ब्रह्मचर्याश्रम- इसमें मनुष्य अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष किसी गुरुकुल में रहकर विद्या प्राप्त करता था। इसमें विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता था।
(ii) गृहस्थाश्रम- इसमें मनुष्य 50 वर्ष की अवस्था तक सांसारिक जीवन का उपभोग करता था। धर्मशास्त्रों में इसको अन्य आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया है।
(iii) वानप्रस्थाश्रम– इसमें मनुष्य 75 वर्ष की अवस्था तक रहता था। इस आश्रम में मनुष्य गृहस्थ जीवन छोड़कर जंगल में चला जाता था। इस काल में वह शारीरिक तपस्या के साथ वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों का अध्यनन करता था।
(iv) संन्यासाश्रम- इस आश्रम में व्यक्ति 100 वर्ष व इससे भी अधिक अवस्था तक रहता था। इसमें मनुष्य संन्यासी बनकर और दण्ड-कमल लेकर निरन्तर घूमता रहता था। वह संसार का अधिक से अधिक कल्याण करता हुआ मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयान करता था।
इन चार आश्रमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना आर्य लोग गौरव का प्रतीक मानते थे। डॉ० आर० सी० मजूनदार के अनुसार, ‘चार आश्रमों का संगठन भारतीय समाज की अनोखी विशेषता है।” डॉ० राजबली पाण्डेय का कथन है कि “मानव-जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति के लिए चारों आश्रमों का विकास हुआ था। वास्तव में मनुष्य के इतिहास में उसके जीवन के वैज्ञानि विभाजन का यह प्रथम शास्त्रीय प्रयास था।”
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति | उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा
- उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति | उत्तर वैदिक काल की धार्मिक दशा | उत्तर वैदिक काल की आर्थिक दशा | उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]