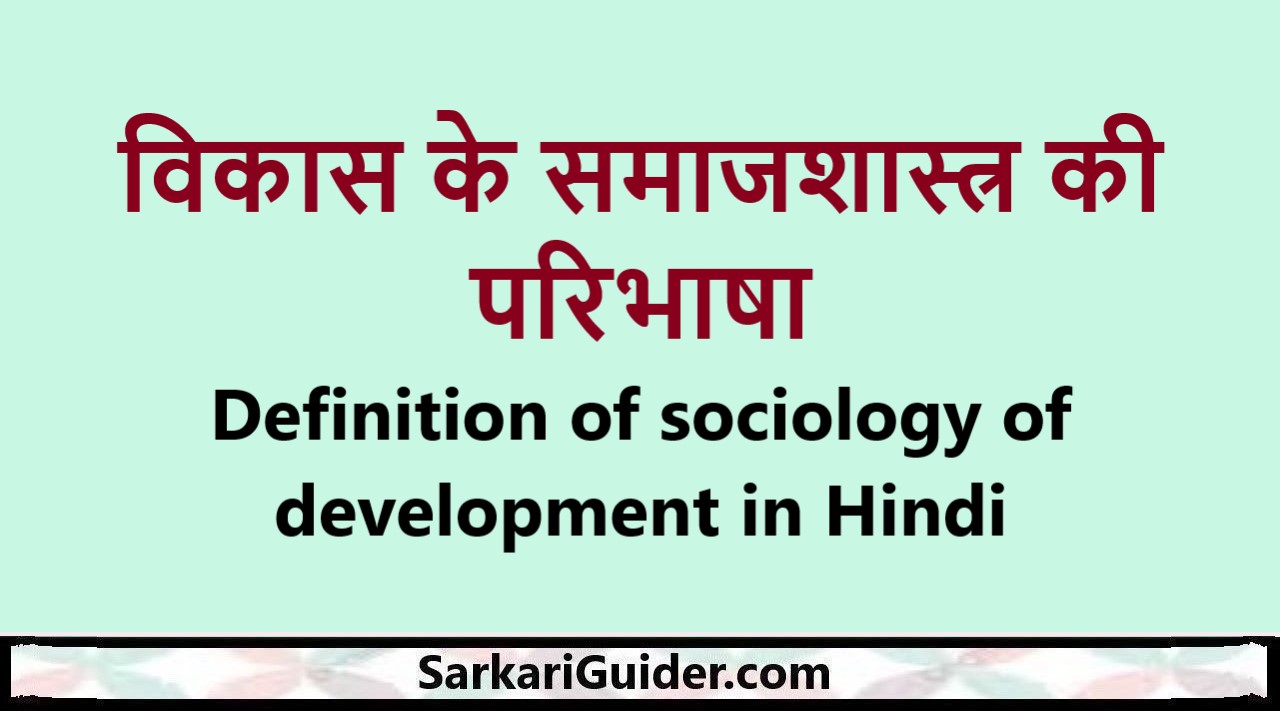विकास के समाजशास्त्र की परिभाषा | Definition of sociology of development in Hindi
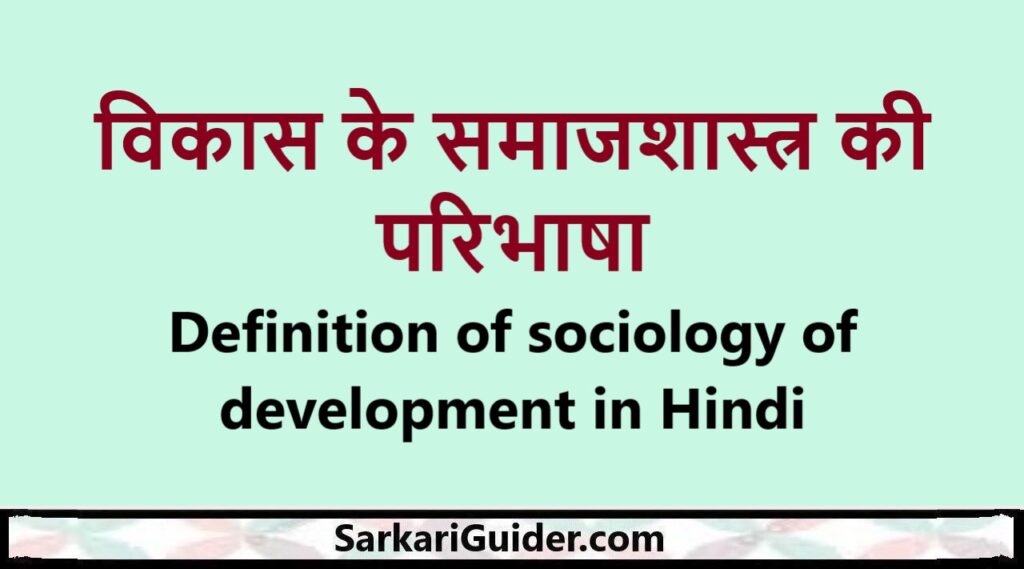
विकास के समाजशास्त्र की परिभाषा | Definition of sociology of development in Hindi
विकास के समाजशास्त्र की परिभाषा
मुख्यतः समाजशास्त्र की बहुत-सी शाखायें हैं, जैसे-कानून का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, पर्यावरण का समाजशास्त्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का समाजशास्त्र, आमीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र आदि। इसी तरह से विकास का समाजशास्त्र भी, समाजशास्त्र की एक शाखा है। यह विकास प्रक्रिया एवं सामाजिक-सांस्कृतिक दशाओं के बीच परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन करती है। इस विषय की मान्यता है कि विकास के प्रत्येक पक्ष का क्रियान्वयन, समाजशास्त्रीय दशाओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर-
- आर्थिक विकास उद्यमिता के विकास पर निर्भर है और उद्यमिता एक सामाजिक- मनोवैज्ञानिक तथ्य है।
- बाजार एवं उपभोग के प्रतिमान सामाजिक रूप से निर्धारित होते हैं।
- बहुत-सी समाजशास्त्रीय दशाएँ विकास को परिभाषित करती हैं। लैंगिक समानता, महिला शिक्षा एवं लाभकर आर्थिक क्रियाओं में उनकी सहभागिता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, साक्षरता में वृद्धि, लोकतांत्रिक प्रगति, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, जन्म एवं मृत्यु दर में कमी यादि, कुछ ऐसे समाजशास्त्रीय तथ्य हैं, जो सम्मिलित रूप से विकास के आयामों का निर्धारण करते हैं।
- विकास का समाजशास्त्र न सिर्फ किसी देश के औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास से सम्बन्ध रखता है बल्कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप उभरते सम्बन्धों की भी जांच-पड़ताल करता है। अतः अल्पविकास एवं निर्भरता के सिद्धान्त, आज विकास के समाजशास्त्रत के ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि अमीर एवं गरीब देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। गरीब देश विकसित देशों के शोषण के कारण विकास की दौड़ में पिछड़े रहे हैं और उनकी पर निर्भरता बढ़ रही है।
- परम्परागत समाजों के मूल्य, विकास में सहायक नहीं होते। अनुरूपता, कट्टरता, हठधर्मिता और अतार्किकता विकास को प्रात्साहित नहीं करते विकास की सहज गति के लिए आधुनिकीकरण एक आधारभूत पूर्व आवश्यकता है। यही कारण है कि आधुनिकीकरण एवं विकास के अधिकांश लक्षण एक समान है।
- अलग-अलग देशों एवं एक ही देश के अलग-अलग भागों में मित्रता पाई जाती है। यह उनकी विशिष्ट अवसंरचनात्मक दशाओं एवं उनके बीच मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक क्षमताओं में भिन्नता के कारण होती है।
विकास के समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को शास्त्रीय अर्थशास्त्र और पिछली सदी के दूसरे अर्द्रांश के शुरुआती वर्षों में उभरे विकास के अर्थशास्त्र के बीच अन्तर स्थापित करके ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। शास्त्रीय या परम्परागत अर्थशास्त्र विशुद्ध रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन था। इसके अन्तर्गत राजनीति और अर्थशास्त्र के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता था तथा एकाधिकार एवं प्रभुत्व के आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया जाता था। संसाधनों और बाजारों का प्रबन्धन तथा उनका सर्वोत्तम उपयोग एवं निरन्तर वृद्धि उनके अध्ययन का सार तत्व रहा है।
विकास के अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत है। एम.पी. टोडारो के अनुसार, विकास के अर्थशास्त्र को उपलब्ध दुर्लभ उत्पादक संसाधनों के प्रभावी आवंटन तथा समय के साथ उनकी सतत् वृद्धि के साथ ही साथ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की आर्थिक, सामजिक और संस्थात्मक प्रणाली पर भी ध्यान देना चाहिए। यह अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीबी, कुपोषण और असाक्षरता से ग्रस्त लोगों के जीवन स्तर में तीव्र (कम से कम ऐतिहासिक मानकों के आधार पर) और व्यापक सुधारों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार विकास का अर्थशास्त्र, संरचनात्मक एवं संस्थात्मक रूपान्तरणों तथा मानव विकास से सम्बन्धित है। विकास के समाजशास्त्र एवं विकास के अर्थशास्त्र में काफी समानता है। दोनों में अन्तर मात्र इतना है कि जहां पहला विकास में योगदान करने वाले समाजशास्त्रीय नियमों एवं क्षेत्रों तथा विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों का पता लगा है, वहीं दूसरा किसी समाज में विकास को निर्धारित करने वाली अनिवार्य सांस्कृतिक और संस्थात्मक दशाओं की खोज से सम्बद्ध है।
टोडारो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह मानव जीवन तथा समाज व्यवस्था से सम्बन्धित है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मूलभूत भौतिक (भोजन, वस्त्र, आवास) तथा अभौतिक आवश्यकताओं (शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्मिक संतुष्टि) की पूर्ति के लिए अपनी क्रियाओं को संगठित करता है। अर्थशास्त्र न तो पूर्ण वैज्ञानिक होने का और न ही अपनी सार्वभौमिक सत्यता का दावा कर सकता है। अतः अर्थशास्त्र अपने अनुसंधानों और विश्लेषणों को उनके संस्थात्मक, सामाजिक और राजनीतिक प्रसंगों से अलग नहीं कर सकता है, खासतौर से तब जब भूख गरीबी और खराब स्वास्थ्य की मानवीय विडम्बनाओं से जुड़ा विषय हो जिससे विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या जूझ रही है। टोडरों ने इस बात पर भी बल दिया है कि नैतिक या आदर्श मूल्यों के परिक्षेत्र की पहचान आवश्यक है ताकि यह तय हो सके कि सामान्य रूप से अर्थशास्त्र विषय के लिए और विशेष रूप में विकास के अर्थशास्त्र के लिए कौन से केन्द्रीय तत्व वांछनीय हैं और कौन से अवांछनीय। आर्थिक और सामाजिक समानता, गरीबी निवारण, सभी के लिए शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संस्थाओं का आधुनिकीकरण, राजनीतिक और आर्थिक सहभागिता, स्वावलम्बन और आत्म संतुष्टि जैसी अवधारणाएँ या लक्ष्य क्या अच्छा और वांछनीय है और क्या नहीं- जैसे व्यक्तिनिष्ठ मूल्य निर्णयों से प्राप्त होते हैं।
अतः विकास का समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो आर्थिक विकास का अध्ययन, सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से करता है। यह आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों तथा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संस्थात्मक क्षेत्रों के मध्य सम्बन्ध तलाशने का प्रयास करता है। यह विषय यह जानने का प्रयास करता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संस्थात्मक कारक किस सीमा तक विकास में सहायक या बाधक हैं। इस निषय का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के गैर-आर्थिक कारकों की खोज करना है।
समाजशास्त्र / Sociology – महत्वपूर्ण लिंक
- धर्म का अर्थ एवं परिभाषा | धर्म के गुण अथवा महत्व | धर्म की प्रमुख विशेषतायें
- संस्कृतिकरण का अर्थ एवं परिभाषा | संस्कृतिकरण की विशेषतायें | संस्कृतिकरण के कारक | संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- वैश्वीकरण का अर्थ एव परिभाषा | भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव | भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण से होने वाले लाभ-हानि
- संस्कृति का अर्थ | संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ | संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं
- संस्कृति का मानव जीवन में महत्व | संस्कृति का महत्व | भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में भेद
- समाज का अर्थ | संस्कृति का अर्थ | समाजीकरण का अर्थ | समाज, संस्कृति और समाजीकरण में सम्बन्ध
- स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण | हिन्दू तथा मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति की तुलनात्मक विश्लेषण
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]