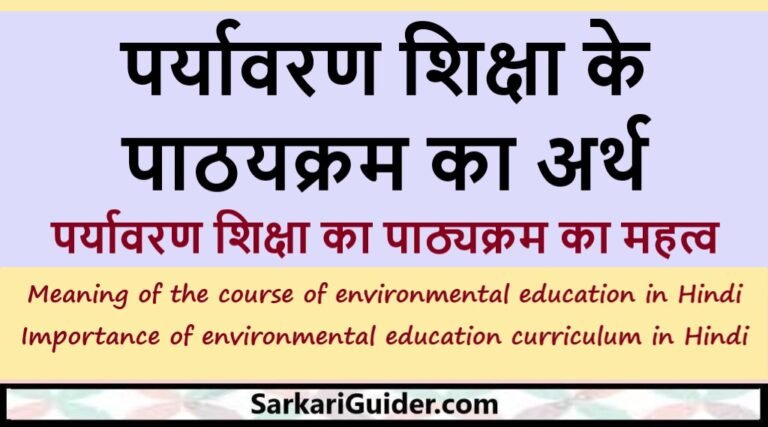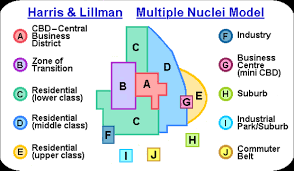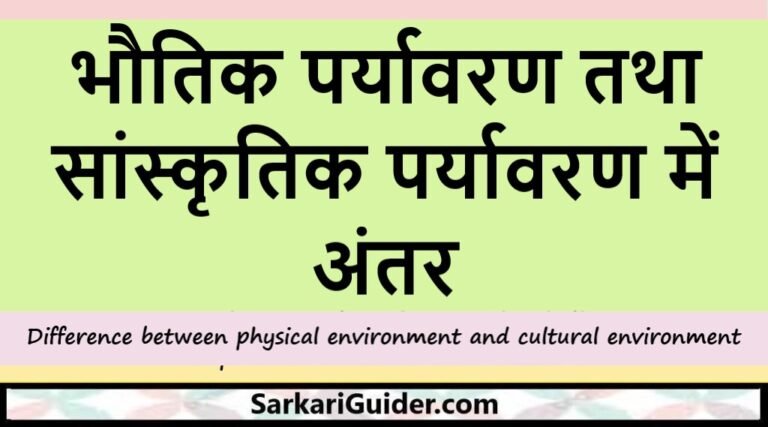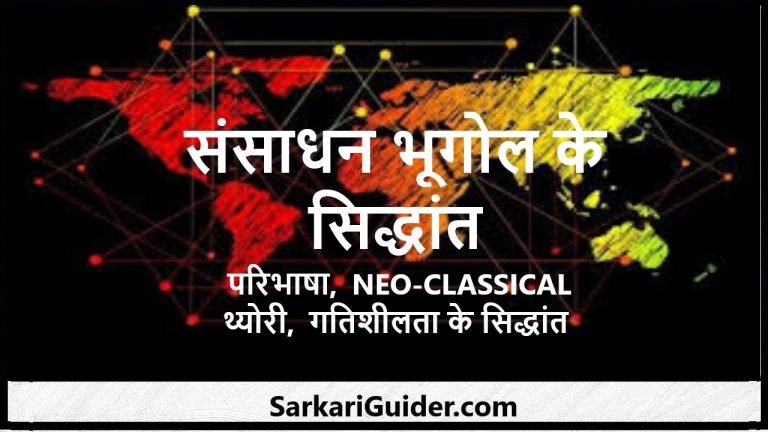पर्यावरण शिक्षा हेतु जन संचार एवं तकनीकी एवं उपयोग | Mass communication and technology and use for environmental education in Hindi

पर्यावरण शिक्षा हेतु जन संचार एवं तकनीकी एवं उपयोग | Mass communication and technology and use for environmental education in Hindi
पर्यावरण शिक्षा हेतु जन संचार एवं तकनीकी एवं उपयोग
पर्यावरणीय संकट ( समस्या ) को कम करने के हेतु जन-संचार माध्यमों एवं शिक्षा की भूमिका
(Role of mass Communication Media and Education for reducing the Environmental Crisis)-
जनसाधारण एवं शिक्षा जगत से सम्बन्धित व्यक्तियों को पर्यावरणीय संकट को समझने तथा उसे कम करने हेतु निम्नलिखित साधनों को प्रयोग में लाना पड़ेगा। यह कार्य शिक्षा विभाग एवं पर्यावरणीय शिक्षा (Environmental Shell) द्वारा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये जन संचार के माध्यम निम्नलिखित रूप में उपयोगी हैं-
-
इकोलाजी क्लब (Ecology Club)-
इस क्लब के अन्दर पारिस्थितिकी से सम्बन्धित चार्ट्स, मॉडल्स, आशुरचित उपकरण, प्रदर्शन की अन्य सामग्री, साहित्य, फिल्म स्ट्रिप्स, समाचार-पत्र, पत्र/पत्रिकाएँ, पूरक पुस्तकें आदि होती हैं।
यह क्लब पर्यावरण शिक्षा से जुड़े शिक्षक द्वारा चलाया जाता है। वह पर्यावरण तथा पर्यावरणीय शिक्षा से सम्बन्धित चार्ट्स, मॉडल्स छात्रों को दिखाते हैं। पर्यावरण विभाग तथा शिक्षा विभाग से सम्बद्ध पर्यावरण की प्रतियोगिताएँ भी शाला स्तर पर आयोजित करवाते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ भी पर्यावरण के सम्बन्ध में वार्ता संगोष्ठी था प्रतियोगिताएँ करती हैं। पोस्टर्स तथा निबन्ध भी लिखवाये जाते हैं।
उपयोगिता (Advantage) –
(1) पर्यावरण से सम्बन्धित साहित्य की जानकारी होती है।
(2) पर्यावरण के संरक्षण की जानकारी तथा प्रदूषण के कारणों की जानकारी होती है।
(3) पर्यावरण की उपयोगिता तथा अच्छे स्वास्थ्य हेतु उसका प्रयोग करना सीखते हैं।
(4) स्पर्धा भावना बढ़ती है। पर्यावरण की वस्तुओं के बारे में नयी जानकारी मिलती है, इससे प्रकृति का रहस्य दूर होता है।
(5) विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में आस्थावान होते हैं।
-
इकोलोजी प्रयोगशाला (Ecology Lab)
पारिस्थितिकी प्रयोगशाला पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख स्रोत है। यह पर्यावरण से सम्बन्धित वस्तुओं का स्थल होता है। पर्यावरण के चार्ट्स, पोस्टर्स तथा अन्य प्रदर्शन सामग्री होती है। इस सामग्री द्वारा पर्यावरण प्रदूषण, उसके संरक्षण, स्वच्छता, पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी मिलती है।
प्रयोगशाला में विभिन्न पौधों (वनस्पतियों), जीव जन्तुओं, मिट्टी, चट्टान, विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि को कटाव से बचाने कर्क उपाय, खाद्य श्रृंखला, पाषण आहार व्यवस्था, सन्तुलित आहार, पर्यावरणीय सन्तुलन (मानव, पशु तथा पक्षी) आदि का सकलन होता है। पत्तियों का संकलन प्लास्टिक की थैलियों में किया जा सकता है। इन्हें कार्ड-बोर्ड शीट पर फिक्स किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में ‘नवाचार’ को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि पर्यावरण सम्बन्धित सामग्री तथा उपकरण आदि निर्मित किये जा सकें।
प्रयोगशाला में प्रकाशित साहित्य, रिपोर्ट् स सन्दर्भ साहित्य चार्ट्स होते हैं। छात्रों के सहयोग से पानी तथा जमीन में रहने वाले जीव-जन्तु, पौधे, पत्तियाँ, पुष्प आदि जलाशय तथा विज्ञान वाटिका से संकलित कर वहाँ रखे जा सकते हैं।
फिल्म स्ट्रिप्स तथा फिल्म का भी यहाँ प्रबन्ध किया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकरण के बारे में क्रमबद्ध जानकारी मिल सके। इस प्रयोगशाला को बनाने में पर्यावरणीय शिक्षा के शिक्षक तथा सामान्य विज्ञान के शिक्षक मिलकर कार्य करते हैं। यदि विद्यालय में हरवेरियम, टरटेरियम, वाइबेरियम, एक्वेरियम तथा विज्ञान वाटिका हो तो बहुत-सी जानकारी छात्र वहीं से ग्रहण कर सकेंगे।
उपयोगिता (Advantage)-
पारिस्थितिकी प्रयोगशाला के निम्नलिखित लाभ हैं-
(1) यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, ताकि सही दिशा में चिन्तन किया जा सके।
(2) छात्र पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, वह प्रकृति एक रहस्य को समझते हैं।
(3) पर्यावरण प्रदूषण (वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि तथा तापीय प्रदूषण) के कारण तथा निराकरण के बारे में जानकारी होती है।
(4) पोषण, स्वच्छता तथा सन्तुलित आहार के बारे में जानकारी होती है।
(5) पर्यावरण सन्तुलन तथा जीव-जन्तु तथा मानव का परस्पर एक-दूसरे से समायोजन होना भी प्रयोगशाला के पोस्टरों द्वारा देखा जा सकता है।
(6) पर्यावरणीय असन्तुलन से क्या-क्या खतरे हो सकते हैं, इनकी भी जानकारी मिलती है।
-
पुस्तकालय तथा प्रकाशन (Library and Publication)-
पर्यावरणीय शिक्षा से सम्बन्धित पुस्तकालय यदि विद्यालय में हो तो अच्छा है अन्यथा प्रकाशित साहित्य पारिस्थितिकी क्लब या प्रयोगशाला में उपलब्ध होना चाहिये।
प्रिन्टेड शब्दों को प्रकाशित साहित्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फोल्डर्स, पोस्टर्स, चार्टस, रिपोर्टस सन्दर्भ साहित्य इस सम्बन्ध में विशद अध्ययन कराते हैं तथा सही निष्कर्ष निकालने को प्रेरित करते हैं; जैसे- यदि पुस्तकालय में पक्षियों से सम्बन्धित कोई पुस्तक है, तो वह पक्षियों के वर्गकरण करने में उपयोगी हो सकती है। इसस विभिन्न पक्षियों के घोसलों के बारे में जानकारी मिल सकती है।
श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग भी सुविधानुरूप पर्यावरणीय शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। टी.वी., वी.सी.आर., फिल्म स्ट्रिप, रेडियो, टेपरिकार्डर आदि के प्रयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित सोपानों को ध्यान में रखना चाहिये-
(i) प्रसारण पूर्व की क्रियाएँ (Pre-broadcast or Pre Telecast Activities)
इसके अन्तर्गत प्रस्तुत किये जा रहे कार्यक्रम की पूर्व जानकारी, उत्प्रेरण तथा ध्यातव्य निर्देश आदि का नियोजन किया जाना चाहिए।
(ii) प्रसारण या प्रस्तुतीकरण समय की क्रियाएँ (Presentation Activities)
विद्यार्थियों द्वारा ध्यान से प्रस्तुत कार्यक्रम सुनने, देखने एवं उसे नोट करने सम्बन्धी क्रियाएँ।
(iii) प्रसारण पश्चात् क्रियाएँ (Past-broadcast or Telecast Activitie)-
कार्यक्रम सम्पन्न होने की बाद की क्रियाएँ जिससे पाठ्यवस्तु का सुदृढ़ीकरण एवं पृष्ठ-पोषण किया जा सके।
एन.सी.ई. आर.टी.एवं एस.सी.ई.आर.टी. ने यूनिसेफ की प्रायोजनाओं के अन्तर्गत बाल-पोषण एवं स्वास्थ्य तथा स्वच्छता नामक प्रोजेक्ट्स तैयार किये हैं। इनमें पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने, सन्तुलित आहार की विद्यालय में व्यवस्था करने सम्बन्धी बातें सम्मिलित हैं। प्रत्येक विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की किट या चार्ट्स भेज जाते हैं और इसके साथ पर्यावरण से सम्बन्धित साहित्य भी भेजा जाता है।
जीव-विज्ञान अथवा सामान्य विज्ञान के जो भी अध्यापक होते हैं, उन्हें राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान (परिषद्) प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जिला स्तर पर भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रधानाचार्य स्तर का एक पद पर्यावरण शिक्षा को विस्तार करने के लिये (हर विद्यालय में) सृजित किया गया है।
पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग माना गया है तथा प्रत्येक विद्यालय में इससे सम्बन्धित कई कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं। औपचारिक, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा की अलग पुस्तक हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- शिक्षा के द्वारा पर्यावरण जन जागरूकता की विशेषताएँ | Characteristics of environmental public awareness through education in Hindi
- पर्यावरणीय संकट को कम करने हेतु जन-संचार माध्यमों की भूमिका
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर्यावरण जागरूकता के प्रयास | National and international level environmental awareness efforts
- पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय | पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न अभिकारणों का योगदान एवं भूमिका
- पर्यावरण शिक्षा के पाठयक्रम का अर्थ | पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम का महत्व
- औपचारिक पर्यावरण शैक्षिक पाठ्यक्रम | औपचारिक पर्यावरण शैक्षिक कार्यक्रम
- पर्यावरण जागरूकता हेतु विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजन
- पर्यावरण संरक्षण के लिये पाठ्यू-सहगामी क्रियायें | Text-related activities for environmental protection in Hindi
- पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियाँ | औपचारिक विधियाँ तथा अनौपचारिक विधियाँ
- भ्रमण विधि | भ्रमण-विधि से लाभ | भ्रमण या पर्यटन की योजना
- समस्या समाधान विधि | समस्या-समाधान विधि के पद | समस्या-समाधान विधि के गुण तथा दोष
- प्रयोजना विधि | प्रायोजना विधि के सिद्धान्त | योजना विधि के गुण तथा दोष
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]