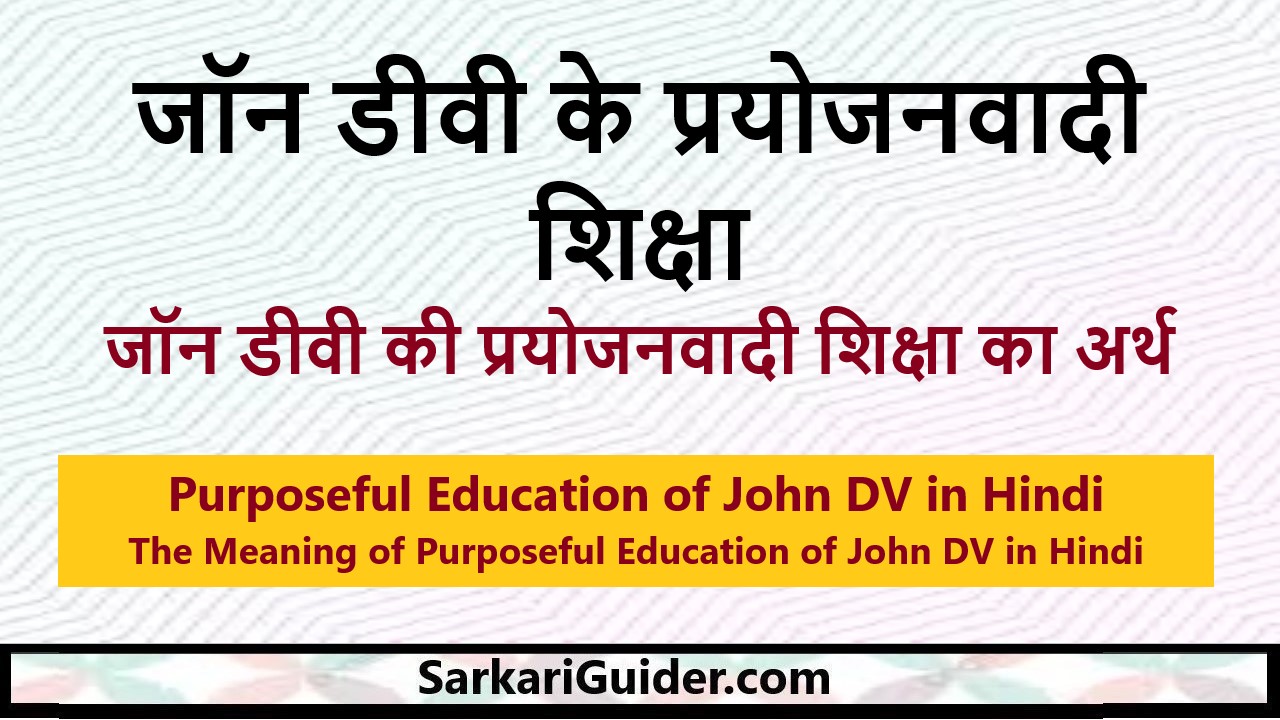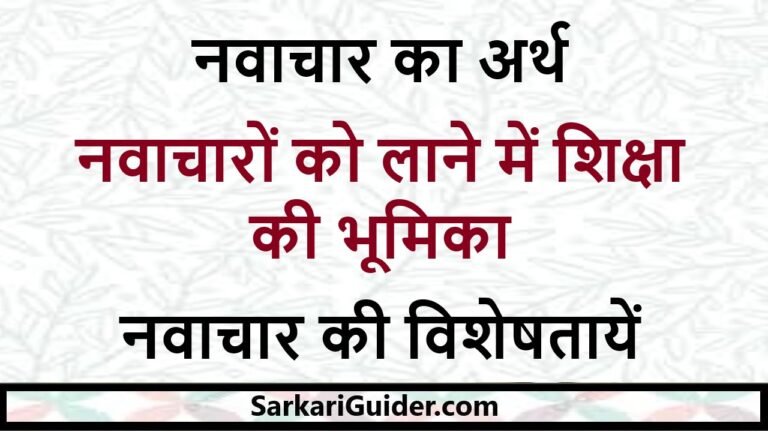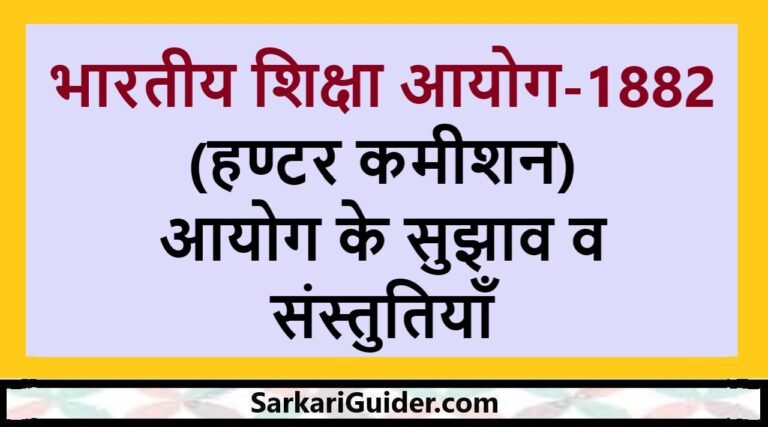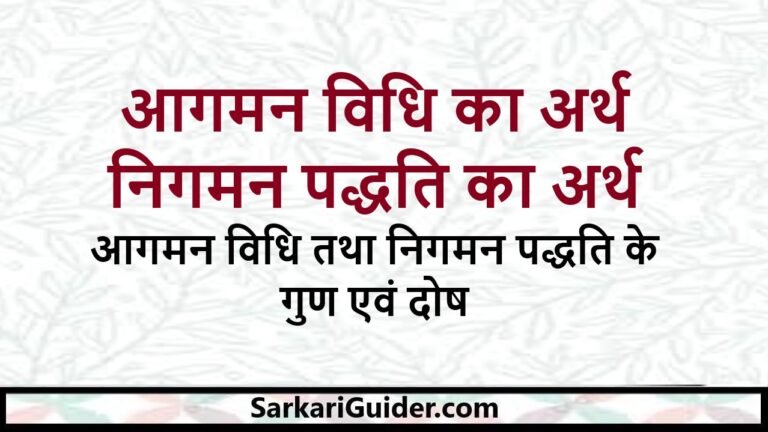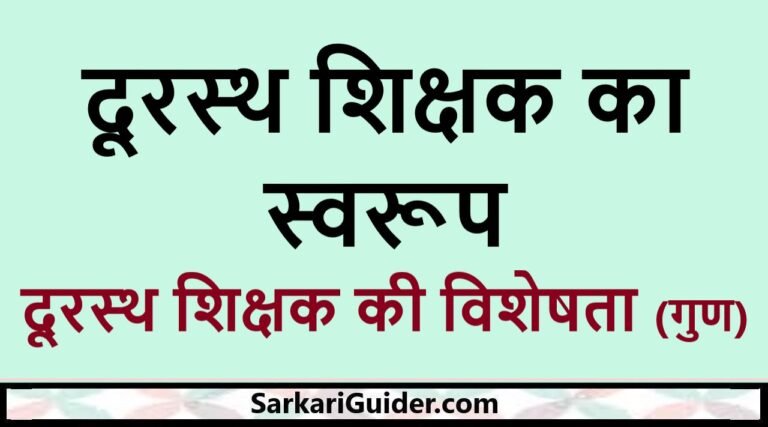जॉन डीवी के प्रयोजनवादी शिक्षा | जॉन डीवी की प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ

जॉन डीवी के प्रयोजनवादी शिक्षा | जॉन डीवी की प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ
जॉन डीवी के प्रयोजनवादी शिक्षा का सविस्तार वर्णन कीजिये।
प्रयोजनवादी अंग्रेजी के प्रेग्मेटिज्म (Pragmatism) शब्द का हिन्दी अनुवाद है। इस शब्द के हिन्दी अनुवाद के विषय में भी बड़ा झमेला है। हिन्दी की पुस्तकों में प्रैग्मेटिज्म के लिए प्रयोगवाद, प्रयोजनेवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद, फलवाद आदि शब्द देखने में आते हैं। प्रैग्मेटिज्म शब्द के लिए हिन्दी के विद्वान किसी एक शब्द पर सहमत नहीं हैं। इस असहमति का कारण हिन्दी भाषा की अनिश्चितता अथवा अक्षमता नहीं है वरन् उस वाद की अनिश्चितता है। यह बात आगे की चर्चा से स्वतः स्पष्ट हो जायगी। मैंने प्रयोजनवाद शब्द को चुना है। इस चुनाव का कारण मेरी अपनी रुचि है।
प्रयोजनवाद के जन्मदाता पीयर्स महोदय हैं। पीयर्स ने सर्वप्रथम प्रैग्मेटिज्म शब्द का प्रयोग किया था किन्तु यह प्रयोग सीमित अर्थ में ही था। प्रेग्मेटिज्म शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटीकोस (Pragmtikos) से निकला है जिसका अर्थ है ‘क्रिया’, ‘व्यवहार’, ‘प्रयोग’ आदि। पीयर्स प्रयोजनवाद को दर्शन की संज्ञा नहीं देता था। प्रयोजनवाद को दर्शन का रूप देने वाले थे विलियम जैम्स। मूलतः एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते विलियम जेम्स ने ‘संकल्प शक्ति को ही मन का आधारभूत तत्व माना। उन्होंने आदर्शवाद का खण्डन करते हुए उसे काल्पनिक एवं अनुपयोगी बताया।
डाक्टर डीवी के हाथों में पड़कर प्रयोजनवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। डॉक्टर डीवी ने प्रयोजनवाद को एक क्रमबद्ध दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। आज प्रयोजनवाद का जो स्वरूप प्रचलित है वह बहुत कुछ डॉक्टर डीवी का ही सिद्धान्त है। डॉक्टर डीवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘जनतन्त्र और शिक्षा’ (Democracy and Education)में अपने शिक्षा सावन्थी विचार व्यक्त किए हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा के स्वरूप का विकास इसी पुस्तक से हुआ है। इस पुस्तक ने डॉक्टर डीवी को प्लेटो और रूसो जैसे दार्शनिकों की श्रेणी में ला दिया है।
प्रयोजनवादी दार्शनिक शिक्षा को मानव की जन्मजात आवश्यकता मानता है। शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकास के लिए निबेलता एवं असहायता का भाव आवश्यक है। स्वभाव से ही मानव-शिशु असहाय होता है। यह स्थिति पशुओं एवं पक्षियों में हम नहीं देखते हैं। गाय का बछड़ा जन्म लेने के कुछ क्षण पश्चात् चलने और दौड़ने लगता है किन्तु मानव-शिशु को इन क्रियाओं को सम्पन्न करने में महीनों लग जाते हैं। प्रकृति ने मानव शिशु को बहुत ही निस्सहाय बनाया है किन्तु यह परवशता मनुष्य के लिए अभिशाप न होकर वरदान है। वस्तुस्थिति यह है कि जो प्राणी जितना ही निस्सहाय उत्पन्न होता है उसमें उतनी ही अधिक शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता होती है।
प्रयोजनवादी दार्शनिक शिक्षा में विभिन्न प्रयोजनों पर बल देते हुए भी एक दो निश्चित उद्देश्यों की ओर ध्यान देता है। वह कहता है शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में सामाजिक दक्षता का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा समाज की वस्तु है। समाज के अस्तित्व के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। समाज शिक्षा के द्वारा ही अपनी विशेषताआं परम्पराओं, मान्यताओं, प्रणालियों आदि को सुरक्षित रखता है। इसलिए शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज के ऊपर है। समाज शिक्षा का संगठन करता है, शिक्षा-सृंस्थाओं की स्थापना करता है, पाठ्यक्रम के सिद्धान्तो का निरूपण करता है और सम्पूर्ण शिक्षा के आर्थिक भार को वहन करने का साहस करता है। समाज अपने इन कार्यों का प्रतिफल भी चाहता है। समाज की यह आकांक्षा होती है कि उसके भावी सदस्य वर्तमान सदस्यों से अधिक सक्षम बनें और समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएं। इसीलिए प्रत्येक छात्र में सामाजिक दक्षता का आना आवश्यक है। सामाजिक दक्षता का तात्पर्य वाक्पटुता नहीं है। सामाजिक दक्षता से यह भी तात्पर्य नहीं है कि समाज के उच्च वर्ग के व्यक्तियों की वेशभूषा आदि का अनुकरण करके छात्र टीमटाम में दक्षता प्राप्त कर लें। इससे यह अभिप्राय है कि बालकों में सामाजिक भावना का उदय हो और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की उनमें क्षमता उत्पन्न हो। किस समाज की क्या आवश्यकता है, इसका निर्णय अनुभव करेगा। प्रयोजनवादी अनुभव पर बड़ा बल देते हैं। उनके लिए अनुभव यथार्थ है। सत्य कोई निश्चित वस्तु नहीं है, यथार्थता पूर्वकाल से कहीं विद्यमान नहीं है। सत्य है नहीं, सत्य हो जाता है अर्थात् सत्य समय-समय पर बनाया जाता है। अनुभव जिसे सत्य माने वही सत्य है। देश और काल के अनुसार अनुभव बदलते रहते हैं, अंतः सत्यं भी बदलता रहता है। किसी एक सत्य की खोज में परिश्रम करने की अपेक्षा अनुभव द्वारा सत्य का निर्माण कर लेना अधिक श्रेयस्कर है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जायेगा कि किसी एक सत्य को शिक्षा का उद्देश्य रखने की अपेक्षा समय-समय पर जो सत्य समझ पड़े उसे ही शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाये।
प्रयोग के द्वारा उपयोगितावाद के आधार पर शिक्षा में उद्देश्य निर्धारित कर लेने के पश्चात् इन उद्देश्यों की प्राप्ति का भी प्रयत्न करना चाहिए। किस विधि से ये उद्देश्य प्राप्त होंगे? सामाजिक दक्षता ही यदि अभीष्ट है तो किस विधि द्वारा इसकी सिद्धि होगी? प्रयोजनवादी शिक्षण-विधि के लिए कुछ निश्चित सिद्धान्त देता है।
उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं-
(1) बालक को अधिकतम स्वतन्त्रता प्रदान की जाये,
(2) बालक की रुचि का ध्यान रखा जाये,
(3) बालक को कक्षा-कार्य में निष्क्रिय न बनाकर सक्रिय बनाया जाये,
(4) वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखा जाये,
(5) बालक में सामाजिकता की भावना को उद्बुद्ध किया जाये और
(6) विद्यालय में शब्दों से अधिक कार्यों पर ध्यान दिया जाये।
इन मूल सिद्धान्तों के आधार पर कुछ प्रयोजनवादियों ने शिक्षा की विशिष्ट पद्धतियों को जन्म दिया। किलपैट्रिक महोदय डॉक्टर डीवी के मेधावी शिष्य हैं। वे ‘प्रोजेक्ट पद्धति’ के जनक हैं। प्रोजेक्ट पद्धति आज एक बहुत अच्छी शिक्षण-पद्धति मानी जाती है। प्रोजेक्ट पद्धति प्रयोजनवादी दर्शन पर आधारित है। अमेरिका में ‘प्रोग्रेसिव एजूकेशन’ का आन्दोलन भी बहुत सक्रिय है। प्रोग्रेसिव एजूकेशन प्रयोजनवादी सिद्धान्तों पर आधारित है। ‘एक्टीविटी स्कूल’ का विचार भी प्रयोजनवाद की देन है। इस प्रकार आधुनिक विशिष्ट पद्धतियों पर प्रयोजनवाद की छाप स्पष्ट है।
जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, प्रयोजनवादी वर्तमान अनुभव को अतीत के अनुभवों एवं भविष्यत् की कल्पनाओं से श्रेष्ठ समझता है। अतीत के वे ही अनुभव आज के पाठ्यक्रम में आ सकते हैं जिनसे वर्तमान को समझने में सहायता मिले। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम की रचना के चार आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। ये चार सिद्धान्त अग्रलिखित हैं-
(1 ) उपयोगिता का सिद्धान्त-शैक्षिक उद्देश्यों पर विचार करते समय हम इस सिद्धान्त पर विचार कर चुके हैं। बालक को केवल वही ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना चाहिए जो उसके सामाजिक जीवन में काम आ सके। इस सिद्धान्त के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में प्रायः सम्मिलित कर लिया जाता है। स्थानीय इतिहास व भूगोल, सामान्य अंकगणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन (Social Studies) आदि कुछ विषयों को इस सिद्धान्त से बड़ा बल मिलता है। किन्तु सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि सामान्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में सर्वोपरि स्थान मिल जाता है।
(2 ) बालक की प्राकृतिक रुचि-यह पाठ्यक्रम निर्माण का दूसरा सिद्धान्त है। बालक की प्रमुख अभिरुचियों को जॉन डीवी ने चार वर्गों में विभक्त किया है- (1) वार्तालाप तथा व्यवहार में रुचि, (2) अन्वेषण में रुचि, (3) रचनात्मक रुचि तथा (4) कलात्मक अभिरुचि। इस सिद्धान्त के आधार पर लिखना, पढ़ना, गिनना, हस्तकला आदि विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान मिल जाता है।
( 3 ) बालक की क्रियाओं एंवं अनुभवों के आधार का सिद्धान्त-प्रयोजनवादी शिक्षा को एक क्रियाशील प्रक्रिया मानते हैं। अतः वे पाठ्यक्रम के केवल रटने पर बल नहीं देते। रटाना एवं कुछ सीमित पुस्तकों का अध्ययन कराना व्यर्थ है यदि बालक की प्रकृतिदत्त क्रियाशीलता का शैक्षिक प्रक्रिया में सदुपयोग न किया गया। पाठ्यक्रम का संगठन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक में क्रियाशीलता का विकास हो सके और छात्र पग-पग पर अपने अनुभवों द्वारा ही सीखता चले। बालक जिस समुदाय में रहता है उसकी झलक पाठ्यक्रम में अवश्य मिलनी चाहिए। स्थानीय इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक अध्ययन पर इस दृष्टि से ध्यान देना चाहिए।
(4) सानुबंधिता का सिद्धान्त-पाठ्यक्रम निर्धारण का चतुर्थ सिद्धान्त सानुबन्धिता का है। इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभाजित करके उन विषयों का पृथक-पृथक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। किसी विषय की शिक्षा संकुचित सीमा के अन्तर्गत नहीं देनी चाहिए। पाठ्यक्रम के सभी विषयों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करके शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।
महत्वपूर्ण लिंक
- गांधी जी का शिक्षा दर्शन – आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का समन्वय है।
- शिक्षा में महात्मा गाँधी का योगदान या शैक्षिक विचार | गाँधीजी के शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं?
- विवेकानन्द का शिक्षा दर्शन शिक्षाशास्त्री के रूप में | विवकानन्द के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां
- मानव निर्माण शिक्षा में स्वामी विवेकानन्द का योगदान | मानव निर्माण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य
- आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य | आदर्शवाद में शिक्षा के सम्प्रत्यय
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]