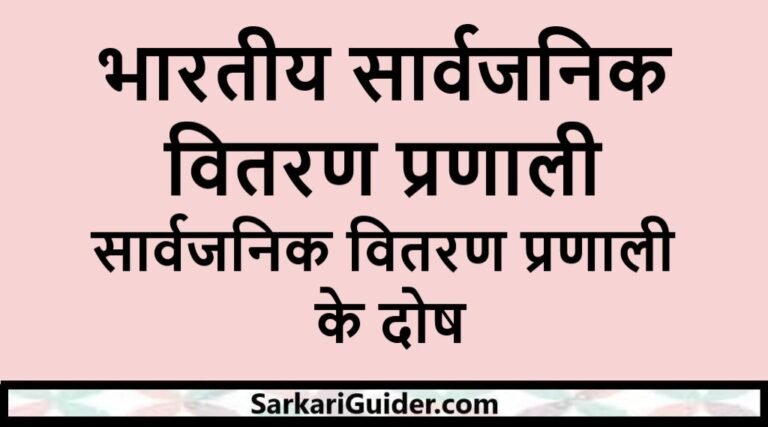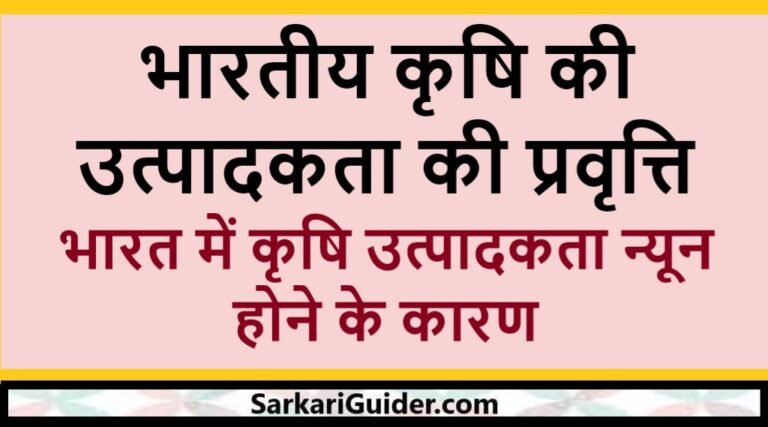लगान सिद्धान्त | प्रकृतिवादियों तथा रिकार्डो के आर्थिक विचार
लगान सिद्धान्त | प्रकृतिवादियों तथा रिकार्डो के आर्थिक विचार
लगान सिद्धान्त
(Theory of Rent)
अर्थशास्त्र में लगान का विचार प्रकृतिवादियों की देन है। प्रकृतिवादियों ने लगान को एक ऐसी बचत माना था जो कि कृषि उत्पादन में प्रकृति की दशा से प्राप्त होती है। एडम स्मिथ तथा माल्थस ने भी प्रकृतिवादियों के इसी मत का समर्थन किया।
रिकार्डो ने लगान को पारिभाषित करते हुए लिखा है, “लगान भूमि की उपज का वह भाग है, जो भू-स्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिये दिया जाता है।” यहाँ रिकार्डो का भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों से तात्पर्य भूमि की उन शक्तियों से है, जिनके कारण भूमि के विभिन्न टुकड़ों के उपजाऊपन में भिन्नता होती है। इस प्रकार भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि की विभिन्न श्रेणियाँ बन जाती हैं। भूमियों के उपजाऊपन की विभिन्नता ही आर्थिक लगान का मुख्य कारण है। सभी टुकड़े समान रूप से एक जैसे उपजाऊ नहीं होते, कुछ कम उपजाऊ होते हैं तो कुछ अधिक उपजाऊ होते हैं। अधिक उपजाऊ टुकड़ों पर उत्पादन कम उपजाऊ टुकड़ों की तुलना में अधिक होता है। उपज का यही अन्तर आर्थिक लगान है।
प्रारम्भ में मानव ने भूमि के सबसे अधिक उपजाऊ टुकड़े पर खेती करनी प्रारम्भ की। जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न को बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए दूसरी श्रेणी की भूमि पर खेती की गयी। और अधिक मांग बढ़ने पर तृतीय श्रेणी की घटिया भूमि पर भी खेतो की जाने लगी। माँग में पुनः वृद्धि होने पर चतुर्थ श्रेणी की निम्न स्तरीय भूमि पर खेती की जाने लगी। चारों श्रेणियों की भूमि के समान टुकड़ों पर बराबर-बराबर श्रम और पूँजी व्यय करने के बावजूद भी उत्पादन एक समान नहीं हुआ। प्रथम श्रेणी की भूमि पर सर्वाधिक, द्वितीय श्रेणी की भूमि पर उससे कम, तृतीय श्रेणी की भूमि पर उससे भी कम तथा चतुर्थ श्रेणी की भूमि पर सबसे कम उत्पादन हुआ। उत्पादन में अन्तर भूमि के उपजाऊपन का कारण था। इस प्रकार से लगान उच्चकोटि की तथा निम्नकोटि की भूमि की उपज के अन्तर के बराबर होता है। अत: लगान एक प्रकार की भेदात्मक बचत (differential surplus) है। रिकार्डो के अनुसार, “लगान अधि- सीमान्त भूमि की उपजों का अन्तर है।”
उदाहरण- रिकार्डो ने अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए निम्म उदाहरण से व्याख्या की। उसने माना कि एक द्वीप है। प्रारम्भ में जबकि वहाँ कोई नहीं रहता है भूमि निःशुल्क उपलब्ध होगी। बाद में कुछ लोग आकर वहां बस गये तो उन्होंने सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती करना प्रारम्भ किया। इस प्रथम श्रेणी की एक एकड़ भूमि की उपज 20 कुन्तल गेहूं हुई। कुछ समय कुछ और लोग वहाँ जाकर बस जाते है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न की मांग बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए द्वितीय श्रेणों को कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाने लगी। इस पर समान श्रम एवं पूजीगत लागत से प्रति एकड़ उत्पादन 15 कुन्तल ही हो पाया। जनसंख्या में और अधिक वृद्धि हो जाने पर तृतीय श्रेणी की भूमि पर खेती करने से प्रति एकड़ उत्पादन 10 कुन्तल रहा। खाद्यान्न की माँग में और अधिक वृद्धि हो जाने पर चतुर्थ श्रेणी की सबसे कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने पर प्रति एकड़ उपज केवल 5 कुन्तल रही। इस प्रकार इन चारों श्रेणियों की भूमि पर लगान का निर्धारण अग्रांकित प्रकार से होगा-
| भूमि की श्रेणी | प्रति एकड़ उत्पादन | सीमान्त भूमि पर उत्पादन | लगान |
| प्रथम श्रेणी | 20 | 5 | 20 -5 = 15 |
| द्वितीय श्रेणी | 15 | 5 | 15 – 5 = 10 |
| तृतीय श्रेणी | 10 | 5 | 10 – 5 = 5 |
| चतुर्थ श्रेणी | 5 | 5 | 5 – 5 = 0 |
इस तरह से अन्तिम श्रेणी की भूमि जो कि सीमान्त भूमि है पर कोई लगान नहीं होगा, तृतीय श्रेणी की भूमि पर लगान 5 कुन्तल, द्वितीय श्रेणी की भूमि पर लगान 10 कुन्तल तथा प्रथम श्रेणी की भूमि पर लगान 15 कुन्तल होगा। इसे साथ के चित्र से अधिक भली प्रकार समझा जा सकता है। चित्र से स्पष्ट है कि D सीमान्त भूमि है जिस पर कोई लगान नहीं है तथा C, B और A पर क्रमशः 5, 10 तथा 15 कुन्तल लगान है।
रिकार्डो इस बात को भली प्रकार समझते थे कि दीर्घकाल में भूमि के सभी टुकड़े मानवीय प्रयासों के परिणामस्वरूप समान रूप से उपजाऊ हो जायेंगे। उस समय लगान का निर्धारण किस प्रकार होगा, इस सम्बन्ध में रिकार्डो ने बताया कि जब भूमि की मात्रा को सीमित रखते हुए श्रम तथा पूँजी की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तब लगान का निर्धारण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय इकाइयों द्वारा उत्पादित मात्रा के आधार पर किया जाता है।
कृषि में घटती हुई उत्पादकता का नियम लागू होता है इसलिए श्रम और पूँजी की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई इकाइयों से समान उत्पादन नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भूखण्ड पर श्रम और पूँजी की एक इकाई से 20 कुन्तल उत्पादन किया जा रहा है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उस पर दो इकाई काम पर लगा दी जाती है तो इससे उत्पादन 40 कुन्तल नहीं होगा, अपितु कुछ कम होगा। माना यह 30 कुन्तल है, अर्थात् प्रति इकाई उत्पादन 15 कुन्तल हुआ। यदि एक और इकाई बढ़ाई जाती है तो प्रति इकाई उत्पादन गिरकर 10 कुन्तल हो गया। चौथी इकाई पर उत्पादन प्रति इकाई उत्पादन मात्र 5 कुन्तल हुआ है, जो इसकी उत्पादन लागत के बराबर है। इसलिए, इस अन्तिम और सीमान्त इकाई पर कोई आर्थिक लगान नहीं होगा और इसके पहले की इकाइयां क्रमश: 5, 10 तथा 15 कुन्तल लगान प्राप्त करती रहेंगी। (देखिए चित्र)
सिद्धान्त की मान्यताएँ-
रिकार्डो ने सिद्धान्त को प्रतिपादित करने से पूर्व इसकी कुछ मान्यताएँ निर्धारित की थीं, जो निम्नलिखित हैं-
(1) यह सिद्धान्त दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है।
(2) लगान सीमान्त भूमि के कारण उत्पन्न होता है।
(3) भूमि की पूर्ति सीमित होती है इसे किसी भी प्रकार बढ़ाया नहीं जा सकता है।
(4) लगान भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के कारण है।
(5) लगान केवल भूमि पर लगता है। उत्पादन के किसी अन्य साधन पर लगान का सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता।
(6) विभिन्न उपजाऊपन वाले भू-खण्डों को उनकी श्रेष्ठता के आधार पर जोता जाता है।
(7) सभी भू-खण्ड समान रूप में उपजाऊ नहीं होते।
(8) कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है।
सिद्धान्त की आलोचनाएँ-
रिकार्डो वह पहला अर्थशास्त्री था जिसने लगान सम्बन्धी अवधारणा को अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। परन्तु उसके सिद्धान्त में कुछ ऐसी मौलिक त्रुटियाँ रह गयीं, जिनका निराकरण वह नहीं कर सका और बाद में आगे चलकर इन्हीं बिन्दुओं पर रिकार्डों के लगान सिद्धान्त की बड़ी आलोचना हुई। वे कमियाँ निम्नलिखित हैं-
(1) यह कहना गलत है कि भूमि में कुछ मौलिक तथा अविनाशी तत्त्व होते हैं, जो उसके उपजाऊपन को प्रभावित करते हैं। आज की वैज्ञानिक खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि रासायनिक उर्वरकों, खाद आदि से भूमि की उर्वराशक्ति नष्ट हो सकती है।
(2) यह कहना भी गलत है कि सर्वप्रथम उस भू-खण्ड पर खेती की जाती है जो सर्वाधिक उपजाऊ होता है। प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति उस जगह खेती करना प्रारम्भ करता है, जो यातायात की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
(3) सीमान्त भूमि अथवा लगान रहित भूमि की कल्पना गलत है। आज वास्तविक जीवन में सरकार द्वारा सबसे निम्न कोटि की भूमि पर भी लगान लिया जाता है।
(4) यह मान्यता भी गलत है कि लगान केवल भूमि को ही प्राप्त है।
(5) पूर्व प्रतियोगित और दीर्घकाल की मान्यतायें अवास्तविक हैं।’
प्रकृतिवादियों तथा रिकार्डो के आर्थिक विचार
(Economic Views of Physiocrats and Ricardo)
यद्यपि रिकाडो प्रकृतिवादियों के इस मत से सहमत थे कि लगान एक प्रकार का बेशी भुगतान था परन्तु इस प्रश्न पर कि यह कैसे प्राप्त होता है, उनका प्रकृतिवादियों से मतभेद था। प्रकृतिवादियों के अनुसार लगान बेशी (अतिरिक्त) आय कृषि में प्रकृति द्वारा मनुष्य के साथ सहयोग में कार्य करने के कारण प्रकृति की उदारता के फलस्वरूप प्राप्त होती है। कृषि उत्पादन में अपने इस सहयोग के लिये प्रकृति मनुष्य से कोई पारितोषक प्राप्त नहीं करती है। परन्तु रिकार्डो के मतानुसार लगान मनुष्य के प्रति प्रकृति की कृपा अथवा उदारता का परिणाम न होकर उसकी कृपणता का परिणाम है। उनके अनुसार प्रकृति मनुष्य के साथ सौतेली माता के समान व्यवहार करती है। रिकार्डो के समय में अधिक लगान के कारण समाज में अधिक चिन्ता फैल गई थी। वे स्वयं व्यापारिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। इसलिये वे यह समझते थे कि किसान को भूस्वामी को आर्थिक लगान सीमित भूमि तथा उत्पादन में हासमान प्रतिफल नियम के लागू होने के कारण देना पड़ता है। यद्यपि प्रकृतिवादी इस बेशी मात्रा की वृद्धि को राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति में वृद्धि का निर्देशक समझते थे परन्तु रिकार्डो को इस लगान वृद्धि में मानव समाज के लिये निराशाजनक भविष्य दिखायी पड़ता था। यद्यपि लगान का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण भूस्वामियों के विरुद्ध किसी प्रकार के वर्ग संघर्ष तथा घृणा को नहीं उत्पन्न करता है परन्तु रिकार्डोवादी लगान इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भूस्वामी ऐसा समाज विरोधी वर्ग है जो अनर्जित आय पर जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार लगान की प्रवृत्ति, उसकी प्राप्ति के कारणों के बारे में प्रकृतिवादी तथा रिकार्डो के दृष्टिकोण में भौतिक अन्तर है।
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन | माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त का महत्त्व
- माल्थस का अल्प उपभोग | माल्थस का अत्युत्पाद्न सिद्धान्त | अत्युपादन सिद्धान्त की विशेषताएँ | माल्थस के अत्युत्पादन सिद्धान्त का मूल्यांकन
- रिकार्डो का मूल्य सिद्धान्त | रिकार्डो के वितरण के सिद्धान्त | रिकार्डो का विश्लेषणात्मक मूल्य सिद्धान्त
- मजदूरी सिद्धान्त | लाभ सिद्धांत | रिकाडों के मजदूरी तथा कर सम्बन्धी सिद्धांत की व्याख्या
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]