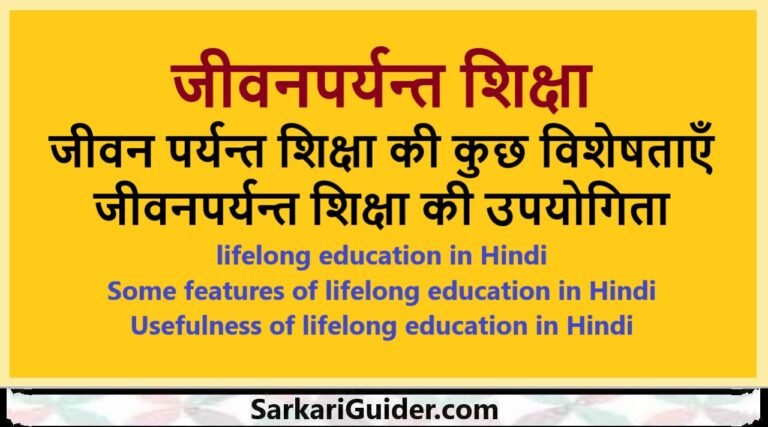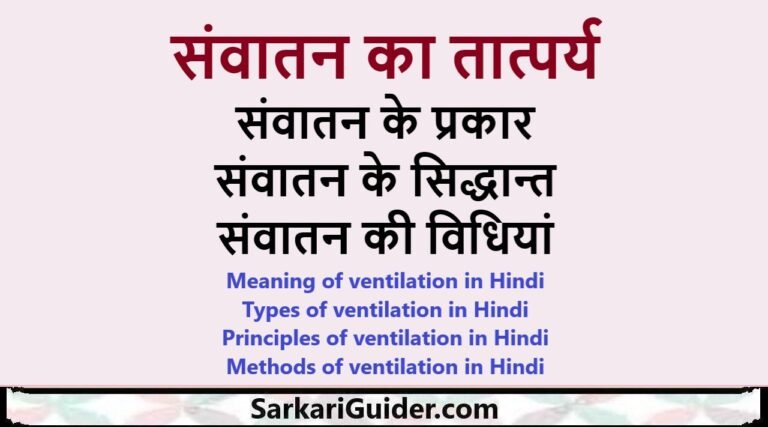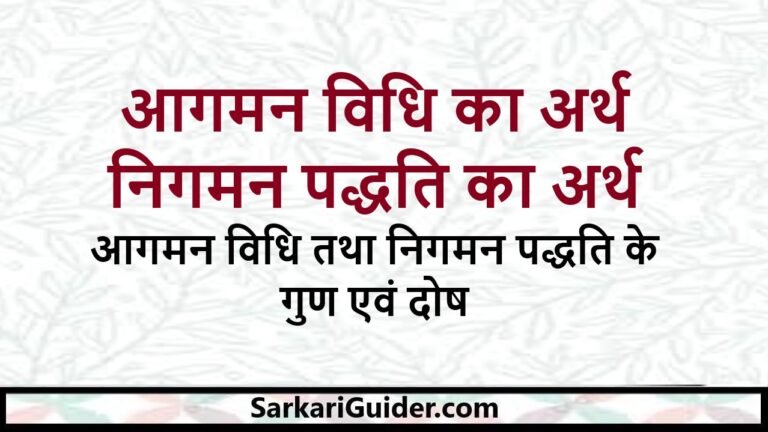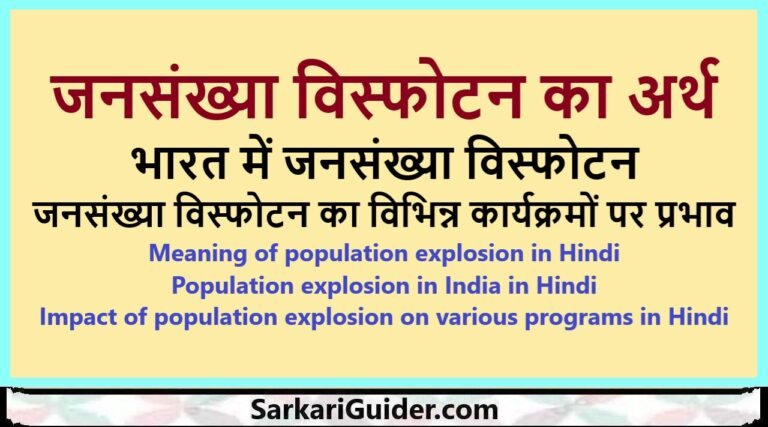रूसो के शैक्षिक विचार | रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ | रूसो के अनुसार शिक्षा के दो प्रकार | रूसो के स्त्री-शिक्षासम्बन्धी विचार
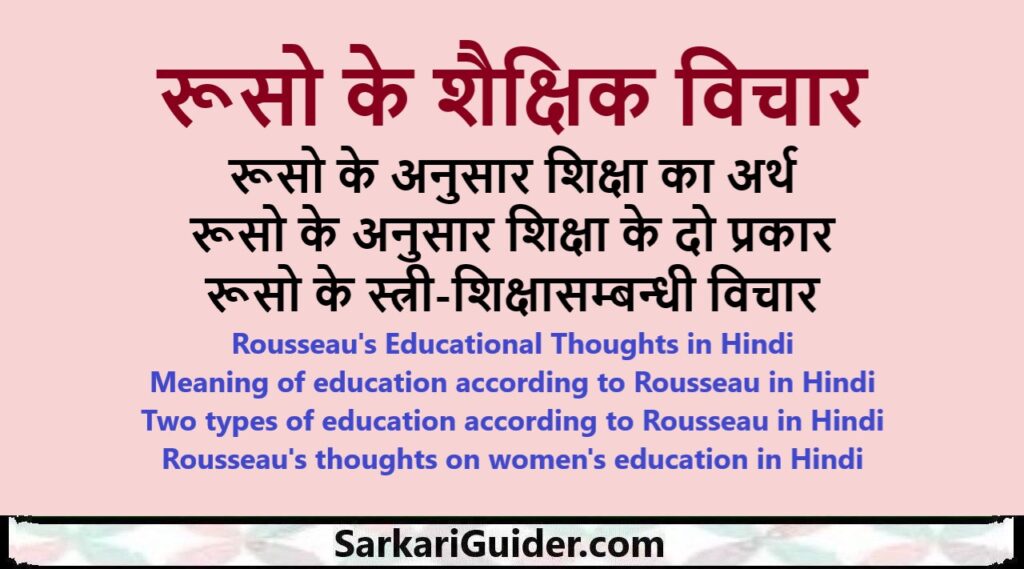
रूसो के शैक्षिक विचार | रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ | रूसो के अनुसार शिक्षा के दो प्रकार | रूसो के स्त्री-शिक्षासम्बन्धी विचार | Rousseau’s Educational Thoughts in Hindi | Meaning of education according to Rousseau in Hindi | Two types of education according to Rousseau in Hindi | Rousseau’s thoughts on women’s education in Hindi
रूसो के शैक्षिक विचार
रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा का समर्थक था। उसके प्रकृतिवादी विचारों का प्रभाव उसके शिक्षासम्बन्धी विचारों पर पड़ा है। उसी के अनुसार उसने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अनुशासन आदि के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किये हैं। इनके सम्बन्ध में उसके विचारों का अलग-अलग वर्णन नीचे किया जा रहा है-
रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ
रूसो शिक्षा का उद्देश्य केवल निर्देश देना अथवा ज्ञान संचय करना ही नहीं मानता। उसके विचार से शिक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लादा जा सके बल्कि उसके अनुसार-“सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अन्दर से प्रस्फुटित होती है। यह व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है।”
शिक्षा का इसी प्रकार का अर्थ प्रकट करते हुए उसने एक स्थान पर और भी लिखा है-“बालक की स्वाभाविक शक्तियों तथा योग्यताओं के आन्तरिक विकास का नाम ही शिक्षा है।”
रूसो के शिक्षासम्बन्धी विचारों को पॉल मुनरो ने इन शब्दों द्वारा स्पष्ट किया है-“शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है न कि कृत्रिम; यह एक आन्तरिक विकास है न किं बाह्य अभिवृद्धिः यह प्राकृतिक मूल-प्रवृत्तियों एवं रुचियों के कार्यशीलन से प्राप्त होती है न कि बाह्य-शक्ति की प्रतिक्रिया से; यह प्राकृतिक शक्तियों का एक विस्तार है न कि सूचनाओं का संग्रह; यह स्वयमेव जीवन है न कि बाल्य जीवन की रुचियों एवं विशेषताओं से दूर भावी जीवन की एक तैयारी।” ये समस्त विचार रूसो की शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण करते हैं।
रूसो ने शिक्षा के तीन मूल स्रोत बतलाये हैं-प्रकृति, मानव और पदार्थ प्रकृति द्वारा शिक्षा से रूसो का अभिप्राय यह है कि बालक को जो शिक्षा प्रदान की जाय वह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल हो, तभी बालक के विभिन्न अंगों और शक्तियों का स्वाभाविक विकास सम्भव है। शिक्षक को बालक की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास तभी सम्भव हो सकता है जबकि बालक में प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना जाग्रत की जाय तथा उसे प्राकृतिक वातावरण में रख कर प्राकृतिक तथ्यों एवं वस्तुओं के अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाय। मानव द्वारा शिक्षा से रूसों का अभिप्राय व्यक्ति के ऊपर उसके समाज तथा समूह के सम्पर्क से पड़ने वाले प्रभाव से है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह किसी न किसी समाज और समूह का सदस्य अवश्य होता है। समाज अथवा समूह के अन्य सदस्यों की भाषा, उनका रहन- सहन, उनकी मान्यताओं, परम्पराओं आदि का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। रूसो के अनुसार यही प्रभाव मानव द्वारा प्राप्त शिक्षा है। इसी प्रकार जो ज्ञान अथवा सूचना व्यक्ति अपने वातावरण में उपस्थित पदार्थों के सम्पर्क से प्राप्त करता है वह पदार्थ द्वारा दी गई शिक्षा हुई। रूसो उक्त दोनों प्रकार की शिक्षा को प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा निम्न स्तर को मानता है; किन्तु फिर भी उसका विचार है कि पूर्ण शिक्षा के लिए इन तीनों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। इस प्रकार रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है। शिक्षा में प्रकृतिवादी दृष्टिकोण के आधार पर उसने दो प्रमुख शिक्षण-सिद्धांतों का प्रतिपादन किया; यथा-(1) ‘प्रकृति की ओर लौटो’ का सिद्धांत और (2) ‘बालक के अध्ययन’ का सिद्धांत । इन सिद्धांतों का तात्पर्य यह है कि बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं का भली- भांति अध्ययन करके प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए।
रूसो के अनुसार शिक्षा के दो प्रकार
रूसो ने शिक्षा के दो प्रकार बतलाये हैं- (1) निश्चयात्मक शिक्षा और (2) निषेधात्मक शिक्षा। उसने निश्चयात्मक शिक्षा का विरोध किया है और निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन । यहाँ दोनों प्रकार की शिक्षा को अलग-अलग समझ लेना श्रेयस्कर होगा-
- निश्चयात्मक शिक्षा- रूसो ने अपने समय में प्रचलित शिक्षा को निश्चयात्मक शिक्षा कहा है और इसका घोर विरोध करते हुए इसके विपरीत चलने का सुझाव दिया है। उस समय शिक्षा बालक को बालक समझ कर नहीं दी जाती थी बल्कि ‘छोटा प्रौद’ समझ कर दी जाती थी। जो कार्य प्रौद्ध व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए उसकी शिक्षा भी छोटे बालकों को दी जाती थी। निश्चयात्मक शिक्षा बालक के बौद्धिक विकास की ही ओर ध्यान देती थी किन्तु उसके शारीरिक एवं अन्य शक्तियों की अवहेलना करती थी। निश्चयात्मक शिक्षा का अर्थ प्रकट करते हुए रूसो ने लिखा है- “मैं निश्चयात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय से पूर्व ही मस्तिष्क को परिपक्व बनाना चाहती है और बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्त्तव्यों को करने का निर्देश देती है।”
निश्चयात्मक शिक्षा में नैतिकता और चरित्र के नाम पर बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो उनके मनोविकास के अनुकूल नहीं हुआ करती थी। निश्चयात्मक शिक्षा मनुष्य की प्रकृति को बुरा समझती है और उसको सुधारने का प्रयास करती है। रूसो इस विचार से सहमत नहीं था; अतः उसने निश्चयात्मक शिक्षा का कड़ा विरोध किया और निषेधात्मक शिक्षा का भारी समर्थन एवं प्रचार किया। निश्चयात्मक शिक्षा के विरोध में रूसो ने लिखा है-“उस क्रूर शिक्षा के बारे में हम क्या विचार करें जो वर्तमान को अनिश्चित भविष्य पर बलि दे देती है, बालक पर भाँति-भाँति के बन्धन लगा देती है, उस काल्पनिक सुख के लिए जो वह कदाचित् कभी न भोगेगा, बहुत पहले से उसे दुखी बनाकर दी जाती है।” इसीलिए वह ऐसी शिक्षा के पक्ष में नहीं था। उसने कहा-“शिक्षा में जितने सिद्धांत व्यवहार में लाये जा रहे हैं, उनके विपरीत काम करो, तभी तुम हमेशा सही काम कर सकोगे।” निश्चयात्मक शिक्षा में निम्नलिखित बातों पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण रूसो ने इस प्रकार की शिक्षा का घोर विरोध किया है :-
(1) पुस्तकीय एवं शाब्दिक ज्ञान पर बल
(2) कर्त्तव्यपरायणता, नैतिकता और धार्मिकता पर बल,
(3) स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की उपेक्षा,
(4) कठोर अनुशासन,
(5) कृत्रिम और दूषित (रूसो के अनुसार) समाज के अनुकूल चलने और उसके नागरिक बनने की शिक्षा,
(6) प्रौढ़ों के कार्य की शिक्षा,
(7) उत्तम स्वभाव एवं आदतों के निर्माण पर बल ।
- निषेधात्मक शिक्षा- रूसो ने तत्कालीन प्रचलित शिक्षा, जिसे उसने निश्चयालक शिक्षा कहा है, का विरोध किया और उसके विपरीत निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन एवं प्रचार किया। निषेधात्मक शिक्षा का उद्देश्य बालक की प्रकृति, प्रवृत्तियों और शक्तियों के अनुसार शिक्षा देना है। यह ज्ञानेन्दियों के विकास में सहायक होती है। यह बालकों को प्रौढ़ों के कार्य की शिक्षा नहीं देती और न ही प्रौढ़ों के गुण प्रदान करती है; किन्तु दुर्गुणों से उनकी रक्षा करती है। रूसां ने निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है-निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान करने से पहले उन अंगों को, जो इसके साधन हैं, पूर्ण बनाने और इन्द्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क (विवेक) का मार्ग तैयार करने का प्रयत्न करती है। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ निठल्लापन नहीं है वरन् इससे बिल्कुल भिन्न है। यह सद्गुण नहीं प्रदान करती, यह दुगुणों से बचाती है; यह सत्य बोलना नहीं सिखलाती, यह झूठ बोलने से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग की ओर उन्मुख करती है जो उसे सत्य की ओर ले जायेगा जबकि वह उसको समझ सकने की अवस्था में पहुँच जाता है तथा उसे अच्छाई की ओर ले जायेगा जबकि इसे पहचानने और इससे प्रेम करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है।”
इस प्रकार निषेधात्मक शिक्षा का आशय यह है कि बालक को उसकी आयु, शक्ति, रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना चाहिए। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन बाल्यावस्था के लिए किया है। उसका विचार है कि बालक हर दृष्टि से साधु-प्रकृति का होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती; अतः उसकी शिक्षा भी स्वाभाविक, अकृत्रिम और इस दूषित समाज से दूर हटकर होनी चाहिए। प्रारंभ में बालक हर प्रकार के दुर्गुणों से रहित होता है; किन्तु सामाजिक जीवन में प्रवेश करते ही वह अनेक दुर्गुण और बुराइयों का शिकार हो जाता है। इस सम्बन्ध में कनिंघम ने लिखा है-“रूसो के अनुसार, सामाजिक संस्थाओं के सम्पर्क में आने पर ही मनुष्य के जीवन में बुराइयाँ प्रवेश करती हैं। सामाजिक जीवन में ही मनुष्य दुराचारी बनता है।” इसी कारण रूसो ने निश्-रात्मक शिक्षा का विरोध किया और निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया। इसके समर्थन में उसने लिखा है-“प्रथम शिक्षा इसलिए पूर्णतया निषेधात्मक होनी चाहिए कि यह शिक्षा सद्गुण या सत्य के सिद्धान्त को सिखाने में नहीं होती बल्कि वह तो हृदय को बुराई से एवं मस्तिष्क को भूल से बचाने में होती है।”
इसके अतिरिक्त निषेधात्मक शिक्षा में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं-
(1) पुस्तकीय शिक्षा का विरोध,
(2) इन्द्रिय प्रशिक्षण पर बल,
(3) शिक्षा में निर्देश देने का विरोध और स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल,
(4) मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल,
(5) बालक को आदतों का दास बनाने का विरोध,
(6) सामाजिक शिक्षा का विरोध,
(7) धर्म और नैतिकता आदि की शिक्षा का विरोध आदि ।
रूसो के स्त्री-शिक्षासम्बन्धी विचार
रूसो ने स्त्री-शिक्षा का जो कार्यक्रम निर्धारित किया है वह बड़ा ही अनुदार दिखलाई पड़ता है। उसके अनुसार स्त्री-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य-पुरुष के सुख-साधनों में वृद्धि करना है। उसने लिखा है कि “स्त्री पुरुष की प्रसन्नता के लिए है।” इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने स्त्री-शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है-
- शारीरिक शिक्षा- रूसो का मत है कि स्त्रियों को सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा देना आवश्यक है। क्योंकि कोई स्त्री पुरुष को तभी प्रसन्न रख सकती है जबकि वह स्वस्थ एवं सुन्दर होगी। इसके अतिरिक्त जब वह स्वयं स्वस्थ एवं सुन्दर होगी तो उसी प्रकार की संतान भी उत्पन्न कर सकेगी। स्वस्थ रह कर ही कोई स्त्री अपने पति की सेवा तथा बच्चों का पालन- पोषण कर सकती है, अतः स्त्री-शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का अपना एक विशेष महत्व है। इसके लिए उनके पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा, खेलना-कूदना, व्यायाम, घूमना- फिरना तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं को रखना चाहिए।
- गृह-कार्य की शिक्षा- रूसो के अनुसार स्त्रियों को शिक्षा द्वारा गृहकार्य में निपुण बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चित्रकारी आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें नाचने, गाने, चित्रकारी आदि कलाओं की शिक्षा, भोजन बनाने की कला का ज्ञान और बच्चों के पालन-पोषण की कला का ज्ञान कराना आवश्यक है।
- आज्ञापालन एवं अध्यवसाय-जैसे गुणों के विकास की शिक्षा- रूसो का विचार है कि स्त्री-शिक्षा इस प्रकार हो जो उसमें आज्ञापालन और परिश्रम करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर सके। प्रत्येक स्त्री को अपने माता-पिता एवं पति की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। रूसो का विचार है कि यदि उसके साथ किसी आदेश से अन्याय भी होता है तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें परिश्रमी बनाया जाय जिससे वे अपने पति की सेवा के लिए परिश्रम से न डरें।
- पुरुषों के स्वभाव का अध्ययन- रूसो के अनुसार प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह पुरुषों के स्वभाव का अध्ययन करके उसी के अनुकूल आचरण करे। उसको पुरुष की आज्ञानुसार चलना चाहिए और वे ही कार्य करने चाहिए जो पुरुष को अच्छे लगे। उसको इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस समय पुरुष क्या चाहता है अथवा उसकी क्या इच्छा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्त्री को पुरुष-मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बिना इस ज्ञान के वह पुरुष के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकती है। स्पष्ट है कि रूसो स्त्री को दर्शन, गणित, विज्ञान आदि गूढ़ विषयों की शिक्षा नहीं देना चाहता। वह तो उन्हें एक आदर्श गृहिणी के रूप में देखना चाहता है। उसने लिखा है-“स्त्री को पुरुषों की भावनाओं को उनके वार्तालाप, कार्यो, दृष्टि और भाव-भंगिमाओं आदि के माध्यम से जानना चाहिए।”
- धार्मिक शिक्षा- रूसो स्त्रियों की धार्मिक शिक्षा में विश्वास करता है। इस सम्बन्ध में उसका कहना है कि उन्हें प्रारम्भिक स्तर से ही धर्म में रूदिबद्ध ढंग से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। रूसो ने लिखा है-“प्रत्येक लड़की को अपनी माता का धर्म तथा प्रत्येक पत्नी को अपने पति का धर्म पालन करना चाहिए।”
- नैतिक शिक्षा- स्त्रियों की नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में रूसो का मत है कि उसकी इस शिक्षा का निर्धारण जनता द्वारा प्रदान की गई सम्मतियों के आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात् स्त्रियों की शिक्षा जनमत को अधिक ध्यान में रखा जाय और उन्हीं बातों का स्थान दिया जाय जो जनता द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- रवीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन-वृत्त | रवीन्द्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचार | रवीन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की समीक्षा
- डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व | डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तिगत स्वभाव का संक्षिप्त चित्रण
- आदर्श शिक्षक के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन | भारतीय संस्कृति के पोषक
- प्लेटो का जीवन-वृत्त | प्लेटो की रचनाएँ | प्लेटो के दार्शनिक विचार
- प्लेटो के शैक्षिक विचार | प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य | प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षा के विभिन्न स्वरूप
- प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधि | प्लेटो के विद्यालय सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षक सम्बन्धी विचार | प्लेटो के अनुशासन सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षा-सिद्धांत की समीक्षा | शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो का योगदान
- रूसो का जीवन-वृत्त | रूसो की रचनाएँ | Biography of Rousseau in Hindi | Rousseau’s works in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]