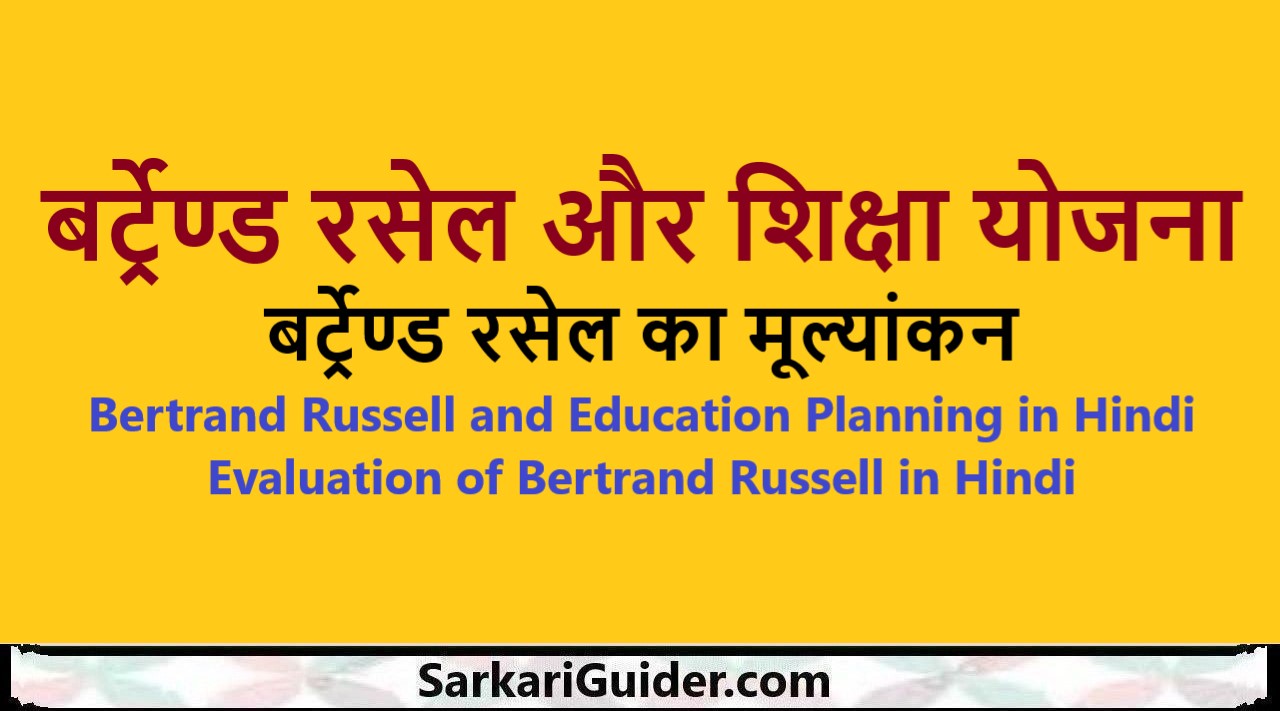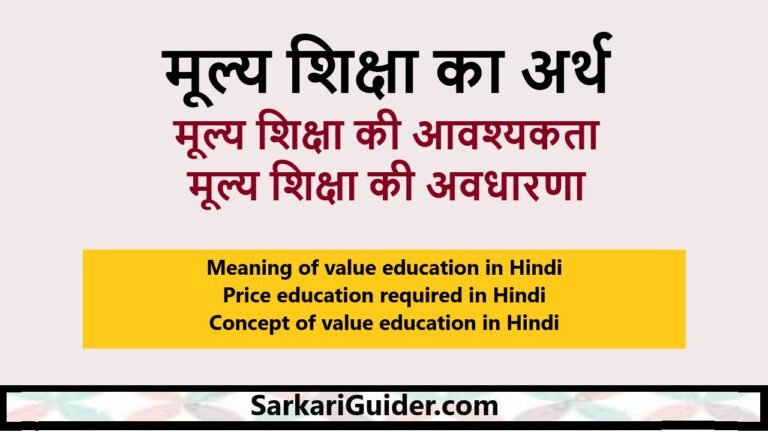बर्ट्रेण्ड रसेल और शिक्षा योजना | बर्ट्रेण्ड रसेल का मूल्यांकन
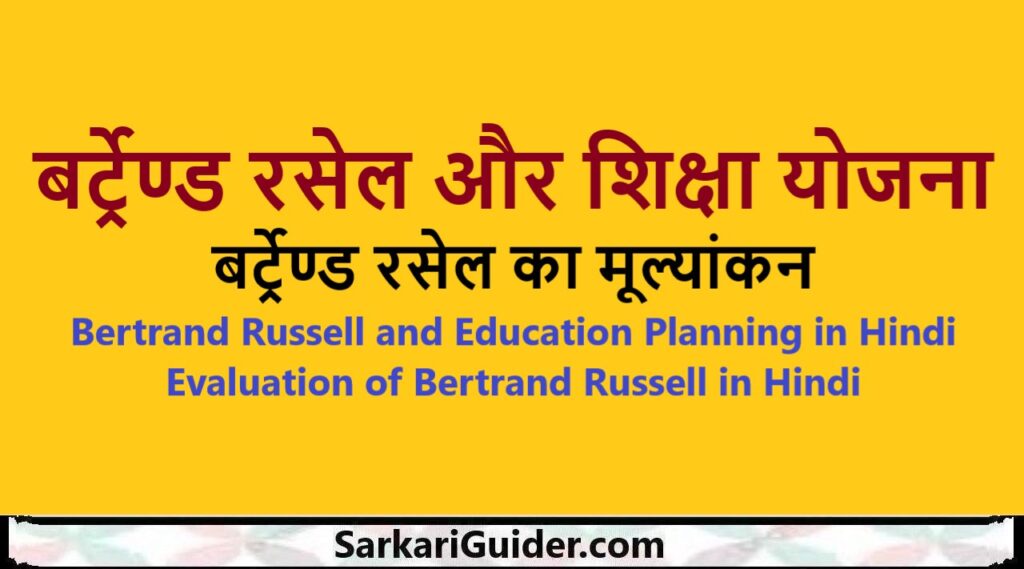
बर्ट्रेण्ड रसेल और शिक्षा योजना | बर्ट्रेण्ड रसेल का मूल्यांकन | Bertrand Russell and Education Planning in Hindi | Evaluation of Bertrand Russell in Hindi
बर्ट्रेण्ड रसेल और शिक्षा योजना
(Russell and Educational Plan)
बर्ट्रेण्ड रसेल के अनुसार बालक की शिक्षा की योजना अनेक स्तरों के अनुसार की जानी चाहिए।
ये स्तर निम्नलिखित हैं-
(1) 1 वर्ष से 2-3 वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा।
(2) 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा
(3) 5 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा।
(4) 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की शिक्षा।
(5) विश्वविद्यालयीय शिक्षा
(1) एक वर्ष से दो-तीन वर्ष तक- रसेल के अनुसार शिशु की शिक्षा जन्म के दो-तीन माह बाद ही प्रारम्भ हो जानी चाहिए। स्तन-पान, स्वच्छता, समय पर दूध देना, बोतल से दूध पिलाना, जब-जब शिशु रोये तब-तब सदा दूध न देना, पेशाब करना सिखाना आदि बातें जन्म के प्रथम वर्ष से ही प्रारम्भ हो जानी चाहिए।
(2) नर्सरी स्कूल- दो-तीन वर्ष की आयु के पश्चात् बालकों के लिए नर्सरी स्कूल ठीक रहेंगे। औद्योगिक समाज में माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं अतः वे बालकों को उचित रूप से शिक्षा नहीं दे सकते। नर्सरी स्कूल, मांटेसरी पद्धति पर आधारित हो सकते हैं। इन स्कूलों में छोटे-छोटे बच्चों की आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। यहाँ पर बच्चों को गाना, नाचना, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाए। पाँच वर्ष की आयु तक के बालक यहां रहेंगे। अन्तिम वर्ष में शिशु को लिखना-पढ़ना भी सिखाना चाहिए।
(3) 5 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा- जब बालक पाँच वर्ष का हो जाए तो उसे मानसिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर पर बालकों को साहसिक कहानियों सुनाई जाएँ। भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों एवं मानचित्रों का होना आवश्यक है। इतिहास में संसार की महान विभूतियों की कहानियां सुनाई जाएँ। बुद्ध, सुकरात, न्यूटन, गाँधी आदि महापुरुषों की महानता के गुणों पर बल देना चाहिए। बीजगणित, विज्ञान, रसायनशास्त्र की शिक्षा 12 वर्ष की आयु पर प्रारम्भ की जाय। इस स्तर पर विशेष योग्यता के लिए शिक्षा का प्रयास नहीं करना चाहिए।
(4) 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की शिक्षा- इस स्तर पर बालकों को विशिष्टीकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीन प्रकार के विशिष्टीकरण का प्रबन्ध किया जा सकता हैं (1) उच्च कोटि का साहित्य, (2) गणित तथा विज्ञान, (3) नवीनतम मानवता। इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणित, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन साथ-साथ चलते रहना चाहिए। विशिष्टीकरण की सुविधा देते समय छात्रों की योग्यता और रुचि का ध्यान रखना चाहिए।
(5) विश्वविद्यालयी शिक्षा- इस स्तर पर रसेल संख्या एवं परिणाम की अपेक्षा गुणात्मकता का समर्थन करते हैं। विश्वविद्यालयी शिक्षा सबके लिए नहीं होनी चाहिए। योग्य छात्रों को ही ‘विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। छात्रों का चुनाव क्षमता के आधार पर होना चाहिए, न कि माता-पिता की समृद्धि एवं कुलीनता के आधार पर।
विश्वविद्यालयी शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं- एक तो यह कि कुछ व्यवसायों के लिए छात्रो को दीक्षित करना और दूसरा उद्देश्य यह है कि सीखने और अन्वेषण के लिये छात्रों को अवसर प्रदान करना। इन्हीं दोनों उद्देश्यों के आधार पर छात्रों का चयन होना चाहिए।
विश्वविद्यालयी शिक्षा पर धनी लोगों का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए! क्षमतो के आधार पर यह सब लोगों को मुलभ हो। प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा हो और अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न दिया जाय। प्रवेश के बाद भी यदि छात्र का काम सन्तोषजनक न हो तो उसे विश्वविद्यालय से हटा देने की व्यवस्था हो । विश्वविद्यालयों को विद्यामन्दिर बनना चाहिए।
शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में छात्रों को दो प्रकार की पुस्तकों के अध्ययन का निर्देश दिया जाय। प्रथम प्रकार की पुस्तकें सभी के लिए अनिवार्य हों और दूसरी प्रकार की पुस्तकों का चयन छात्रों पर छोड़ दिया जाय। इस स्तर पर अध्यापक के समक्ष मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
बर्ट्रेण्ड रसेल का मूल्यांकन
(Evaluation of Russell)
दर्शन की दृष्टि से रसेल तर्कीय प्रत्यक्षवादी तर्कीय परमाणुवादी और नव्य-वास्तववादी हैं। रसेल के शिक्षा दर्शन पर उनके जीवन दर्शन का प्रभाव बहुत कम है जबकि अन्य शिक्षा- दार्शनिकों का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन से ही ओतप्रोत रहता है। रसेल के शिक्षा दर्शन में आदर्शवादी और व्यावहारिकतावादी तत्वों का प्रभाव विद्यमान है। अच्छी आदत, सदाचार, अनुशासन, अच्छे साहित्य आदि पर बल देकर रसेल आदर्शवाद की ओर अपना झुकाव प्रदर्शित करते हैं तो प्रयोगात्मकता एवं उपयोगिता पर बल देकर वे व्यावहारिकतावाद की ओर झुकते दिखाई पड़ते हैं। नर्सरी स्कूलों की स्थापना एवं प्राकृतिक वातावरण की वकालत करके वे प्रकृतिवाद का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं तो उपयोगिता, यथार्थता, एवं वैज्ञानिकता पर बल देकर वे यथार्थवादी होने का परिचय देते हैं। रसेल के शिक्षा दर्शन पर यथार्थवाद का सर्वाधिक प्रभाव है।
रसेल ने स्वयं किसी मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया, किन्तु तत्कालीन मनोवैज्ञानिक खोजों का उन पर प्रभाव पड़ा है। वे विकासवाद के समर्थक हैं। गाडर्ड, टरमैन और गाल्टन के आनुवंशिकता के सिद्धान्त का वे समर्थन नहीं करते। वातावरण के प्रभाव के वे समर्थक हैं। फ्रायड की खोजों से वे प्रभावित हैं और वासनाओं के दमन का वे विरोध करते हैं।
रसेल समाज की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं किन्तु व्यक्तित्व के विकास के वे प्रबल समर्थक हैं। युद्ध के वे कट्टर विरोधी हैं और शान्ति के अग्रदूत कहे गये हैं। एक विश्व-सरकार की स्थापना का वे समर्थन करते हैं। कुलीनता का वे विरोध करते हैं।
रसेल विज्ञान को मानव-जीवन का आधार बनाना चाहते हैं और वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा समस्याओं के समाधान पर बल देते हैं।
रसेल ने शिक्षा पर अटूट आस्था व्यक्त की है। उनके द्वारा समर्थित शिक्षा के उद्देश्य सराहनीय हैं। चरित्र-निर्माण एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का सर्वाधिक समर्थन करके उन्होंने शिक्षा को एक नयी दिशा देने का प्रयास किया है।
पाठ्यक्रम के क्षेत्र में रसेल व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। विभिन्न विषयों के समावेश का वे परामर्श देते हैं। धार्मिक कट्टरता से छात्र को वे बचाना चाहते हैं।
शिक्षा योजना में अध्यापक की भूमिका को रसेल ने महत्त्वपूर्ण माना है। स्वतन्त्रता और अनुशासन के क्षेत्र में अतिवाद से बचने का उन्होंने परामर्श दिया है।
उपर्युक्त गुणों के होते हुए भी रसेल के शिक्षा-दर्शन में कुछ दोष भी हैं।
रसेल ने कक्षा के अन्दर की पढ़ाई पर अत्यधिक बल दिया है। औपचारिक शिक्षा तक शिक्षा को सीमित करना ठीक नहीं है।
रसेल का शिक्षा दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है। रसेल ने एक प्रकार से सामाजिक ‘अन्तः क्रिया की उपेक्षा की है।
रसेल ने आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा की है। इसीलिए उनके द्वारा किये गये शान्ति- स्थापना के प्रयास पंगु हो गये हैं। आध्यात्मिकता-विहीन व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। उसे शान्ति और चैन कैसे मिलेगी?
रसेल ने बौद्धिकता पर बहुत बल दिया है। मनुष्य का जीवन केवल बुद्धि से संचालित नहीं होता। व्यक्ति भाव एवं क्रिया के अन्तर्गत सर्वाधिक घूमता है। रसेल ने इस दृष्टि से एकांगी दृष्टिकोण अपनाया है।
रसेल ने धर्म का विरोध करके मानव जाति को एक सुखद अनुभूति से वंचित करने का प्रयास किया है और व्यक्ति को सांस्कृतिक विरासत से काटने का प्रयत्न किया है।
नैतिकता को धर्म से पृथक् करके तार्किक समझ तो आ सकती है किन्तु बालक का अधिक कल्याण नहीं किया जा सकता। रसेल ने नैतिकता को धर्म से नितान्त पृथक् रूप में देखा है।
एक ओर तो रसेल यौन-वृत्ति को जीवन की साधारण क्रिया मानते हैं और दूसरी ओर इस पर आवश्यकता से अधिक बल यौन-वृत्ति को असाधारण बना देते हैं। जिस उन्मुक्त व स्वच्छन्द संभोग की रसेल ने वकालत की है उससे व्यक्ति पशु के स्तर पर आ जायेगा। यदि रसेल की बात मान ली जाए तो स्त्री-पुरुषों में व्यभिचार बढ़ेगा और वे और अधिक कुण्ठाओं एवं मानसिक प्रन्थियों के शिकार होंगे जिनसे बचने के लिए रसेल ने प्रयोगात्मक सम्भोगों की बात कही है।
रसेल ने शिक्षण विधि पर कोई नई बात नहीं कही और प्रचलित बातों का संकलन मात्र कर दिया है।
अनुशासन के सामाजिक पक्ष की ररोल ने उपेक्षा की है। केवल बालक की रुचियों का ध्यान रखने से ही अनुशासन नहीं स्थापित हो जाता।
रसेल के सिद्धान्त अनेक स्थलों पर परस्पर विरोधी हैं। एक स्थान पर वे नकारात्मक शिक्षा को स्वीकार करते हैं तो अन्यत्र उसे अस्वीकार कर देते हैं। दार्शनिक मान्यताओं के क्षेत्र में भी उनके सिद्धान्त बदलते रहे हैं।
लॉक की भाँति रसेल भी तर्कबुद्धि का आश्रय लेने की बात करते हैं किन्तु लॉक कुलीन शिक्षा के समर्थक थे, जबकि रसेल ने इसका विरोध किया है।
ह्वाइटहेड की भाँति रसेल ने अनुशासन और स्वतन्त्रता में अतिवाद से बचने का सुझाव दिया किन्तु ह्वाइटहेड ने जिस अनुशासन योजना की रूपरेखा दी है वह अधिक व्यवस्थित है। ह्वाइटहेड ने ‘इनर्ट आइडिया’ को महत्त्वपूर्ण माना है और उस विचार से अलग विचार को कोई स्थान नहीं दिया। रसेल ने ‘इनर्ट आइडिया’ की बात को स्वीकार नहीं किया है।
हक्सले की भाँति रसेल भी वैज्ञानिक शिक्षा के समर्थक थे किन्तु हक्सले ने अपने को वैज्ञानिक शिक्षा तक ही सीमित किया जब कि रसेल ने अधिक विस्तृत क्षा योजना प्रस्तुत की।
हरबर्ट स्पेन्सर की भाँति रसेल ने जीवन के लिए शिक्षा की बात की किन्तु स्पेन्सर ने सम्पूर्ण ‘जीवन के लिए शिक्षा की बात की तो रसेल ने सुखी जीवन की बात की।
रूसो की भाँति रसेल भी अन्तर्विरोधों के शिकार थे। फ्रायड की भाँति वे भी यौन-वृत्ति को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देते थे।
उपर्युक्त कमियों के बावजूद रसेल ने जिस उच्च कोटि के शिक्षा दर्शन का प्रतिपादन किया वह सराहनीय है। उनका जीवन ऋषिवत् था। वे जीवन भर संघर्ष करते रहे, युद्ध के विरुद्ध नारा बुलन्द करते रहें, अन्याय एवं उत्पीड़न का डटकर मुकाबला करते रहे एवं मानवता के कल्याण के लिए जीवन भर जूझते रहे।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- प्लेटो का जीवन-वृत्त | प्लेटो की रचनाएँ | प्लेटो के दार्शनिक विचार
- प्लेटो के शैक्षिक विचार | प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य | प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षा के विभिन्न स्वरूप
- प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधि | प्लेटो के विद्यालय सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षक सम्बन्धी विचार | प्लेटो के अनुशासन सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षा-सिद्धांत की समीक्षा | शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो का योगदान
- रूसो का जीवन-वृत्त | रूसो की रचनाएँ | Biography of Rousseau in Hindi | Rousseau’s works in Hindi
- रूसो के शैक्षिक विचार | रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ | रूसो के अनुसार शिक्षा के दो प्रकार | रूसो के स्त्री-शिक्षासम्बन्धी विचार
- बट्रेण्ड रसेल का जीवन | बट्रेण्ड रसेल का कार्य | रसेल का दर्शन
- बर्ट्रेण्ड रसेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य | रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम | रसेल और यौन-शिक्षा | रसेल और धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा | रसेल और शिक्षण-पद्धति
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]