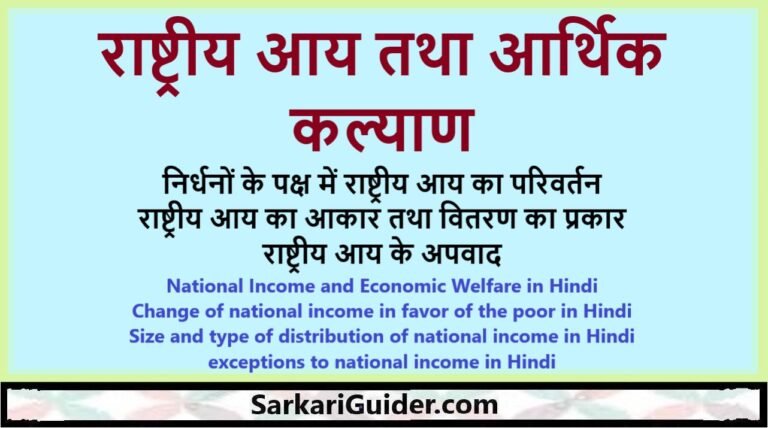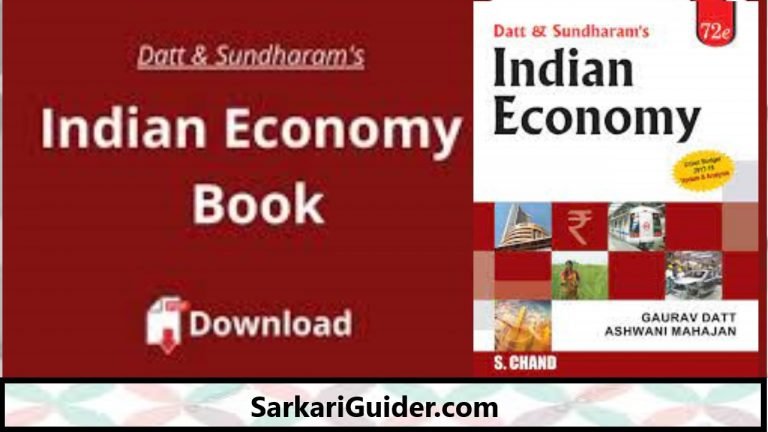भारतीय कृषि संरचना में विद्यमान असंतुलन | भारतीय कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असन्तुलन | भारतीय कृषि क्षेत्र में वैयक्तिक असंतुलन
भारतीय कृषि संरचना में विद्यमान असंतुलन | भारतीय कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असन्तुलन | भारतीय कृषि क्षेत्र में वैयक्तिक असंतुलन
भारतीय कृषि संरचना में विद्यमान असंतुलन
(क) भारतीय कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन
(Regional Imbalance)
भारत में नई कृषि युक्ति को 1966-67 में 18 लाख 90 हजार हैक्टर भूमि पर शुरू किया गया। 1993-94 में यह क्षेत्र बढ़कर 6 करोड़ 66 लाख हैक्टर हो गया। परन्तु यह कुल कृषि क्षेत्र के एक-तिहाई से थोड़ा ही अधिक है। स्वाभाविक है कि नई कृषि युक्ति का लाभ केवल इसी क्षेत्र तक सीमित रहा है। इसके अलावा, कई वर्षों तक हरित क्रांति का प्रभाव केवल गेहूं का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, इसलिए लाभ ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों को मिले जिनमें गेहूं बोया जाता था। वस्तुतः यह भी सही नहीं है। यदि इस बात को याद रखा जाए कि गेहूं के अधीन क्षेत्रों में लाभ उन्हीं क्षेत्रों को हुआ है जिनमें पानी की उचित व्यवस्था थी तथा अन्य धन भी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध थे, तो हरित क्रान्ति से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र और कम रह जाता है। यह लाभान्वित होने वाला क्षेत्र मुख्यतया पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। वास्तव में जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि उत्तरी राज्यों (पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) का खाद्यान्न उत्पादन में हिस्सा जो 1970-71 से 1972-73 के बीच औसतन 29.5 प्रतिशत था, 1991-92 से 1993-94 के बीच, बढ़ कर औसतन 37.6 प्रतिशत हो गया। पश्चिमी राज्यों (गुजरात तथा महाराष्ट्र) के हिस्से में इसी अवधि में थोड़ी वृद्धि हुई (7.9 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत) जबकि अन्य सभी राज्य-समूहों के हिस्से में कमी आई।
इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि नई कृषि युक्ति के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। परन्तु अपने ऊपर चर्चित लेख में हनुमंत राव ने यह दावा किया है कि 1978-79 से बाद की अवधि में क्षेत्रीय असमानताएँ उतनी व्यापक नहीं थीं जितनी कि 1967-68 से 1977-78 के दशक में थीं। इसका मुख्य कारण यह है कि चावल, दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई और ये सब फसलें वर्षा-आश्रित क्षेत्रों (अर्थात् असिंचित क्षेत्रों) में अधिक बोई जाती हैं। हनुमन्त राव के अध्ययन से पता चलता है कि कई राज्यों में वहां व्यापक निर्धनता है तथा जिनमें हरित क्रांति प्रथम दशक में खाद्यान्न उत्पादन में संवृद्धि कम हो गई थी (जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल) उनमें पिछले दशक में आशातीत संवृद्धि हुई है। वास्तव में, इन राज्यों का का निष्पादन पूरे देश के लिए औसत के बराबर अथवा उससे भी अधिक रहा है। उदाहरण के लिए, बिहार में जहां 1967-68 में 1977-78 के बीच खाद्यानों के उत्पादन में मात्र 1.14 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। इसी अवधि में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर 1.23 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़कर 4.36 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई। पूरे देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर 1967-68 से 1977- 78 के बीच 2.31 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा 1978-79 से 1988-89 के बीच 2.68 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। आठवें दशक के दौरान पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन की संवृद्धि दर काफी कम हो गई थी। परन्तु 1978-79 से 1988-89 के बीच इन सभी राज्यों में चावल उत्पादन को संवृद्धि दर बढ़ी है तथा कुछ में तो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा रही है। इसका मुख्य कारण नई कृषि युक्ति का विस्तार तथा कम विकसित राज्यों में शुष्क खेतों पर जोर दिया जाना है।
खाद्यान्न उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा
| (कुल का प्रतिशत) | ||
| क्षेत्र
(1) |
1970-71 से 1972-73 (औसत)
(2) |
1991-92 से 1993-94 (औसत)
(3) |
| 1. उत्तरी राज्य (पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश) | 29.5 | 37.6 |
| 2. पूर्वी राज्य (उड़ीसा, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल) | 22.3 | 19.1 |
| 3. पश्चिमी राज्य (गुजरात व महाराष्ट्र) | 7.9 | 9.1 |
| 4. राजस्थान तथा मध्य प्रदेश | 17.2 | 14.6 |
| 5. दक्षिणी राज्य (आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल) | 20.3 | 16.7 |
| 6. अन्य राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश | 2.8 | 2.8 |
| कुल | 100 0 | 100.0 |
(ख) भारतीय कृषि क्षेत्र में वैयक्तिक असंतुलन
(Personal Imbalance)
हरित क्रांति के आरम्भिक काल में बड़े किसानों को, छोटे व सीमान्त किसानों की तुलना में, नई कृषि युक्ति से ज्यादा लाभ हुआ। यह अप्रत्याशित भी नहीं था क्योंकि नई कृषि युक्ति के लिए काफी निवेश की आवश्यकता थी और इतना निवेश छोटे व सीमान्त किसानों के वश के बाहर था। केवल बड़े व धनी किसान ही आवश्यक निवेश करने की क्षमता रखते थे (जैसा कि हमने भी कहा है नई युक्ति एक पैकेज प्रोग्राम था जिसमें उन्नत किस्म के बीचों के प्रयोग के साथ-साथ अन्य आगतों, जैसे- सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं इत्यादि की भी जरूरत थी)। इसलिए अधिक उत्पादकता के लाभ भी अधिकतर बड़े किसानों को ही प्राप्त हुए जिससे अन्तः वैयक्तिक असमानताएँ बढ़ गईं। हरित क्रान्ति के आरम्भिक वर्षों में किये गये फ्रैन्मिन आर0 फ्रैंकल, प्रणव वर्धन तथा नी0आर0 सैनी के अध्ययनों में यह बातें उभर कर सामने आई। परन्तु समय के साथ छोटे किसानों को संस्थागत ऋणों में वृद्धि हुई (हालांकि, संस्थागत ऋणों के एक बड़े अंश पर बड़े किसानों का कब्जा बना रहा)। इसके परिणामस्वरूप तथा नई युक्ति के बारे में बढ़ती जानकारी के परिणामस्वरूप छोटे किसानों ने व्यापक पैमाने पर नई कृषि युक्ति को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समय के साथ हरित क्रांति का लाभ छोटे किसान तक भी पहुंचने लगा है। इस प्रकार के निष्कर्ष उषा नागपाल, जार्ज ब्लाइन जे० आर० वेस्टले तथा जी० एस० भल्ला व जी0 के0 चड्ढा के अध्ययनों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब के छोटे व सीमान्त किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव का अध्ययन करते हुए, जी० एस० भल्ला व जी0 के0 चड्ढा इस निष्कर्ष पर पहंचते हैं कि “पंजाब में हरित क्रांति के आगमन से सभी किसान-वर्गों को कल मिलाकर लाभ हुआ है।” परन्तु इसी अध्ययन में एक अन्य स्थल पर यह स्वीकार किया गया है कि एक तिहाई सीमान्त किसान तथा 24 प्रतिशत छोटे किसान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।
जहां तक कृषि श्रमिकों का प्रश्न है सभी लोगों का मानना है कि उनकी मौद्रिक आय में वृद्धि हुई है। परंतु वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई है अथवा नहीं, इस बारे में मतभेद है। अपने अध्ययन Land, Labour and Rural (1984) में पी0के0 बर्धन ने खेतिहार मजदूरों के लिए 1964-65 तथा 1975-76 में की गई जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि सम्पूर्ण भारत के लिए, खेतिहर मजदूर परिवारों के पुरुषों को कृषि गतिविधियों से होने वाली आय वास्तविक रूप से (in real terms) 12 प्रतिशत कम हुई है। राज्य स्तर पर सभी राज्यों में वास्तविक मजदूरी में गिरावट हुई है, केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर जहां इसमें वृद्धि हुई है तथा कर्नाटक को छोड़कर (जहां यह पूर्ववत् बनी रही है)। परन्तु हाल में जी0 पार्थसारथी ने यह मत व्यक्त किया है कि 1974-75 का वर्ष कृषि के लिहाज से अच्छा नहीं था इसलिए यदि मजदूरी के साथ अन्य आय स्रोतों से आय को भी कुल वार्षिक आय ज्ञात करते समय शामिल कर लिया जाए तो स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। अपने लेख “Trends in Real Wages in Rural India, 1880-1980″ में दीपक लाल सिद्ध करते हैं कि वास्तविक मजदूरी दरों में 1970 से 1979 के बीच बहुत धीरे-धीरे वृद्धि हुई। कई राज्यों जैसे कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में तो वास्तविक मजदूरी दरों में वस्तुतः गिरावट हुई। परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों का दावा है कि आठवें दशक के उत्तरार्द्ध से कृषि मजदूरी में अन्तः राज्यीय अन्तर (Inter-State disparities) कम होने लगे हैं। उदाहरण के लिए ए0वी0 जोस के अनुसार, आठवें दशक के उत्तरार्द्ध से पंजाब में विद्यमान वास्तविक मजदूरी दरों और बिहार में विद्यमान वास्तविक मजदूरी दरों में अन्तर कम होने लगे हैं। वास्तविक मजदूरी दरों में अन्तर कम होने के प्रमुख कारण हैं- “कम विकसित क्षेत्रों से श्रमिकों का उच्च-मजदूरी वालेक्षक्षेत्रों की ओर गमन; कम विकसित क्षेत्रों में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार अवसरों में वृद्धि; तथा हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में होने वाला कृषि विकास।”
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- विदेशी निजी पूंजी पर नियन्त्रण | विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 | विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम का कार्यान्वयन
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम | सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य | प्राकृतिक योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- भारत में पंचायती राज | स्वतंत्रता के बाद पंचायतों का विकास | पंचायती राज की कमजोरियाँ एवं सुझाव
- भारत में ग्रामीण बेरोजगारी | ग्रामीण बेरोजगारी के कारण | ग्रामीण बेरोजगारी के निदान | ग्रामीण बेरोजगारी दूर करन के सरकारी निदान
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]