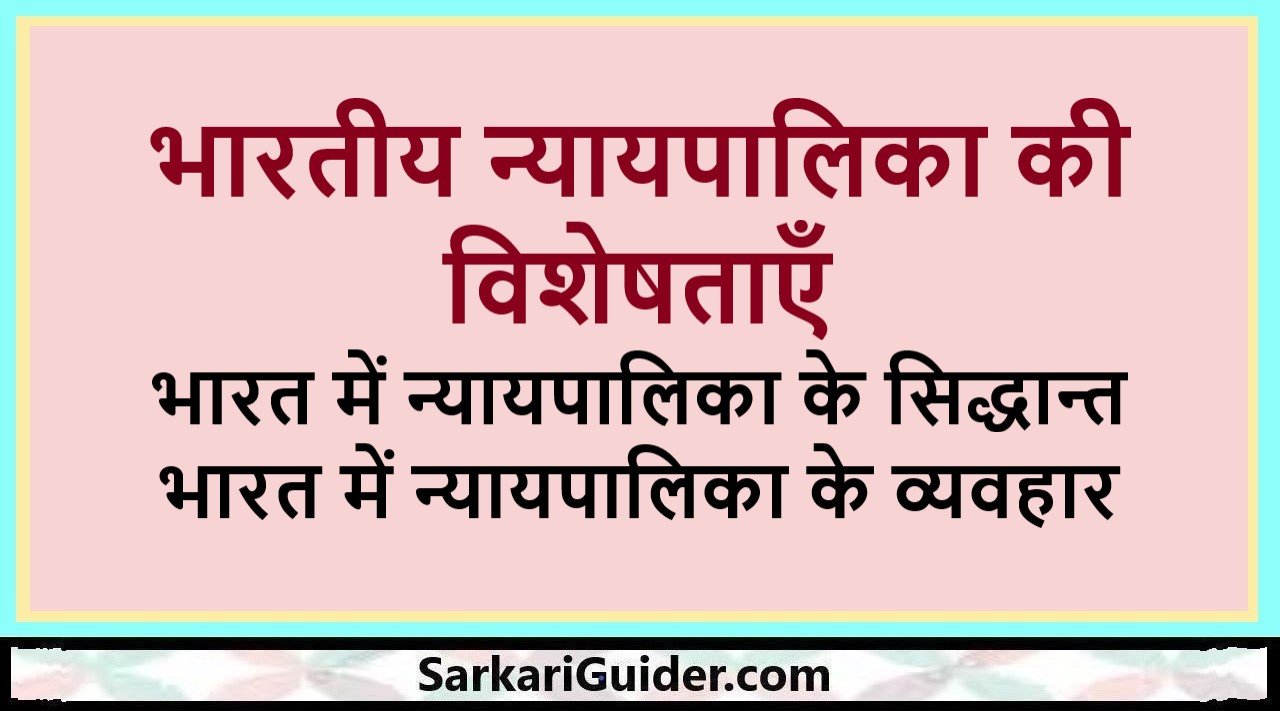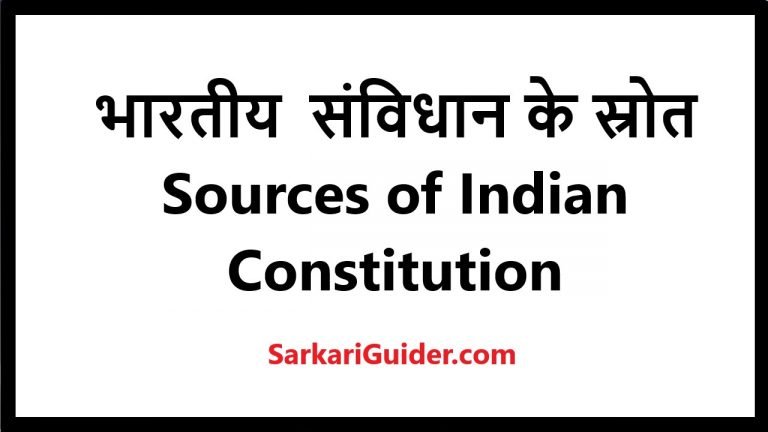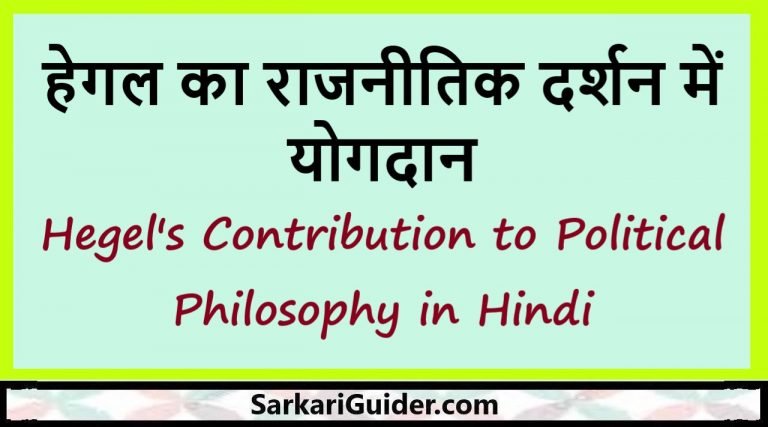भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएँ | भारत में न्यायपालिका के सिद्धान्त | भारत में न्यायपालिका के व्यवहार

भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएँ | भारत में न्यायपालिका के सिद्धान्त | भारत में न्यायपालिका के व्यवहार
भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएँ
भारतीय न्यायपालिका की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है:-
(1) भारत की न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है।
(2) भारतीय न्यायपालिका अत्यन्त सुनियोजित रूप से ऊपर से नीचे तक एक संगठन के रूप में कार्य करती है।
(3) भारत में एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। भारत में भी इंग्लैण्ड की भाँति ‘विधि के शासन’ को मान्यता प्रदान की गई है।
(4) भारत की न्यायपालिका की एक विशेषता यहाँ पर प्रमुख रूप से दो प्रकार के न्यायालय है-दीवानी और फौजदारी का पाया जाना है
(5) भारत में संविधान को ही सर्वोपरि माना गया है। यहाँ की न्यायपालिका ही संविधान की संरक्षक है।
सर्वोच्च न्यायालय- संविधान के अनुसार भारतीय उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। इसका एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य सात न्यायाधीश होते हैं। अब संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या चौदह कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। वह चाहे तो इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। यदि संसद के दोनों सदन दो-तिहाई बहुमत से किसी न्यायाधीश को अयोग्य या दुराचारी सिद्ध कर दे और उसको अपने पद से हटाये जाने की अनुमति दे दे तो वह न्यायाधीश अपने पद से हटा दिया जाता हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं।
हमारे संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये गये हैं:-
(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार- जब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा इस न्यायालय द्वारा किया जाता है।
(2) मौलिक अधिकारों की रक्षा- यह न्यायालय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है।
(3) अपीलसम्बन्धी अधिकार- इस न्यायालय को राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध तीन प्रकार की अपीलें सुनने का अधिकार है-(अ) संवैधानिक, (ब) दीवानी, और (स) फौजदारी सम्बन्धी।
(अ) संवैधानिक अपीलें- जब किसी विवाद में उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाणपत्र दे दे कि इस मामले में संविधान की व्यवस्था से सम्बन्धित कोई कानूनी प्रश्न निहित है तो उच्चतम न्यायालय ऐसी अपीलों पर विचार कर सकता है।
(ब) दीवानीसम्बन्धी अपीलें- किसी राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी सम्बन्धी अपीलें उच्चतम न्यायालय में तभी सुनी जा सकती हैं जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद बीस हजार रुपये से कम का नहीं है अथवा यह मामला उच्चतम न्यायालय में अपील करने के योग्य है।
(स) फौजदारीसम्बन्धी अपीलें- फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध तभी अपील की जा सकती है जब किसी उच्च न्यायालय ने अपील में निचले न्यायालय द्वारा मुक्त किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड की सजा दी हो अथवा जब उच्च न्यायालय ने किसी निचली अदालत से मामले को परीक्षण के लिए मँगाकर अपराधी को फाँसी की सजा दी हो अथवा उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाणपत्र दें दे कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है।
(4) विशिष्ट अपीलें-उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार भी है कि वह सैनिक- न्यायालयों के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है एवं अपील को सुन सकता है।
(5) राष्ट्रपति को परामर्श का कार्य- उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को किसी कानून या सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्न पर उसके परामर्श माँगने पर परामर्श दे सकती है।
(6) पुनरावलोकन का अधिकार- उच्चतम न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपने द्वारा किये गये किसी निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है और उसके दोषों को दूर कर सकता है।
संसद कानून बनाकर इसके अधिकारों को बढ़ा भी सकती है। इस न्यायालय द्वारा निर्मित नियम भारत के सभी न्यायालयों में लागू होते हैं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय अत्यन्त शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायालय है।
अन्य न्यायालय- उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त राज्यों के लिए भी ऊपर से नीचे तक न्यायपालिका का संगठन एक पिरामिड के रूप में किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। उसके लिए अपीलीय न्यायालय होते हैं— फौजदारी, दीवानी और राजस्व न्यायालय। ग्रामों में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था है। इस प्रकार भारत की न्यायपालिका पूर्ण रूप से संगठित है।
राजनीतिक शास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- न्यायपालिका | न्यायपालिका का महत्त्व | न्यायपालिका का संगठन | न्यायपालिका के कार्य | न्यायपालिका की स्वतन्त्रता
- ब्रिटेन में न्यायपालिका | अमरीका में न्यायपालिका | फ्रान्स की न्यायपालिका | स्विट्जरलैण्ड की न्यायपालिका
- न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ | अमरीका में न्यायिक पुनरावलोकन | भारत में न्यायिक पुनरावलोकन | न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान
- प्रजातंत्र का अर्थ एवं परिभाषा | प्रजातंत्र का व्यापक अर्थ | प्रजातंत्र के प्रकार | विशुद्ध प्रजातंत्र | प्रत्यक्ष प्रजातंत्र | प्रतिनिधित्यात्मक प्रजातंत्र | अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]