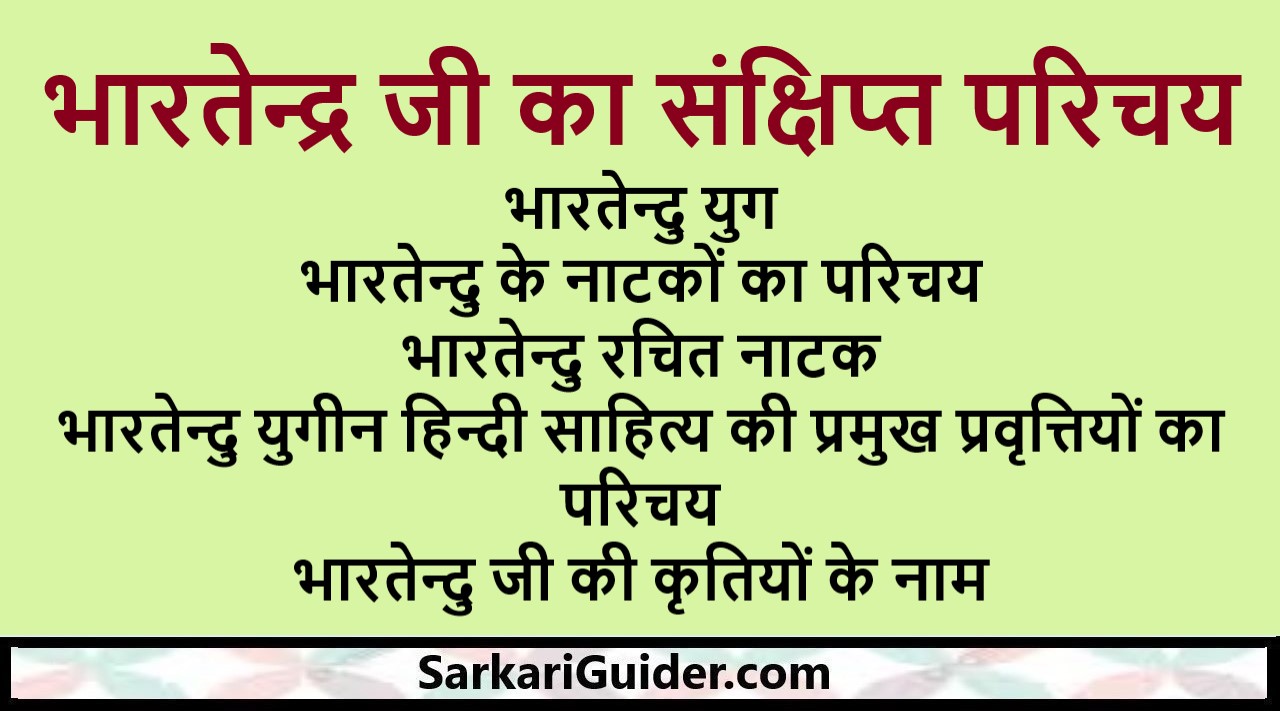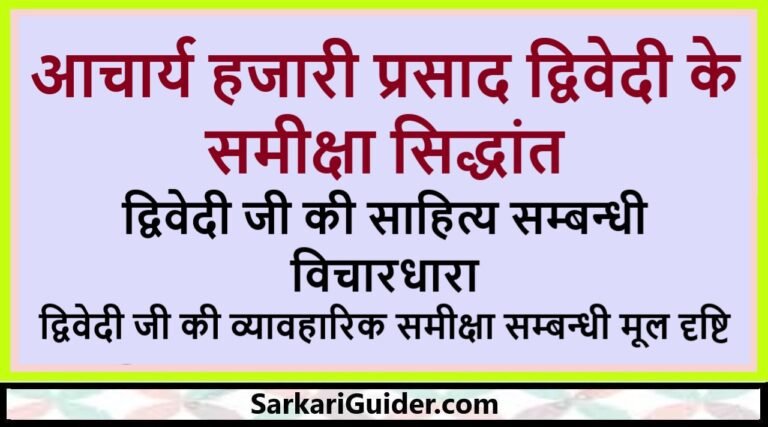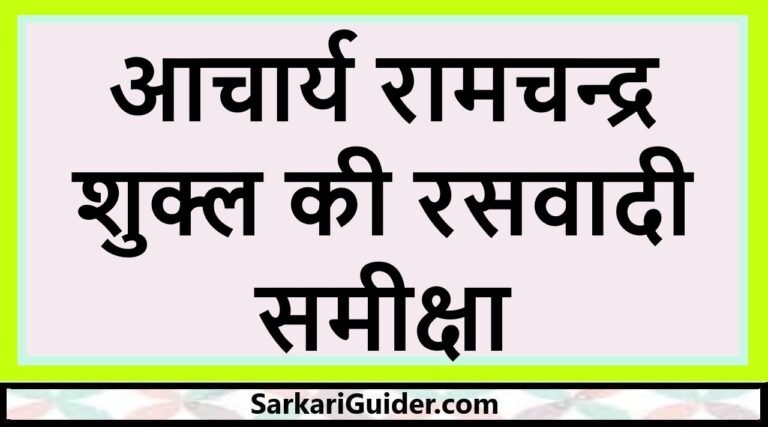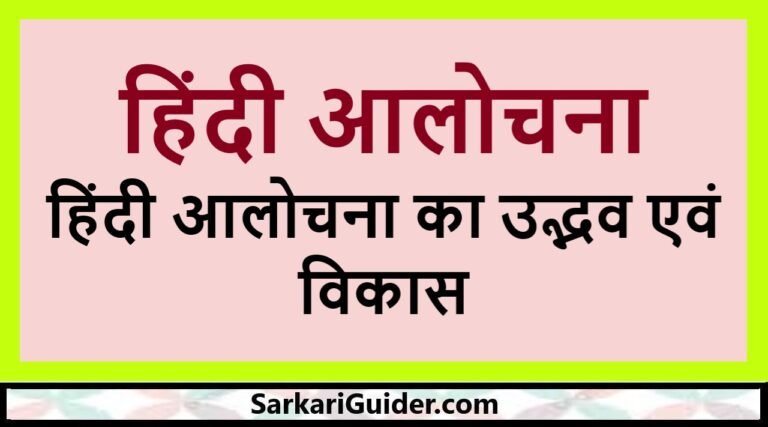भारतेन्द्र जी का संक्षिप्त परिचय | भारतेन्दु युग | भारतेन्दु के नाटकों का परिचय | भारतेन्दु रचित नाटक | भारतेन्दु युगीन हिन्दी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय | भारतेन्दु जी की कृतियों के नाम
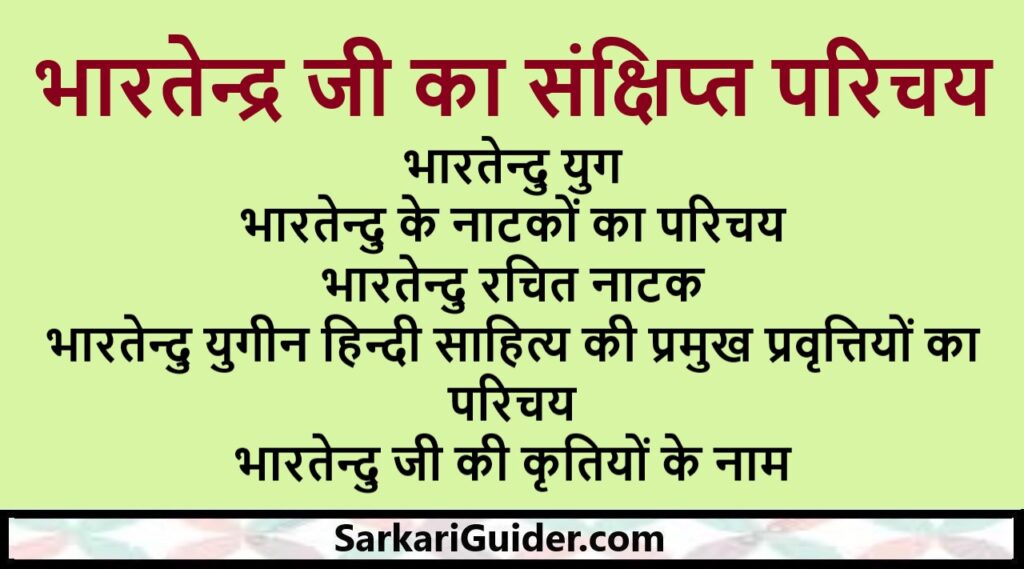
भारतेन्द्र जी का संक्षिप्त परिचय | भारतेन्दु युग | भारतेन्दु के नाटकों का परिचय | भारतेन्दु रचित नाटक | भारतेन्दु युगीन हिन्दी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय | भारतेन्दु जी की कृतियों के नाम
भारतेन्द्र जी का संक्षिप्त परिचय
भारतेन्दु हरिशन्द्र-इनका जन्म काशी के एक सम्पन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 सम्वत् 1907 को और मृत्यु 35 की अवस्था में माघ कृष्ण 6 सम्वत् 1941 को हुई।
सम्वत् 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बँगला में नए ढंग से सामाजिक, देश देशान्तर- सम्बन्धी ऐतिहासिक ओर पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिन्दी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया, सम्वत् 1925 में उन्होंने विद्यासुन्दर नाटक बैंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिन्दी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने ‘कविवचन सुधा’ नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। 1930 में उन्होंने ‘हरिचन्द्र मैगजीन’ नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरान्त ‘हरिश्चन्द्रचन्द्रिका’ हो गया। हिन्दी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले-पहल इसी ‘चन्द्रिका में प्रकट हुआ जिस प्यारी हिन्दी को देश ने अपनी विभूति समझा जिसको जनता ने उत्कण्ठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन पत्रिका में हुआ। भारतेन्दु ने नई सुधरी हुई हिन्दी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नामकी अपनी पुस्तक में नोट किया है कि ‘हिन्दी नई चाल में ढली, सन् 1873 ई०।
भारतेन्दु युग
भारतेन्दु युग आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास का प्रथम चरण है। हिन्दी में नई विचारधारा के समावेश का प्रयास इसी काल में हुआ जिसके अग्रणी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे। भारतेन्दु जी भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और नए सामाजिक सुधारों को साहित्य में स्वीकारने एवं साहित्य के माध्यम से समाज को उद्बोधित करने वाले पहले कवि थे। उनकी प्रेरणा से उस युग के समस्त साहित्यकारों ने इसी को लक्ष्य बनाया। इसीलिए इस प्रथम चरण के उन्मेष का श्रेय भारतेन्दु को है। सन् 1868 में प्रकाशित कवि वचन सुधा ने उस युग के साहित्य को प्रसारित करना आरम्भ कर दिया था। इस पत्रिका के संचालक एवं सम्पादक भारतेन्दु हरिशन्द्र जी थे। इसीलिए भारतेन्दु युग का प्रारम्भ भी सन् 1868 से माना जाता है। इस युग के प्रवर्तक भारतेन्दु जी थे। उन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा न केवल साहित्य को प्रकाश में लाने का श्लाघनीय प्रयास किया, अपितु साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी दिया। उन्होंने युगीन समस्याओं एवं सामाजिक रूढ़ियों को चित्रित करने के साथ राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रयास भी किया। भारतेन्दु ने गद्य एवं पद्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलायी।
अन्य कवि- इस युग के अन्य कवियों में बदरीनारायण चौधरी ‘प्रेमघन’ विजयानन्द त्रिपाठी, अम्बिका दत्त व्यास, राधाकृष्ण दास, पं) प्रताप नारायण मिश्र आदि उल्लेखनीय हैं।
प्रवृतियाँ- इस युग के कवियों की निम्नलिखित विशेषतायें हैं- (1) भारतीय समस्याओं का चित्रण करना (2) देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना (3) हास्य व्यंग्य एवं विनोदप्रियता, (4) इतिवृत्तात्मक (5) प्राचीन एवं नवीन काव्यधाराओं का समन्वय, (6) जनजागरण
भारतेन्दु के नाटकों का परिचय
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी नाट्य परम्परा के युग प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपने नाटकों में संस्कृत नाट्य परम्परा का अनुसरण करते हुए भी नवीनता जोड़ी है। उन्होंने पहली बार नाटकों से समाज सुधार तथा राष्ट्रीय भावना जगाने का महान कार्य किया। उन्होंने मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं-
मौलिक नाटक- भारतेन्दु जी के मौलिक नाटकों में सत्य हरिश्चन्द्र, चन्द्रावली, विषस्य विषमौसधम, भारत दुर्दशा, नील, देवी, अन्धेर नगरी, सती प्रताप, बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत जननी एवं प्रेम जोगिनी हैं।
अनूदित नाटक- विद्या सुन्दर, रत्नावली, प्रबोध चन्द्रोदय, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस भारतेन्दु जी के संस्कृत परम्परा के नाटक हैं जबकि दुर्लभ बन्धु अंग्रेजी का अनुवाद है।
भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों के माध्यम से सामाजिक कुप्रथाओं एवं कुसंस्कारों को दूर करने का पूर्ण प्रयास किया तथा भारतीय जनता को अपने देश की हो रही दुर्दशा के लिए सावधान किया।
भारतेन्दु रचित नाटक
गद्य रचना के अन्तर्गत भारतेन्दु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी ‘नाटक’ नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिन्दी में मौलिक नाटक उनके पहले दो ही लिखे गये थे महाराज विश्वनाथसिंह का ‘आनन्दरघुनन्दन नाटक’ ओर बाबू गोपालचन्द्र का ‘नेहुष नाटक’ कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रजभाषा में थे। भारतेन्दु प्रणीत नाटक ये हैं-
मौलिक- वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चन्द्रावली, विषस्य विषमौषधम् भारतदुर्दशा, नीलादेवी, अन्धेरनगरी, प्रेमयोगिरी, सतीप्रताप (अधूरा)
अनुवाद- विद्यासुन्दर, पाखण्डविडम्बन, धनंजयविषय, कर्पूरमंजरी, मुद्राराक्षस, सत्यहरिचन्द्र, भारतजननी, ‘सत्यहरिश्चन्द्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बँगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता हैं कहते हैं कि ‘भारत जननी’ उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित ‘भारतमाता’ का अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते सारा फिर से लिख डाला।
भारतेन्दु युगीन हिन्दी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय
भारतेन्दु जी के समय विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों की अपनाए हुए थे। उस समय हिन्दी गद्य की भाषा के दो प्रमुख रूप थे-एक में संस्कृतिनिष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू-फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कुछ रचनाओं की भाषा क्षेत्रीय लोकभाषाओं से प्रभावित थी, जो एक क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी थी। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। संस्कृत, उर्दू एवं फारसी के कठिन शब्दों से युक्त भाषा सामान्य जन-मानस से अपना भावात्मक सम्बन्ध नहीं जोड़ पा रही थी भारतेन्दु हरिचन्द्र का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बंगला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेन्तु जी ने बंगला के नाटक ‘विद्यासुन्दर’ का हिन्दी में अनुवाद किया है और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया।
1868 ई0 में भारतेन्दु जी ने ‘कवि-वचन सुधा’ नामक पत्रिका का सम्पादन प्रारम्भ किया। इसके पाँच वर्ष उपरान्त 1873 ई0 में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका ‘हरिचन्द्र मैगजीन’ का सम्पादन प्रारम्भ किया। आठ अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम ‘हरिश्चन्द्र पत्रिका’ हो गया। हिन्दी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिन्दी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है।
भारतेन्दु जी ने हिन्दी में संस्कृत एवं उर्दू-फारसी के जटिल शब्दों को निकालकर बोलचाल के सामान्य शब्दों का प्रयोग किया। इससे हिन्दी को एक नया रूप मिला और यह भाषा लोगों से जुड़ गई।
भारतेन्दु जी ने नाटक, निबन्ध तथा यात्रावृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य-रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आर्दश मानते थे और इनसे दिशा-निर्देश प्राप्त करते थे। सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेन्दु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने इन्हें 1800 ई0 में ‘भारतेन्दु’ की उपाधि से सम्मानित किया।
भारतेन्दु जी ने अपने युग के हिन्दी साहित्य के उत्थान हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अपने सहयोगी लेखकों को प्रोत्साहन देकर इन्होंने कई पत्रकारों का प्रकाशन प्रारम्भ कराया और उन्हें दिशा निर्देश दिया। कई साहित्यिक संस्थाएँ इनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता पर ही संचालित हो पाती थी। ये उदार हृदय से साहित्य के लिए धन दिया करते थे। इस प्रकार साहित्य के विकास हेतु इन्होंने यथासम्भव उपाय किए।
भारतेन्दु जी की कृतियों के नाम
कृतियाँ इतनी आल्पायु में ही भारतेन्दु जी ने हिन्दी को अपनी रचनाओं का अप्रीतम कोष प्रदान किया। इनके प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं।
- नाटक: भारतेन्दु जी ने मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार हैं- (i) मौलिक (1) सत्य हरिशन्द्र (2) नीलदेवी (3) श्री चन्द्रावली (4) भारत-दुर्दशा, (5) अन्धेर नगरी, (6) वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, (7) विषस्य विषमौषधम, (8) सती-प्रलाप तथा (9) प्रेम-योगिनी। (ii) अनूदित (1) मुद्राराक्षस, (2) रत्नावली (3) भारत-जननी, (4) विद्यासुन्दर, (5) पाखण्ड विडम्बन (6) दुर्लभ-बन्धु, (7) कर्पूरमंजरी तथा (8) धनंजय विजय |
- निबन्ध-संग्रह (1) सुलोचना, (2) परिहास-वंचक, (3) मदालसा, (4) लीलावती एवं (5) दिल्ली दरबार दर्पण
- इतिहास (1) कश्मीर-कुसुम (2) महाराष्ट्र देश का इतिहास तथा (3) अग्रवालों की उत्पत्ति।
- यात्रा वृतान्त (1) सरयू पार की यात्रा (2) लखनऊ की यात्रा आदि ।
- जीवनियाँ- (1) सूरदास की जीवनी (2) जयदेव (3) महात्मा मुहम्मद आदि।
हिंदी साहित्य का इतिहास– महत्वपूर्ण लिंक
- प्रगतिवाद | प्रगतिवादी की परिभाषायें | प्रगतिवाद का जन्म और विकास | प्रगतिवादी प्रमुख कवि | प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां (विशेषताएं)
- द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य | द्विवेदी युगीन पत्रकारिता | द्विवेदी युगीन काव्य को इतिवृत्तात्मक काव्य की संज्ञा क्यों दी जाती है?
- छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता | छायावाद का स्वरूप विश्लेषण करते हुए इसकी विशेषता
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]