प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधि | प्लेटो के विद्यालय सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षक सम्बन्धी विचार | प्लेटो के अनुशासन सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षा-सिद्धांत की समीक्षा | शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो का योगदान
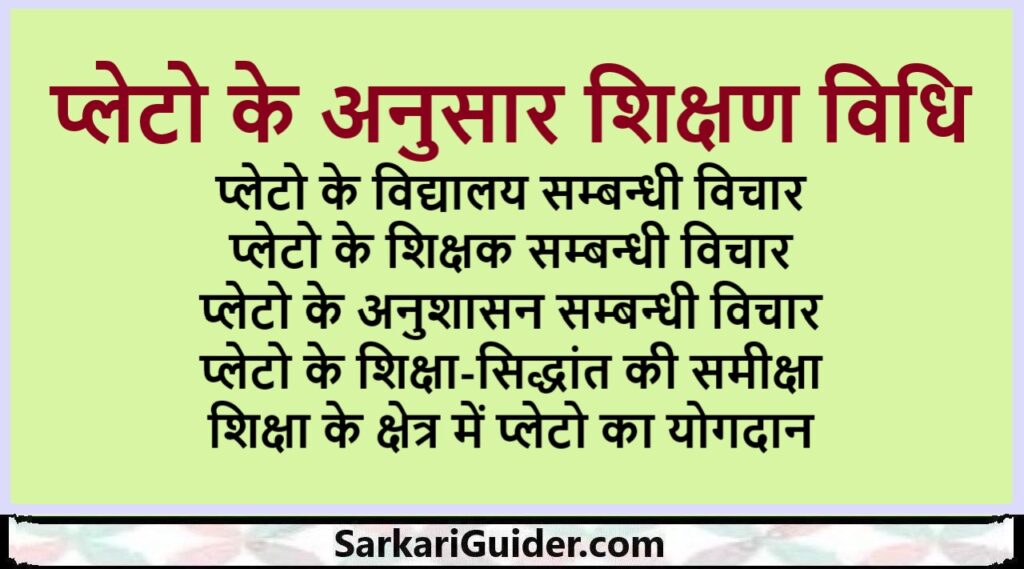
प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधि | प्लेटो के विद्यालय सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षक सम्बन्धी विचार | प्लेटो के अनुशासन सम्बन्धी विचार | प्लेटो के शिक्षा-सिद्धांत की समीक्षा | शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो का योगदान | Teaching method according to Plato. Plato’s School of Thoughts in Hindi | Plato’s thoughts on the teacher in Hindi | Plato’s Disciplinary Thoughts in Hindi | Review of Plato’s Theory of Education in Hindi | Plato’s contribution in the field of education in Hindi
प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधि
प्लेटो ने निम्नलिखित शिक्षण-विधियों का समर्थन किया है-
(1) तर्क या वाद-विवाद विधि-इस विधि को शुभारम्भ तो प्लेटो के गुरु सुकरात ने ही कर दिया था किन्तु इसका श्रेष्ठतम रूप प्लेटो की ही शिक्षा में दिखलाई पड़ता है। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए वॉयड ने अपनी पुस्तक ‘हिस्ट्री ऑव वेस्टर्न एजुकेशन में लिखा है- “तर्क क्या है? अपने शाब्दिक अर्थ में यह विचारवान् व्यक्तियों का वाद-विवाद या तर्कयुक्त राष्टीकरण है।”
(2) प्रश्नोत्तर विधि- इस विधि का सूत्रपात सुकरात के द्वारा हुआ जिसके कारण इसे श्रेयकहीं-कहीं पर सुकराती विधि भी कहा गया है। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि में तीन सोपान दिखलाई पड़ते हैं –
- उदाहरण का सोपान- इसका आरम्भ वार्तालाप से होता है।
- परिभाषा का सोपान- इसमें एक प्रकार से आवश्यक व्याख्या होती है और सामान्य गुणों का निर्धारण किया जाता है।
- निष्कर्ष का सोपान- इसमें परिणाम प्राप्त होता है।
(3) वार्तालाप विधि- इस विधि को प्रश्नोत्तर-विधि का ही एक अंग कहा जा सकता है। सुकरात, प्लेटो और आगे चलकर अरस्तु भी तर्क एवं वाद-विवाद के समय वार्तालाप किया करते थे। आज उच्च शिक्षा में यही विधि माध्यम बन गई है जहाँ पर कि इसे व्याख्यान- विधि कहा जाता है।
(4) प्रयोगात्मक- विधि– इस विधि का प्रयोग अधिकांशतः विज्ञान एवं कला-कौशल के विषयों के अध्ययन में किया जाता है। सैनिक शिक्षा, जिमनास्टिक या व्यायाम और संगीत आदि की शिक्षा में इसी विधि को अपनाने से पूर्णतया आती है।
(5) अनुकरण- विधि- प्लेटो ने अनुकरण विधि को भी अपनाने का समर्थन किया था किन्तु वह विशेषकर दासों की शिक्षा के लिए। वर्तमान युग में इस विधि का प्रयोग छोटे बच्चों की शिक्षा में अधिक होता है।
(6) स्वाध्याय-विधि- इस विधि का प्रयोग 50 वर्ष की अवस्था के बाद की शिक्षा में दिखलाई पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर दर्शन, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और अलौकिक ज्ञान के विषयों का अध्ययन स्वाध्याय-विधि से करता है।
(7) तार्किक विधि- प्लेटो की शिक्षा में तर्क-वितर्क के अधिक प्रयोग से तार्किक विधि का भी प्रयोग होना प्रायः दिखाई पड़ता है। इसमें दो प्रकार की विधियाँ आती है–आगमनात्मक एवं निगमात्मक उपर्युक्त ‘डाइलेक्टिक’ विधि में इन विधियों का भी प्रयोग साथ-साथ होता रहा है।
(8) खेल-विधि- फोटो की ‘रिपब्लिक’ में यह संकेत मिलता है कि उन्होंने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए खेल-विधि का समर्थन किया है।
प्लेटो के विद्यालय सम्बन्धी विचार
प्लेटो ने भारतीय आश्रम’ या ‘गुरुकुल’ की भाँति ही एक ‘अकादमी’ नामक संस्था की स्थापना किया। क्योंकि वह अपने गुरु सुकरात की भाँति सड़कों और गलियों में घूम-घूमकर यूनानी युवकों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि प्लेटो को एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित स्थान पर ही शिक्षा देना पसन्द था इसीलिए उन्होंने ‘अकादमी’ की स्थापना ‘किया। ‘अकादमी’ एक निश्चित स्थान पर सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित संस्था थी, अतः ऐसे ही विद्यालयों की स्थापना के लिए प्लेटो ने विचार व्यक्त किये हैं। उनके अनुसार विद्यालय ही वह स्थल है जहाँ बालक को सच्चे मानव के रूप में सामाजिक जीवन की कला सिखाया जा सकता है और उसके अंतर्निहित मानवीय गुणों को सुविकसित किया जा सकता है।
प्लेटो के शिक्षक सम्बन्धी विचार
प्लेटो ने शिक्षक के विषय में अलग से तो कहीं भी कोई विचार नहीं प्रकट किया है, परन्तु उन्होंने स्वयं अपनी ‘अकादमी’ में एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य किया। उनके गुणों एवं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श शिक्षक के गुणों तथा कर्त्तव्यों का निर्धारण किया जा सकता है। प्लेटो ने दार्शनिकों को समाज का कर्णधार एवं नेता माना है। इन्हीं दार्शनिकों में शिक्षक भी शामिल हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो प्लेटो ने शिक्षण को समाज में ऊँचा स्थान दिया है। वे एक शिक्षक से आदर्श गुणों की अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि वह अपने इन आदर्श गुणों के कारण अपने महान् कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वाह करता चलेगा।
प्लेटो के अनुशासन सम्बन्धी विचार
प्लेटो अनुशासनपूर्ण जीवन में विश्वास करते थे। उनके लिए अनुशासन एवं नियंत्रण समानार्थी थे। उन्होंने शारीरिक, मानसिक, आदेशात्मक तथा सामाजिक अनुशासन का समर्थन किया है। उन्होंने बतलाया कि आत्मानुशासन के लिए शरीर और मन दोनों का नियंत्रण आवश्यक है। इसीलिए प्लेटो ने शिक्षा का पाठ्यक्रम भी शारीरिक और मानसिक नियंत्रण को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किया है। शारीरिक नियंत्रण के लिए उन्होंने खेल-कूद, व्यायाम या ‘जिमनास्टिक’ आदि पर बल दिया तथा मानसिक नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से संगीत, कला, दर्शन और गणित के साथ विभिन्न विषयों के अध्ययन का समर्थन किया। सामाजिक अनुशासन के लिए प्लेटो ने सामुदायिक एवं सहयोगी जीवन के साथ आदेशात्मक अनुशासन का भी समर्थन किया। उनका विचार है कि “चाहे युद्धकाल हो या शान्तिकाल, प्रत्येक को अपने नेता का अनुगमन करना चाहिए।” अर्थात् नेता या बड़ों की आज्ञा का पालन करना सबका कर्तव्य है। इसी विचार से अध्यापक की आज्ञा मानना भी छात्रों का कर्त्तव्य है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो एक सीमा तक अनुशासन के दमनात्मक सिद्धांत में विश्वास करते थे। प्लेटो ने आत्मानुशासन एवं सामाजिक अनुशासन दोनों को शिक्षा के द्वारा स्थापित करना चाहा है।
प्लेटो के शिक्षा-सिद्धांत की समीक्षा
प्लेटो के शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित दोष अथवा कमियाँ दिखलाई पड़ती हैं-
दोष-
(1) प्लेटो की शिक्षा योजना मुख्यतः शासकों और प्रशासकों के लिए थी। इस प्रकार उन्होंने जन-साधारण के अधिकांश भाग को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से लाभान्वित होने का अवसर नहीं दिया।
(2) प्लेटो ने व्यावसायिक शिक्षा के विषय में अधिक कुछ नहीं कहा है। इससे उनकी निर्णय-शक्ति की अनुदारता और शिथिलता प्रकट होती है।
(3) प्लेटो ने गणित को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है और व्यावहारिक कलाओं तथा साहित्य की ओर विशेष रुचि नहीं दिखलायी है।
(4) प्लेटो ने दास प्रथा के विषय में कोई विशेष मत नहीं प्रकट किये हैं। इससे स्पष्ट है कि वह उन्हें उसी स्थिति में पड़े रहने देने के समर्थक थे।
उपर्युक्त कुछ छोटे-मोटे दोषों के होते हुए भी प्लेटो के शिक्षा-सिद्धांत उच्चकोटि के हैं। यही कारण है कि आज भी वे सिद्धांत हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। प्लेटो के शिक्षा- सिद्धान्त में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं-
गुण-
(1) प्लेटों के शिक्षा-सिद्धांत समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। उन्होंने स्त्री एवं पुरुषों की एक समान शिक्षा का समर्थन करके उक्त सिद्धान्त की पुष्टि कर दिया है।
(2) प्लेटो के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का सर्वप्रथम एवं परमावश्यक कर्तव्य है।
(3) प्लेटो ने शिक्षा को व्यक्ति के नैतिक प्रशिक्षण के लिए अत्यावश्यक माना है और उसके आध्यात्मिक पहलू पर अधिक बल दिया है।
(4) प्लेटो ने व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास पर बल दिया है। इनकी शिक्षा योजना में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास का पूरा ध्यान रखा गया है।
(5) प्लेटो के शिक्षा-सिद्धान्त वर्तमान शिक्षा एवं शिक्षाशास्त्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणा प्रदान करते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो का योगदान
(1) प्लेटो ही वह सर्वप्रथम पश्चिमी शिक्षा-दार्शनिक थे जिन्होंने एक आदर्श राज्य और शिक्षा योजना का निर्माण करके उसे कार्य रूप प्रदान किया है।
(2) प्लेटो ने ही शैशवावस्था से लेकर संपूर्ण जीवन तक की शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करके आज हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
(3) प्लेटो ने जीवन के शाश्वत मूल्यों-सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् को प्राप्त करने का साधन शिक्षा को ही बतलाया है।
(4) शिक्षा के क्षेत्र में संगीत एवं व्यायाम को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का सम्पूर्ण श्रेय प्लेटो को ही है।
(5) शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी सिद्धान्त को लाने का सिद्धान्त भी प्लेटो को ही प्राप्त है। उन्होंने समाज को प्राणी के समान माना है और उसे व्यक्ति से अधिक महत्व दिया है। इसी कारण प्लेटो ने शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा है, परिवार को नहीं।
(6) प्लेटो ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने शिक्षा को समाज का कर्णधार, शासक एवं दार्शनिक माना है।
(7) शिक्षा के क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास, खेल-कूद और व्यायाम आदि को महत्वपूर्ण स्थान देने का श्रेय प्लेटो को ही प्राप्त है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- ज्ञानोपार्जन परीक्षण | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के उद्देश्य | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के प्रकार | निबन्धात्मक परीक्षण | निबन्धात्मक परीक्षणों में सुधार
- भारत में बुद्धि परीक्षण | intelligence test in India in Hindi
- पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन | हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना | महात्मा गांधी एवं महामना मालवीय के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन
- रवीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन-वृत्त | रवीन्द्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचार | रवीन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य | रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की समीक्षा
- डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व | डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तिगत स्वभाव का संक्षिप्त चित्रण
- आदर्श शिक्षक के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन | भारतीय संस्कृति के पोषक
- प्लेटो का जीवन-वृत्त | प्लेटो की रचनाएँ | प्लेटो के दार्शनिक विचार
- प्लेटो के शैक्षिक विचार | प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य | प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षा के विभिन्न स्वरूप
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]



