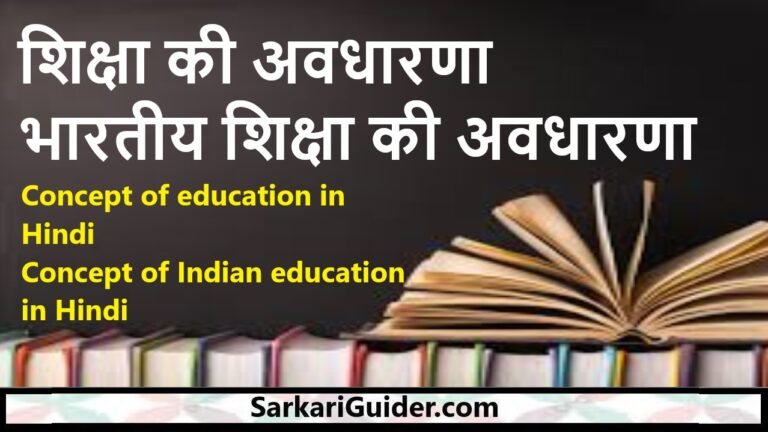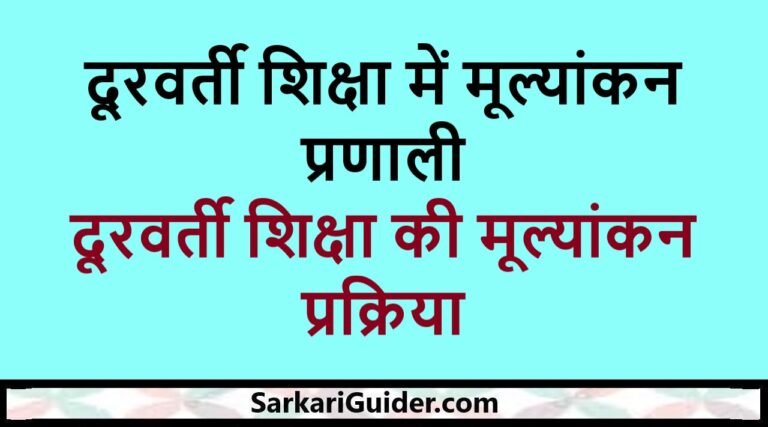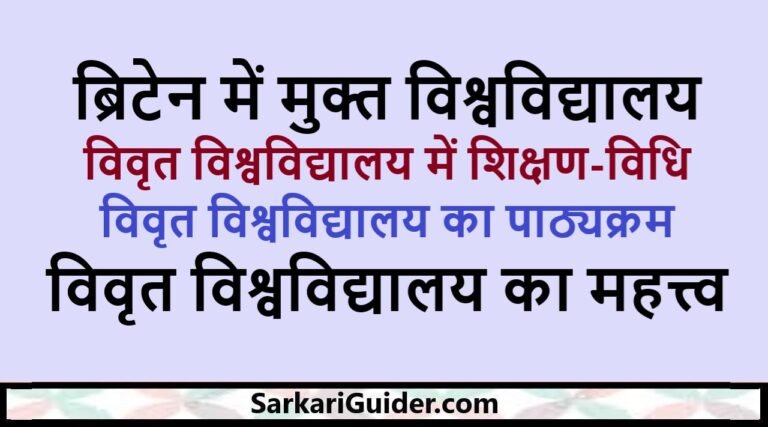सीखने का स्थानान्तरण | अधिगम स्थानान्तरण की परिभाषा | स्थानान्तरण के प्रकार | अधिगम स्थानान्तरण के सिद्धान्तवाद
सीखने का स्थानान्तरण | अधिगम स्थानान्तरण की परिभाषा | स्थानान्तरण के प्रकार | अधिगम स्थानान्तरण के सिद्धान्तवाद
प्रो० रूश ने लिखा है कि “करीब-करीब हरेक आदमी को एक नये स्थान में होने पर भावात्मक अनुभव होता है कि वह स्थान उसे परिचित हैं। यह अनुभव बहुत है। साधारण होता है। किस प्रकार कोई व्यक्ति एक स्थान या स्थिति को “याद” रखता है जहाँ वह पहले नहीं रहा? कुछ संस्कृतियों के प्राचीन लोगों ने यह धारणा बनाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि दूसरे शरीर में उसकी आत्माएँ वहाँ रह चुकी हैं। मनोविज्ञानी इस घटना को एक साधारण तत्व के स्थानान्तरण के रूप में देखता है।”
एक प्रयोजन से प्रो० रुश के शब्दों से मालूम होता है कि मनुष्य जो कुछ सीखता है उसे वह धारण किये रहता है। विद्यालय की शिक्षा के बारे में लोग आलोचना करते पाए जाते हैं कि वह कहाँ तक प्रभावकारी और उपयोगी रही है। ऐसी आलोचना में शिक्षा लेने वालों : “उदाहरण के लिए, विचार कीजिए अंकगणित के शिक्षण की जो आलोचना का सतत केन्द्र बिन्दु होता है, बहुधा व्यापारी लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनके नए काम करने वाले-हमारे स्कूलों के नए सातक पर्याप्त रूप से मूल अंकगणितीय प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है ?” (प्रो० मोर्स और विंगों) । इसका सीधा उत्तर है “अधिगम का स्थानांतरण” न होना।
सीखने के स्थानान्तरण का तात्पर्य
सभी शिक्षण और प्रशिक्षण की मुख्य कसौटी क्या है ? उत्तर सीधा है परन्तु विवेक एवं बुद्धि लगानी पड़ेगी। साधारणतः लोग इसके उत्तर में कहेंगे ही कि जो कुछ लड़के ने पढ़ा-पढ़ाया है उसे काम में लाने की योग्यता उसमें अवश्य होनी चाहिए। मनोविज्ञान में इस कसौटी को “अधिगम का स्थानांतरण’ कहा गया है। ‘अधिगम स्थानान्तरण’ इन दो शब्दों को अलग-अलग करने पर इसका अर्थ होता है “अधिगम का स्थान बदलना ।” अधिगम का स्थान विद्यालय है। यदि विद्यालय की स्थिति से उसका स्थान समाज के जीवन की स्थिति में कर दिया जाये तो अधिगम का स्थानान्तरण होता है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे ढंग से अधिगम, शिक्षण या प्रशिक्षण देना है कि विद्यार्थी समाज के पर्यावरणानुकूल अपने को समायोजित कर सके। हरेक अध्यापक की मनोभावना यही रहती है कि विद्यार्थी ने विद्यालय में जो ज्ञान, कौशल, क्रिया धारण किया, वह उसे बाद के जीवन में प्रयोग कर सके। अतः अधिगम के स्थानांतरण का तात्पर्य हुआ-विद्यालय में सीखे हुए ज्ञान, कौशल, क्रिया को सरलतापूर्वक जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में प्रयोग करना।
सीखने में स्थानान्तरण, प्रशिक्षण स्थानान्तरण, शिक्षण स्थानान्तरण- ये तीनों शब्द प्रयोग में आते हैं इसलिए हमें इन तीनों शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए। अधिगम स्थानान्तरण से तात्पर्य विद्यार्थी द्वारा स्वयं अर्जित ज्ञान कौशल का जीवन में प्रयोग करना है। शिक्षण स्थानान्तरण का तात्पर्य विद्यार्थी को अर्जित कराये गये ज्ञान-कौशल का स्थानान्तरण। शिक्षण शिक्षक की क्रिया है अर्थात् शिक्षक अधिक प्रयलशील होता है और विद्यार्थी कम परन्तु इसमें भी अधिगम या सीखना होता है अच्छा तो यह है कि हम इसे ‘सीखना’ कहें। प्रशिक्षण में सीखना-सिखाना दोनों बराबर होता है। विद्यार्थी सीखता है और शिक्षक सिखाता है, लेकिन एक विशेष नियंत्रण, अनुशासन एवं नियम के आधार पर। प्रशिक्षण का सम्बन्ध कौशल होता है। इसलिए अधिगम स्थानान्तरण, शिक्षण स्थानान्तरण एवं प्रशिक्षण स्थानांतरण में दृष्टिकोण एवं बलाघात का अन्तर पाया जाता है, वस्तुतः तीनों में अर्जित ज्ञान-कौशल का सरलतापूर्वक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने की कुशलता, प्रवीणता, योग्यता पाई जाती है।
अधिगम स्थानान्तरण की परिभाषा
(क) प्रो० डब्ल्यू० एस० मनरो- जब कोई व्यक्ति किसी विशेष उत्तेजक के प्रति अनुक्रिया करता है तो अधिगम होता है। जब अधिगम के विशेष अनुभव व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित करते हैं और उनका रूप भिन्न होता है तो वह क्रिया अधिगम-अन्तरण कही जाती है।
(ख) प्रो० क्रो और क्रो- जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत, ज्ञान, या कौशलों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह प्रशिक्षण (अधिगम) कह कर संकेत किया जाता है।
(ग) प्रो० डबल्यू० बी० कोल्सनिक- पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशलों, आदतों, अभिवृत्तियो, अथवा अन्य अनुक्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना स्थानान्तरण है।
(घ) प्रो० एच० सोरेन्सन- अधिगम अन्तरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जहाँ तक एक परिस्थिति में अर्जित योग्यताएँ दूसरी परिस्थिति में सहायता करती हैं।
निष्कर्ष- अधिगम का स्थानान्तरण मनुष्य की वह क्षमता व सप्रयोजन मानसिक प्रक्रिया है जिससे कि वह पहले सीखे हुए अधया अर्जित ज्ञान, कौशल, क्रिया का अनुप्रयोग दूसरी परिस्थिति में करता है और अपनी बाद की परिस्थिति में सुधार करता है और अपने को योग्य, प्रवीण, चतुर सिद्ध करता है।
स्थानान्तरण के प्रकार
(i) धनात्मक स्थानान्तरण ।
(ii) ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानान्तरण ।
(i) धनात्मक स्थानान्तरण- यह वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति एक परिस्थिति में ज्ञान- कौशल प्राप्त करके उसे दूसरी परिस्थिति में आसानी से अनुप्रयोग कर सकता है अथवा सरलतया समायोजित कर लेता है। धनात्मक स्थानान्तरण में बीते हुए और नवीन कार्य में समान उत्तेजना अनुक्रिया का मेल पाया जाता है। जब दो अधिगम स्थितियों में सामान्य बातें मिलती हैं तो अधिगम स्थानान्तरण सरल हो जाता है। यही धनात्मक स्थानान्तरण होता है। उदाहरण के लिए सितार बजाने वाले सरोद या बेला आसानी से बजा लेते हैं। अंग्रेजी बोलने वाला फ्रांसीसी भी बोल लेता है।
(ii) ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानान्तरण- यह वहाँ होता है जहाँ वर्तमान क्रिया से अलग अनुक्रियाओं के साथ पूर्व क्रियाओं के उत्तेजकों का सम्बन्ध प्रयत्नपूर्वक जोड़ना पड़ता है। धनात्मक स्थानान्तरण में एक पूर्व स्थिति से सीखे ज्ञान, कौशल का प्रयोग सहायक होता है परन्तु ऋणात्मक स्थानान्तरण में पूर्व स्थिति में सीखे ज्ञान, कौशल बाधक बन जाते हैं, अतएव इसमें समायोजन करना कठिन हो जाता है। परिणामस्वरूप दोनों में मेल नहीं रहता है और पूर्व अधिगम से कोई लाभ नहीं उठाया जाता है। अंग्रेजी भाषा विज्ञानी हिन्दी नहीं बोल सकता, जापान के लोग अंग्रेजी में बातचीत नहीं कर सकते यद्यपि चीनी और जापानी परस्पर एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं।
धनात्मक एवं ऋणात्मक स्थानान्तरण दोनों का महत्व होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बुरी आदतों का स्थानान्तरण ऋणात्मक ही होना चाहिए अच्छी चीजों का स्थानान्तरण धनात्मक होना चाहिए। दोनों क्रियाएँ स्वाभाविक भी कही जाती हैं क्योंकि विशेष परिस्थितियों में अधिगम होता ही रहता है। विशेषीकरण एवं अलगाव के कारण यह आवश्यक है कि ऋणात्मक स्थानान्तरण होगा। विद्यालय में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, भाषा, गणित, समाजशास्त्र सभी विषयों का ज्ञान मिलता है परन्तु एक व्यक्ति सभी को समझ ले और विभिन्न परिस्थितियों में उनका प्रयोग कर ले यह सम्भव नहीं है। यह जरूर है कि कुछ थोड़ा जो सीख लेता है उनका प्रयोग ही है फिर भी गणितज्ञ के तथ्यों से अनभिज्ञ होता है अतएव ऐसी दशा में ऋणात्मक स्थानान्तरण होगा। यही दशा कलाकार एवं विज्ञानी के अधिगम के साथ पाया जाता है।
अधिगम स्थानान्तरण के सिद्धान्तवाद
(अ) समान तत्व सिद्धान्तवाद- इसके अनुसार विषय-वस्तु में समानता होने पर एक विषय का अधिगम दूसरे में सहायक होता है। “एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उसी सीमा तक अन्तरण होता है जहाँ तक कि दोनों स्थितियों में समान तत्व या घटक पाये जाते हैं।’’
-प्रो० सोरेन्सन।
उदाहरण के लिये शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का स्थानान्तरण इसी सिद्धान्तवाद के आधार पर होता है क्योंकि दोनों विषयों की पाठ्यवस्तुओं में समानता पाई जाती है। इस सिद्धान्तवाद के पोषक एवं प्रतिपादक प्रो० थार्नडाइक ने इसका आधार स्नायविक संयोग बताया है।
(ब) सामान्यीकरण का सिद्धान्तवाद- इसके प्रतिपादक प्रो० जुड़ हैं। “एक अध्यापक यदि ज्ञान के एक क्षेत्र का एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है तो वह विद्यार्थी को सत्य का केवल सारांश मात्र की सूचना ही नहीं बल्कि संकेतों का पूर्ण रूप प्रदान करेगा जिससे कि केन्द्रीय सत्य सारे संसार को जोड़ देता है।”
-प्रो० जुड।
उदाहरण के लिए यदि दर्शनशास्त्र का व्यापक अध्ययन कर लिया जावे तो निश्चय ही उससे सभी क्षेत्रों में ज्ञान की खोज की जा सकती है। सामान्यीकरण करने में केवल सूक्ष्म सिद्धान्त ही नहीं मिलते हैं बल्कि सभी चीजों को समझना भी पड़ता है।
(स) दो तत्वों का सिद्धान्तवाद- इस सिद्धान्तवाद के प्रतिपादक प्रो० स्पीयरमैन ने लिखा है कि “विशेष योग्यता में स्थानान्तरण नहीं होता है बल्कि सामान्य योग्यता में कुछ ही होता है।”
प्रो० स्पीयरमैन ने मनुष्य में दो प्रकार की योग्यताओं को माना है सामान्य और विशेष । सामान्य योग्यता मनुष्य की वह योग्यता है जिससे ज्ञान के सभी क्षेत्र में वह पहुँचता है। इसलिए गणित का ज्ञान रखकर इतिहास, भूगोल, आदि में भी पहुँच हो जाती है। परन्तु यदि केवल गणित का ही ज्ञान दिया जावे और अन्य विषय न छुए जावें तो स्थानांतरण नहीं हो सकता।
(द) औपचारिक अनुशासन का सिद्धान्तवाद- प्रो० ग्लेशब्रुक ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “स्मृति नैतिक अध्ययनों से प्रशिक्षित होती है बल्कि भाषा एवं इतिहास में सबसे अधिक उच्च भाषा अध्ययनों से रुचि प्रशिक्षित होती है और अंग्रेजी साहित्य से और अच्छी तरह से, कल्पना सभी उच्चतर शिक्षण से बल्कि मुख्यतः ग्रीक और लैटिन कविता से, निरीक्षण प्रयोगशाला में विज्ञान के कार्य में प्रशिक्षित होता है।”
इस प्रकार के विचार एवं सिद्धान्तवाद का आधार शक्ति मनोविज्ञान है। हरेक विषय मस्तिष्क की अलग-अलग शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। परन्तु अब इस सिद्धान्तवाद एवं मनोविज्ञान को महत्व नहीं देते।
(इ) समग्रवादी सिद्धान्तवाद- इसके मानने वाले विषयवस्तु एवं अधिगम क्रिया के पूर्णाकार पर बल देते हैं। सूझ या अन्तर्दृष्टि के साधन से समन अधिगम होता है और एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानान्तरण होता है। प्रो० कोहलर के प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों से पता चला है कि “सामान्य प्रशिक्षण में अत्यधिक महत्व की बात है अपनी सभी सम्बन्ध के साथ परिस्थिति में अन्तर्दृष्टि होना ।” यदि मनुष्य एक परिस्थिति में अपनी सभी शक्ति उसे समझने में लगा देता है तो उसे तत्सम्बन्धी सूझ या अन्तर्दृष्टि होती है। ऐसी अन्तर्दृष्टि सभी प्रकार के ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक होती है और इसका प्रशिक्षण अभ्यास से किया जाता है। अभ्यास होने पर अधिगम का स्थानांतरण होता है, यह इस सिद्धांतवाद के द्वारा बताया गया है।
(फ) मूल्य-प्रत्यभिज्ञान का सिद्धांतवाद- इसका प्रतिपादन करने वाले प्रो० बैग्ले ने कहा है कि किसी ज्ञान और क्रिया के सम्पादन एवं अर्जन करने के लिए कुछ आदर्श को मान्यता देना आवश्यक है। ऐसी मान्यता या प्रत्यभिज्ञान के आधार पर अधिगम का स्थानांतरण सम्भव होता है। उदाहरण के लिए एक छात्र यदि कविता याद करता है क्योंकि उसमें सत्य, अहिंसा, वीरता के आदर्श है तो इसका स्थानांतरण इतिहास, गणित, विज्ञान के अध्ययन में हो सकता है क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ मूल्य एवं आदर्श सामान्यतः मिलते हैं। इसके स्पष्टीकरण में प्रो. सारी और टेलफोर्ड ने कहा है कि सामान्यीकरण पूरी कहानी नहीं है बल्कि उसके साथ एक आदर्श भी हो और एक संवेगात्मक अन्तर्वस्तु हो । कहना यह है कि सामान्यीकरण गुणांकन के साथ अवश्य होना चाहिए यदि स्थानांतरण को पूरा किया जाना है।”
यदि मनुष्य में किसी ज्ञान के मूल्य की परख-क्षमता आ जाये और वह उसका गुणांकन कर ले तो वह उस आदर्श के आधार पर भी अन्यत्र वह अधिगम कर सकता है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ | मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषाएँ | मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्त्व
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र | विद्यालयी बालक की व्यवहार सम्बन्धी समस्यायें
- मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ | मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण
- मानसिक अस्वास्थ्य | मानसिक अस्वस्थता के प्रकार
- मानसिक अस्वस्थता के कारण | मानसिक अस्वस्थता का उपचार | साधारण मानसिक अस्वस्थता का उपचार | गम्भीर मानसिक अस्वस्थता का उपचार
- मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम के तरीके | मानसिक अस्वस्थता के उपचार के उपाय
- बालकों का मानसिक स्वास्थ्य | पाठशाला के बालकों में मानसिक स्वास्थ्य | मानसिक स्वास्थ्य के संवर्द्धन में परिवार की भूमिका
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]