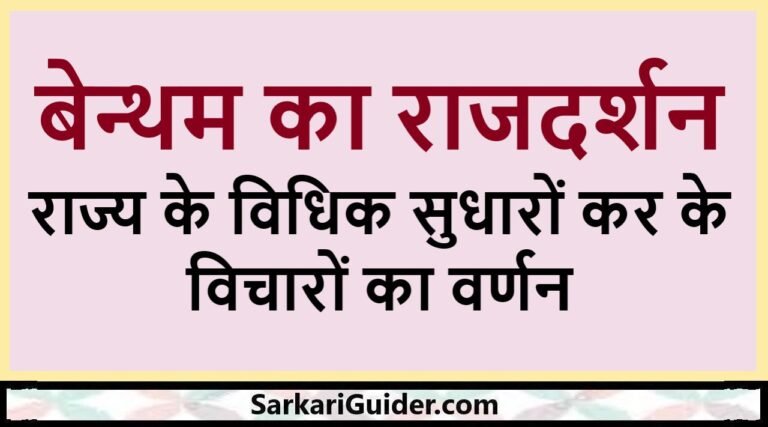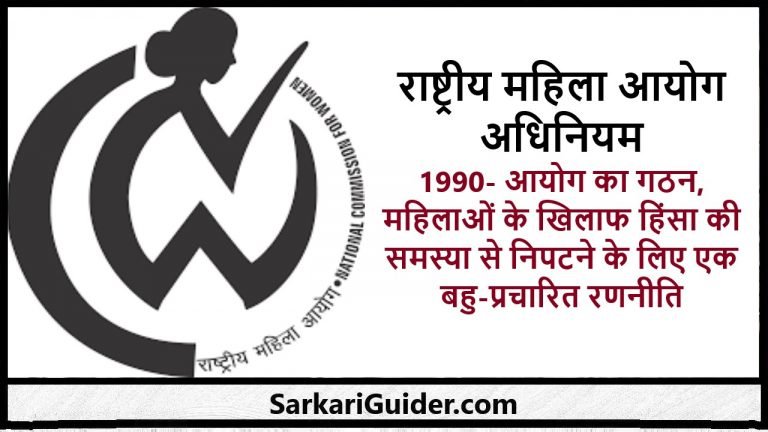भारत में संघवाद | Federalism in India in Hindi

भारत में संघवाद | Federalism in India in Hindi
भारत (India) में संघवाद
भारत का संविधान संघात्मक है। किन्तु इसमें अनेक ऐसी विशेषताएँ भी हैं जिनके कारण इसे एकात्मकता की ओर झुका हुआ बताया जाता है। चूंकि संविधान का रूप संघात्मक है, अतएव यह आवश्यक है कि संघ और सरकारों के अधिकार-क्षेत्र अलग-अलग हो तथा उसमें आपसी सम्बन्ध भी हों। यह सच है कि विभिन्न राज्य अपने-अपने क्षेत्र में स्वाधीन हैं। फिर भी सम्पूर्ण देश में शान्ति एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व अन्तिम रूप में संघ सरकार पर ही है। संघ शासन की सफलता विभिन्न सरकारों के आपसी सहयोग पर निर्भर करती है। संघ और राज्यों के आपसी सम्बन्धों को मुख्यतः तीन शीर्षकों के अन्तर्गत विवेचन किया जायेगा-
(1) विधायी सम्बन्ध
संघ एवं राज्यों के विधायी सम्बन्धों का संचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता है जिनको संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का नाम दिया जाता है।
(1) संघ सूची- इस सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में एक प्रकार की नीति का अनुकरण आवश्यक कहा जा सकता है। इस सूची के सभी विषयों पर विधि- निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं-रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध तथा सन्धि, देशीयकरण, नागरिकता, रेल, बन्दरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन तथा बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंकिग, बीमा आदि।
(2) राज्य सूची- इस सूची में साधारणतः वे विषय रखे गये हैं जो क्षेत्रीय महत्त्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को ही प्राप्त है। इस सूची में 62 विषय हैं, जिनमें कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं-पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और सड़कें इत्यादि । मूल रूप से इस सूची में 66 विषय पाये जाते थे, लेकिन संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार इस सूची में से शिक्षा, वन, नाप-तोल, पशु-पक्षियों की रक्षा समवर्ती सूची में शामिल कर दिये गये हैं।
(3) समवर्ती सूची- समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। उदाहरणार्थ, इसमें बिजली, दीवानी कानून, पागलखाने, जीवनसम्बन्धी महत्वपूर्ण आँकड़े, जिनमें जन्म और मृत्यु सम्बन्धी आँकड़े भी शामिल हैं, फौजदारी कानून, समाचारपत्र, पुस्तकें, छापेखाने, विवाह कानून, आर्थिक और सामाजिक योजना कानून, मूल्य नियन्त्रण और खाद्य-पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मिलावट इत्यादि शामिल हैं। मूल रूप से इस सूची में 47 विषय सम्मिलित थे। लेकिन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, नाप-तोल, पशु-पक्षियों की रक्षा, जनसंख्या नियन्त्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
समवर्ती सूची पर राज्य के विधान मण्डलों और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु संविधान में लिखा गया है कि यदि दोनों एक-दूसरे के विरोधी कानून बना दें तो उस समय राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्मित कानून रद्द समझा जायेगा और संसद का कानून लागू होगा।
(4) अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers)- भारतीय संविधान में इन्हें केन्द्र को दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विषय जो न तो राज्य सूची में हैं, न संघ सूची में और न ही समवर्ती सूची में हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा।
विधायी सम्बन्धों की समीक्षा- ऊपर लिखे हुए केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष प्रयल किये गये हैं। न केवल संसद को संघ-सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है बल्कि निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है l
(1) राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर।
(2) राज्यों के विधान मण्डल द्वारा प्रार्थना करने पर।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए भी संसद कानून बना सकती है।
(4) राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर।
(5) संकट काल की घोषणा होने पर।
चूँकि शेष शक्तियाँ केन्द्र को दी गई हैं, अतः केन्द्र की शक्तियाँ सदैव बढ़ती रहेंगी और राज्यों की शक्तियाँ सीमित रहेंगी।
(2) प्रशासकीय सम्बन्ध
श्री दुर्गादास बसु के शब्दों में—“संघीय व्यवस्था की सफलता और दृढ़ता संघ की विविध सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है।” भारतीय संविधान- निर्माता इस तथ्य से परिचित थे, इसी कारण प्रशासनिक सम्बन्धों की व्याख्या करते जहाँ राज्यों को अपने-अपने क्षेत्र में सामान्यतः स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, वहाँ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि राज्यों के प्रशासकीय यन्त्र पर संघ का नियन्त्रण बना रहे और संघ तथा राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की भावना रहे। राज्य सरकारों पर संघीय शासन के नियन्त्रण की व्यवस्था निम्नलिखित उपायों के आधार पर की गई है-
(1) राज्य सरकारों को निर्देश- केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश सामान्यतया संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल समझे जाते हैं, लेकिन भारतीय संघ में केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश देने की व्यवस्था है।
(2) राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंपना- संघीय सरकार राज्य सरकारों को कोई भी कार्य सौंप सकती है। यदि राज्यों की सरकार या उसके अधिकारी उसे पूरा न करें, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संकटकालीन घोषणा कर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लें
(3) अखिल भारतीय सेवाएँ- संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की भी व्यवस्था है जो संघ तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य है। इन्हें अखिल भारतीय सेवायें कहते हैं और इन सेवाओं के अधिकारियों पर संघीय सरकार का विशेष नियन्त्रण रहता है।
(4) सहायता-अनुदान- संघीय शासन राज्यों को आवश्यकतानुसार सहायता एवं अनुदान भी दे सकता है। अनुदान देते समय संघ राज्यों पर कुछ शर्ते लगाकर उनके व्यय को भी नियन्त्रित कर सकता है।
(5) अन्तर्राज्यीय नदियों पर नियन्त्रण- संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यीय नदी अथवा इनके जल के प्रयोग, वितरण या नियन्त्रण के सम्बन्ध में व्यवस्था करें।
(6) अन्तर्राज्यीय परिषद्- विभिन्न राज्यों के पारस्परिक विवादों की जाँच करने और लोकहित की रक्षा की दृष्टि से उनके सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अन्तर्राज्यीय परिषदों (Inter-State Councils) की स्थापना कर सकता है।
(7) राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति- इन सबके अतिरिक्त राज्य सरकारों पर संघीय शासन के नियन्त्रण का एक प्रमुख उपाय यह है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है जो वहाँ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
प्रशासकीय सम्बन्धों की समीक्षा- इस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र में राज्यों पर भारत सरकार का प्रभावपूर्ण नियन्त्रण है। लेकिन इसके साथ ही यह नहीं भूल जाना चाहिये कि ये प्रावधान बहुत अधिक सावधानीपूर्वक और केवल संकट काल में ही उपयोगी हैं। सामान्यतया राज्यों को कानून निर्माण और प्रशासन के सम्बन्ध में अपने निश्चित क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी।
(3) वित्तीय सम्बन्ध
वित्तीय क्षेत्र में भी संविधान के द्वारा संघ एवं राज्य सरकारों के क्षेत्र पृथक्-पृथक् हैं। दोनों सरकारें सामान्यतया अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करती हैं। इस सम्बन्ध में संविधान द्वारा की गई व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार है-
(1) संघीय आय के साधन- संघ सरकार को आय के अलग साधन प्राप्त हैं। इन साधनों में कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, उत्पादन शुल्क, निगम कर, कम्पनियो के मूलधन पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति शुल्क आदि प्रमुख है।
(2) राज्यों की आय के साधन- वित्त के क्षेत्र में राज्य की सरकारों की आय के साधन भी अलग कर दिये गये हैं। उनमें भू-राजस्व, कृषि, आय कर, कृषि भूमि का उत्तराधिकारी शुल्क एवं सम्पत्ति शुल्क, मादक वस्तुओं पर उत्पादन कर, बिक्री कर, यात्री कर, मनोरंजन कर और दस्तावेज कर आदि प्रमुख हैं।
(3) व्यय की प्रमुख मदें- संघीय शासन के व्यय की मुख्य मदें सेना, परराष्ट्र सम्बन्ध आदि हैं, जबकि राज्य शासन के व्यय की मुख्य मदें पुलिस, कारावास, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वशासन आदि हैं।
(4) राज्यों को वित्तीय सहायता- क्योंकि राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त साधन पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये संघ शासन द्वारा राज्यों की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है-
(i) केन्द्रीय करों का राज्यों को अनुदान- प्रथम प्रकार के कर ऐसे हैं जो केन्द्र द्वारा लगाये और वसूल किये जाते हैं, पर जिनकी सम्पूर्ण आय राज्यों को बाँट दी जाती है। इस प्रकार के करों में प्रमुख रूप से उत्तराधिकार कर, सम्पत्ति कर तथा समाचारपत्र कर आदि आते हैं।
(ii) राज्यों द्वारा केन्द्रीय करों का उपयोग- द्वितीय प्रकार के कर वे हैं जो केन्द्र निर्धारित करता है किन्तु राज्य एकत्रित करते हैं और उसे प्रयोग में लाते हैं। स्टाम्प शुल्क का कर ऐसा ही कर है। केन्द्र शासित क्षेत्रों में इन करों की वसूली केन्द्रीय सरकार ही करती है।
(iii) करों का संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन- तृतीय श्रेणी के कर वे हैं जो केन्द्र द्वारा लगाये तथा वसूल किये जाते हैं पर जिनकी शुद्ध आय संघ और राज्यों के बीच बाँट दी जाती है। कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर प्रमुख रूप से इसी प्रकार का कर है।
(iv) राज्यों को अनुदान- संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार जिन राज्यों को संघ विधि द्वारा जिन राज्यों को अनुदान देना निश्चित करे, उन राज्यों को अनुदान दिया जायेगा। ये अनुदान पिछड़े हुए वर्गों को ऊँचा उठाने और अन्य वविकास योजनाओं को पूरा करने के लिए दिये जायेंगे।
(v) सार्वजनिक ऋण प्राप्ति की व्यवस्था- संघीय सरकार अपनी संचित निधि की जमानत पर संसद की आज्ञानुसार ऋण ले सकती है तथा संघ सरकार विदेशों से भी ऋण ले सकती है। राज्यों की सरकारें भी विधान मण्डल के द्वारा निर्धारित सीमा तक ऋण ले सकती हैं। संघीय सरकार विदेशों से भी ऋण ले सकती है किन्तु राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकतीं।
(6) वित्त-आयोग– संविधान के अनुच्छेद 280 में व्यवस्था की गई है कि प्रति 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। इस आयोग के द्वारा संघ और राज्य सरकारों के बीच करों के वितरण, भारत की संचित निधि में से धन के व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य विषयों की सिफारिशें करने का कार्य किया जायेगा।
(7) महालेखा नियन्त्रक तथा परीक्षक द्वारा नियन्त्रण- भारत सरकार का लेखा नियन्त्रक एवं परीक्षक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के हिसाबों की निष्पक्ष तरीके से जाँच करता है।
(8) वित्तीय संकटकाल- यदि देश में वित्तीय संकटकाल की घोषणा कर दी जाती है तो केन्द्र सरकार वित्तीय क्षेत्र में राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के मंत्रियों, कर्मचारियों के वेतन में भी कमी कर सकती है।
संघ और राज्य में उपर्युक्त वित्तीय सम्बन्धों की डॉक्टर जेनिंग्स ने कड़ी आलोचना की है। उनके विचार में राज्यों को केन्द्रीय सरकार पर बहुत निर्भर बना दिया गया है। योजना- आयोग का भी राज्यों के ऊपर प्रतिदिन नियन्त्रण बढ़ता जा रहा है।
वस्तुतः हमारे संविधान द्वारा विधायी, प्रशासकीय तथा वित्तीय क्षेत्रों में संघ सरकार को इकाई राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
राजनीतिक शास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- अधिनायकतन्त्र किसे कहते हैं? | आधुनिक अधिनायकतंत्र | आधुनिक अधिनायकतन्त्र के लक्षण | अधिनायकतन्त्र के गुण | अधिनायकतन्त्र के दोष | आधुनिक अधिनायकतन्त्र के उदय के प्रमुख कारण | तानाशाही शासकों के प्रमुख गुण तथा दोष
- संसदीय व्यवस्था एक दलीय सरकार और मिलीजुली सरकार | संसदीय व्यवस्था | दलीय सरकार | मिलीजुली सरकार | मिलीजुली सरकारों के लक्षण
- मिलीजुली सरकार के प्रमुख प्रतिमान | Major Patterns of Combined Government in Hindi
- संघवाद का अर्थ | संघवाद की परिभाषाएँ | संघवाद के आधारभूत सिद्धान्त | एकात्मक और संघात्मक सरकारें | एकात्मक और संघात्मक सरकारों में अन्तर | एकात्मक सरकार के गुण | एकात्मक सरकार के दोष
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]