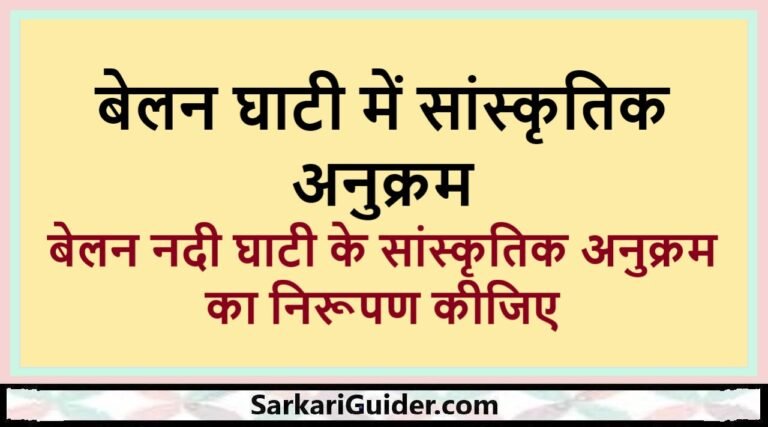स्तूप वास्तुकला | स्तूप वास्तु का उद्भव व विकास | भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका
स्तूप वास्तुकला | स्तूप वास्तु का उद्भव व विकास | भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका
स्तूप वास्तुकला
स्तूप वास्तु का उद्भव व विकास-
हमारे देश में अतिप्राचीन काल संभवतः रामायण एवं महाभारत से भी पूर्व वैदिक युग से, स्तूप निर्माण की परम्परा प्रचलित है। वैदिक आर्यों में मृत व्यक्ति को दफनाने की परम्परा थी। ऋग्वेद के 10/18/10/19 मंत्र में पृथ्वी से यह प्रार्थना की गई है कि वह मृत व्यक्ति को कोमलता के साथ अपनी गोद में स्थान दे, उसकी मिट्टी उसे अपने भार से न दबाये। वैदिक युग में शव-समाधियों के ऊपर मिट्टी का तूदा निर्मित कर दिया जाता था, तथा कभी-कभी दार-क्रिया के पश्चात् अस्थियों को एकत्र कर, उन्हें दफना दिया जाता था। ऐसी स्मारक समाधियों के ऊपर निर्मित मिट्टी के तूदे ही, स्तूप के प्राचीन रूप हैं। उत्तरी बिहार के लोरिया नन्दनगढ़ में इसी प्रकार की एक समाधि प्राप्त हुई है। विद्वानों ने इस समाधि का समय लगभग 700-800 ई० पू० माना है। वैदिक काल में कभी-कभी प्रस्तर को गोल तथा अन्दर से खोखला कर, उसमें अस्थियाँ रख दी जाती थीं। प्रस्तर से निर्मित ऐसे स्मारक पात्र को ‘लयण’ कहा जाता है। लयण के बीच छेद में प्रस्तर का पतला सा डंण्डा रख दिया जाता था। मलाबार- तट पर मन्त्रापुरम में इसी प्रकार का एक लयण मिला है। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जुये दुब्रुइल ने इस लयण को वैदिकयुगीन खोखला स्तूप बतलाया है।
‘भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका’-
नामक पुस्तक में स्तूप के विषय में लिखा है- “स्तूप अपने आरम्भिक रूप में शव-समाधि से सम्बद्ध रहा है।” पहले स्तूप का उद्देश्य केवल अस्थि संचय था, तदुपरान्त वे निर्वाण या महत्त्वपूर्ण घटनाओं इत्यादि के स्मारक भी बन गये तथा तब उनका निर्माण बिना उन्हें अस्थि स्थापना के लिये खोखला बनाये जग्गुरत के सदृश्य केवल ठोस प्रस्तर, ईंट अथवा मिट्टी का होने लगा। वह केवल भक्ति कार्य था।”
यद्यपि, प्रस्तर से बने लयण अथवा मिट्टी के तूदे के रूप में स्तूप बनाने की परम्परा वैदिकयुग से ही प्रचलित है तथापि स्तूप परम्परा का वास्तविक इतिहास बौद्ध एवं जैन धर्मों के साथ आरम्भ होता है। यदि जैन एवं बौद्ध धर्मों को स्तूप परम्परा का जन्मदाता कहा जाय तो अनुचित न होगा। आज, जितने भी स्तूप अथवा उनके ध्वंसावशेष प्राप्त हैं, वे समस्त अवशेष बौद्धों एवं जैनों के ही हैं। जैनों के स्तूप तो लगभग खण्डित हो चुके हैं, केवल बौद्ध स्तूप ही आज विद्यमान हैं। हिन्दू समाधि स्तूप के रूप में विकसित न हो सकी। इसका प्रमुख कारण यह था कि उपनिषदों के आध्यात्मिक ज्ञान आन्दोलन की प्रचण्डता में, किसी शव-समाधियों द्वारा अमर हो जाने के विचार लुप्त हो गये।
बौद्ध धर्म की परम्परा में स्तूप का निर्माण ‘स्मारक’ के रूप में किया गया। बौद्ध धर्म ग्रन्थ ‘महापरिनिब्बासुत्त’ में स्तूप चार प्रकार के बताये गये हैं (1) तथागत के स्मारक, (2) प्रत्येक बुद्ध के स्मारक, (3) मुख्य बौद्ध-श्रावकों के स्मारक तथा (4) चक्रवर्ती राजाओं के स्मारक। इनके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध की प्राचीन खण्डित प्रतिमाओं अथवा चिन्हों के ऊपर उनके प्रति सम्मान अभिव्यक्त करने की भावना से, बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध घटनाओं एवं स्थानों को अमर एवं पूजनीय बनने के उद्देश्य से और बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ व दान देने हेतु भी, कालान्तर में स्तूप निर्मित किये जाने लगे। मौर्यों से पूर्व तथा मौर्ययुगीन स्तूपों का आकार छोटा होता था। तदुपरान्त छोटे स्तूपों को बड़े रूप में परिवर्तित करने की परम्परा का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथ “महावंश” में महेशाख्य (बड़े) स्तूपों को ‘महाथूप’ अथवा “महाचेतिय’ कहा गया है। इसी ग्रंथ में महाचेतिय के निर्माण की विधि भी विस्तारपूर्वक दी गई है। स्तूप बनाने से पहले, भूमि का चुनाव, भू परीक्षा, भूमिपूजा, वास्तु-पुरुष विकल्पना इत्यादि वास्तु शास्त्री कार्य किये जाते थे
महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्, उनकी अस्थियों को आठ बौद्ध राजाओं में विभक्त कर दिया गया था। इनमें से प्रत्येक स्माट ने अपने-अपने हिस्से पर महात्मा बुद्ध की स्मृति में समाधि बनवाई थी। लेकिन आज इनमें से एक भी समाधि उपलब्ध नहीं है। सम्राट अशोक से पहले की मात्र दो बौद्धं समाधियाँ उपलब्ध हुई हैं-
इनमें से एक समाधि का रूप टीलों के समान है तथा दूसरी समाधि स्तूप के रूप में है। लौरिया नन्दनगढ़ पाटलिपुत्र से लुम्बिनी जाने वाले मार्ग पर, चम्पारण जिले में ये समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ मिट्टी के अनेक प्राचीन तूदे भी प्राप्त हुए हैं, जिनको शव समाधियों के रूप में निर्मित किया गया था। कनिंघम महोदय के विचार में ये तूदे विज्जियों के ऊर्चा-स्मारक थे ब्लॉख महोदय ने इन्हें वैदिक समाधि माना बस्ती जिले में पिपरवा में प्राङ्ग मौर्यकालीन एक स्तूप मिला है। ‘डब्ल्यू० सी० पेप्पी ने इस स्तूप की खोज की थी। इस स्तूप का धरातल पर व्यास 116 फीट तथा ऊँचाई 22 फीट है। यह स्तूप अशोक से भी पुराना है तथा संभवतः महात्मा बुद्ध के कुछ समय पश्चात् निर्मित हुआ होगा। पिपरवा में ही, उत्खनन में ब्राह्मी लिपि में लिखित एक स्थित मंजूषा व स्वर्ण-पत्र पर अंकित एक स्त्री-मूर्ति भी प्राप्त हुई है।
सम्राट अशोक का, बौद्ध स्तूपों के निर्माण की परम्परा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उसने कलिंग युद्ध के उपरान्त बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा अपने पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघामित्रा को भी बौद्ध धर्मानुयायी बनाकर, सम्पूर्ण भारतवर्ष तथा विदेशों तथा चीन, स्याम, लंका, तिब्बत इत्यादि में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये भेजा। अशोक ने महात्मा बुद्ध की स्मृति में व बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने हेतु भारत एवं अफगानिस्तान में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कतिपय पालिग्रन्थों में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों की संख्या 84 लाख तक बतायी गयी है। अशोक के लगभग 900 वर्ष पश्चात् चीनी यात्री हेनसांग भारत आया। उसने मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, कन्नौज, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु वैशाली, थानेश्वर, बनारस गया इत्यादि स्थानों का भ्रमण किया। इन विभिन्न स्थानों पर उसने अशोक द्वारा निर्मित सैकड़ों स्तूप देखे। इन स्तूपों की ऊंचाई 70 से 300 फीट तक थीं। इन समस्त स्तूपों का वर्णन अपने यात्रा-विवरण में विस्तारपूर्वक किया है। काबुल एवं पेशावर के मध्य नगरहार नामक जगह पर अशोक द्वारा निर्मित 300 फुट ऊँचा स्तूप भी ह्वेनसांग ने देखा था। अशोक के समय के निर्मित अनेक स्तूप अब नष्ट हो गये हैं। तत्कालीन शेष स्तूपों में भरहुत, साँची, सारनाथ एवं तक्षशिला के स्तूप विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं।
तक्षशिला में अशोक ने अपने पुत्र कुणाल की यादगार में भी एक स्तूप का निर्माण करवाया था। आरम्भ में यह स्तूप छोटा होगा तदुपरान्त अशोक के उत्तराधिकारियों ने इस स्तूप को विशाल रूप प्रदान किया। इस स्तूप का नाम अशोक के समय में ‘कुणाल स्तूप’ था, कालान्तर में धर्मराजिका स्तूप के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। पुरातत्व विभाग ने तक्षशिला की खुदायी में कुणाल स्तूप के अवशेष खोज निकाले हैं। कतिपय विद्वानों ने इस स्तूप को मौर्यकाल के उपरान्त का बताया है।
वाराणसी के निकटवर्ती स्थान सारनाथ में भी, अशोक ने एक विशाल स्तूप निर्मित करवाया था। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने ‘धर्मचक्र’ का प्रवर्तन किया था। अब इस स्तूप का केवल तल का भाग ही शेष रहा है। सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार “अब से कुछ वर्ष पूर्व तक यह स्तूप विद्यमान था, पर सन् 1793-94 में काशी के नरेश चेतसिंह ने अपने दीवान बाबू जगतसिंह के नाम से जगतगंज मुहल्ला बनवाने हेतु इस स्तूप को तुड़वाकर इसके ईंट प्रस्तर आदि मंगवा लिये थे।” इस स्तूप के तल को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह गोल आकार का स्तूप था, तथा इस स्तूप का व्यास लगभग 60 फुट रहा होगा। स्तूप के निकट ही एक पाषाण वेदिका प्राप्त हुई है। यह वेदिका एक बड़े प्रस्तर को काटकर निर्मित की गई है, जो बेजोड़ है। उसके ऊपर चमकीली पॉलिश, आज भी यथावत् है। इसके सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह वेदिका, धर्मराजिका स्तूप की हर्मिका थी, जो कालान्तर में गिर जाने पर पृथक् स्थान पर रख दी गयी होगी।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- भरहुत की स्तूप | भरहुत में निर्मित स्तूप का संक्षिप्त परिचय
- सांची का स्तूप | सांची का बड़ा स्तूप | सांची के अन्य स्मारक
- अमरावती का स्तूप | बोध गया का स्तूप
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]