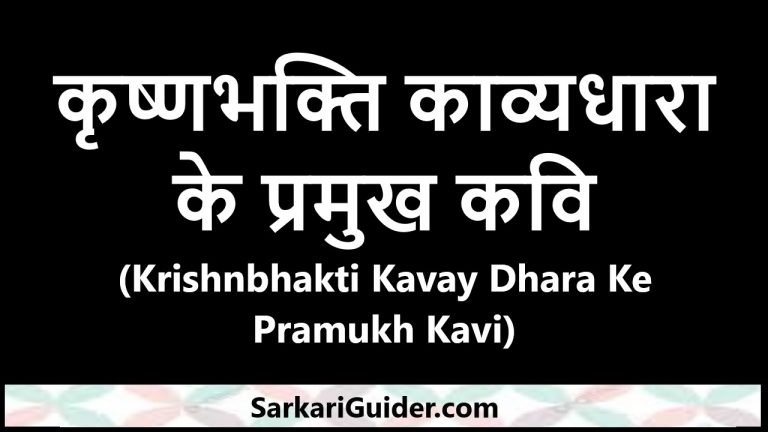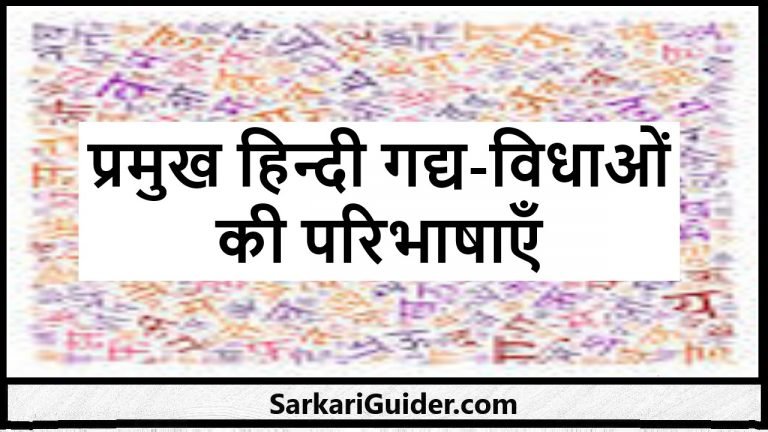रहस्यावादी काव्य की विशेषताएँ | रहस्यवाद की परिभाषा | रहस्यवाद के प्रकार | हिंदी के रहस्यवादी कवि और उनका काव्य | आधुनिक युग का रहस्यवादी काव्य | हिंदी रहस्यवादी काव्य की विशेषताएँ
रहस्यावादी काव्य की विशेषताएँ | रहस्यवाद की परिभाषा | रहस्यवाद के प्रकार | हिंदी के रहस्यवादी कवि और उनका काव्य | आधुनिक युग का रहस्यवादी काव्य | हिंदी रहस्यवादी काव्य की विशेषताएँ
रहस्यावादी काव्य की विशेषताएँ
प्रस्तावना
कवि युगों से प्रकृति में व्याप्त रहस्य को समझने के लिए प्रयास करता जा रहा है। उनके इसी सतत प्रयास ने रहस्यसमयी भावनाओं का बीजारोपण किया है। आदिकाल से ही वह विश्व में व्याप्त रहस्यात्मक सत्ता के प्रति अनुरक्त रहा है। अपनी इसी अनुरक्तता के कारण ही पंत सरीखा कवि व्याकुल एवं भाव विभोर होकर पूछ उठता है।
कौन तुम कौन अये द्युतिमान?
फूंक देते रंधों में प्राण।
हिंदी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ प्रत्येक युग के काव्य से मिलती हैं।
रहस्यवाद की परिभाषा एवं स्वरूप
विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से रहस्यवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है, किन्तु आज तक कोई सर्वमान्य परिभाषा सामने नहीं आयी है। डॉ. रामकुमार वर्मा के अनुसार, रहस्यवाद जीवात्मा की उस तिनिहत प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह काव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निशल संबंध जोड़ना चाहता है और वह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी प्रकार महादेवी जी ने रहस्यवाद को मानवीय भावनाओं की अभिव्यंजना का प्रेरणा स्रोत माना है। पं. परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार, ‘रहस्यवाद शब्द काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है। वह प्रधानतः उसमें लक्षित होने वाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है जो विश्वात्मक सत्ता की प्रत्यक्ष गंभीर एवं तीव्र अनुभूति के साथ संबंध रखती है।’ इसी प्रकार रहस्यवाद का विश्लेषण करते हुए डॉ. भगीरथ दीक्षित लिखते हैं कि, ‘रहस्यवाद में भारतीय वेदांत का ब्रह्मचिंतन भक्तों की भगवान विषयक भावना दिव्य प्रणयानुभूति और लौकिक रूपों के माध्यम से पार्थिव अभिव्यक्ति की एक साथ रहस्यपूर्ण स्थिति अनिवार्य है।’ इस प्रकार हम देखते हैं कि रहस्यवाद की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिस पर सभी विद्वान एकमत हों।
रहस्यवाद के प्रकार
आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के दो रूप स्वीकार किये हैं। प्रथम भावात्मक रहस्यवाद तथा दूसरा साधनात्मक रहस्यवाद। किंतु डॉ. जगदीश नारायण त्रिपाठी के अनुसार रहस्यवाद सात प्रकार के होते हैं, यथा-
(1) सत्ता रहस्यवाद
(2) दार्शनिक रहस्यवाद,
(3) भक्तिपरक रहस्यवाद
(4) सौंदर्य मूलक रहस्यावाद
(5) प्रेममूलक रहस्यबाद
(6) प्रकृतिमूलक रहस्यवाद और (7) बालक रहस्यवाद।
(क) रहस्यवाद का उद्गम- पाश्चात्य विद्वान् सेमेटिक धर्म-भावना से रहस्यवाद का उद्भव मानते हैं, किंतु डॉ. एस. राधाकृष्णन् के अनुसार वेदों में भी रहस्यवादी स्वर मिलते हैं। प्रसाद जी स्वयं ईसा और मंसूर को आर्यों की अद्वैत भावना से प्रभावित मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रहस्यवाद की मूल भावना वैदिक युगीन है। उपनिषदों में आत्मा एवं परमात्मा की एकता को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि ‘सत्सत्यं स आत्मा तावमसि।’ इसके अनंतर पौराणिक एवं भक्ति सूत्रों में अद्वैत विचार का प्रायः प्रभाव सा ही रहा है किंतु आठवीं- मवीं शताब्दी में शंकराचार्य ने पुनः अद्वैतवाद की स्थापना की किंतु उनके परवर्ती आचार्यों ने विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतों का प्रचार कर अद्वैत विचाराराधक मार्ग अवरूद्ध सा कर दिया है।
(ख) हिंदी में रहस्यवाद- हिंदी में रहस्यवाद के दर्शन हमें सर्वप्रथम सिद्धानाथों एवं योगियों के साहित्य में होते हैं। किंतु सिद्धों एवं नाथों का रहस्यवाद बड़ा ही स्पष्ट है और रहस्यवाद का परिपुष्ट एवं विकसित रूप सर्वप्रथम हमें कबीर के काव्य में ही देखने को मिलता है। डॉ. शिवनंदन प्रसाद के अनुसार कबीर जी हिंदी के आदि रहस्वादी कवि हैं।’ तब से लेकर आज तक रहस्यवाद की यह अनुगूंज हिंदी में बराबर ध्वनित होती रही है। यद्यपि समय के पविर्तन ने रहस्यवादी अभिव्यक्ति के रूप में परिवर्तन ला दिया है। तथापि उनके मूल रूप में किसी प्रकार की भिन्नता के दर्शन नहीं होते। प्राचीन रहस्यवादियों में उपासना एवं साधना की प्रवृत्ति सदैव जागरूक रही है। कबीर, दादू, जायसी, आदि प्राचीन रहस्यावादी है। वर्तमान युग में रहस्यवाद वैयसक्ति कल्पना या चित्रण का विषय बनकर काव्य भूमि पर प्रकट हुआ यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्राचीन रहस्यवादी जहाँ थे, साधक थे, उपासक थे, वहीं वर्तमानकाल के रहस्यवादी कवि सांसारिक हैं।’ इसलिए आज का रहस्यवादी काव्य-कल्पना चिंतन एवं ज्ञान पर आधारित है, प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा का नाम आधुनिक रहस्यवादियों में आदर के साथ लिया जाता है। इन कवियों के रहस्यवादी काव्य पर पाश्चात्य विचारधारा का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है।
हिंदी के रहस्यवादी कवि और उनका काव्य
हिंदी काव्य में रहस्यवाद का प्रारंभ संत काव्य से हुआ है। यद्यपि उनके पूर्व भी रहस्यात्मक सत्ता का उल्लेख अवश्य मिलता है किंतु क्रमबद्ध वर्णन संतकाव्य से ही देखने को मिलता है। रहस्यवादी काव्य की दृष्टि से संत शिरोमणि कबीरदास का काव्य अत्यंत उच्चकोटि का है। वे इस धारा के प्रथम एवं अन्यतम कवि हैं। अब यहाँ पर क्रमानुसार हिंदी के रहस्यवादी कवि एवं उनके काव्य का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा।
- संत शिरोमणि कबीर दास- कबीर ने प्रेम की पृष्ठभूमि पर रहस्यात्मक भावनाओं को प्रतिष्ठित किया है और उस रहस्यात्मक सत्ता से आत्मा के मिलन का चित्रण रहस्यात्मक रूप में किया है। इतना ही नहीं कबीर के काव्य की तीव्रतर मर्मस्पर्शी भावनाओं का भी निदर्शन हुआ है। देखिए-
ऑखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारि-निहारि।
जीभड़िया छाल्या पड़ा, राम पुकारि-पुकारि।।
- जायसी- जायसी का रहस्यवाद सूफी साधना की पद्धति पर आधारित है। यही कारण है कि उनके रहस्यवाद में प्रेम की प्रधानता है। ‘वे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का संदेश देते हैं।’ ‘पद्मावत’ उनका श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है, जिससे पग-पग पर रहस्यवादी भावनाओं के दर्शन होते हैं। ‘पद्मावती’ को परब्रह्म परमेश्वर की आभा से मंडित दिखाया है और राजा रत्नसेन सूफी साधक है, जो पद्मावती रूपी ब्रह्म को पाने के लिए साधना करता है और उत्कृष्ट साधना द्वारा उसे प्राप्त भी करता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि सूफी साधना में आत्मा को पुरूष माना गया है और परमात्मा को स्त्री। ‘जायसी के प्रेम मूलक रहस्यवाद में मिलन और विरह दोनों ही स्थितियों का वर्णन मिलता है। ‘मिलन की स्थिति का वर्णन देखिए-
देखि मानसर रूप सुहावा। हिय हुलास पुरइन होई छावा।
गा अँधियार रैन मसि छूटी। भा भिनसार किरन रवि फूटी।
आधुनिक युग का रहस्यवादी काव्य
आधुनिक काल में रहस्यवाद ने पुनः अंगड़ाई ली और नवयुग की नूतनता से अनुप्राणित हो पुनः हिंदी काव्यसाहित्य में अवतरित हुआ। किंतु यहाँ यह द्योतक है कि प्राचीन और अर्वाचीन रहस्यवाद में पर्याप्त अंतर है। डॉ. गोविंदनाथ शर्मा प्राचीन रहस्यवाद के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि प्राचीन रहस्यवाद में बौद्धिक चेतना की प्रधानता है किंतु आधुनिक रहस्यवाद में प्रेम संबंध तथा प्रणय निवेदन को प्रमुख स्थान दिया गया है।
‘प्राचीन रहस्यवाद में धार्मिक अनुभूति एवं साधना का प्राधान्य है किंतु आज का रहस्यवाद धार्मिक साधना का फल न होकर मुख्यतया कल्पना पर आधारित है। आधुनिक रहस्यवाद में परमात्मा के मिलन की काल्पनिक अनुभूति की अभिव्यंजना पाते हैं। उसमें प्रतीक्षा, विरह, असीम का संबंध प्रकृति में विराट परोक्ष शक्ति की कल्पना वेदना और करूण की व्यापक रहस्यमय अनुभूति आदि विषयों का समावेश दिखायी देता है।’
- ‘श्रीजयशंकर प्रसाद’- आधुनिक काल के रहस्यवादी कवियों में ‘प्रसाद’ का प्रमुख स्थान है। इन्होंने रहस्यवाद का माधुर्य एवं सौंदर्य से युक्त रूप उपस्थित किया है, ‘प्रसाद’ के काव्य में कल्पना का प्राचुर्य है। इनकी ‘कामायनी’ में रहस्यवाद का पूर्ण उन्मेष दिखाई देता है। जिज्ञासा एवं अव्यक्त सत्ता के प्रति कौतूहल की भावना इनके काव्य में पग-पग पर देखने को मिलती है। देखिये-
महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान।
ग्रह नक्षत्र और विद्युत्कण, किसका करते हैं संधान?
- श्री सुमित्रानंदन पंत- पंत की रहस्यमयी सत्ता विश्व के कण-कण में व्याप्त है। वह ही प्रकृति के परिवर्तन एवं सृष्टि के संपूर्ण कार्य कलापों की संचालिका है। प्रकृति में परिव्याप्त यह अदृश्य शक्ति कवि को बारंबार अपनी ओर आकृष्ट करती है। देखिए-
स्तब्ध ज्योत्स्ना में संसार चकित रहता शिशु सा नादान
विश्व के पलकों पर सुकुमार बिचरते हैं जब स्वप्न अजान
न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देना मुझको मौन।
- महादेवी वर्मा- वर्मा जी का रहस्यवाद कल्पना, अनुभूति एवं तत्वज्ञान के आधार पर अवतरति हुआ। इनके संपूर्ण काव्य में रहस्यवाद की अनुपम अनुगूंज सुनाई पडती है। अंतस की करूणा, भारतीय दार्शनिक ज्ञान तथा एकान्तिक जीवन की अनुभूतियों ने वर्मा जी के गीतों को रहस्यवादी बना दिया है। इनके इन गीतों में एक कसक है, एक वेदना है, एक टीस है। दुःख ही उनका साथी है। उनका काव्य विरह-वेदना की साकार प्रतिमा है। प्रकृति में व्याप्त इस अदृश्य सत्ता को महादेवी जी ने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया है। किंतु उनका उस प्रियतम से वियोग मिलन सरीखा आनंददायक है। देखिए-
विरह का दुःख आज दीखा, मिलन के मधुपल सरीखा।
दुःख सुख से कौन तीखा, मैं न जानी औ न सीखा।
- सूर्यकांत त्रिपाठी निराला- निराला जी अद्वैत के प्रकांड पंडित थे। इसलिए उन्होंने मानव को अभेद दृष्टि से विश्व में व्याप्त इस परम सत्ता का अंश स्वीकार किया है। उनके काव्य में बौद्धिकता एवं भावात्मकता का मणिकांचन योग उपस्थित हुआ। इस विरह सत्ता से मिलन की मधुमयी कल्पना को निराला के ही शब्दों में देखिये-
हमें जाना है जन के उस पार, जहाँ नयनों से नयन मिले।
ज्योति के स्वरूपसहस्त्र खिलें, सदा ही बहती नव रसधार।।
वहीं जाना इसे जग के पार।।
हिंदी रहस्यवादी काव्य की विशेषताएँ
- आध्यात्मिकता का प्राधान्य- हिंदी के रहस्यवादी काव्य में आध्यात्मिक तत्त्वों का अनुपम संयोग देखने को मिलता है। यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति लौकिक रूप में हुई तथापि उनकी सांकेतिकता अलौकिकता की ओर इंगित करती है। कहीं-कहीं पर तो आध्यात्मिकता अपने पूर्ण रूप से ही निखर उठी है। कबीर की निम्न पंक्तियों को लीजिए-
जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर-भीतर पानी।
फूटा कुंभ जल जलधि समाना, यह तत कथौ गियानी॥
- अव्यक्त सत्ता प्रति आकर्षण- हिंदी का रहस्यवादी कवि सदैव उस अव्यक्त सत्ता के प्रति आकृष्ट होकर उससे मिलने को आकुल एवं व्याकुल रहा है एवं उसे जानने को लालायित हो रहा है। प्रसादजी लिखते हैं-
हे अनंत रमणीय कौन तुम।
- प्रेमतत्त्व की प्रधानता- वस्तुतः प्रेस रहस्यवाद का प्राण है। भारतीय कवि ‘प्रेम’ के ही द्वारा लौकिक एवं अलौकिक जीवन में सामंजस्य उपस्थित करता है। कबीरदास जी इस ‘प्रेम’ को सर्वस्व मानते हुए लिखते हैं-
‘हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से क्या यारी।
कबीर की ही भांति प्रसाद जी लिखते हैं-
अरे कहीं देखा है तुमने, मुझे प्यार करने वाले?
- आत्मसमर्पण की भावना- हिंदी रहस्यवादी काव्य में आत्मसमर्पण की भावना का प्राधान्य है, क्योंकि जब तक साधक अपने अहं को मिटाकर अपने प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक वह उस अव्यक्त सत्ता से भिन्न हो नहीं सकती। आत्मसमर्पण की इस भावना को वर्मा जी के शब्दों में देखिए-
तू जल जल होता जितना क्षण, वह समीप आता छलनामय।
मधुर मिलन मिट जाता तू, उसकी उज्ज्वल स्थिति में घुलमिल।।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ- राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
- प्रमुख हिन्दी गद्य-विधाओं की परिभाषाएँ
- आदिलकाल के विभिन्न नाम | आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत | आदिकाल के नामकरण की समस्या
- हिन्दी साहित्य के काल विभाजन की समस्या | काल विभाजन के सन्दर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विभिन्न मत
- साहित्य के इतिहास संबंधी कुछ समस्याएँ | हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएँ
- आदि कालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ | आदिकाल के प्रमुख रासो काव्य | रासो काव्य परंपरा का सामान्य परिचय
- आदिकालीन धार्मिक साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ | सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य एवं जैन साहित्य की प्रवृत्तियाँ
- सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएँ | सगुणोपासक कवियों की समान्य प्रवृत्तियाँ
- भक्तिकाली के विभिन्न काव्यधाराओं का नाम | ज्ञानमार्गी संत काव्य की मूल प्रवृत्तियाँ | निर्गुण संत काव्य के सामाजिक चेतना का मूल्यांकन
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]