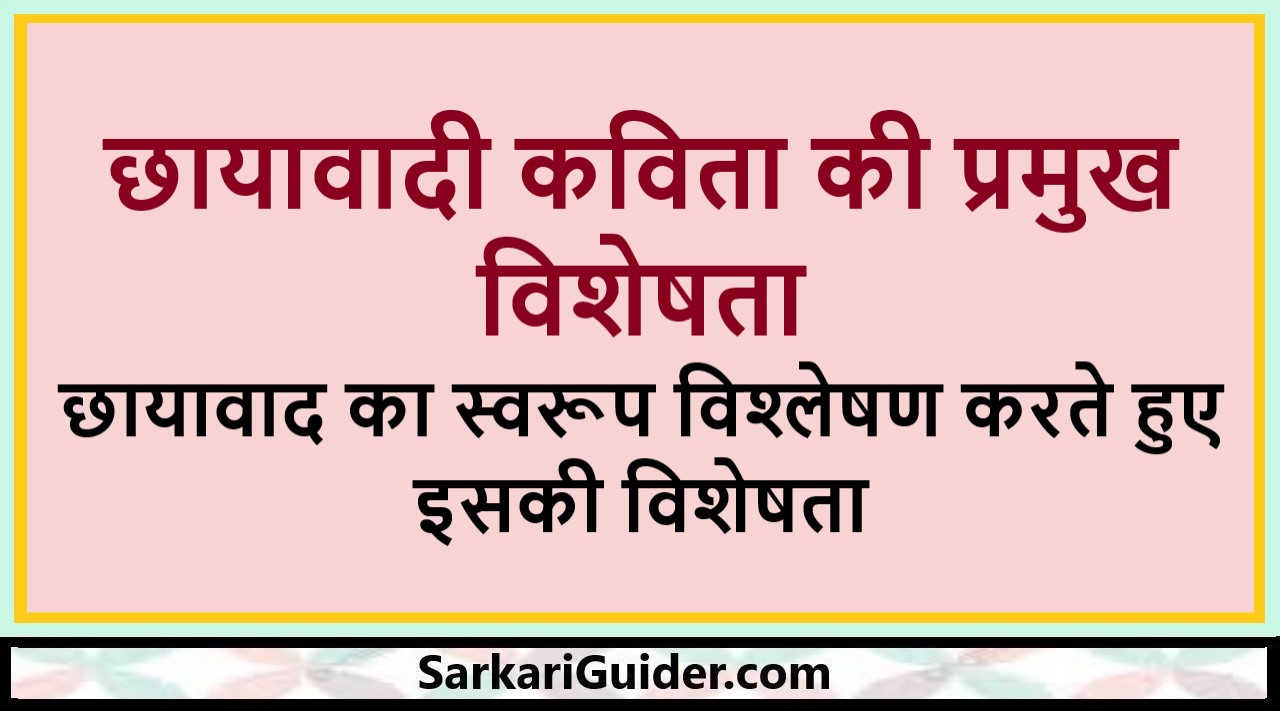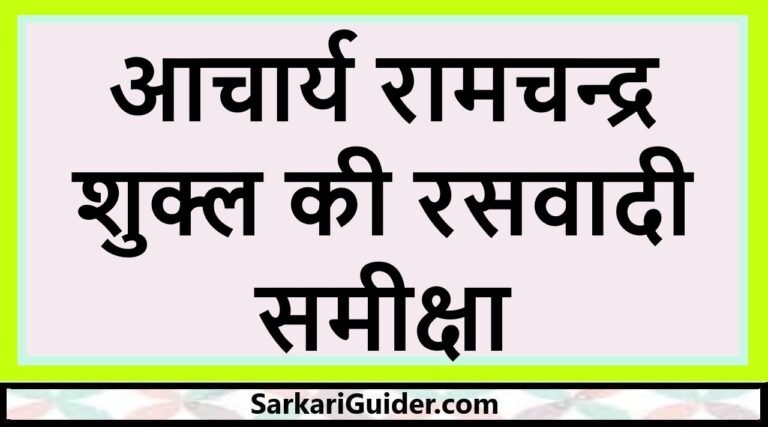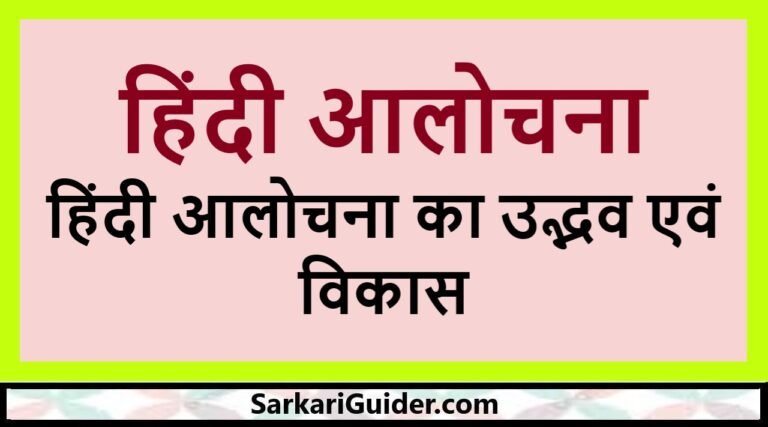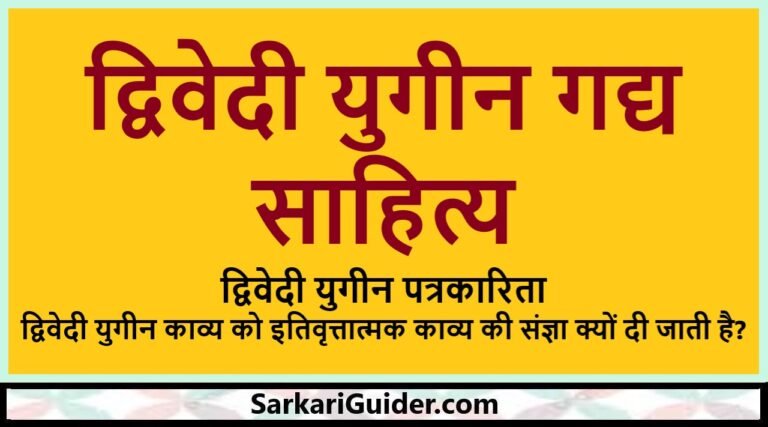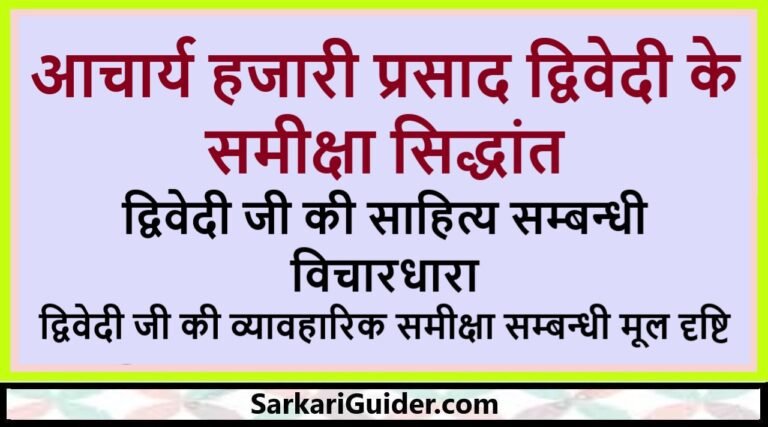छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता | छायावाद का स्वरूप विश्लेषण करते हुए इसकी विशेषता
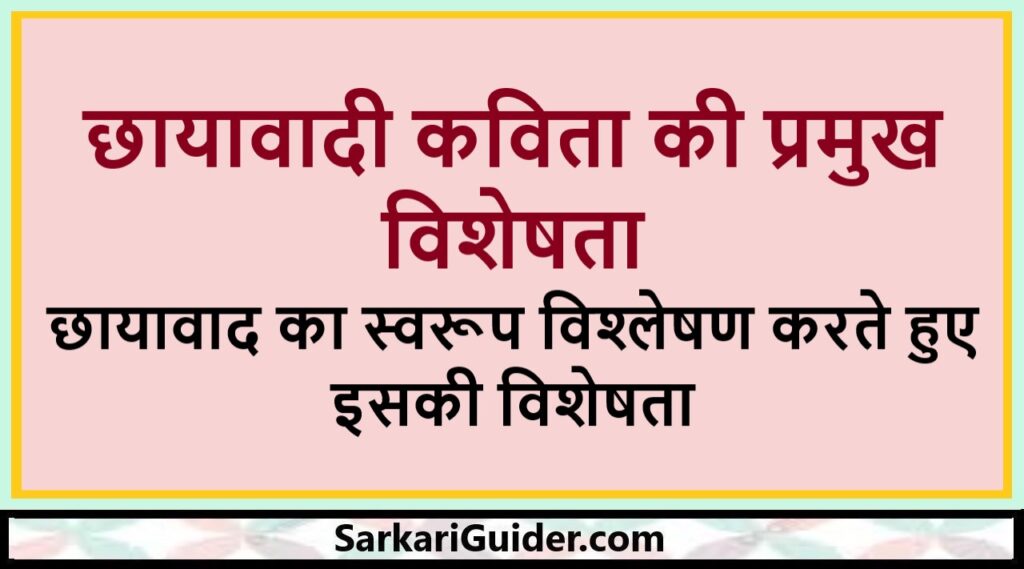
छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता | छायावाद का स्वरूप विश्लेषण करते हुए इसकी विशेषता
छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता
प्रकृति वर्णन की एक अखण्ड परम्परा है- प्रकृति और मानव का अटूट सम्बन्ध है। मानव प्रकृति के क्रोड़ में ही लालित पालित और विकसित होता है। प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शन से उसका मन सहज आनन्द से अभिभूत हो जाता है। उसको प्रकृति द्वारा जीवन की प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, वह जीवन का रस और जीवन के समाधान को प्रकृति से ही प्राप्त करता है। यही कारण है कि विजन सदा से प्रकृति के प्रति आकर्षित होते आए हैं।
प्रकृति सदा से कविजनों का प्रिय विषय रहा है। यह बात दूसरी है कि देश काल और पात्र के अनुसार उसके प्रति दृष्टिकोण तथा वर्णन के प्रकार बदलते रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि काव्य में प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण की परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है और आधुनातन कवियों ने उसके प्रति उत्साह का प्रदर्शन किया है।
छायावाद के पूर्ववर्ती काव्य में प्रकृति-वर्णन का अभाव रहा- वैदिककाल से लेकर संस्कृत साहित्य के पूर्वकाल तक प्रकृति परम आकर्षक व्यक्तित्व लिए रही और कविजन ने प्रकृति के अनेक बिम्ब-ग्राही संश्लिष्ट वर्णन प्रस्तुत किए। उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में वह प्रायः निर्वासित सी हो गई। उस युग का साहित्यकार नगर की चहार दीवारी में बन्द होकर रह गया। हमारे हिन्दी के कवियों को यही परम्परा प्राप्त हुई। वे स्वयं भी युद्ध के वातावरण में उलझ जाने के कारण प्रकृति के रम्य वातावरण से बहुत दूर जा पड़े थे। परिणाम यह हुआ कि काव्य में उसका प्रयोग यथा तो उपदेशात्मकता के रूप में हुआ या आलंकारिक रूप में।
छायावाद का युग और प्रकृति-वर्णन-
आधुनिक युग में आकार प्रकृति ने फिर एक बार उन्मुक्त वातावरण में साँस ली और छायाबाद के युग में तो प्रकृति-सुन्दरी को पंख फैलाकर नीलगगन में पूरी उड़ान भरने का अवसर प्राप्त हुआ। ‘छायावाद’ के काव्य के अन्तर्गत प्रकृति के वर्णन इतनी विभिन्न विधाओं में तथा इतनी पुष्कल मात्रा में किये गये कि कतिपय आलोचक तो उसे प्रकृति काव्य ही कहने लगे। इतना अवश्य है कि छायावाद में प्रकृति ने कवि की अभिव्यक्ति के लिए पग-पग पर सहायता की है। प्रकृति को अलग कर दिया जाए तो छायावाद पंगु हो जाता है।
महादेवी वर्मा और प्रकृति-
महादेवी वर्मा ने भी अन्य छायावादी कवियों की भाँति प्रकृति को अपने काव्य में उचित एवं उपयुक्त स्थान प्रदान किया है उनकी विराद् तक पहुंचने की साधना में प्रकृति सदैव उनके साथ दिखायी देती है उन्होंने छायावाद और प्रकृति के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए लिखा कि ‘छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिये जो प्राचीन काल से बिम्ब-प्रतिबिम्ब रूप में चला जा रहा था, और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट हुए एक महाप्राण बन गई, अतः अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के जल कण और पृथ्वी के ओस बिन्दुओं का एक ही कारण एक ही मूल्य है। प्रकृति लघुतृण और महान वृक्ष कोमल कलियाँ और कठोर शिलाएँ अस्थिर जल और स्थिर पर्व, निविड़ अन्धकार और उज्ज्वल विद्युत रेखा मानव की लघु- विशालता, कोमलता, कठोरता, चंचलता-निश्चलता और मोहन ज्ञान का केवल प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट से उतपत्र सहोदय है। जब प्रकृति अनेकरूपता में परिवर्तनशील विभिन्नता में कवि ने ऐसा तादात्म्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर किसी असीम चेतन और दूसरा छोर उसके समीप हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक-एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा।
(अपनी यात, यामा)
महादेववी वर्मा का प्रकृति-चित्रण-
उपर्युक्त उद्धरण द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति के प्रति महादेवी वर्मा में उत्कृष्ट अनुराग है तथा उन्होंने प्रकृति को परम्परामुक्त होकर देखा ही नहीं है अपितु उसके साथ नवीन सम्बन्धों की सद्भावना भी की है।
महादेवी वर्मा ने प्रकृति का वर्णन प्रायः निम्नलिखित रूपों में किया-
(1) प्रकृति के साथ तादात्म्य
(2) विराट की छाया
(3) मानवीकरण
(4) रस्यवादी भावना
(5) आलम्बन रूप से कोमल और उम्र दोनों रूप।
(6) उद्दीपन रूप में
(7) अलंकार रूप में
(8) उपदेशिका रूप
(9) निराशा और वेदना का प्रेरक रूप
(10) प्रतीक रूप में। (11) नवीन विधाओं में-(क) नारी भावना का आरोप (ख) ब्रह्म और आत्मा के मिलन में सहायिका (ग) प्रतीकात्मक रूप (घ) सर्वदात्मक रूप तथा (ङ) तल्लीनता।
महादेवी वर्मा कृत प्रकृति-
वर्णन की इन विधाओं का विवेचन संक्षेप में इस प्रकार है-
(1) प्रकृति के साथ तादात्म्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति चित्रण- महादेवी वर्मा ने प्रकृति में विराट के अतिरिक्त अपनी भी छाया देखी है। प्रकृति उनके हृदय में भित्र न होकर उनके जीवन का एक अंश ही बनकर सम्मुख आती है। समीक्षक इसे प्रकृति के साथ तादात्म्य की स्थिति मानते हैं। तादात्म्य की यह स्थिति महादेवी के काव्य में विशेषतः मिलती है। मैं बनी मधुमास आली’मैं नीर भरी दुःख की बदली, तिरह का जलजात जीवन रात सी-नीरव व्यथा तथा तम सी आगम मेरी कहानी आदि कविताओं में हमें यह तादात्म्य स्थित देखने को मिलती है। निम्नलिखित उद्धरण में वह सन्ध्या से अपनी तुलना करती हुई कहती हैं कि-
प्रिय सान्ध्य गगन, मेरा जीवन।
यह क्षितिज बना धुंधला विराग,
नव अरुण-अरुण मेरा सुहाग
छाया सी काया वीतराग,
सुधि भीने स्वप्न रंगीले धन
साधों का आज सुनहलापन
घिरता विषाद का तिमिर गहन
संध्या का नभ से मूक मिलन-
यह अनुमती हँसती चितवन-
(2) विराट की छाया के रूप में प्रकृति-चित्रण- महादेवी वर्मा प्रकृति को एक ऐसा साधन मानती हैं जिससे सहज तथा विराट् की छाया देखी जा सकती है। यथा-
उषा के छू आरक्त कपोल किलक पड़ता तेरा उन्माद
देख तारों के बुझते प्राण न जाने क्या आ जाता याद?
हेरती है सौरभ की हाट कहो किस निर्मोही की बाट?
मानवीकरण की शैली के अन्तर्गत हम बताएंगे कि महादेवी जी विराट प्रकृति के ही अंग रूप प्रकृति के समस्त उपादानों को देखती हैं।
(3) प्रकृति का मानवीकरण करते समय कवयित्री- कभी-कभी प्रकृति के उपादानों को लेकर ‘विराट्’ का भी चित्रण करने लगती हैं वह ‘नश्वरता’ की बात करते हुए कहती है-
काल ही लहरों में अविराग
बुलबुले होते अन्तर्धान
हाथ उनका छोटा आश्चर्य
डूबता लेकर प्यासे प्राण
(4) रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति-चित्रण- रहस्य भावना छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति हैं। रहस्यवादी भावना के अन्तर्गत प्रकृति-चित्रण के दो कारण हैं- (1) जब प्रकृति के असीम व्यापारों के प्रति जिज्ञासा भाव के कारण कवि के भावों में दार्शनिकता का प्रधान्य हो जाता है तथा (2) जब कवि प्रकृति के माध्यम से असीम और ससीम में प्रणय सम्बन्ध स्थापित करता है। महादेवी वर्मा को कविता में हमको इन दोनों रूपों में प्रकृति का चित्रण उपलब्ध होता है।
जिज्ञासा भाव से युक्त यह चित्रण देखिए-
उषा के छू आरक्त कपोल किलक पड़ता तेरा उन्माद
देख तारों के बुझते प्राण न जाने क्या आ जाता याद।
लाए कौन संदेश, नए घन, ‘मुसकाता संकेत-भरा नभ अलि क्या प्रिय आने वाले है।’
निम्नलिखित पंक्तियों में कवियित्री के प्रणय का वर्णन है जिनका सम्बन्ध असीम सत्ता से है। महादेवी जी ने प्रकृति माध्यम से इस प्रकार का प्रणय वर्णन बहुत सफलता के साथ किया है-
स्मित ले प्रभात आता नित, दीपक दे सन्ध्या जाती,
दिन ढलता सोना बरसा, निशि मोती दे मुसकाती।
(5) आलम्बन रूप में प्रकृति-चित्रण- जब प्रकृति कवि के भावों का आधार बनती है तो वह प्रकृति का आलम्बन रूप या स्वतन्त्र चित्रण कहलाता है। हिमालय के निम्नांकित वर्णन में इसी पद्धति का आलम्बन किया गया है। रूप और रंग की सजीवता दृष्टव्य है-
तू भू के प्राणों का शतदल।
सित क्षीर-फेन हीरक रज से
जो हुए चाँदनी में निर्मित
पारद की रेखाओं में चिर
चांदी के रंगों से चित्रित
खुल रहे दलों पर दल झलमल
सीपी से नीलम से दुतिमय
कुछ पिंग अरुण, कुछ हित श्यामल
कुछ सुख चंचल, कुछ दु:के मंत्र
फैले तम से कुछ तूल- विरल
मंडराते शत-शत अलि-बादल
(6) उद्दीपन रूप में प्रकृति-चित्रण- महादेवी वर्मा ने परम्परागत उद्दीपन प्रणाली को भी अपनाया है। इस प्रणाली का प्रयोग मुला विरहावस्था के वर्णन के अन्तर्गत किया जाता है। महोदवी जी ने भी यहीं किया है। उनके प्रकृति-चित्रण में हमकों विरह का आवेग प्रायः दिखायी पड़ता है। प्रकृति के मादक तथा उत्तेजक रूप को देखकर विरहिणी को अपना प्रियतम याद आ जाता है और विरह-वेदना के कारण नेत्रों से अश्रु-धार बहने लग जाती है-
पिक की मधुमय वंशी बोली
नाच उठी सुन अलिनी भोजी, अरुण सजक पाटल बरसाता,
तम पर मृदु पराग की रोली।
मृदुल अंक घट दर्पण सा सार,
आंक रही निशि वृग-इंदीवर
आज नयन आते क्यों भर-भर।
महादेवी जी प्रकृति के माध्यम से अपने अन्तर्दहन को शान्ति प्रदान करती हुई भी देखी लघ सकती है-
उड़ उड़ कर जो धूलि करेगी
मेघों का नभ में अभिषेक
अमिट रहेगी उसके अंचल
में मेरी पीड़ा की रेख।
(7) अलंकरण रूप में प्रकृति-चित्रण- जिस प्रकार भावों से अधिक तीव्रता एवं प्रभविष्णुता लाने के लिए काव्यालंकारों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार अभिव्यक्ति की सबलता के लिए प्रकृति का अलंकार के रूप में प्रयोग होता है। अपनी वेदना की समता प्राकृतिक उपकरणों से करती हुई महादेवी जी कहती हैं-
पावस घन-सी उमड़ बिखरती
शरद-निशा-सी नीरव घिरती
महादेवी वर्मा ने अन्य कवियों की भाँति प्रकृति से अनेक उपमान ग्रहण किए हैं। इन्होंने अधिकांशतः बसन्त और पावस ऋतुओं से उपमान ग्रहण किए हैं। इसका कारण साधक का आँखों में आँसू होठों पर मुस्कान दो ही सम्बल-रूप पदार्थ होते हैं। पावस आँसू से सम्बद्ध हैं और बसन्त मुस्कान से। वैसे देखा जाए तो अन्य कवियों ने प्रायः इन्हीं दो ऋतुओं को विशेष रूप से अपनाया है। कामशास्त्र के अनुसार बसन्त ऋतु पुरुष के लिए तथा पावस ऋतु नारी के लिए विशेषतः उद्दीपनकारी मानी गई है। अस्तु
कवयित्री ने इन ऋतुओं से सम्बन्धित पक्षियों में भ्रमर, चात, मयूर, कोकिल तथा चकोर को लिया है। फूलों में कमल, गुलाब और हरसिंगार का विशेष उल्लेख हुआ है।
(8) उपदेशिका के रूप में प्रकृति-चित्रण- भावुक एवं साधक कवि प्रकृति के प्रांगण में घटित होने वाली घटनाओं से जीवन-निमार्ण के संकेत ग्रहण करते हैं। रामचरित मानस के ‘किष्किंधा काण्ड’ में वर्णित वर्षा-वर्णन इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा को भी प्रकृति उपदेश देती हुई दिखायी देती है। परन्तु बहुत कम अवसरों पर।
(9) निराशा और वेदना के प्रेरक रूप में प्रकृति-चित्रण- महादेवी जी प्रकृति के कतिपय तत्वों को विषाद प्रेरित अभिव्यक्ति भी प्रदान करती हैं। निम्नलिखित उदाहरण में सुषमा और सुवास से पूरित प्रसून की इससे रहित होने पर जो करुण दशा होती है, उसका चित्रण करते हुए वह लिखती है कि-
देकर सौरभ दान पवन से
कहते जय मुरझाये फूल
जिसके पथ में बिछे वही
क्यों भरता इन आँखों में धूल?
प्रारम्भ में प्रकृति उनके लिए विस्मय से भरी हुई थी। परन्तु धीरे-धीरे वह उसमें डूबती गई। यही कारण है कि सांध्यगीत’ और ‘दीपशिखा’ के अधिकांश गीतों में प्रकृति अनुभूर्ति का अंग बनकर ही आई है।
दुःख और निराशा में, विरह और विकलता के लिए महादेवी जी बौद्ध दर्शन की ऋणी है। इन भावों के लिए वह प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करती हैं। दुःख के सुखद परिणाम की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पंक्तियों में वह कितनी कुशलता के साथ करती हैं-
जब मेरे शूलों पर शत-शत मधु के युग होंगे अवलम्बित
मेरे क्रन्दन से आतप के
दिन सावन हरियाले होंगे
तब क्षण-क्षण मधु प्याले होंगे?
वह अपनी हीनता में भी केवल यही वरदान चाहती हैं कि-
घन बनूँ वर दो मुझे प्रिय।
जलधि मानस से नव जन्म पा
सुभग तेरे ही दृग व्योम में,
सजल श्याम मघर मूक सा
तरल अश्रु विनिर्मित गात ले
नित फिरु झर-झर मिटॅ प्रिय
घन बनूँ वर दो मुझे प्रिय
(10) प्रतीक रूप में प्रकृति-चित्रण– छायावादी काव्य में प्रतीकों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। अधिकांशता प्रतीक प्रकृति से लिए गये हैं। इन्होंने अपने व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण भी प्रतीकों के माध्यम से किया है-
प्रिय। सान्ध्य गगन मेरा जीवन।
यह क्षितिज बना धुँधला विराग,
नव अरुण-अरुण मेरा सुहाग
छाया-सी काया वीतराग
सुधि भीने स्वप्न रंगीले घन।
(11) नवीन विधाओं में प्रकृति चित्रण- छायावादी कवियों ने प्रकृति-चित्रण की कतिपय नवीन विधाएँ अपनाई हैं। महादेवी जी की कविता में भी हमें इनके दर्शन होते हैं।
यथा-
(क) प्रकृति पर नारी-भावना का आरोप- महादेवी जी प्रकृति में नारी के सौन्दर्य एवं उसकी कोमलता का दर्शन करती हैं। इसीलिए इन्होंने प्रकृति में नारी-रूप का आरोप किया है। महादेवी जी ने प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया है। निम्नलिखित पंक्तियों में वह प्रकृति को अपनी या सजनी के रूप में सम्बोधित करती हैं-
पुलकित स्वप्नों की रोमावलि
कर में हो स्मृतियों को अञ्जलि,
मलयानिल का चल दुकूल अलि
चिर छाया-सी श्याम, विश्व को आ अभिसार बनी।
सकुचती आ बसन्त रजनी ।
यहाँ कवयित्री भी प्रकृति को सखी मान कर उसे अभिसार के लिए प्रेरित कर रही है।
(ख) ब्रह्म और आत्मा के मिलन में सहायिका के रूप में प्रकृति-चित्रण- निर्गुण कवियों ने प्रकृति को माया का रूप माना है और इसको ब्रह्म -मिलन में सहायिका बताया है। महादेवी की कविता में प्रकृति के अनेक ऐसे चित्र मिलते हैं जिन्हें देखकर असीम प्रियतम की सुधि आ जाता है-
मैं फूलों में रोती वे बालारुण में मुस्काते,
मैं पथ में बिछ जाती हूं वे सौरभ में उड़ जाते
X X X
कुसुम-दल से वेदना के दाग को
पोंछती जब आँसुओं से रश्मियाँ,
चौंक उठती अनिल के निश्वास छू
तारिकाएँ चकित-सी अनजान-सी,
तब बुला जाता मुझे उस पार जो,
दूर के संगीत-सा वह कौन है?
(ग) सर्ववादात्मक प्रकृति-चित्रण- इस विधा के अन्तर्गत प्रकृति में परम सत्ता का वर्णन किया जाता है। महादेवी जी ने भी प्रकृति के समस्त सौन्दर्यागार को उसी सत्ता की आभा का प्रतिविम्ब माना है-
तेरी आभा का कण नभ को
देता अगणित दीपक दान,
दिन को कनक-राशि पहिनाता,
विधु को चांदी का परिधान ।
(घ) तल्लीनता के रूप में प्रकृति चित्रण- महादेवी जी प्रकृति के साथ घनिष्ठ आत्मीयता का अनुभव करती हैं। इस आत्मीयता के कारण इनके प्रकृति वर्णन में अपेक्षित तल्लीनता दिखायी देती हैं-
फैलते सान्ध्य नभ में
भाव ही मेरे रंगीले।
तिमिर की दीपावली हैं,
रोम मेरे पुलक गीले ।
निष्कर्ष-
उपयुक्त विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि महादेवी जी प्रकृति को अपनी सजीव संगिनी, जीवन का अंग समझती है।
महादेवी जी एक ओर प्रकृति में उस विरादू की छाया देखती हैं और दूसरी ओर अपनी छाया भी देखती हैं। इस प्रकार वह प्रकृति के साथ पूर्ण तादाम्य स्थापित कर लेती हैं।
प्रकृति ने महादेवी का भावपक्ष का ही नहीं कला पक्ष का भी शृंगार किया है। उनके प्रकृति निरीक्षण में सूक्ष्मता दिखायी देती हैं सच तो यह है कि प्रकृति महादेवी के लिए शृंगार की वस्तु है, जीवन का अपरिहार्य अंश हैं उनके प्रकृति-चित्रण के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष उपलब्ध होता है कि “यद्यपि उनके काव्य का मूल वर्ण्य आध्यात्मिक अनुभव रहा है तथापि उन्होंने प्रकृति सौन्दर्य को अपनी आत्मा में संचित कर उसे जिस रम्य रीति से उपस्थित किया है वह हिन्दी छायावादी काव्य में अत्यन्त सुलभ होने पर भी रहस्यवादी काव्य में नितान्त दुर्लभ है।
कदाचित् महादेवी की कोई कविता ऐसी नहीं है जिसमें प्रकृति का कोई रूप-रंग, उसकी कोई भंगिमा, उसका कोई इंगित लक्ष्य-अलक्ष्य रूप से न आ जाता हो।
महादेवीं के प्रकृति-चित्रण पर उनके प्रकृति-विषयक विचार पूर्णतः लागू होते हैं। यथा-
“छायावाद का कवि न प्रकृति के किसी रूप को लघु या निरपेक्ष मानता है न अपने जीवन को क्योंकि वे दोनों ही एक विराट रूप समष्टि में स्थित रहते हैं और एक व्यापक जीवन से स्पन्दन पाते हैं जीवन के रूप दर्शन के लिए प्रकृति अपना अक्षय सौन्दर्य-कोष खोल देती है और प्रकृति के प्राण परिचय के लिए जीवन अपना रंगमय भावकाश दे डालता है। काव्य जब प्रकृति का आधार लेकर चलता है तब कल्पना में सूक्ष्म रेखाओं का बाहुल्य और दीप्त रंगों का फैलाव स्वाभाविक ही रहेगा। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच में जीवन का उद्घोष है। अतः कल्पनाएँ बहुरंगी और विविध रूपी हैं।”
निष्कर्ष यह है कि महादेवी वर्मा ने परम्परागत विधाओं तथा छायावादी कवि द्वारा ग्रहीत नवीन विधाओं में प्रकृति का चित्रण किया है और इसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त है।
हिंदी साहित्य का इतिहास– महत्वपूर्ण लिंक
- प्रगतिवाद | प्रगतिवादी की परिभाषायें | प्रगतिवाद का जन्म और विकास | प्रगतिवादी प्रमुख कवि | प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां (विशेषताएं)
- द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य | द्विवेदी युगीन पत्रकारिता | द्विवेदी युगीन काव्य को इतिवृत्तात्मक काव्य की संज्ञा क्यों दी जाती है?
- भारतेन्द्र जी का संक्षिप्त परिचय | भारतेन्दु युग | भारतेन्दु के नाटकों का परिचय | भारतेन्दु रचित नाटक | भारतेन्दु युगीन हिन्दी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय | भारतेन्दु जी की कृतियों के नाम
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]