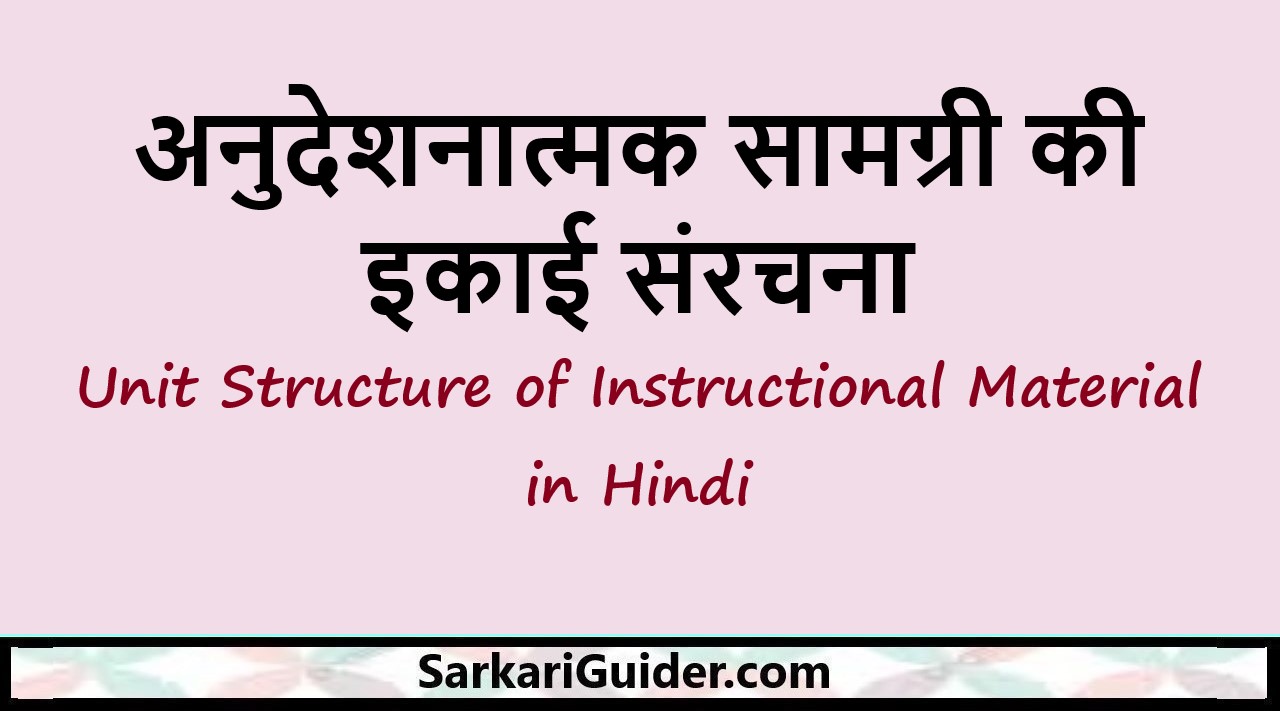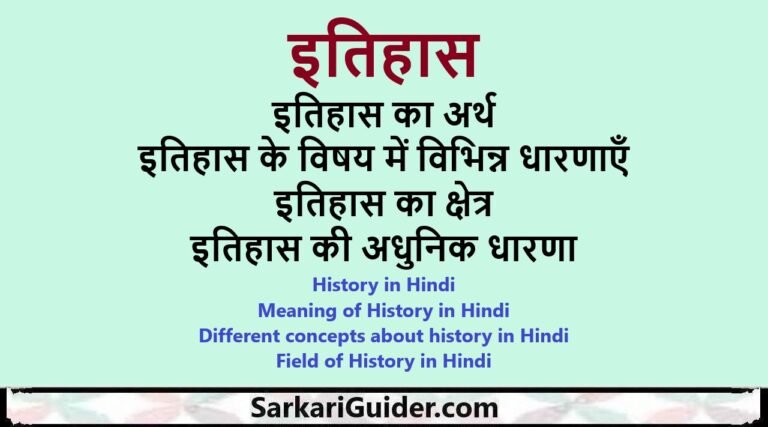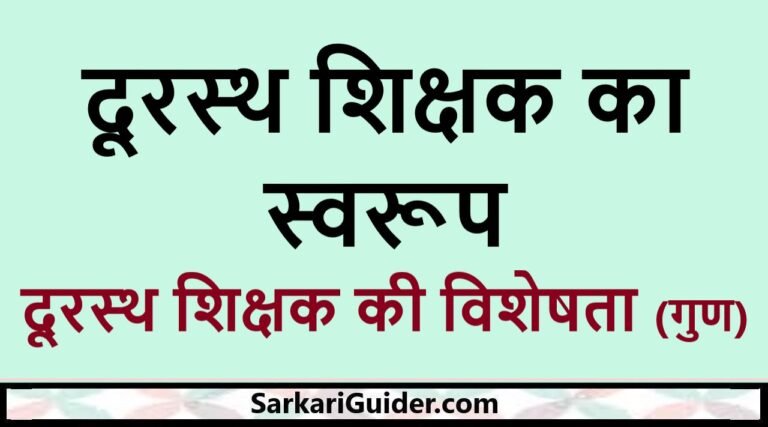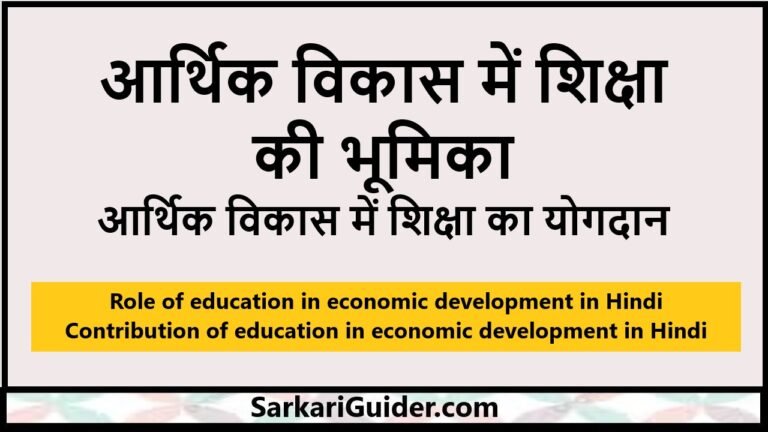अनुदेशनात्मक सामग्री की इकाई संरचना | Unit Structure of Instructional Material in Hindi

अनुदेशनात्मक सामग्री की इकाई संरचना | Unit Structure of Instructional Material in Hindi
अनुदेशनात्मक सामग्री की इकाई संरचना (Unit Structure of Instructional Material)-
दूरवर्ती शिक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण पाठ्य- वस्तु को शिक्षण-अधिगम की सुविधा की दृष्टि से अनेक छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। चूँकि इस प्रणाली में शिक्षार्थी को स्वयं अध्ययन करना होता है, अतः इकाई की सामग्री का स्वरूप अधिक से अधिक स्वतः अनुदेशनात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। स्वतः अनुदेशनात्मक सामग्री से तात्पर्य ऐसी सामग्री से होता है जिसे पढ़ते समय शिक्षार्थी को ऐसा आभास हो सके कि वह शिक्षक के सामने कक्षा में बैठकर पढ़ रहा है। अतः इस प्रकार का सामग्री के प्रस्तुतीकरण में शिक्षार्थी को अभिप्रेरित रहने हेतु पर्याप्त पुनर्बलन एवं पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। इसलिए इकाई की संरचना बहुत सावधानीपूर्वक एवं कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष बल प्रदान करते हुए की जाती है। यद्यपि प्रत्येक दूरवर्ती शिक्षण संस्थान की सामग्री प्रस्तुतीकरण की अपनी शैली होती है किन्तु उनकी इकाइयों की संरचना में प्रमुख बिन्दु एक जैसे होते हैं। इकाई की संरचना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं-
(i) इकाई का प्रारम्भ (Beginning of a Unit)-
इकाई का प्रारम्भ ‘इकाई परिचय’ के रूप में किया जाना चाहिए। दूरवर्ती शिक्षार्थी इकाई के नवीन ज्ञान, उसकी अध्ययन विधि, उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व आदि से अपरिचित होता है। अतः इकाई परिचय में इन सब बातों के बारे में शिक्षार्थी को सामान्य जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही नवीन ज्ञान की ओर शिक्षार्थी को प्रवृत्त करने हेतु इसका सम्बन्ध उसके पूर्व ज्ञान से स्थापित करना भी आवश्यक होता है। इसलिए इकाई परिचय अथवा इसकी भूमिका में सामान्यतया निम्नलिखित त्त्वों को समाविष्ट किया जाता है-
(a) उद्देश्य कथन (Stamen of Aims and Objectives) – इसके अन्तर्गत शिक्षार्थी को इकाई की ‘विषय-वस्तु’ उसे प्रस्तुत करने के उद्देश्य तथा उसे सही ढंग से अध्ययन कर लेने के पश्चात् सम्भावित व्यवहार परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। उद्देश्यों की जानकारी होने से शिक्षार्थी में विषय -सामग्री के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित होता है तथा वह अध्ययन हेतु सही दिशा में प्रवृत्त होता है।
(b) विषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण (An Overview of the Study Material)- इसके अन्तर्गत इकाई की विषय -सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करते हुए शिक्षार्थी को इस बात के संकेत भी दिये जाते हैं कि विषय-वस्तु को क्यों चुना गया है तथा इस विशिष्ट ढंग से क्यों प्रस्तुत किया गया है । इससे शिक्षार्थी की विषय-वस्तु के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है तथा वह अध्ययन हेतु अभिप्रेरित होता है।
(c) अन्तर्वस्तु की सूची (List of Contents) – सामान्य पाठ्य-पुस्तकों में सम्पूर्ण पुस्तक की अन्तर्वस्तु की एक ही सूची बनाई जाती है किन्तु दूरवर्ती शिक्षण की पाठ्य-पुस्तकों में सम्पूर्ण सामग्री में प्रत्येक इकाई की अपनी अन्तर्वस्तु सूची होती है। इससे शिक्षार्थी को इकाई के संगठन एवं उसकी अन्तर्वस्तु के विभिन्न तत्त्वों का सही ज्ञान हो जाता है। इकाई को पढ़ने में शिक्षार्थी को कई घंटे एवं कई दिन (लगभग एक सप्ताह) लगते हैं। अतः उसे इकाई को बार-बार पढ़ने हेतु खोलना पड़ता है। इकाई को खोलते ही अन्तर्वस्तु की सूची पर दृष्टि पड़़ने से शिक्षार्थी उन्हें त्वरित गति से प्रत्यास्मरण करता है। इस प्रकार शिक्षार्थी को विषय-वस्तु को धारण करने में सुविधा होती है।
(d) अध्ययन हेतु सामान्य निर्देश (General Guidance for Study)- पाठ्यक्रम की इकाई सम्पूर्ण अध्ययन का केवल एक भाग होती है। अतः अध्ययन की पूर्णता के लिए शिक्षार्थी को पाठ से सम्बन्धित अन्य तत्त्वों के बारे में निर्देशन की आवश्यकता होती है। पाठ से सम्बन्धित अन्य प्रमुख तत्त्व इस प्रकार के हो सकते हैं-
- संदर्भ पुस्तवकें एवं सम्बन्धित अध्ययन सामग्री,
- प्रयोगात्मक कार्य,
- श्रव्य-दृश्य सामग्री,
- अध्ययन एवं स्व-मूल्यांकन का तरीका तथा
- अन्य व्यावहारिक सूचनायें एवं निर्देश।
उपर्युक्त सूचनाओं के बारे में सही निर्देश दिये जोने पर शिक्षार्थी को अध्ययन में सुविधा होती है तथा उसे अनावश्यक समय एवं श्रम नष्ट नहीं करना पड़ता है।
शिक्षार्थियों के बोझ को कम करने तथा उन्हें अधिक से अधिक सुविधाजनक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करने की दृष्टि से इकाई के प्रारम्भ के सभी तत्त्वों को तीन विशेषताओं के रूप में समाविष्ट किया जाता है-
- अन्तर्वस्तु सूची
- उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य
- प्रस्तावना
(ii) इकाई का मुख्य भाग (The Body of the Unit)-
इकाई के मुख्य भाग में पाठ की मूल विषय-वस्तु को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पाठ शीर्षक को कई उपशीर्षकों अथवा अनुभागों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग किसी नये विचार बिन्दु से सम्बन्धित होता है तथा इसका अपना अलग प्राप्य उद्देश्य होता है। प्रत्येक अनुभाग की अध्ययन सामग्री के पश्चात् शिक्षार्थी को स्वतः मूल्यांकन हेतु कुछ अभ्यास कार्य दिये जाते हैं। इन अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर अथवा उत्तर संकेत इकाई के अन्त में दिये जाते हैं। शिक्षार्थी अपने उत्तरों की, पुष्टि इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से करता है जिससे उसे पृष्ठपोषण मिलता है।
इकाई को अनेक उपभागों में विभक्त करके प्रस्तुत करने से शिक्षार्थी को अध्ययन में बहुत सुविधा होती है। चूँकि शिक्षार्थी पूरी इकाई को एक ही बार में नहीं पढ़ता है बल्कि उसे इस अध्ययन हेतु कई घंटों/दिनों का समय देना होता है। अतः छोटे-छोटे अनुभागों को पढ़ने, समझने एवं अभ्यास कार्यों/गृहका्ों को करने में शिक्षार्थी को थकान अथवा बोझ का अनुभव नहीं होता है।
(iii) इकाई का समापन (Ending the Unit) –
इकाई के समापन का उद्देश्य यह होता है कि उसे पढ़ते हुए शिक्षार्थी इस बात की स्वयं जाँच कर सके कि उसने इकाई की सभी प्रमुख बातों का अध्ययन एवं आवश्यक क्रियाओं का सम्पादन पूर्ण कर लिया है। अतः इकाई के समापन में निम्नलिखित विशेषताओं को अनिवार्य रूप से समाविष्ट किया जाता है-
(a) इकाई का सारांश (Summary of the Unit) – इसके अन्तर्गत इकाई के मुख्य अंश या भाग के सभी प्रमुख बिन्दुओं को सूचीबद्ध किया जाता है अथवा उनका संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। इससे शिक्षार्थी को मुख्य भाग की विषय-वस्तु को दुहराने एवं प्रत्यास्मरण करने में सहायता मिलती है।
(b) उद्देश्यों की प्राप्ति की पुष्टि हेतु जाँच सूची (Confirmation of objectives achieved in the form of Checklist) I
(c) गृहकार्य (Assignment)- इकाई के अन्त में शिक्षार्थी को स्वयं करने हेतु इस प्रकार के कार्य दिये जाते हैं जिससे उसे इस बात का स्वयं पता चल सके कि उसने विषय-सामग्री का कितनी अच्छी तरह समझा एवं सीखा है। इकाई के अन्त में दिये गये इन कार्यों को कर लने से शिक्षार्थी को वास्तविक गृहकार्य (Assignment for Assessment) पूर्ण करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- शिक्षकों के कार्य तथा दशाओं का सुधारा | Improvement of teachers’ work and conditions in Hindi
- अध्यापकों के सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम | programmes for In-service Education of Teachers in Hindi
- सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता | सेवारत प्रशिक्षण का महत्व
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार हेतु कोठारी आयोग के सुझाव
- दूरदर्शन | दूरदर्शन का शैक्षिक उपयोग | दूरदर्शन का गुण तथा दोष | शैक्षणिक टेलीविजन की प्रमुख योजनाएँ
- ओवर हेड प्रोजेक्टर | OHP की कार्यप्रणाली | OHP की संरचना | ओवर-हेड प्रोजेक्टर की विशेषतायें
- ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग | ओवरहेड प्रोजेक्टर के लाभ
- रेडियो | भारत में शैक्षिक रेडियो का विकासात्मक इतिहास | रेडियो के उपयोग | रेडियो द्वारा शिक्षण | शैक्षिक समाचारों में रेडियो
- वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कम्प्यूटर का प्रयोग | Use of computer in current education system in Hindi
- टेलीकांफ्रेंसिंग का अर्थ | टेलीकांफ्रेंसिंग के प्रकार | The meaning of teleconferencing in Hindi | Types of teleconferencing in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]