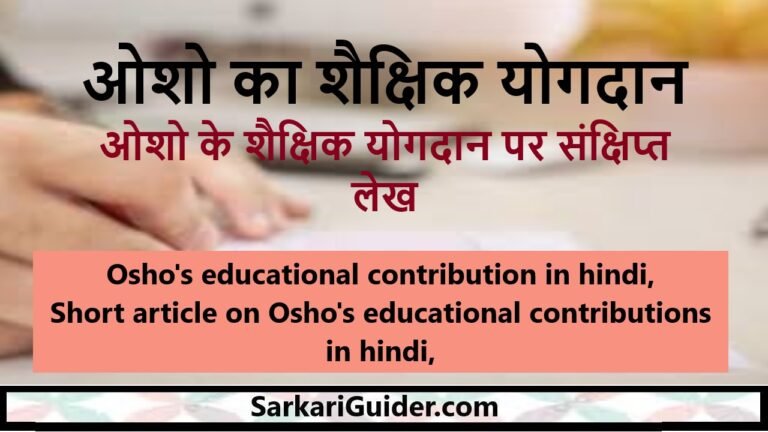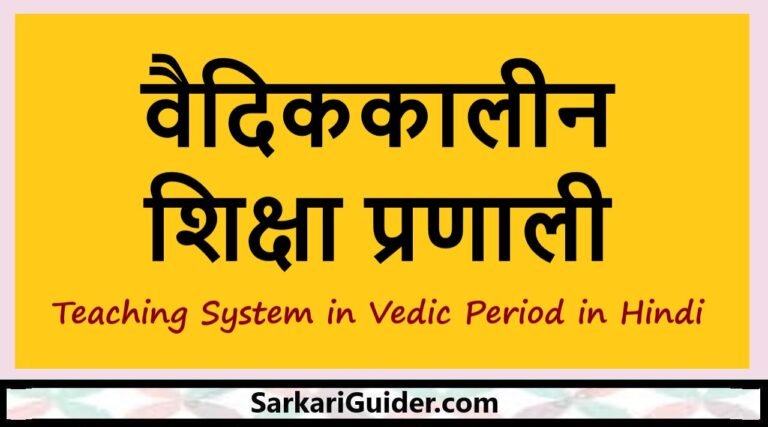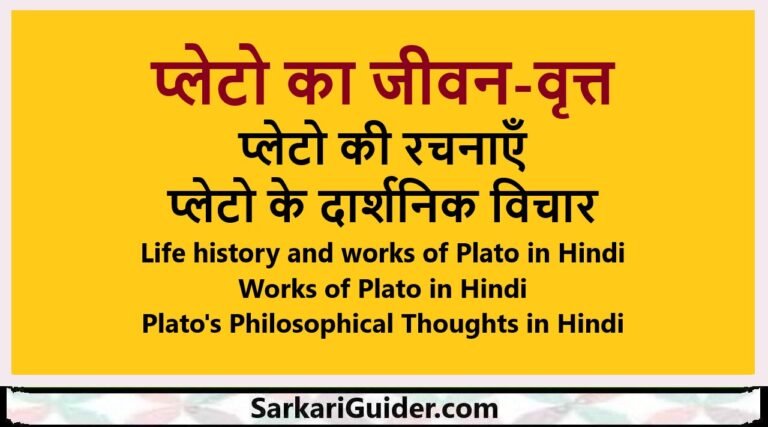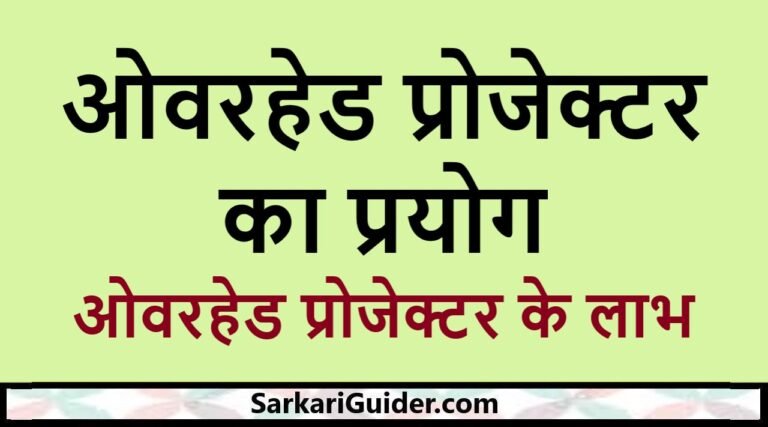भारत में उच्च शिक्षा की समस्यायें | The problems of Higher Education in India in Hindi

भारत में उच्च शिक्षा की समस्यायें | The problems of Higher Education in India in Hindi
भारत में उच्च शिक्षा की समस्यायें
(Problem of Higher Education)
शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं। इनमें से प्रत्येक स्तर के अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य होते हैं।
प्रो० हुमायूँ कबीर के शब्दों में, “अनेक बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, वह व्यक्ति को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान नहीं करती हैं। विशेषत: यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम तथा ग्रामीण जीवन के प्रति अरुचि हो जाती है। इस प्रकार विश्वविद्यालय एक ऐसा अभिकरण बन गया है जो गाँवों के योग्य तथा होनहार युवकों को शहर से खींच लाते हैं, लेकिन इस प्रकार गाँवों की हानि होती है, उनसे शहरों को लाभ होता है ऐसी बात नहीं है। गाँवों के छोटे-से समाज में नेता बनने के बजाय जो अत्यन्त सहजता से बन सकते थे, वे शहर की अज्ञात जनसंख्या के एक हताश और कटु भावना से भरे सदस्य बन जाते हैं।”
इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्यायें हैं, जो निम्नलिखित है-
(1) दोषपूर्ण पाठ्यक्रम-
पाठ्यक्रम की समस्या, उच्च शिक्षा से सम्बन्धित एक गंभीर समस्या है। अनेक विद्यालयों में परंपरागत पाठ्यक्रम दिखाई देते हैं। उनकी पाठ्य-सामग्री से कुछ उद्देश्यों को संकेत नहीं मिल पाता और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम भी छात्रों की रुचि, मनोवृत्ति और अभिरुचि के अनुरूप नहीं है। एन० सी० ई० आर० टी० इस सम्बन्ध में बिल्कुल अनभिज्ञ है कि किस विषय विभाग में किस स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।
(2) विस्तार की समस्या-
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं एवं विकास क्रम के अंतर्गत अनेक कॉलिजो तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है। इससे दिन प्रतिदिन उच्च शिक्षा में विस्तार से अनेक दुष्परिणाम सामने आये हैं, जैसे-शिक्षित बेरोजगारी, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या, उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट, उपयुक्त शैक्षणिक प्रशिक्षण का अभाव, प्रवेश की समस्या आदि।
(3) शिक्षा के माध्यम की समस्या-
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है। आज के नवयुवक अंग्रेजी को अधिक महत्त्व दे रहे हैं, वे अंग्रेजी भाषा से होने वाली हानि तथा अहित को नहीं समझ पा रहे हैं। गाँधी जी के अनुसार-“विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है। उसने व्यक्तियों की आय को कम कर दिया है, उसने उन्हें जनसाधारण से अलग कर दिया है तथा इसने शिक्षा का अनावश्यक रूप से महँगी बना दिया है।”
(4) शिक्षा का गिरता हुआ स्तर-
उच्च शिक्षा के स्तर गिरने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
(i) कक्षा में छात्रों को अत्यधिक संख्या होना।
(ii) शिक्षकों द्वारा छात्रों पर ध्यान न देना।
(iii) पुस्तकालयों में अध्ययन की समुचित व्यवस्था न होना।
(iv) शिक्षा का व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित न होना।
(v) शिक्षकों को वेतन कम देना।
(vi) शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि न लेना।
(5) दोषयुक्त परीक्षा प्रणाली-
आज उच्च स्तर पर निबन्धात्मक परीक्षायें आयोजित की जाती है। इससे छात्रों की योग्यता के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसका कारण यह है कि इन परीक्षाओं में रटकर ही छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं। फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। राधाकृष्णन् आयोग के अनुसार-“यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा के मात्र एक विषय में सुधार का सुझाव दें तो वह परीक्षाओं के सम्बन्ध में होगा।”
(6) मार्ग प्रदर्शन तथा समुपदेशन की समस्या-
भारतवर्ष की उल्ला शिक्षा में विद्यार्थियों के मार्ग दर्शन तथा परामर्श की कोई व्यवस्था नहीं है। परामर्श तथा मार्ग दर्शन के अभाव में अधिकतर विद्यार्थी ऐसे विषयों का चयन कर लेते हैं। जिनसे वे उचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उचित ज्ञान प्राप्त न कर पाने के कारण वे परीक्षा में असफल हो जाते हैं। फलस्वरूप की भावना का जाती है। इस सम्बन्ध में धर्मयुग में प्रकाशित एक लेख में लिखा है- “देश में यह तो यह जानने की सुविधा बहुत कम है कि कौन बालक किस विषय का अध्ययन करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के परीक्षण हमारे देश में उच्च शिक्षा में नहीं है। दूसरे, अभिभावक इस तरह का परामर्श मानने को तैयार नहीं है। लड़के की सामर्थ को बिना समझे यह निश्चित कर लिया जाता है कि उसे क्या बनाएंगे?”
(7) अनुशासनहीनता की समस्या-
विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए छात्र तथा शिक्षक दोनों ही उत्तरदायी हैं। प्रवेश को लेकर कुलपति का घेराव, तोड़-फोड़, आगजनी आदि घटनायें घटित होती रहती हैं, परिणामस्वरूप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बंन्द करना पड़ता है। उच्च शिक्षा पर कुछ राजनीतिक तथा सामाजिक वर्गों का प्रभाव पड़ रहा है। फलस्वरूप छात्र वर्ग का अन्य वर्गों के साथ संघर्ष बढ़ रहा है। आजकल अध्यापकों से दुर्व्यव्हार, परीक्षा में नकल को लेकर होने वाली हिंसा, अनैतिकता, अनुशासनहीनता इसके ज्वलंत प्रमाण हैं।
(8) उद्देश्यहीनता की समस्या-
उद्देश्यहीनता उच्च शिक्षा की अत्यन्त गंभीर समस्या है। उद्देश्यहीनता की समस्या के कारण छात्रों का भावी जीवन अंधकारमय प्रतीत हो रहा है। आज का छात्र समाज का मात्र चेतनाहीन सदस्य बनकर ही रह गया है। इसका मुख्य कारण किसी विशिष्ट उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त न करना है। इस सम्बन्ध में गुन्नार मिरडल ने लिखा है- “विश्वविद्यालयों की उपाधियाँ, सरकारी नौकरियों हेतु पासपोर्ट थीं। शिक्षा, शिक्षार्थियों को नौकरी हेतु न कि जीवन हेतु तैयार करने के संकीर्ण उद्देश्य से दी जाती है।”
(9) शिक्षा में विशिष्टीकरण की समस्या-
उच्च शिक्षा में विभिन्न विषयों के विशिष्टीकरण पर जोर दिया जाता है। फलस्वरूप किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात् छात्रों का दृष्टिकोण अत्यन्त संकीर्ण बन जाता है। इस सम्बन्ध में श्री सैयदेन ने लिखा है-“विशिष्टीकरण में एक तरह की संकीर्णता अकाल्पनिकता होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि विज्ञान वर्ग के शिक्षार्थियों को कला, कविता तथा सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता विज्ञान और वैज्ञानिक विधियों ने इस संसार को, जिससे वे रहते हैं, किस तरह बदल दिया है?”
(10) अनुसंधान की समस्या-
आज भारतवर्ष में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें अनुसंधान की समस्या अत्यधिक गंभीर समस्या है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का अभाव है। आज प्रत्येक छात्र एम० ए० (स्नातकोत्तर) परीक्षा पास करने के उपरान्त अनुसंधान कार्य करना चाहता है। इसी कारण अनुसंधान की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।
(11) छात्र संघ तथा छात्र समितियों की समस्या-
उच्च स्तर पर छात्र संघ की समस्या भी अत्यधिक गंभीर समस्या बनी हुई है। छात्र संघ, प्रधानाचार्यो तथा प्रबन्धकों के कार्यों में अपना हस्तक्षेप करते हैं। वर्तमान युग में छात्र संघ विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अभिशाप सिद्ध हुए हैं।
इस सम्बन्ध में श्री वी० के० आर० वी० राव ने लिखा है- “छात्र समितियों के प्रश्न पर वे अपने सहयोगियों के विचार तथा स्वयं के विचारों को अनुकूल बनाने हेतु विशेष रूप से चिन्तित हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की समितियों की संख्या अत्यधिक है, जिनमें अनेक रजिस्टर्ड भी नहीं होती। हम यह भी जानते हैं कि उनको अपना फण्ड कहाँ से प्राप्त होता है या वे इनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि कभी-कभी हमें चिन्ता में डाल देने वाले विशाल विदेशी फण्ड भी उनको मिल जाते हैं। हमारा विचार यह है कि ऐसी समितियों की मौजूदगी के कारण ही छात्र राजनीतिज्ञों का निर्माण होता है।”
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- अध्यापक शिक्षा में अलगाव | अलगाव का अर्थ | अध्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार के उपाय | अध्यापक शिक्षा के सुझाव
- बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त | basic principles of basic education in Hindi
- नवोदय विद्यालय | नवोदय विद्यालय के उदेश्य | नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषतायें
- माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन | मुदालियर कमीशन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य | माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित मुदालियर आयोग के सुझाव | तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष
- माध्यमिक शिक्षा की समस्यायें | माध्यमिक शिक्षा की समस्यायें एवं उनका समाधान
- भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास | ब्रिटिश काल में माध्यमिक शिक्षा का विकास | स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का विकास
- उच्च शिक्षा के निजीकरण की समस्या | शिक्षा के निजीकरण का अर्थ | उच्च शिक्षा के निजीकरण की समस्या का स्वरूप | उच्च शिक्षा के निजीकरण की समस्या के कारण
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]