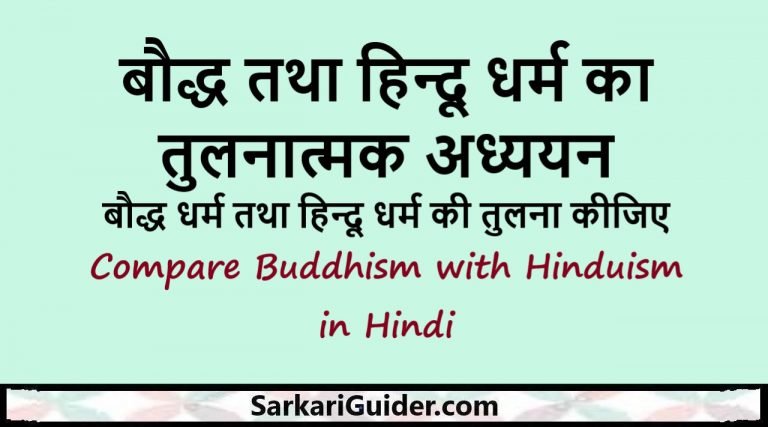भारतीय चित्रकला का प्रारम्भिक रूप | पूर्व ऐतिहासिक काल की चित्रकला | प्रस्तरकाल की चित्रकला | नवीनकाल की चित्रकला | धातुकला की चित्रकला | प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला
भारतीय चित्रकला का प्रारम्भिक रूप | पूर्व ऐतिहासिक काल की चित्रकला | प्रस्तरकाल की चित्रकला | नवीनकाल की चित्रकला | धातुकला की चित्रकला | प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला
भारतीय चित्रकला का प्रारम्भिक रूप (पूर्व ऐतिहासिक काल की चित्रकला)
यह काल ईसा से 3500 ई० पूर्व तक रहा। इसका प्रमाण शिलालेखों, धातु के अस्त्र शस्त्रों, गहनों मिट्टी के बर्तनों, आदमी तथा जानवरों के उन अस्थि पिंजरों, जो भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, से मिलता है। कंदराओं की चित्रकारियां भी इसका प्रमाण हैं।
प्रस्तरकाल की चित्रकला-
इस समय मनुष्य हाथी जैसे बली और विशाल जानवर का शिकार करते और उनके दांतों पर बड़ी सुन्दर चित्रकारी करते थे। इससे प्रतीत होता है कि इस काल के मनुष्य चित्रों के बनाने में बड़ी अच्छी-अच्छी रेखाओं का प्रयोग करते थे। उनकी रेखाओं में कोमलता तथा बल का आभास होता था।
नवीनकाल की चित्रकला-
प्राचीन प्रस्तर काल के पश्चात् इस काल का आरम्भ होता है। इस काल के मनुष्य पहले से अधिक सभ्य हो गये थे। इन मनुष्यों ने सिन्ध तथा गंगा जैसी बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे पर अपने खेत बनाये और खेती करना आरम्भ कर दिया। परिवार के रूप में निवास करना सीख लिया। खेती को अधिक सफल बनाने के लिए वनों तथा पहाड़ों से जानवर पकड़कर उनको पालतू बनाते थे।
इस काल के चित्रकारों ने हाथी दांत पर प्रस्तर काल की अपेक्षा कुछ अच्छे चित्र बनाए और आभूषणों तथा वस्तुओं पर सुन्दर जानवरों की आकृतियों से सजावट की। इस काल के चित्रों में रेखाओं का अच्छा प्रयोग हुआ है, जिसके जोड़ अच्छे हैं।
धातुकला की चित्रकला-
धातुकला के चित्र समय के कारण नष्ट हो चुके हैं। कहीं-कही पर कुछ चित्रों के भाग देखते को मिलते हैं, जिनके आधार पर इस काल के चित्रों पर कुछ लिखा जा सकता है। धातुकाल के चित्रकारों ने रेखाचित्र बनाए, जिनमें मनुष्यों को भागते दौड़ते तथा शिकार खेलते हुये या शिकार करने के पश्चात् मनुष्य की खुशियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए बड़े ही सुन्दर ढंग से दर्शाया है। इस काल के चित्रकारों ने शिकार खेलने के दृश्य भी चित्रित किये हैं, जिनकी रेखाओं के जोड़ बहुत ही सुन्दर हैं। धातुकाल के चित्रकारों ने अपने समय के धातुओं से बने हुये हथियारों के चित्र भी बहुत ही सुन्दर विधि से बनाये हैं जो देखने योग्य हैं। हथियारों की जो रेखायें हैं, वे सुन्दर हैं और उनमें गति है। रेखाओं के जोड़ आंखों को भले लगते हैं।
धातुयुग के चित्रों की मुख्य विशेषता उनकी रेखाएँ हैं जिनमें गति है और वे सुन्दर भी हैं। इन रेखाओं में वह भद्दापन नहीं हैं, जो हम नवीनकाल के चित्रों में देखते हैं। इस काल के चित्रों में चित्रकारों ने रेखाओं के जोड़ों को इस विधि से बनाया है, कि जोड़ नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस समय के चित्रकारों ने शिकारी जीवन के चित्र इतने सुन्दर बनाये हैं, जो आज भी अच्छी दृष्टि से देखे जाते हैं। अन्न उपजाने का ज्ञान उनको अधिक नहीं था। खेती बाड़ी का ज्ञान उनको कम था। अधिकतर शिकार ही उनकी भोज्य सामग्री थी।
इस समय के चित्रकार अपने हृदय की भावनाओं को गेरू तथा तूलिका से प्रकट करते थे, जिनकी आकृतियाँ सुन्दर हैं और भावों से पूर्ण है। इन चित्रों की शैली क्या है ? इसका ज्ञान हमें चित्रों को देखने से नहीं होता है। इनकी शैली यथार्थतापूर्ण तथा प्राचीन है, जो अपने समय के सामाजिक जीवन का अच्छा दर्पण है। इनको देखने से इस समय के सामाजिक जीवन की हल्की-सी रूप रेखा हमारी आँखों के सामने आ जाती है।
प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला-
इस समय के चित्रों में एक चित्र अत्यन्त सुन्दर है, जिसमें कुछ मनुष्य एक नंगली बैल का शिकार कर रहे हैं। शिकारियों में से कुछ गिरे पड़े हैं, और कुछ शिकारियों के घावों से खून बह रहा है। इन्हीं चित्रों में दूसरा चित्र भैंसे का है, जो दम तोड़ रहा है, जिसको देखते ही इस बात का पता चलता है कि वह बहुत जल्दी ही मर जायेगा। इसके चारों ओर मनुष्य खड़े हैं जो अपने शिकार को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं।
इन चित्रों को देखने से प्रतीत होता है कि उस काल के मनुष्य शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। इस काल के चित्रों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि जंगली मनुष्यों में भी चित्रकला की प्रवृत्ति विद्यमान थी, और वे अपने भावों को गेरू तथा तूलिका से प्रकट करते थे। इसी काल की चित्रकारी के कुछ उदाहरण मिर्जापुर में भी पाये जाते हैं। इन चित्रों की शैली यथार्थतापूर्ण और प्राचीन है! इन चित्रों को इस समय के चित्रकारों ने गेरू, रामरज तथा हिरौंजी से बनाया है। कुछ सिले भी मिली है जिनको देखने से यह कहा जा सकता है कि उस काल में चित्रशालायें भी थीं। इस युग के चित्रों में उस समय के सामाजिक जीवन का पता चलता है, जो चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। चित्र जिन भावनाओं को लेकर अंकित किये गए हैं वे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं। इन चित्रों को देखने से उस काल के सामाजिक जीवन की एक धुंधली रूप रेखा आंखों के सामने खिंच जाती है।
जो रंग उनके समय के अनुसार प्राप्त हुये उन्हीं का प्रयोग उन्होंने किया है। रंगों का मिलाप अधिक सुन्दर नहीं है तथा लाइट शेड के सिद्धांतों का पालन इस समय नहीं हुआ है। चित्रों की रेखाओं में कहीं-कहीं भद्दापन दिखाई पड़ता है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि समय के परिवर्तन के कारण इस काल के चित्रकारों के चित्रों की रेखायें कहीं-कहीं पर खराब हो गई है। प्रथम दृष्टि से इस प्रकार का दोष इस समय के चित्रकारों के ऊपर जाता है, परन्तु गहरी दृष्टि से इन चित्रों को देखने से पता चलता है कि यह दोष इस काल के चित्रकारों का नहीं है, बल्कि प्रकृति के कारण ऐसा हुआ है।
कला आकृतियाँ-
जब हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि इस काल में कलाकृतियों को अधिक उन्नति मिली। वर्तमान काल के चित्रकार इन कलाकृतियों को ज्यामितिक अलंकार कहते हैं। कुछ भी क्यों न हो लेकिन यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को रेखाओं का अच्छा ज्ञान था। इनको बनाने में कोण; आयत और वृत्तों आदि का प्रयोग इस ढंग से किया गया है कि उनको देखते ही हृदय कांप उठता है कि इनमें केवल आत्मा डालना और रह गया है। यदि ईश्वर उस काल के चित्रकारों को यह शक्ति प्रदान कर देता तो ये कलाकार आत्मा ) डाल देते। इस समय की कलाकृतियों में ज्यामितिक आकारों की संख्या अधिक है। वर्तमान चित्रकार इसको ज्यामितिक अलंकार कहते हैं और इनको कलाकृति से पृथक् कर दिया है। कहीं-कहीं पर इन कलाकारों ने रिक्त स्थान को आभूषित करने में पशु-पक्षियों तथा फूल पत्तियों को बनाया है जिनको वर्तमान काल में प्राकृतिक अलंकारों के नाम से पुकारा जाता है। अलंकारों को देखने से भली प्रकार प्रतीत हो जाता है कि प्राचीन चित्रकारों को ज्यामितिक आकारों का अच्छा अभ्यास था, जिनको इन्होंने अपने कृतियों को सुन्दरता से दिखाया है।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- स्तूप वास्तुकला | स्तूप वास्तु का उद्भव व विकास | भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका
- भरहुत की स्तूप | भरहुत में निर्मित स्तूप का संक्षिप्त परिचय
- सांची का स्तूप | सांची का बड़ा स्तूप | सांची के अन्य स्मारक
- अमरावती का स्तूप | बोध गया का स्तूप
- गुप्त काल में कला का विकास | गुप्तकालीन गुफाएँ और स्तूप | गुप्तकालीन मन्दिर | गुप्तकालीन मन्दिरों की विशेषाएँ
- गुप्त काल की मूर्ति कला | गुप्तकाल की कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां | गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएँ | गुप्तकालीन मृण्मूर्तियाँ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]