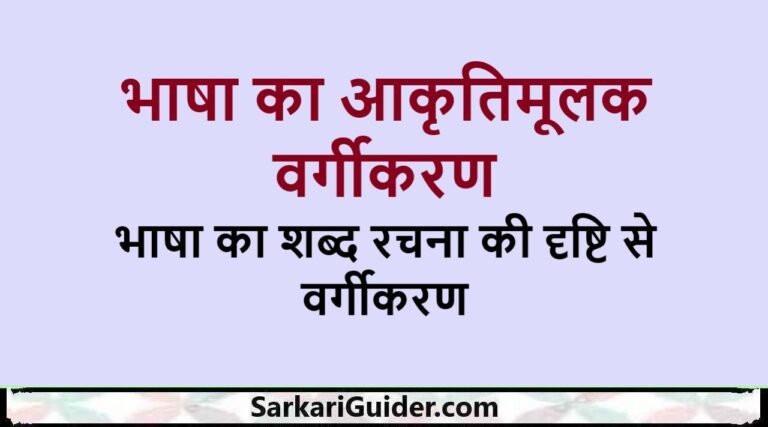भक्तिकाली के विभिन्न काव्यधाराओं का नाम | ज्ञानमार्गी संत काव्य की मूल प्रवृत्तियाँ | निर्गुण संत काव्य के सामाजिक चेतना का मूल्यांकन
भक्तिकाली के विभिन्न काव्यधाराओं का नाम | ज्ञानमार्गी संत काव्य की मूल प्रवृत्तियाँ | निर्गुण संत काव्य के सामाजिक चेतना का मूल्यांकन
भक्तिकाली के विभिन्न काव्यधाराओं का नाम
प्रस्तावना
हिंदी साहित्य का भक्तिकाल सं. 1375 से सं. 1700 तक माना जाता है। निःसंदेह इस काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती एवं परवर्ती कालों के साहित्य से उत्तम है। इस काल के साहित्य में अनुभूति की गहनता है और भाव-प्रवणता भी। यह दोनों गुण ऐसे हैं जो उसे आदिकालीन और रीतिकालीन साहित्य से श्रेष्ठ प्रमाणित करते ही हैं साथ ही आधुनिक काल से व्यापक एवं विविधतापूर्ण साहित्य से भी उसे ऊँचा उठा देते हैं। इतना ही नहीं इस काल के साहित्य में सभी प्रकार की विचारधारा वाले-कविताओं के लिए सामग्री उपलब्ध है। इसलिए प्रायः सभी विचारक इस काल की महत्ता का उद्घोष करते हैं। भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख धारायें निम्नांकित हैं-
-
निर्गुण पंथ की ज्ञानाश्रयी शाखा-
संत कवियों ने निर्गुणवाद में हिंदू एवं मुसलमानों के समन्वय की सम्भावना पायी क्योंकि मुसलमान एकेश्वरवादी थे उनके लिए ‘रसूल अल्लाह’ के सिवा कोई दूसरा अल्लाह अल्लाह नहीं था। हिंदू लोग भी सभी देवताओं को एक परमात्मा का ही रूप देखते थे। इस प्रकार हिंदुओं का निर्गुणवाद मुसलमानों के खुदावाद के बहुत निकट था। इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा के कावियों ने निर्गुणवाद के आधार पर हिंदू-मुस्लिम एकता काप्रसार किय। डॉ0 श्यामसुंदर दास के शब्दों में संत कवियों ने निर्गुणवाद के आधार पर ही राम और रहीम की एकता एवं हिंदू-मुसलमानों की निरर्थक रूढ़ियों का विरोध कर दोनों जातियों में अविरोध भाव उत्पन्न करने का उद्योग किया। महात्मा कबीर धारा के कवि थे।
-
निगुर्ण पंथ की प्रेमाश्रयी शाखा-
प्रेममार्गी काव्य धारा सूफियों और मुसलमान संतों की सद्भावना का परिणाम थी। अधिकांश हिंदू सर्वेश्वरवादी थे। सूफी लोग हिंदूओं के सर्वेश्वरवाद के अत्यधिक निकट हैं क्योंकि वे ईश्वर को अपने प्रेममात्र के रूप में देखते हैं कि इन सूफी संतों ने हिंदुओं की बोली में हिंदू -प्रेम-गाथाओं को लेकर काव्य रचनाएँ की हैं। जायसी इस धारा के महान् कवि हैं।
-
सगुण भक्तिमार्गी शाखा-
इस धारा का स्रोत उन भक्तों के अंतःस्थल से फूटा जो अपने इष्टदेवों की पूजा और उपसना में तल्लीन थे। मानव जाति का कल्याण भगवत् भजन में ही देखते थे। भोग-विलास को हेय समझते थे। ऐश्वर्य का उन्हें आकर्षण न था। वे यद्यपि मुसलमानों के विरोधी नहीं थे। फिर भी उनसे उन्हें मिलने की इच्छा भी न थी। यह भक्तिमार्गी शाखा ही दो उपधाराओं (1) रामभक्ति शाखा (2) कृष्णभक्ति शाखा में प्रवाहित हुई। सूरदास जो कृष्णभक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं और तुलसी रामभक्ति शाखा के। यहाँ यह ध्यातव्य है कि हिंदू धर्म में भगवान् के निर्गुण एवं सगुण दोनों ही रूप मान्य हैं। भक्तों ने जहाँ सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों को अपनाया है, वहीं संतों ने केवल निर्गुण रूप को। इन भक्तों, संतों का काव्य बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है। ‘बहुभाव’ एवं भाषा की दृष्टि से अद्वितीय है। उनकी अलंकार योजना सुष्ठु है। रस योजना एवं छंद विधान उत्तम कोटि का है। इस काल के साहित्य की विशेषताएँ निम्नांकित है-
(क) काव्य सौंदर्य- भक्तिकालीन कवियों का काव्य दृष्टिकोण बहुत ही उदात्त है। उन्होंने प्राकृत जनों के गुणगान में अपनीव ाणी का उपयोग नहीं किया। उनकी कविता आत्मप्रेरणा का परिणाम थी। इस कारण उनकी कविता स्वान्तः सुखाय न होकर सर्वजन सुखाय थी। उन्हें किसी का भय न था। वे निर्भय थे। इसीलिए राजदरबारों में बुलाया जाने पर वे स्पष्ट कह देते थे, ‘संतन कहा सीकरी सो काम’ उनका काव्य उनके हृदय की पुकार थी जो सत्य उल्लास एवं आनंद से परिपूर्ण थी। उसमें युग निर्माण की भावना थी। इसीलिए तो एक समीक्षक ने कहा, लगभग तीन सौ वर्षों की इस हृदय की मन की साधना के आधार पर ही हिंदी साहित्य उन्नतोमुखी हो सका है। कबीर, सूर, तुलसी, नंददास, मीरा, रसखान, हितहरिवंश इनमें से किसी पर संसार का साहित्य गर्व करता है। ये वैष्णव कवि हिंद भारतीय के कंठमाल हैं।”
(ख) भावपक्ष और कलापक्ष का अनुपम समन्वय- इस काल की कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है वैसी अन्य कालों की कविता में देखने को नहीं मिला। इस संदर्भ में प्रो. शिवकुमार वर्मा का कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता है। देखिये- भक्ति काव्य में मर्त्य और अमर्त्य लोक का एक सुखद संयोग है उसमें भावपक्ष और कलापक्ष परस्पर इतने घुल- मिल गये हैं कि उन्हें अलग करना सहज व्यापार नहीं है। भान-काव्य का अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष संतुलित सशक्त और परस्पर पोषक हैं।’
इतना ही नहीं, भक्तिकाल विश्वजनीन एवं शाश्वत काव्य है। रीतिकाल का भावपक्ष अपेक्षाकृत शिथिल और कलापक्ष अपेक्षाकृत अधिक सबल है। उसमें अलंकरण एवं प्रदर्शन की प्रवृत्ति का प्राधान्य है। इस युग के प्रायः समस्त कवियों ने शृंगार को रसराज सिद्ध करते हुए इस प्रकार की रचनाएँ लिखी है-
चमक, तमक, हाँसी, चमक, ससक मसक झपटानि।
ऐ जेहि रति, सो रति मुकति, और मुकति अति हानि।।
रीतिकालीन साहित्य की भांति आदिकालीन साहित्य भी इस काल के साहित्य के समक्ष प्रतिद्वन्द्रिता कर पाता क्योंकि भक्तिकालीन कवियों के काव्यों में अपूर्व बल था। डॉ.) रामकुमार वर्मा के शब्दों में- “कबीर ने अपनी प्रखर भाषा और तीखी भाव्यंजना में जिस काव्य की सृजन किया उनके द्वारा साहित्य में युगांतर अवश्य आया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक प्रभाव को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था।
(ग) भाषा एवं काव्य रूप- जहाँ तक भाषा का प्रश्न है इस काल में अवधी और ब्रज दोनों अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची दृष्टिगत होती हैं। सूर और नंददास ने यदि ब्रजभाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया तो तुलसी ने अवधी को अपनाकर उसका उद्धार किया है। जहाँ तक आदिकालीन भाषा का प्रश्न है, वह तो भाषा का संक्रमण काल ही था और रीतिकाल में तो ब्रजभाषा के साथ जैसे खिलवाड़ ही हुआ है। अब रहा काव्यरूपों की विविधता का प्रश्न। इस दृष्टि से यद्यपि आधुनिक काल भक्तिकाल से समुन्नत प्रतीत होता है किंतु काल में भी प्रबंध, मुक्तक, कथाकाव्य, गेय नाटक, जीवन-चरित्र आदि सभी कुछ उपलब्ध होता है जो आदिकाल और रीतिकाल दोनों उसे ऊंचा उठा देते हैं।
(घ) भारतीय संस्कृति का चित्रण- भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता आचार आदि सभी दृष्टियों से भक्तिकाल साहित्य समुन्नत है। इतना ही नहीं आधुनिक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के नियामक तुलसी हैं। उन्होंने अपने मानस के माध्यम से संपूर्ण उत्तरी भारत को राममय बना दिया। उन्होंने इस काव्य में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित की है। एक आलोचक के विचार से तुलसी के राम और सीता तो अलौकिक आदर्श व्यक्ति हैं ही सूर, नंददास आदि के कृष्ण तथा राधा भी समग्ररूप में रीतिकालीन राधाकृष्ण के समान असंयत नहीं हैं। वे पतितपावन बहुत अधिक हैं और लीला विलासी बहुत कम। कुल मिलाकर भक्तिकालीन साहित्य तत्कालीन जनता का उद्धारक, प्रेरक एवं उद्धर्ता है तथा भारतीय संस्कृति और आदर्श का सशक्त उपदेष्टा है।
(ङ) गीति की प्रधानता- भक्तिकालीन काव्य द्वारा संगीत की भी अत्यधिक उन्नति हुई। उस काल के गीतों में आत्मविश्वास की भावना है। अनुभूति की प्रधानता है और अंतःप्रेरणा, जो सहज ही मानव मन को आकृष्ट करने में सफल होती है। इस काल के गीतों का अपना निजी महत्व है।
(च) लोकरंजक एवं लोकरक्षक रूपों की अवतारणा- भक्तिकालीन साहित्य में भगवना के इन दोनों रूपों की अवतारण हुई। प्रो. शिवकुमार शर्मा के शब्दों में तुलसी के राम में शील, भक्ति और सौंदर्य का सुखद समन्वय है। सूर के कृष्ण में सुंदरता की प्रधानता है। तुलसी ने जहाँ मृतक हिंदू राष्ट्र की धमनियों में नव-निर्माण के लिए नवीन रक्त का संचार किया है वहाँ सूर ने जीवन में सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन करके जीवन के प्रति आसक्ति और आस्था को प्रतिष्ठित किया। भक्ति-काव्य जहाँ एक ओर परलोक की ओर झाँकता है वहीं इहलोक को भी पैनी दृष्टि से देखता है। भक्तिकाल एक साथ हृदय, मन और आत्मा की बभक्षा को शांत करता है।
निष्कर्ष
उपर्युकत विवेचन से स्पष्ट है कि इन भक्त कवियों ने भक्ति की ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित की है जिसमें अवगाहन करके भारत के नर-नारी परम पवित्र हो गये। युग-युग की तापित आत्मायें शीतल हो गयीं। उनका रोम-रोम भगवान् की रूप माधुरी का पान करने के लिए लालायित हो उठा। उनकी लीलाओं का सहचर बनने के लिए मचल उठा। धन्य है भक्ति-कवियों की वह अमरवाणी जिसकी अनुगूंज से समग्र भारत रामकृष्णमय हो उठा। फलतः भक्त कवियों की यह अमरवाणी लीलाधर की वाणी बनकर जनमानस का अनुरंजन करने लगी। धन्य है ऐसी व्यापक प्रभावशाली भक्तिकालीन कविता। निःसंदेह भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग ही है।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ- राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
- प्रमुख हिन्दी गद्य-विधाओं की परिभाषाएँ
- आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ- प्रवृत्तियों की विशेषताएँ, आदिकालीन साहित्य का महत्त्व
- गीति काव्य का स्वरूप | गीति काव्य की विशेषताएँ | गीतिकाव्य परम्परा में मीरा के स्थान का निरूपण | मीरा के गीति काव्य परम्परा की विशेषताएँ
- आदिलकाल के विभिन्न नाम | आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत | आदिकाल के नामकरण की समस्या
- हिन्दी साहित्य के काल विभाजन की समस्या | काल विभाजन के सन्दर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विभिन्न मत
- साहित्य के इतिहास संबंधी कुछ समस्याएँ | हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएँ
- आदि कालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ | आदिकाल के प्रमुख रासो काव्य | रासो काव्य परंपरा का सामान्य परिचय
- आदिकालीन धार्मिक साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ | सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य एवं जैन साहित्य की प्रवृत्तियाँ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]