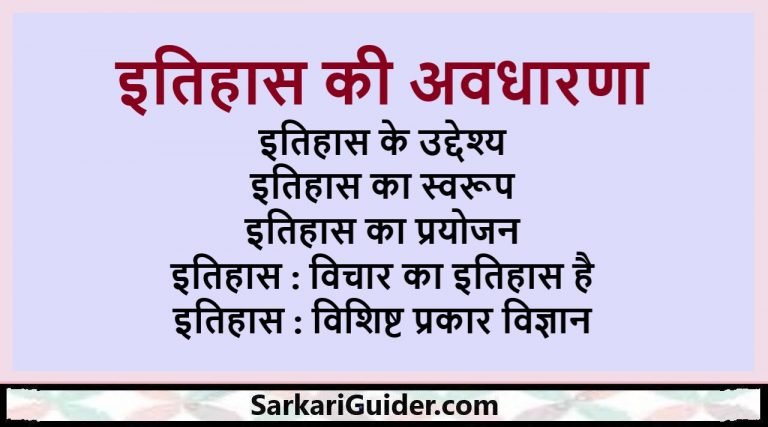दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति | Neolithic culture of South India in Hindi
दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति | Neolithic culture of South India in Hindi
दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति
ऋतु-अपक्षय के फलस्वरूप घिसा-पिटा दक्षिण भारत का पठारी भाग भूतात्त्विक बनावट की दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भू-खण्ड है। इसमें अनेक छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, ताम्रपर्णी और बैगाई आदि नदियों की घाटियों में दक्षिण भारत के नव पाषाण काल के अधिकांश पुरास्थल पहाड़ियों पर या तलहटियों में स्थित हैं।।
दक्षिण भारत से ही सर्वप्रथम नव पाषाणिक ओपदार प्रस्तर उपकरण सन् 1842 में कर्नाटक के लिंगसिगुर नामक पुरास्थल से मिले थे। नव पाषाण काल के सम्बन्ध में अध्ययन एवं अनुसंधान की दृष्टि से भी इस क्षेत्र का अध्यन्त विशिष्ट स्थान है। सन् 1947 में मार्टीमर ह्वीलर के द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरि के उत्खनन के पूर्व दक्षिण भारत की नव पाषाण काल की संस्कृति के काल-क्रम आदि के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। ह्वीलर के द्वारा संचालित इस उत्खनन के फलस्वरूप सांस्कृतिक विशेषताओं तथा कालानुक्रम आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। विगत तीन-चार दशकों में इस क्षेत्र के अनेक पुरास्थलों की खोज तथा कतिपय के उत्खनन किये गए हैं। बहुसंख्यक उत्खनित पुरास्थल कर्नाटक प्रदेश में स्थित है, जब काय अन्य आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विद्यमान हैं। कर्नाटक प्रदेश के उत्खनित पुरास्थलों में ब्रह्मगिरि के अतिरिक्त संगनकल (बेलारी जिला), पिकलीहल (रायचूर जिला), मास्की (रायचूर जिला), टेक्कल-कोटा (बेलारी जिला), हल्लूर (धारवाड़ जिला), टी० नरसीपुर (बलारी जिला), कुपगल (बेलारी जिला), हेम्मिगे (मैसूर जिला), तेरदल (बीजापुर जिला) तथा कोडेकल (गुलबर्गा जिला), का उल्लेख किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश में उतनूर (महबूबनगर जिला), नागार्जुनीकोण्डा (सुन्दूर जिला) पलवॉय (अनंतपुर जिला) तथा सिंगनपल्ली कर्नूल जिला) का अभी तक उत्खनन हुआ है। उत्तर आर्काट जिले में स्थित पैय्यमपल्ली तमिलनाडु प्रदेश का प्रमुख उत्खनित पुरास्थल है। इस प्रकार उपर्युक्त पुरास्थलों के प्रसार पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि मैंये समस्त पुरास्थल गोदावरी नदी के दक्षिण में कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियों की घाटियों में स्थित हैं। दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति के निर्माता प्रारम्भ में पहाड़ियों के ऊपर अथवा ढलान पर निवास करते थे।
सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति को दो या तीन उपकालों में विभाजित किया जा सकता है प्रथम उपकाल के अंतर्गत उतनूर प्रथम काल, पिकलीहल का प्रारम्भिक नव पाषाण काल, मास्की का प्रथम काल, ब्रह्मगिरि का प्रथम ‘अ’ काल रखा जा सकता है। इस उपकाल में गिनी चुनी ओपदार प्रस्तर की कुल्हाड़ियाँ, ब्लेड- प्रधान लघु पाषाण उपकरण, हस्त-निर्मित हल्के धूसर रंग तथा काले रंग के मृद्भाण्ड, ककुदमान, पशुओं की मृणमूर्तियाँ, मवेशियों और भेड़-बकरियों की हड्डियाँ आदि पुरावशेष मिलते हैं। गोबर के ढेर के जलने से निर्मित राख के टीले इसी काल से सम्बन्धित हैं।
द्वितीय उपकाल में ओपदार प्रस्तर-कुल्हाड़ियों एवं लघु पाषाण उपकरणों का आधिक्य मिलता है। धूसर या सलेटी तथा काले मृद्भाण्ड लगभग अत्यल्प हो जाते हैं और इनका स्थान चमकाये हुए धूसर मृद्भाण्ड ले लेते हैं। पिकलीहल के उत्तर नव पाषाण काल, ब्रह्मगिरि प्रथम ‘ब’ काल, संगनकल प्रथम, टेक्कलकोटा प्रथम, हल्लूर द्वितीय उपकाल को इस काल में रख सकते हैं। इस काल में बाँस-बल्ली की झोपड़ियों का निर्माण होने लगा जिनके फर्श मिट्टी से लीप-पोत कर चिकने बनाये जाते थे।
तीसरे उपकाल में दूसरे उपकाल की अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त चाक पर बने हुए पाण्डु रंग के बिना चमकाये हुए मृद्भाण्ड मिलते हैं। इनके साथ ही ताम्र-उपकरण भी मिलने लगते हैं जिससे यह इंगित होता है कि दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति महाराष्ट्र की ताम्र-पाषाणिक जोर्वे संस्कृति से प्रभावित हो रही थी।
आवास
दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति के लोग बाँस-बल्ली से निर्मित गोलाकार अथवा अण्डाकार झोपडियों में रहते थे। ब्रह्मगिरि, मास्की, पिकलीहल आदि के उत्खननों से झोपड़ियों के बनाने में प्रयुक्त स्तम्भों के गर्त मिले हैं। झोपड़ियों के फर्श को गोबर तथा मिट्टी से लीप-पोत कर साफ-सुथरा बनाया जाता था। कभी-कभी चूने के घोल से भी पुताई की जाती थी। झोपड़ियो के फर्श की प्रायः समय-समय पर मरम्मत होती रहती थी तथा कभी-कभी फर्श को ऊँचा भी किया जाता था।
मिट्टी के बर्तन
हस्त-निर्मित मृद्भाण्डं बनाने की कला से प्रारम्भ से ही ये लोग परिचित प्रतीत होते हैं। धूसर या सलेटी तथा लाल रंग के मृद्भाण्ड मुख्यतः प्रचलित थे। पकाने के बाद मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण भी किया जाता था। ब्रह्मगिरि, पास्की तथा पिकलीहल से चित्रकारी से युक्त मृद्भाण्ड के ठीकरे मिले हैं। चित्रित अभिप्रायों में रेखाकृतियाँ प्रमुख हैं जिन्हें पकाने के बाद बैंगनी रंग से बनाते थे। सलेटी रंग के बर्तनों पर गैरिक अथवा कपिश रंग से पट्टी (Band) बनाते थे। कभी-कभी बर्तन की बाहरी सतह को रगड़ कर चमकाया जाता था। प्रमुख पात्र-प्रकारों में तश्तरियाँ, कटोरे, घड़े तथा बर्तनों के ढक्कनों आदि का उल्लेख किया जा सकता है।
उपकरण
प्रमुख प्रस्तर उपकरणों में त्रिभुजाकार समन्तान्त वाली ओपदार कुल्हाड़ियों, बसूलों, छेनियों एवं गैंतियों आदि का उल्लेख किया जा सकता है। उपकरणों के निर्माण के लिए ट्रैप तथा बेसाल्ट नामक प्रस्तरों का उपयोग किया जाता था। हथौड़े, सिल-लोढ़े, गदाशीर्ष तथा प्रस्तर उपकरणों को चिकना एवं चमकदार बनाने वाले पाषाणों आदि की भी गणना कर सकते हैं। टी नरसीपुर को छोड़कर अन्य सभी पुरास्थलों पर चर्ट, चाल्सेडनी, क्वार्ट्ज, जैस्पर, फ्लिण्ट, अगेट आदि के बने हुए लघु पाषाण उपकरण प्रारम्भ से अन्त तक बराबर मिलते हैं। दाँतेदार(Serrated), कुण्ठित पृष्ठवाले ब्लेड, स्क्रेपर, चान्द्रिक, समलम्ब चतुर्भुज तथा बेधक आदि प्रमुख लघु पाषाणिक उपकरण मिलते हैं। कतिपय पुरास्थलों से हड्डी के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। इन पुरास्थलों में पलवॉय का उल्लेख किया जा सकता है। वहाँ से हड्डी के बाण मिले हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति में हड्डी के बने हुए उपकरणों की संख्या बहुत सीमित प्रतीत होती है। सिलखड़ी के मनके तथा ककुदमान पशुओं की हस्त-निर्मित कतिपय मृण्मूर्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं।
कृषि तथा पशु-पालन
दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति के लोग कृषि तथा पशु- पालन से परिचित प्रतीत होते हैं। टेक्कलकोटा और पैय्यमपल्ली से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग चना, मूंग, कुलथी तथा रागी की खेती करते थे। भेड़- बकरियों के अतिरिक्त गाय-बैल तथा भैंस और सुअर आदि प्रमुख पालतू पशु थे। आन्ध्र प्रदेश के उतनूर तथा पलवॉय और कर्नाटक के कुपगल एवं कोडेकल नामक राख के टीलों के उत्खनन से भी पशु-पालन की पुष्टि होती है। पिकलीहल के पास शिला-चित्रों में भी ककुदमान बैलों के चित्र अंकित मिलते हैं। इनके अलावा कुकुदमान बैलों की मृण्मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। उतनूर के राख के टीले के उत्खनन से पशु-बाड़े में प्राप्त पशुओं के खुरों के निशान के प्रमाण से भी पशु-पालन प्रधान अर्थ-व्यवस्था का संकेत मिलता है।
शवाधान
दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति से सम्बन्धित कई पुरास्थलों से शवाधान के प्रमाण मिलते हैं। मुर्दो को मकान के अन्दर फर्श के नीचे या मकान के समीप ही बाहर दफनाया जाता था लेकिन नागार्जुनीकोण्डा में आवास क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान मिला है। विस्तीर्ण शवाधान (Inhumation), आंशिक शवाधान (Fractional burial) तथा अस्थि कलश (Urn burial) ये तीन प्रकार की अन्त्येष्टि-संस्कार की परम्पपराएँ प्रचलित थीं। जमीन में कब्र खोदकर प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों को चित लिटाकर दफनाया जाता था। अन्त्येष्टि- सामग्री के रूप में मृद्भाण्ड और यदा-कदा प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ तथा लघु पाषाण उपकरण भी रखे हुए मिलते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को शव-कलशों में भर कर दफना दिया जाता था। शिशुओं के अस्थि-कलशों में अन्त्येष्टि-सामन का प्रायः अभाव मिलता है।
कालानुक्रम
दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति से सम्बन्धित अनेक पुरास्थलों से रेडियो कार्बन तिथियाँ उपलब्ध हैं। संगनकल, टेक्कलकोटा, हल्लूर, टी० नरसीपुर, तेरदल, कोडेकल, उतनूर, नागार्जुनीकोण्डा, पलवॉय, पैय्यमपल्ली आदि पुरास्थलों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों के आलोक में दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति के प्रथम उपकाल का कालानुक्रम 2,500 से 2,000 ई०पू० के मध्य तथा द्वितीय उपकाल का काल-मान 2,000 या18,00 ई०पू० से 1,400 ई०पू० के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। तृतीय उपकाल का तिथिक्रम 1,400 ई०पू० से 1,000 ई०पू० के मध्य रखा जा सकता है। इस बात की प्रबलतम सम्भावना है कि इस संस्कृति के प्रथम उपकाल की प्रारम्भिक सीमा रेखा और पीछे खींची जा सकती है।
सादृश्य तथा उत्पत्ति
दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है। मार्टीमर ह्वीलर ने ऐसी सम्भावना प्रकट की थी कि दक्षिण भारत की नव पाषाण काल की संस्कृति दक्षिण-पूर्व एशिया की नव पाषाणिक संस्कृति से प्रभावित मानी जा सकती है। उनका विचार था कि चीन के रास्ते मध्य एशिया के क्षेत्र से नव पाषाण काल की संस्कृति का दक्षिण भारत में आगमन हुआ होगा। दूसरे शब्दों में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पूर्व को इस प्रकार का संचरण हुआ होगा। इस सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि यदि दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति दक्षिण-पूर्व एशिया की नव पाषाण काल की संस्कृति से प्रभावित होती तो दक्षिण भारत के पुरास्थलों पर भी स्कन्धित तथा गोलसमन्तान्त वाली प्रस्तर की कुल्हाड़ियाँ मिलतीं। इसके विपरीत दक्षिण भारत के पुरास्थलों से नुकीले समन्तान्त वाली त्रिभुजाकार प्रस्तर-कुल्हाड़ियाँ ही मिलती हैं। इस प्रकार प्राप्त पुरातात्त्विक साक्ष्यों के अवलोकन से ह्वीलर के मत की पुष्टि नहीं होती है।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- विध्य क्षेत्र की नव पाषाणकालीन संस्कृति | Neolithic culture of the Vindhya region in Hindi
- मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति | Neolithic Culture of the Middle Ganga Valley in Hindi
- भारत में प्रागैतिहासिक काल | पुरापाषाण काल | मध्य-पाषाण काल | उत्तर-पाषाण काल | ताँबे और काँसे का काल | लौह-काल | भारत में प्रागौतिहासिक काल के इतिहास
- निम्न पुरापाषाण काल | निम्न पुरापाषाणकाल के अनुक्रम की विवेचना
- मध्य गंगा घाटी का सांस्कृतिक अनुक्रम | अनु-पुरापाषाण काल | आरम्भिक मध्य पाषाण काल | परवर्ती मध्य पाषाण काल | सराय नाहर राय | गंगाघाटी के सांस्कृतिक अनुक्रम की विवेचना
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]