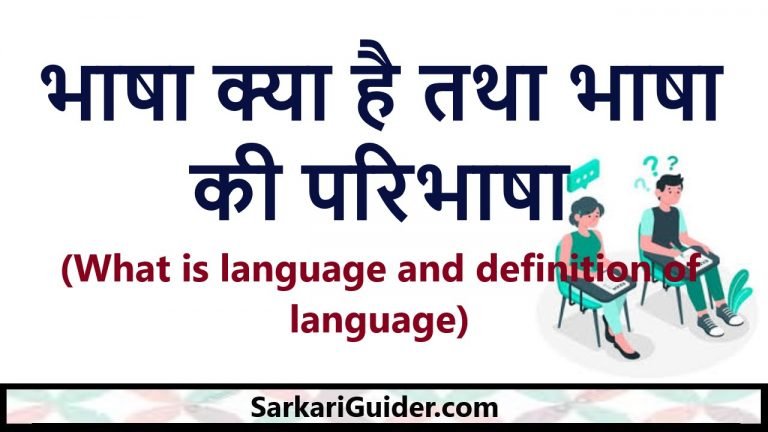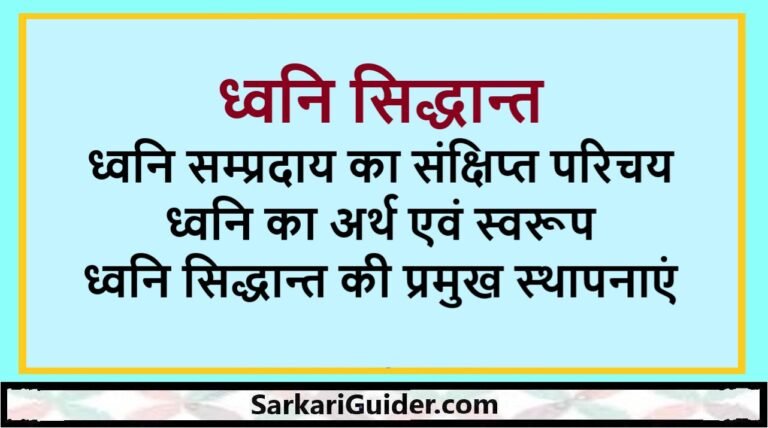घने नीम तरु तले | विद्यानिवास मिश्र- घने नीम तरु तले
घने नीम तरु तले | विद्यानिवास मिश्र- घने नीम तरु तले
घने नीम तरु तले
- वैसे आजीवन मेरा प्राप्य है नीम की गिलोय, जिसे मुए संस्कृत वाले अमृत कहते है, पर मैं इस प्राप्य के साथ अपना मन न मिला सका। न जाने कितनी बार आँखे करुआ आयी हैं, जीभ लोढ़ा हो गयी है, कान झनझना उठे और मन तिता गया है, पर तब भी इस नीम से भी अधिक तीती दुनिया से मैं तीता न हो सका, यह जले स्वभाव का दोष नहीं तो क्या है, नीम तो सुनता हूँ लगता भर तीता है, पर अपने परिणाम में मधुर होता है, पर इसके प्रतिरूप मानव जगत् का सप्तातिक्त तो आदि तो से अन्त तक एकरस है। वैसे दुःख की स्मृति कभी-कभी बहुत प्यारी होती है पर तिक्त अनुभवों की स्मृति तो पहले से चौगुनी असह्य होती है और इसीलिए वह तभी उभरती थी जब कोई वैसा ही अनुभव सामने आता है।
सन्दर्भ- प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक युग के प्रतिभा सम्पन्न ललित निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र के ‘घने नीम तरु तले’ नामक निबन्ध संग्रह से लिया गया है। निबंधकार ने ‘घने नीम तरु तले’ नामक निबंध में जीवन और नीम के वृक्ष के सम्बन्ध सूत्र को उजागर किया है।
प्रसंग- ललित निबंधकार ने प्रस्तुत निबंध में नीम के वृक्ष और जीवन के सम्बन्ध सूत्र को रेखांकित किया है।
व्याख्या- निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि बचपन से ही मुझे नीम की दातून अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि वह तिताती है जिसके कारण मुझे बबूल की गिलोय अच्छी लगती है। वैसी मेरी आजीवन प्राप्त वस्तु नीम की दातून थी जिसे संस्कृत वाले अमृता कहते हैं किन्तु मैं इस तितायी के कारण इससे अभी तक अपना मन नहीं मिला सका हूँ और इस दातून को करते समय न जाने कितनी बार आँखे मेरी कड़वाहट के कारण आँसुओं से भर आयी थीं, और जीभ लोढ़ा अर्थात् मोटी (अस्वादमय) हो गयी है। जिससे कान झनझना गये तथा मन कटुमय हो गया किन्तु इस नीम से तीती दुनिया उसमें (छल, कपट) आदि भरा हुआ है मैं इस दुनिया से तीता नहीं हो सका जिससे कहा जा सकता है कि मैं नीम से जलता हूँ, नीम के बारे में तो सिर्फ कहा जाता है कि यह तीता भर लगता किन्तु इसके सेवन से परिणाम सुखद मिलता है किन्तु इसके विपरीत मानव जगत् का जो यह छल कपट है वह सदैव एक सा रहता है। किन्तु दुःख की स्मृति कभी-कभी बहुत प्यारी होती है किन्तु तिक्त अनुभवों की स्मृति तो पहले की अपेक्षा बाद में अत्यधिक कष्टमय होती है। इसलिये वह उसी समय याद आती है जब कभी कोई वैसा ही अनुभव या दर्द सामने प्रस्तुत होता है।
- जीवन लघु है, लघु प्रेम है, लघु स्वप्न है और अन्त में दिन सलामत और जीवन व्यर्थ है, लघु आशा है, लघु घृणा है और अन्त में है रात सलामत। कषायरस दिन और रात दोनों की सलामत मानता है और साहित्य भी। साहित्य जीवन की व्यर्थता और बेईमानी से व्यथित नहीं होना जानता, इसलिए उसे पर ज्ञान हो पाने पर भी कि जीवन वह छलना है जो अपने प्रियतम को एक दिन तज ही देती है, इतना आश्वासन रहता है कि उस जीवन-छलना को गाली देने का अधिकार तो बच रहा है और यही बहुत है।
संदर्भ- पूर्ववत्।
व्याख्या- ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि यह जीवन अत्यन्त लघु है, प्रेम भी अत्यन्त लघु है, स्वप्न भी अत्यन्त छोटा है और अन्त में यह दिन सलामत है और यह जीवन ही पूरा व्यर्थ है, लघु रूप में आशायें हैं, लघु रूप में यह घृणा है और अन्त में दिन की भांति रात्रि भी सलामती है और यह जो नीम का यह कयासरस अर्थात कडुआ रस है यह दिन और रात दोनों की सलामती की दुआ मानता है साथ ही साथ साहित्य भी इन सभी की सलामती की दुआ माँगता है और यह साहित्य जीवन रूपी व्यर्थता और बेईमानी से व्यथित (घबराना) नहीं होना जानता है, इसलिये उसको इसका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी कि यह जीवन एक न एक दिन अन्त में अपने प्रियतम को अन्ततः त्याग ही देता है, किन्तु दोनों में अन्तर मात्र यह रह जाता है कि उस जीवन रूपी छलना को गाली देने का अधिकार तो बच जाता है और यही बहुत है, जिस कडुये पर के साथ ही हमारा जो अन्तर्विरोध है, जिससे मुझे शान्ति की प्राप्ति भी मिलती है।
- अब सोचिए, नीम में क्या मिलता हैं, गन्ध असह्या, स्वाद असह्या, यहाँ तक कुसुमित नीम का रूप भी असह्या, चारों ओर सफेद बुन्दियाँ छिटकी हुई, पत्तियाँ इतनी दूर-दूर कटी-कटी कि पेड़ की जड़ विचारी ओट के लिए तरसती रहती है। इसलिए आम में फल न आये, महुए में कूँचे न लगे, गुलाब में कली न आये और मधुमास सूना चला जाय, पर नीम बराबर फूलेगा, मनों फूलेगा, बराबर फरेगा और इतना फरेगा कि अकुला देगा, इतना बेशर्म कि कट जाने पर भी इसकी लकड़ी में घुन न फटकेगा, यदि कहीं नीम की शहतीर लग गयी हो तो वर्षा होते ही जो आकूल दुर्गन्धि व्यापती है तो प्रान औतियाताप हो उठते हैं। पर हाय रे नियति का विधान कि घर-घर बिना जतन-सेवा के नीम धरती की छाती का स्नेह छीनकर खड़ा मिलेगा।
संदर्भ- पूर्ववत्।
व्याख्या- निबंधकार जी कहते है कि अब सोचिए कि इस नीम में वस्तुतः हमें क्या प्राप्त होता है, इसकी गन्ध असहनीय होती है, स्वाद असहनीय होता है, यहाँ तक कि उसका जो फूल रूप है वह भी मन को शोभा या आकृष्ट नहीं कर पाता है जिन पर चारों ओर छोटी-छोटी बुन्दियाँ छिटकी हुयी होती हैं, और उसकी पत्तियाँ दूर-दूर तक कटी होती हैं कि पेड़ की जड़ भी उसकी छाया के लिये तरसता रहता है। आम में फल नहीं लगता है तो नहीं लगे, महुये में फँचे न लगें, गुलाब में कली न आये किन्तु यह नीम का पेड़ सदैव फूलता रहता है, और इतना फरता है कि वह आकुल कर देगा। वह इतना ही नहीं यदि उसके पेड़ की लकड़ी काट भी दी जाये तो उसमें घुन भी नहीं लगता है और यदि कहीं नीम की लकड़ी की शहतीर घर में लगा दी जाये तो वह भी बरसात होने पर दुर्गन्ध देने लगती है जिससे प्राण तक भी छटपटाने लगते हैं। पर हाय रे नियति कि प्रत्येक घर- घर में बिना सींचे-जुताई, के यह नीम का पेड़ धरती की स्नेह छाती चीरकर आपकों हर जगह दिखायी देगा।
4.”सुनो तुम लोग जो इस विषैली इमली के नीचे छहाँ रहे हो, यह ठीक नहीं, एक आदमी ने विलायत में यह प्रयोग किया, लगातार छः महीने पहले वे इमली के पेड़ के नीचे विश्राम करते, इमली खाते, इमली का पना पीते और इमली की लकड़ी से रसोई पकाते यात्रा करते रहे और उन्हें भयंकर राजयक्ष्मा हो गया, तब उन्होंने छ: महीने नीम के साथ यही प्रयोग किया और वे नीरोग हो गये। सो इस कहानी से यह शिक्षा ग्रहण करो कि इमली कितनी हानिकारक होती है?”
संदर्भ- पूर्ववत्।
व्याख्या- निबन्धकार जी कहते हैं कि मेरे अध्यापक ने एक बार आकर कक्षा में कहा कि तुम लोग जो इस इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुये होतो यह इमली अत्यन्त विषैली है क्योंकि इस पेड़ का विलायत में एक बार प्रयोग किया गया था कि जो व्यक्ति इमली के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, इमली खाते हैं, इमली का पना पीते हैं तथा इमली की लकड़ी से खाना बनाते हैं उन्हें भंयकर कष्टसाध्य क्षय रोग हो गया किन्तु जब उन्होंने नीम के साथ छः महीने तक यही प्रयोग किया तो वे सभी स्वस्थ्य व निरोगी हो गये। इसलिये इस प्रयोग से यह शिक्षा लेनी चाहिये कि नीम का पेड़ कितना अनमोल है।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- पारिभाषित शब्द | पारिभाषिक शब्द के प्रकार | पारिभाषित शब्दों की आवश्यकता
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अनुवाद का महत्व | रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व
- मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन का प्रारूप | मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन की प्रविधि
- समाचार लेखन | समाचार लेखन की परिभाषा | समाचार की कुछ परिभाषाएँ | समाचार के प्रमुख तत्व | समाचार लेखन की प्रक्रिया | वैविध्यपूर्ण समाचार लेखन | समाचार का प्रारूप
- सम्पादकीय | सम्पादकीय की संरचना | सम्पादकीय की भाषा शैली | सम्पादक समाचार पत्र का प्रमुखी शिल्पी
- अनुवाद के क्षेत्र | अनुवाद का क्षेत्र राष्ट्रीय ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय है
- सम्पादन के आधारभूत तत्व | सम्पादन कला
- भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है सन्दर्भः- प्रसंग- व्याख्या | भारन्तेन्दु हरिश्चन्द्र भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है
- कुटज सन्दर्भः- प्रसंग- व्याख्या | हजारी प्रसाद द्विवेदी – कुटज
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]