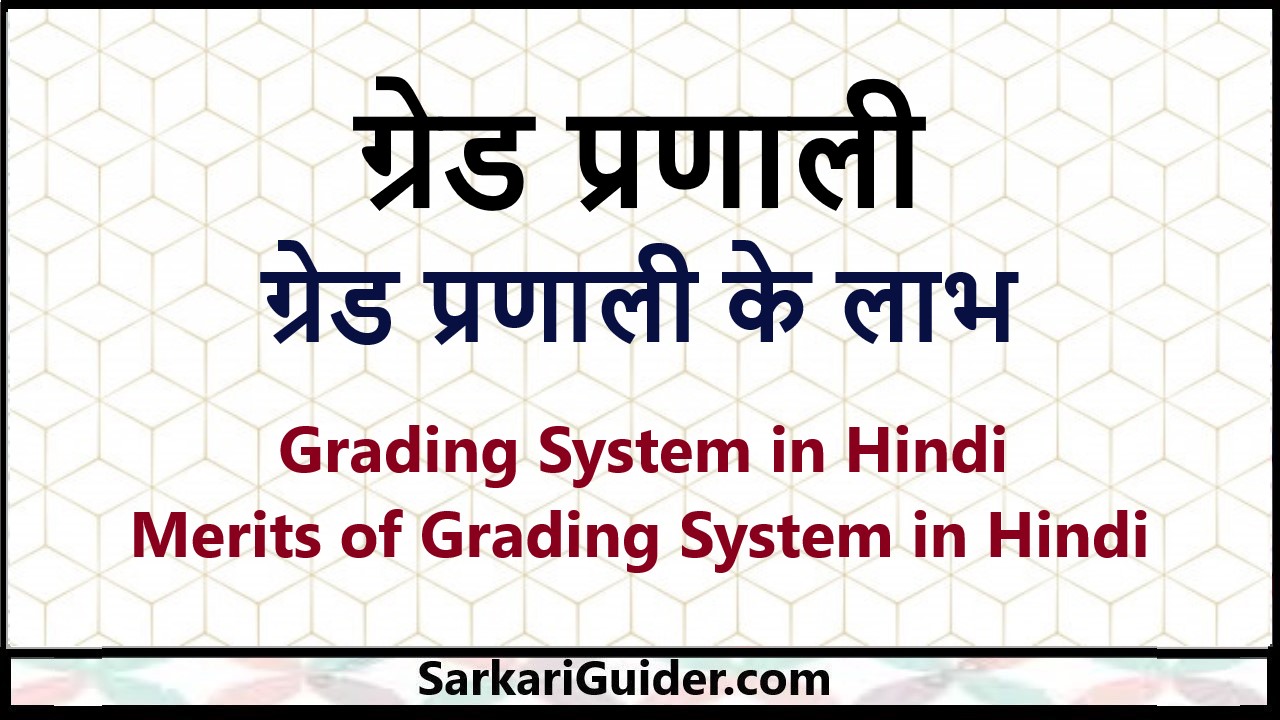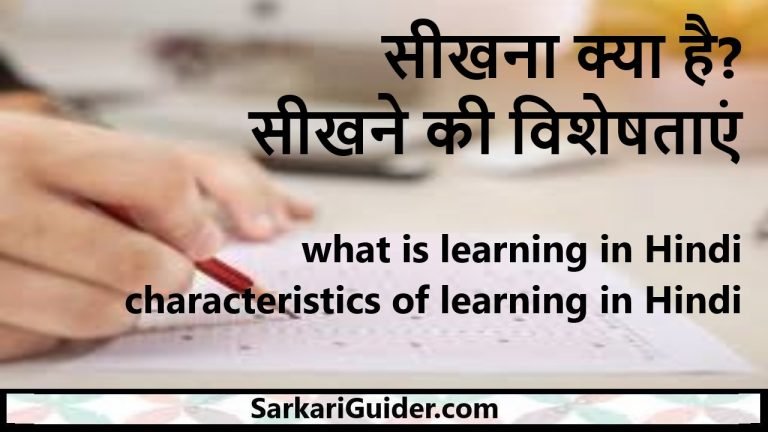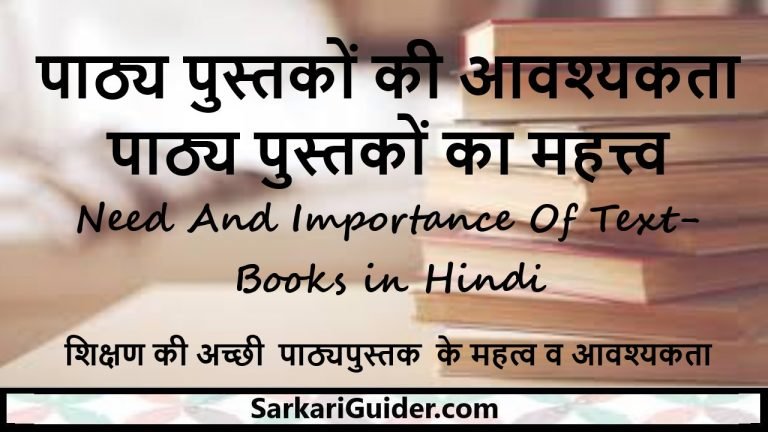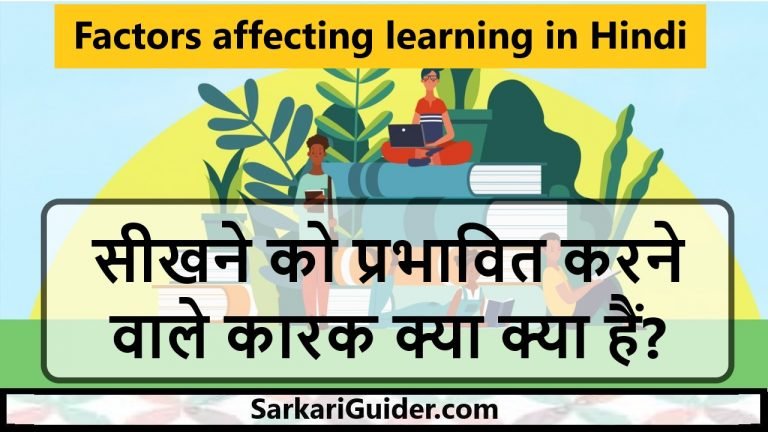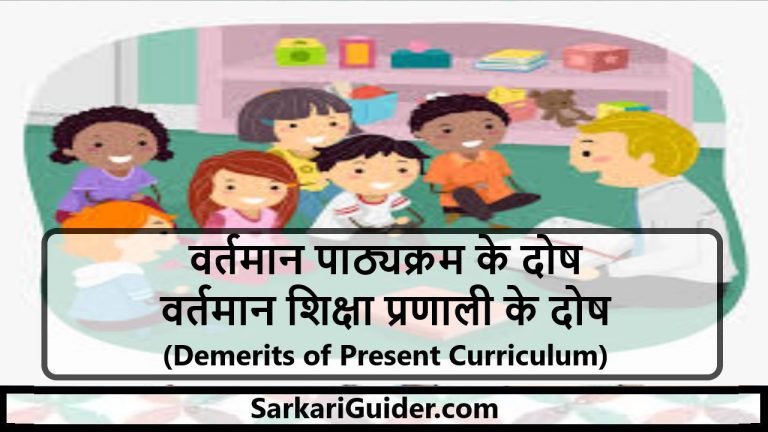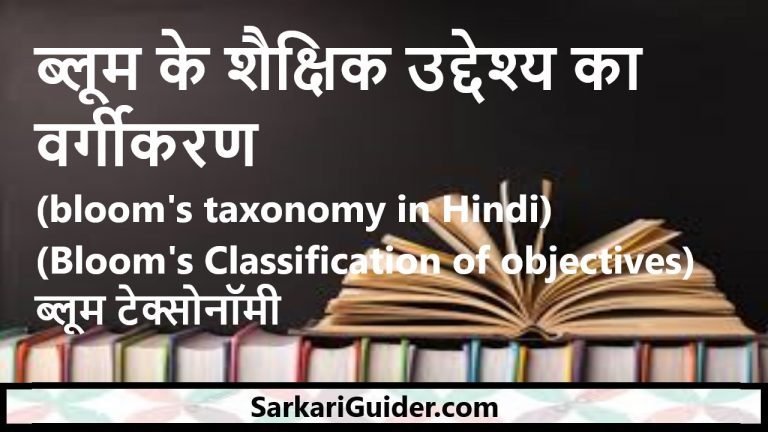ग्रेड प्रणाली | ग्रेड प्रणाली के लाभ | Grading System in Hindi | Merits of Grading System in Hindi

ग्रेड प्रणाली | Grading System in Hindi | ग्रेड प्रणाली के लाभ | Merits of Grading System in Hindi
ग्रेड प्रणाली
हमारे राष्ट्र में वर्तमान समय में विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धि मापने के लिए छात्रों के द्वारा परीक्षा में दिये उतरों के लिये परीक्षकों के द्वारा अंक प्रदान करने की विधि ही अधिक प्रचलित है जिसमें सामान्यतः 101 बिन्दु अंकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है अर्थात छात्रों को 0 से 100 तक के कुल 101 प्राप्तांकों में से कोई एक प्राप्तांक प्रदान किया जाता है । इसके साथ-साथ छात्रों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी देने तथा अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए पूर्व निर्धारित मन चाहे विभाजन बिन्दुओं Pre decided Arbitrary Cut-off point का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के मनचाहे विभाजन बिन्दु न केवल वर्षों बल्कि अनेक दशकों तक बिना किसी संशोधन के चलते रहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि ये विभाजक बिन्दु बिना किसी तर्कसंगत आधार के सदियों पूर्व निर्धारित किये गये हैं। अंकन की इस परम्परागत प्रणाली की आलोचना समय-समय पर शिक्षाविज्ञ, अध्यापकगण, अभिभावकंवृन्द, शोधकर्ता तथा छात्रों के द्वारा की जाती रही है। अंकन विधि का जटिल, समस्यात्मक तथा त्रुटियुक्त होना इस आलोचना के प्रमुख कारण हैं। वास्तव में अंकन की इस परम्परागत विधि में दो अत्याधिक घातक कमियाँ हैं। प्रथम, परीक्षक के निर्णय में जरा सी चूक या अन्तर कभी-कभी मात्र एक या दो अंक के कारण छात्र की श्रेणी अथवा उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल सकती है। उदाहरण के लिए सामान्यतः वर्तमान परीक्षा प्रणाली में 59.75 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को द्वितीय श्रेणी तथा 60 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी दी जाती है। स्पष्ट है कि एक दो अंकों के इस जरा से अन्तर से द्वितीय श्रेणी वाला छात्र प्रथम श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी वाला छात्र द्वितीय श्रेणी पा सकता है। इसी प्रकार के जरा से अन्तर से छात्र उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण भी हो सकता है। उत्तीर्ण- अनुत्तीर्ण करने तथा श्रेणी प्रदान करने की यह विधि उपयुक्त तथा वैध स्वीकार की जा सकती थी, यदि अंकन पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित ढंग से करना सम्भव होता। अर्थात यदि परीक्षकों के द्वारा छात्रों को प्रदान अंक उन की योग्यता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाले होते, परन्तु ऐसा नहीं है। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान अंकन प्रणाली में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ हैं तथा परीक्षकों द्वारा प्रदान अंक उनकी व्यक्तिगत मानसिक विचारधाराओं (Idiosyncrasies) के प्रभाव से युक्त रहते हैं। सांख्यकीय अनुसंधानों के अनुसार अंक प्रदान करने में 5 प्रतिशत से अधिक की त्रुटि होने की सम्भावना लगभग 50 प्रतिशत होती है। इसके अलावा परीक्षकों के द्वारा प्रदान अंक छात्रों की योग्यता, ज्ञान, स्मृति, बुद्धि या, अभिव्यक्ति क्षमता आदि में से किसी एक अथवा एक से अधिक के द्योतक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षक के द्वारा प्रदान किये गये अंकों में व्यक्तिनिष्ठता हो सकती है। वस्तुतः छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को इतनी यथार्थ (Accuracy) तथा असंदिग्धत (Precise) ढंग से नहीं मापा जा सकता है कि इस मापन के लिए 101 बिन्दु मापनी का प्रयोग तर्कसंगत ढंग से किया जा सके।
वर्तमान अंकन विधि की दूसरी कमी विभिन्न विषयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के मानदण्डों में प्रयाप्त विभिन्नताओं का होना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कुछ विषयों में परीक्षकों के द्वारा कम अंक आवंटित होते है। उदाहरण के लिए गणित या विज्ञान जैसे विषयों में प्रायः शून्य मे 100 तक के पूर्ण प्रसार में परीक्षकों द्वारा प्राप्तांक प्रदान किये जाते हैं। जबकि भाषा या इतिहास जैसे विषयों में प्रायः 20 से 70 प्रतिशत तक ही प्राप्तांक प्रदान किये जाते हैं। परीक्षकों के द्वारा प्राप्तांकों की न्यूनतम व उच्चतम सीमाओं तथा प्रसार के निर्धारण में उनकी अपनी व्यक्तिगत पसन्द के साथ-साथ विषय की प्रकृति की भी अवांछित भूमिका रहती है। ऐसी स्थिति में बिभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का योग करके श्रेणी ज्ञात करने की प्राचीन परम्परा का कोई वैज्ञानिक आधार प्रतीत नहीं होता। विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों के योगफल के आधार पर छात्रों का योग्यता क्रम Rank Order विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों के प्रसार, मध्यमान, तथा मानक विचलन से बुरी तरह से प्रभावित होता है । जैसे यदि हिन्दी व गणित विषयों में प्राप्तांको का प्रसार क्रमशः 30 से 75 तक ( प्रसार = 45) तथा 5 से 95 तक ( प्रसार = 90) हो तथा इन दो विषयों के प्राप्तांको को जोड़कर यदि सामूहिक योग्यता क्रम बनाया जायेगा तो गणित को हिन्दी की अपेक्षा दो गुना भार (Weightage) मिलेगा । कुल अंकों की गणना में छात्र की गणित योग्यता का महत्व हिन्दी योग्यता की अपेक्षा दो गुना होने के कारण सम्भावना यही होगी कि गणित योग्यता वाले छात्र ही सामूहिक योग्यता सूची में श्रेष्ठ क्रम प्राप्त करेंगे। यह बात सारिणी में प्रस्तुत काल्पनिक प्राप्तांकों से स्पष्ट हो सकेगी।
दो विषयों में 6 छात्रों के काल्पनिक प्राप्तांक
(Hypothetical Marks of Six Students in Two Subjects)
(दोनों विषयों में प्राप्तांकों का प्रसार भित्न-भित्र है )
|
विषय |
छात्र |
|||||
|
रमेश |
मनोज |
रवि |
सोनाली |
मनीष |
आरती |
|
|
हिन्दी |
30 |
39 |
48 |
57 |
66 |
75 |
|
गणित |
95 |
77 |
59 |
41 |
23 |
5 |
|
कुल प्राप्तांक |
125 |
116 |
107 |
98 |
89 |
80 |
सारणी से स्पष्ट है कि रमेश तथा आरती दोनों ही एक विषय में सर्वश्रेष्ठ तथा एक विषय में सबसे कमजोर हैं। परन्तु इसके बावजूद भी कुल योग की दृष्टि से छहों छात्रों में रमेश सर्वश्रेष्ठ तथा आरती सबसे कमजोर प्रतीत हो रही है। यह विसंगति दोनों विषयों के प्राप्तांकों के प्रसार के अन्तर के कारण है। वास्तव में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का मानक विचलन समान होने पर ही कुल प्राप्तांकों के योगफल में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को समान भार (Weightage) मिलता है।
101 बिन्दु अंकन की इन दो मुख्य कमियों के कारण शिक्षाविज्ञ, विशेष कर परीक्षा सुधार के कार्य में सलग्र शिक्षाशास्त्री व अनुसंधानकर्ता, समय-समय पर वर्तमान अंकन प्रणाली में परिवर्तन करने का सुझाव देते रह हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) तथा शिक्षा आयोग (1964-66) ने अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग करने का सुझाव दशकों पूर्व दिया था। परीक्षा सुधार पर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय के कार्यदल ने भी सन् 1971 में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने का सुझाव दिया था। सन् 1975 में ष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के द्वारा भी ग्रेड के प्रणाली प्रयोग की सिफारिश का गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के द्वारा प्रकाशित “परीक्षा सुधार : एक कार्य योजना” Examination Reforms: A Plan of Action) नामक प्रतिवेदन में भी ग्रेड को स्वीकार करने का समर्थन किया गया है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्रियान्वयन योजना (Plan of Action) में भी विश्वविद्यालय तर पर ग्रेड प्रणाली को स्वीकार करने की बात कही गयी है। अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को नान के प्रस्ताव में मूलभूत मान्यता यह है कि छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 101 समूहों विभाजित करना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। क्योंकि न तो अंक प्रदान करने का कोई पर्याप्त, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा सार्थक आधार उपलब्ध होता है तथा न ही परीक्षकों में इतनी क्षमता होती है कि वे छात्रों को 101 समूहों में त्रुटि रहित ढंग से बाँट सकें। परीक्षक अधिक से अधिक छात्रों को कुछ सीमित संख्या वाली गुणात्मक श्रेणियों 5, 7, या 9 आदि में ही सफलता पूर्वक विभाजित कर सकते हैं। इन गुणात्मक श्रेणियों को ही ग्रेड श्रेणी कहा जाता है। इन श्रेणियों को संकेताक्षर जैसे ए (A), बी (B), सी (C), डी (D), ई (E) तथा एफ (F) आदि से अथवा संकेतांक जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि से प्रदर्शित किया जाता है। इन ए (A), बी (B), सी (C), डी (D), ई (E) तथा एफ (F) आदि अक्षरों को अथवा 0, 1, 2, 3, 4 आदि बिन्दुओं को ही ग्रेड कहा जाता है । स्पष्टतः अंक प्रणाली के विपरीत ग्रेड प्रणाली वास्तव मे छात्रों को कुछ गुणात्मक श्रेणियों में बाँटती है।
परीक्षा सुधार के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों का ध्यान इस विचार की ओर शीघ्रता से आकर्षित हुआ एवं उन्होंने माना कि अंकन वर्गों (Marking Categories) की संख्या को कम करके अंकन की त्रुटियों को काफी सीमा तक सभाप्त किया जा सकता है, इसलिये उन्होंने ग्रेड प्रणाली को अपनाये जाने का सुझाव दिया। अमेरिका आदि विकसित देशों में तो काफी समय से ग्रेड प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में भी कुछ प्रगतिशील शिक्षा संस्थाओं, माध्यामिक शिक्षा परिषदों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं ने ग्रेड प्रणाली का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने के प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार करने के बावजूद भी ग्रेड की संख्या पर कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो पाया है। कुछ 5 बिन्दु ग्रेड प्रणाली को उपयुक्त बताते हैं, कुछ विद्वान 7 विन्दु ग्रेड प्रणाली को, तथा कुछ विद्वान 9 बिन्दु ग्रेड प्रणाली को उचित ठहराते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से ग्रेड प्रणाली में कितने भी बिन्दु हो सकते है। पाँच बिन्दु एवं सात बिन्दु ग्रेड प्रणाली के विभिन्न ग्रेडों तथा उनका शाब्दिक वर्णन सारिणी में प्रस्तुत किया है।
सारणी
विभिन्न ग्रेडों का शाब्दिक वर्णन (Verbal Description of Different Grades)
पाँच बिन्दु ग्रेड प्रणाली (Five Point Grading System)
|
ग्रेड |
A |
B |
C |
D |
F |
|
ग्रेड बिन्दु |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
शाब्दिक अर्थ |
विशिष्ट |
उत्तम |
औसत |
निम्न |
अनुत्तीर्ण |
सात बिन्दु ग्रेड प्रणाली (Seven Point Grading System)
|
ग्रेड |
O |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
ग्रेड बिन्दु |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
शाब्दिक अर्थ |
विशिष्ट |
अति उत्तम |
उत्तम |
औसत |
संतोषप्रद |
निकृष्ट |
निकृष्टम |
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) के द्वारा 1975-1976 में ग्रेड प्रणाली पर आयोजित की गई क्षेत्रीय कार्यशालाओं (Zonal Workshops) में 7 बिन्दू ग्रेड प्रणाली को अपनाये जाने पर आम सहमति थी क्योंकि इससे मूल्यांकन में आवश्यक परिमार्जन रहेगा तथा किसी भी ग्रेड के अन्दर बहुत अधिक विभिन्नताएँ नहीं होंगी। इसके अलावा 7 बिन्दु ग्रेड प्रणाली इसलिए भी उपर्युक्त है क्योंकि छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर बाटते समय अध्यापकों के द्वारा भी साधारणतः सात श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है। ये सात श्रेणी हैं- विशिष्ट अतिउत्तम, उत्तम, सन्तोषप्रद, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट । इनको क्रमशः ओ. ए. बी. सी. डी. ई. व एफ. अक्षर ग्रेड से व्यक्त किया जा सकता है। कार्यशालाओं में यह भी कहा गया कि कुछ कृषि विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं ने 5 विन्दु ग्रेड प्रणाली प्रारम्भ कर दी है, यह उनकी परिस्थतियों में उपयुक्त हो सकती हैं क्योंकि इन संस्थाओं में छात्र अधिक सजातीय (Homogeneous) होते हैं। चिकित्सा तथा इन्जीनियरिंग संकायों में आवश्यकतानुसार 7 बिन्दु ग्रेड के अतिरिक्त अन्य प्रणाली भी प्रयोग में लाई जा सकती है।
वैसे तो परीक्षकों के द्वारा सीधे-सीधे ग्रेड प्रदान किया जाना अधिक वांछनीय हैं, परन्तु आवश्यकता होने पर प्राप्तांकों को भी ग्रेड में बदला जा सकता है। प्राप्तांकों को ग्रेड में बदलने के लिए प्राप्तांकों के विवरण को सामान्य प्रायिकता वक्र (NPC) के आधार पर 7 भागों में विभाजित करके उन्हें ग्रेड प्रदान किया जा सकता है। विभिन्न विषयों या पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम ग्रेड औसत विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह निर्धारण उस क्षेत्र की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करेगा फिर भी सामान्यतः सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम औसत ग्रेड डी. या (D) होने चाहिए तथा यदि किसी छात्र का औसत ग्रेड डी. (D) या इससे श्रेष्ठ हो परन्तु उसने यदि किसी एक प्रश्नपत्र में डी. (D) से कम ग्रेड प्राप्त किये हो तो उसे इस शर्त पर अगली कक्षा में भेजा जा सकता है कि वह उस प्रश्नपत्र को अगले वर्ष उत्तीर्ण कर लेगा । छात्रों के उत्तरों को सीधे-सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकित करने की स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को परीक्षक अलग-अलग ग्रेड प्रदान करेगा तथा फिर सम्पूर्ण उत्तरपुस्तिका के लिए ग्रेड औसत ज्ञात कर लिया जायेगा। ग्रेड औसत ज्ञात करने के लिए पहले सभी ग्रेडों को ग्रेड बिन्दुओं (Grade Points) में बदला जायेगा, तब इनका औसत ज्ञात कर लिया जायेगा जिसे ग्रेड बिन्दु औसत (Grade Point Average) कहा जायेगा । सात बिन्दु ग्रेड प्रणाली में ओ. (O) को 6, ए. (A) को 5, बी (B) को 4, सी. (C) को 3, डी. (D) को 2, ई. (E) को 1, तथा एफ (F) को 0 अंक दिये जा सकते हैं। जब विभिन्न प्रश्नों के लिए महत्व (Weightage) असमान होता है तब विभिन्न प्रश्नों के लिए ग्रेड बिन्दुओ को उनके प्रतिशत महत्व (Percentage Weightage) से गुणा करके उनका योग ज्ञात कर लेते हैं। जिसे 100 से भाग देने पर ग्रेड बिन्दु औसत (GPA) ज्ञात हो जाता है। यदि विभिन्न प्रश्ना का महत्व (Weightage) भिन्न के रूप में दिया होता है तब ग्रेड बिन्दुओं को उनके महत्व (Weightage) से गुणा करके योग लेने पर प्रेड बिन्दु औसत प्राप्त हो जाता है।
ग्रेड प्रणाली के लाभ (Merits of Grading System)
एक सौ एक बिन्दु अंकन प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का उपयोग करने के अनेक लाभ हो सकते हैं। ग्रेड प्रणाली के मुख्य लाभ निम्नवत् है:
- विभिन्न परीक्षा संस्थाओं या विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित छात्रों के परिणामों की तुलना करने की दृष्टि से मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली अत्याधिक उपयोगी है। विभिन्न संस्थाओं या विश्वविद्यालयों का अंकन स्तर (Marking Standard) भिन्न-भिन्न होने पर प्राप्तांकों के द्वारा परीक्षार्थियों की तुलना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। ग्रेड प्रणाली ऐसी स्थिति में एक उपयोगी साधन का कार्य कर सकेगी।
- ग्रेड की सहायता से छात्रों का मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय ढंग से हो सकता है। अतः ग्रेड प्रणाली का प्रयोग परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता को बढाता है।
- ग्रेड प्रणाली विभिन्न विषयों तथा संकायों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करने के लिए एक उभयनिष्ठ पैमाने (Common Scale) का कार्य सफलता पूर्वक कर सकती है।
- छात्रों की अभिरूचि तथा योग्यता के आधार पर भावी पाठ्यक्रम के चयन करने की दृष्टि से ग्रेड प्रणाली अधिक उपयुक्त तथा वैज्ञानिक है।
- ग्रेड प्रणाली को अपनाये जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रक्रेजन (Migration) कारते समय होने वाली कठिनाईयाँ काफी कम हो सकेगी जिससे अन्तक्षत्रीय स्थानान्तरण में सविधा हो सकेगी।
शिक्षक शिक्षण – महत्वपूर्ण लिंक
- संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन | Formative and Summative Measurement in Hindi
- सामान्यीकृत मापन किसे कहते हैं? | इप्सेटिव मापन किसे कहते हैं? | Normative Measurement in Hindi | Ipsative Measurement in Hindi
- निकष संदर्भित मापन तथा मानक संदर्भित मापन | निकष सन्दर्भित तथा मानक सन्दर्भित मापन की तुलना
- सतत्- आन्तरिक मूल्यांकन | Continuous-Internal Evaluation in Hindi
- प्रश्न बैक किसे कहते हैं? | प्रश्न बैंकों के प्रमुख प्रकार |Question Bank in Hindi
- खुली पुस्तक परीक्षा | Open Book Examination in Hindi
- सेमेस्टर प्रणाली क्या है? | इसकी सम्पूर्ण जानकारी | Semester System in Hindi
- स्केलिंग प्रणाली क्या है | What is scaling system
- परीक्षा में कम्प्यूटर का उपयोग | Use of Computer in Examination in Hindi
- सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रमापीकरण | Standardization of Public Examinations in Hindi
- सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता (Transparency in Public Examinations)
- चर के प्रकार | गुणात्मक चर एवं मात्रात्मक चर | Types of Variables in Hindi
- मापन के स्तर | मापन के प्रकार | Levels of Measurement in Hindi
- मापन के आवश्यक तत्व | Essential Elements of Measurement in Hindi
- मूल्यांकन का अर्थ | मूल्यांकन का प्रत्यय | Concept and meaning of Evaluation in Hindi
- शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य | मापन तथा मूल्यांकन का महत्व
- मापन तथा मूल्यांकन के कार्य | Functions of Measurement and Evaluation in Hindi
- मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान | Steps of Evaluation Process in Hindi
- मापन की त्रुटियाँ | Errors of Measurement in Hindi
- संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन | Formative and Summative Measurement in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]