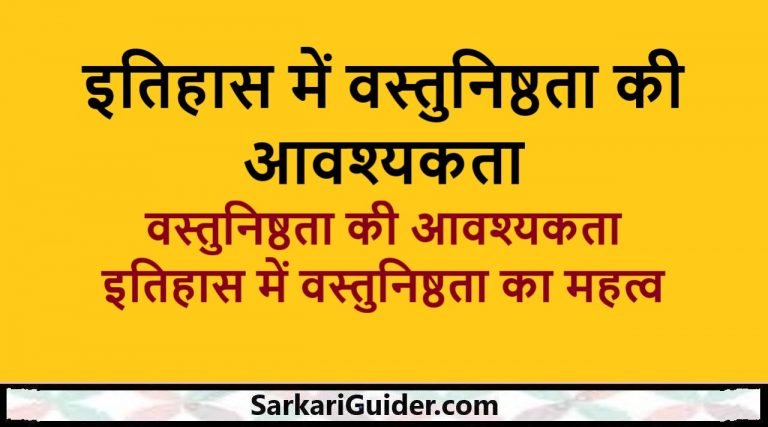गुप्त युग की कला की प्रमुख विशेषताएं | गुप्त युग की कला की विशिष्टताओं का वर्णन
गुप्त युग की कला की प्रमुख विशेषताएं | गुप्त युग की कला की विशिष्टताओं का वर्णन
गुप्त युग की कला की प्रमुख विशेषताएं
डॉ० आर० सी० मजूमदार का कथन है कि “गुप्त युग के साथ हम भारतीय मूर्तिकला को श्रेण्य प्रावस्था में प्रवेश करते हैं। शताब्दियों के प्रयत्न से कला पूर्णता को प्राप्त हुई; कला के सुनिश्चित रूपों का विकास हुआ और सौन्दर्य के आदर्श परिशुद्धिपूर्वक निर्धारित किये गये।” गुप्त युग में कला अपनी चरम उन्नति पर पहुँच गई।
जब यह प्रश्न उठता है कि गुस युग की कला की विशिष्टताएं कौन-सी हैं, तब हमें अपनी ओर से यह अनुमान करना पड़ता है कि प्रश्नकर्ता का आशय मूर्ति कला की और सम्भवतः चित्र कला की विशिष्टताओं से है। कारण यह है कि ये दो ही कलाएं ऐसी है, जिन पर एक साथ समान रूप से विचार हो सकता है। इस प्रकार गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित थीं-
(1) भावाभिव्यंजकता-
गुसकालीन कला में सबसे अधिक महत्व भावाभिव्यक्ति को दिया गया था। अंग-सौष्ठव तथा लालित्य का यथेष्ठ ध्यान रखते हुए भी कलाकार का मुख्य प्रयत्न यह रहा कि अभीष्ट भाव को प्रबलतम रूप में प्रकट किया जाये। अन्य क्षेत्रों में: गुप्त युग की कला का मुकाबला किया भी जा सकता है, परन्तु इस क्षेत्र में नहीं।
(2) अनमिता-
इस युग की कला को दूसरी विशेषता यह है कि इतनी उत्कृष्ट कलाकृतियों-मूर्तियों और चित्रों के निर्माताओं के नाम अज्ञात हैं। किसी कलाकार ने अपना नाम प्रकट करने का प्रयास ही नहीं किया।
(3) शालीनता-
गुप्तकालीन कला पूर्णत: शिष्ट एवं शालीन है। उसमें अश्लीलता और नग्नता का पूर्ण बहिष्कार किया गया है। सौन्दर्य पर सर्वत्र धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता का पुट दे कर उसे भव्य बना दिया गया है। श्री कुमारस्वामी ने लिखा है कि “गुप्त काल की शिल्प कला प्रगाढ़ आध्यात्मिकता से युक्त है।”
(4) जीवन के विविध पक्षों का अंकन-
गुप्तकालीन कला में जीवन के इतने अधिक विविध पक्षों का अंकन हुआ है कि भारत में अन्य किसी काल में नहीं हुआ। मैत्री, करुणा, प्रेम, घृणा आदि विविध भाव, और तप, ध्यान, प्रेम क्रीड़ा, श्रृंगार आदि विविध मानव-व्यापार, इसमें प्रदर्शित किये गये हैं।
(5) विदेशी प्रभाव का अभाव-
इससे पूर्व कुषाण कला पर यूनानी और ईरानी प्रभाव था। परन्तु गुप्त. काल में जैसे देश विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गया था, उसी प्रकार कला भी विदेशी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी। गुप्तकालीन कला पूर्णतया भारतीय कला है।
(6) रूढ़िवाद से मुक्ति और संतुलन-
गुप्तकालीन कला रूढ़ियों के बन्धन से मुक्त हो गई थी। उसमें एक प्रकार की स्वतंत्रता और संतुलन दृष्टिगोचर होता है।
(7) एक समन्वित राष्ट्रीय शैली-
कुषाण काल में हमें कला की गान्धार, मथुरा, अमरावती, सारनाथ आदि विभिन्न शैलियाँ दिखाई पड़ती हैं, परन्तु गुप्त युग तक इन सबका एक सम्मिलित समन्वित रूप विकसित हो गया था, जिसे ‘राष्ट्रीय कला शैली’ कहा जाता है। इस शैली की सौन्दर्य की एक अपनी ही अलग संकल्पना थी, जिसका मूल मंत्र था कि “शिव (कल्याणकारी) ही सुन्दर है।”
(8) उदात्तता के लिए सौन्दर्य का सृजन-
गुप्त काल की कलाकृतियों का लक्ष्य जीवन को ऊंचा उठाना, उसे उदात्त तथा गौरवपूर्ण बनाना था। मूर्तियों तथा चित्रों के रूप में सौन्दर्य सृजन को इसका समर्थ साधन बनाया गया।
(9) बाह्य रूप और आन्तरिक भावना का समन्वय-
गुप्तकालीन कला का बाह्य रूप भी उतना ही सरल और सादा है, जिनती कि उसकी आन्तरिक धार्मिक भावना। उसके विषय और प्रविधि (तकनीक), दोनों में एकरूपता है।
(10) उदारता, सहिष्णुता और सर्व धर्म समन्वय-
गुप्तकालीन कला किसी सम्प्रदाय या धर्म-विशेष की कट्टरता से बंधी हुई नहीं थी। उसमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता का पुट गहरा था परन्तु, उसमें शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि सभी धार्मिक सम्प्रदायों को आदर तथा महत्त्व का स्थान प्राप्त था। न केवल गुस सम्राट धार्मिक दृष्टि से उदार तथा सहिष्णु थे, अपितु वे कलाकार भी, जिन्होंने मूर्तियाँ और चित्र बनाये हैं, सभी धर्मों के प्रति समान रूप से श्रद्धालु थे। ऐसे प्रतीत नहीं होता कि केवल पारिश्रमिक की लालसा से इतनी साधना की गई हो। कलाकारों की अपनी निष्ठा और लगन का संभवतः पारिश्रमिक से अधिक महत्त्व रहा था।
(11) ऐन्द्रियिकता और प्रतीकात्मक अमूर्त भावना, दोनों का अभाव-
डा० हरिदत वेदालंकार ने लिखा है कि “गुप्त कला में न तो पिछले कुषाण युग की ऐन्द्रियिकता है, न परवर्ती मध्य युग की प्रतीकात्मक अमूर्त भावना। इसमें दोनों का सन्तुलन और सामंजस्य है।”
अन्त में, हम श्री बी० एन० लूनिया के शब्दों में कह सकते हैं कि “सारांश में गुप्तकाल की कला की विशेषताएँ अद्भुत भावोद्रेक, लालित्य, शैली की सरलता, भावव्यंजना, स्वाभाविकता, गाम्भीर्य, रमणीयता, माधुर्य, अभिव्यक्ति की सादगी व सजीवता और आध्यात्मिक अभिप्राय का प्राधान्य है।’
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- गुप्त काल में कला का विकास | गुप्तकालीन गुफाएँ और स्तूप | गुप्तकालीन मन्दिर | गुप्तकालीन मन्दिरों की विशेषाएँ
- गुप्त काल की मूर्ति कला | गुप्तकाल की कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां | गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएँ | गुप्तकालीन मृण्मूर्तियाँ
- गुप्तकालीन चित्रकला | गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषताएँ | अजन्ता के प्रमुख चित्र
- गुप्त युग की कला की प्रमुख विशेषताएं | गुप्त युग की कला की विशिष्टताओं का वर्णन
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]