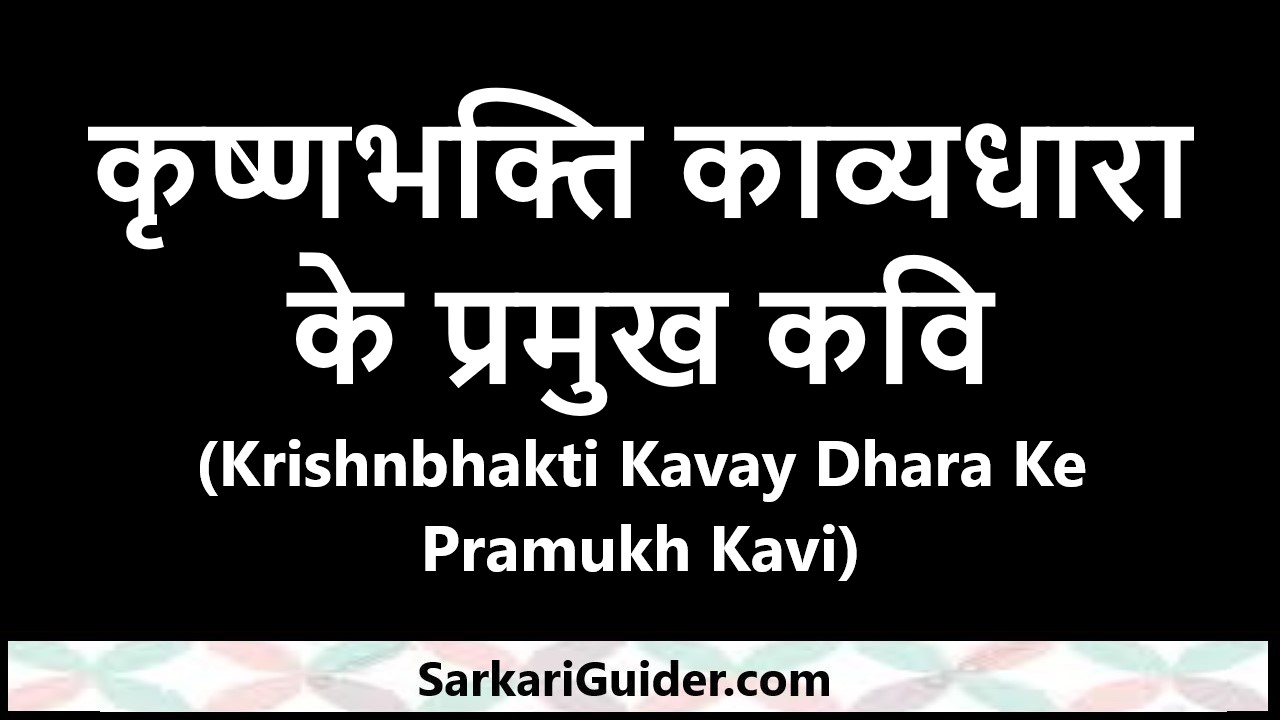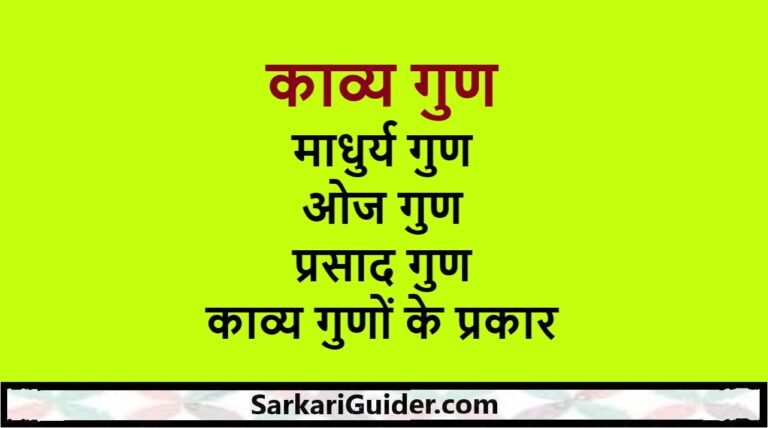कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि (Krishnbhakti Kavay Dhara Ke Pramukh Kavi)

कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि (Krishnbhakti Kavay Dhara Ke Pramukh Kavi)
कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि
सूरदास (1478-1583)
सूरदास के जीवन-वृत्त के लिए बहिस्साक्ष्य के रूप में भक्तमाल ( नाभादास), चौरासी वैष्णवन की वार्ता (गोकुल नाथ) और बल्लभ दिग्विजय (यदुनाथ) का आधार लिया गया है। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार, वे दिल्ली के निकट ‘सीही’ के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। वार्ताग्रंथों के अनुसार, सूरदास से महाप्रभु बल्लभाचार्य की भेंट 1509-10 ई. में हुई थी और तब से वे बल्लभाचार्य के शिष्य बनकर पारसोली गाँव में रहने लगे थे। उनका जन्म 1478 ई. तथा निधन 1583 ई. में माना जाता है। वे जन्मांध थे, या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विवाद है। उनके निधन पर गोसाई विट्ठलनाथ ने कहा था-” पुष्टिमारग को जहाज जात है सो जाकों कछु लेनौ होय सो लेउ।”
गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने 1519 ई. में करवा दी थी इसी मंदिर में कीर्तन-सेवा सूरदास को बल्लभाचार्य ने सौंपी थी।
सूरदास के बारे में आगे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। (कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि )
नंददास (1533-1583)
नंददास की गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। इन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप में अपना शिष्य बनाकर शामिल किया था। नंददास जी के बारे में जो बिवरण गोकुलनाथ कृत ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ में है, उसे शुक्लजी ठीक नहीं मानते। वार्ता ग्रंथों में उन्हें प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है, जो नितांत गलत सिद्ध हो चुका है। संभवतः बल्लभ संप्रदाय को महिमामोडित करने हेतु बार्ताग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है। डॉ. नगेंद्र के अनुसार, नंददास का जन्म 1533 ई. में शूकर क्षेत्र ( सोरों) के रामपुर गाँव में हुआ था तथा मृत्यु 1583 ई. में मानसी गंगा के तट पर हुई। गोसाईं विट्ठलनाथ से पुष्टिमार्ग की दीक्षा लेने पर उनका जीवन ही बदल गया तथा सूरदास के संपर्क में आकर और उनकी भक्ति भावना देखकर उनका शास्त्र-मोह भंग हुआ।
ब्रजभाषा काव्य में ‘सूरदास’ के उपरांत ‘नंददास’ ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ हैं –
- अनेकार्थ मंजरी
- रसमंजरी
- रूपमंजरी
- विरहमंजरी
- मानमंजरी
- श्याम सगाई
- प्रेम बारहखड़ी
- रुव्म्मिणी मंगल
- सुदामा चरित
- भंवरगीत
- सिद्धांत पंचाध्यायी
- रास पंचाध्यायी
- दशमस्कंध भाषा
- गोवर्द्धन लीला
- नंददास पदावली
अनेकार्थमंजरी और मानमंजरी दोनों ही शब्दों के पर्यायकोश हैं। मानमंजरी चमत्कार प्रधान रचना है छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची हैं और दूसरी पक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दुती द्वारा राधा के शृंगार का वर्णन किया है। यह उनके प्रकांड पांडित्य का बोधक ग्रंथ है । विरह मंजरी में कृष्ण के विरह में एक ब्रजवासी की विरह दशा का भावात्मक चित्रण है। रूपमंजरी को प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना गया है।
रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें कवि ने लौकिक और पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। वियुक्त आत्मा (गोपी) रासलीला के माध्यम से रसरूप परमात्मा ( श्रीकृष्ण) से मिलने को व्याकुल है, प्रयत्नशील है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट एवं काव्यत्व को देखकर ही नंददास के बिषय में यह कहा गया है-‘और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया।’
भंवरगीत भ्रमरगीत परंपरा का ग्रंथ है जिसमें कविवर नंददास ने उद्धव-गोपियां की विरह दशा का निरूपण किया है। यह उनके दार्शनिक विचारों, परिपक्व ज्ञान एवं विवेक बुद्धि के साथ भक्ति भावना का भी परिचायक है।
‘सिद्धांत पंचाध्यायी’ में कृष्ण की रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृदांवन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक रूप प्रदान किया हैं। नंददास की भाषा, कवित्व शक्ति, शब्द चयन की योग्यता, विद्वता उत्कृष्ट कोटि की है। मधुर, सरस ब्रजभाषा का जैसा प्रयोग उन्होंने किया वैसा सूर के अतिरिक्त और किसी ने नहीं किया।
मीरा (1504-1563)
मीराबाई का जन्म 1504 ई. तथा मृत्यु 1563 ई. में हुई। उनका जन्म ‘मेड़ता’ के समीपवर्ती गाँव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था, उनके पिता का नाम रत्नसिंह था मीरा की माता का निधन बचपन में ही हो गया था, अत: वे मेड़ता में राव दूदा के पास रहीं जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ई. में हुआ और दुर्भाग्यवश वे सात वर्ष बाद ही विधवा हो गईं। वे तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई परिणामतः राज परिवार में उन्हें विरोध झेलना पड़ा। वे अपना अधिकांश समय पूजापाठ एवं भक्ति में व्यतीत करने लगीं। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रमसिंह ने मीरा को अनेक यातनाएँ दीं पर गिरधर गोपाल के प्रति मीरा की भक्ति भावना अविचल रही।
मीरा के बारे में आगे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। (कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि )
रसखान (1533-1618 ई.)
हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ‘दो सौ बावन वैष्णवों की बार्ता’ में इनका उल्लेख हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से बल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। डॉ. नगेंद्र ने रसखान का जन्म 1533 ई. में स्वीकार किया हैं। पहले ये दिल्ली में रहते थे बाद में ये गोवर्द्धन धाम आ गए। ‘मूल गोसाई चरित’ में यह उल्लेख है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। ‘प्रेमवाटिका’ रसखान की अंतिम कृति है जिसकी रचना 1614 ई. में हुई। उसके कुछ समय बाद 1618 ई. में रसखान का देहावसान हो गया। रसखान की दो कृतियाँ उपलब्ध होती हैं- प्रेमवाटिका और वानलीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित ‘संकलन सुजान’ रसखान है जिसमें 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। ‘अष्टयाम’ नामक उनकी एक कृति और मिली है जिसमें कई दोहों में श्रीकृष्ण के प्रात: जागरण से रात्रिशयन पर्यन्त की दिनचरयां एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है।
प्रेमवाटिका में कवि ने राधा-कृष्ण को मालिन-माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सुक्ष्म निरूपण किया है। इस रचना में 53 दोहे हैं।
दानलीला केवल 11 दोहों की छोटी-सी कृति है जिसमें राधा-कृष्ण संवाद है ।
रसखान ब्रजभाषा के मर्मज्ञ एवं सशक्त कवि हैं। प्रेमतत्व के निरूपण में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा एवं गोपियों की मन:स्थिति का मनोरम चित्रण उन्होंने किया है । उनके काव्य में कृष्ण के बाल सौंदर्य का भी चित्रण हुआ है। श्रिंगर एवं वात्सल्य उनके काव्य के प्रमुख रस हैं। सवैया, कवित्त, दोहा छंद उन्हें प्रिय हैं। उनका प्रेम स्वच्छंद प्रेम है किंतु उसमें सूफियों के प्रेम का अनुकरण नहीं है । ब्रजभूमि के प्रति उनका अनुराग निम्न सवैये में प्रकट होता है-
‘मानुस हीं तो वहै रसखानि’
बसौं ब्रज गोंकुल गाँव के ग्वारन।”
इसी प्रकार कृष्ण के रूप का मनोहर चित्रण उनके काव्य में हुआ है कृष्ण की लकुटी और कामरिया उन्हें इतनी प्रिय है कि वे इस पर तीनों लोकों का राज त्यागने को तत्पर हैं-
“या लकुटी अरु कामरिया पर
राज तिहूंपुर को तजि डारौ।”
उनके दो प्रसिद्ध सर्वैयों की पंक्तियाँ भी यहाँ उद्धृत हैं-
- मार पखा सिर ऊपर रारित हो
गुंज की माल गरे पहिरोंगीं। - संस महेस गर्नेस दिनेस
सुरेसहु जाहे निरंतर ध्यावे - धूरि भरे अति सोभित स्यामाजू
वैसी बनी सिर सुंदर चोटी।
रसखान की भाषा शुद्ध साहित्यिक, परिमार्जित ब्रजभाषा है, जिसमें माधुर्य और प्रसाद गुणों के कारण सरसता एवं सजीबता आ गई है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित पद शौली न अपनाकर कवत्त-सबैया शैलो को अपनाया जो उनकी स्वच्छन्द वृत्ति का सूचक हैं।
- आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ- राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
- प्रमुख हिन्दी गद्य-विधाओं की परिभाषाएँ
- नाटक- परिभाषा, प्रथम नाटक, नाटक के तत्त्व, प्रमुख नाटककारों के नाम, प्रसिद्ध नाटकों के नाम
- आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ- प्रवृत्तियों की विशेषताएँ, आदिकालीन साहित्य का महत्त्व
- हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]