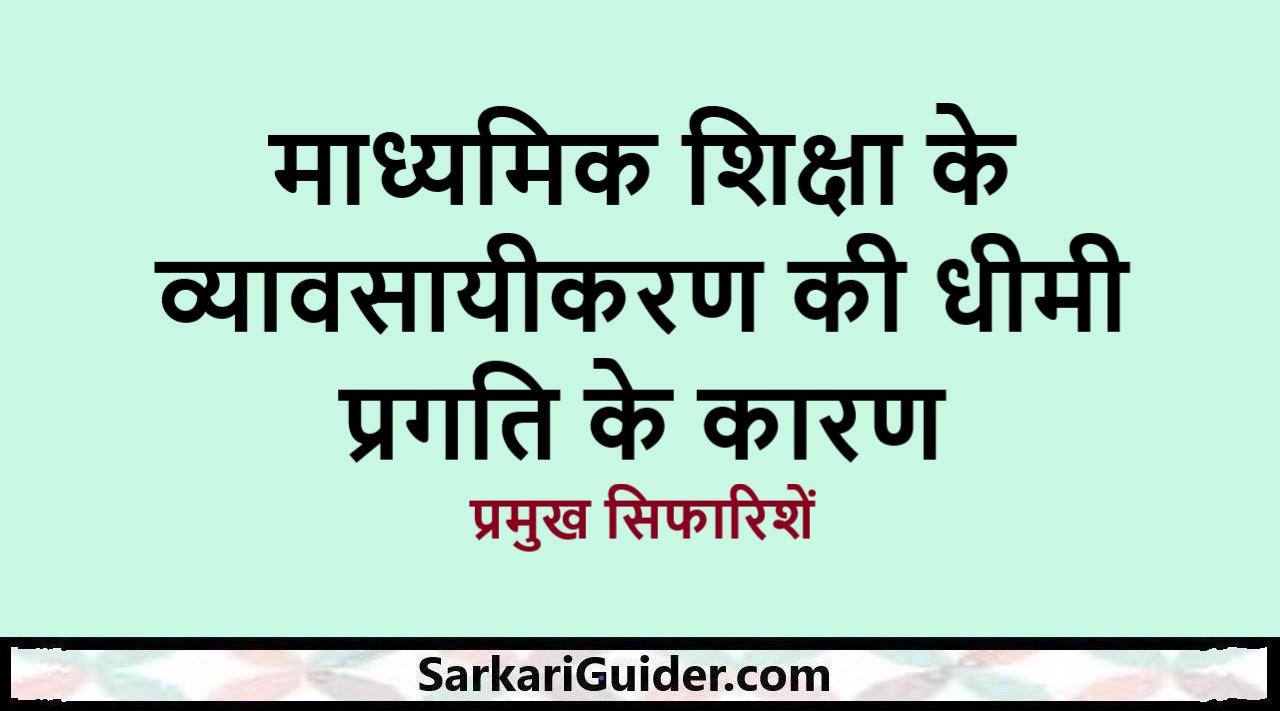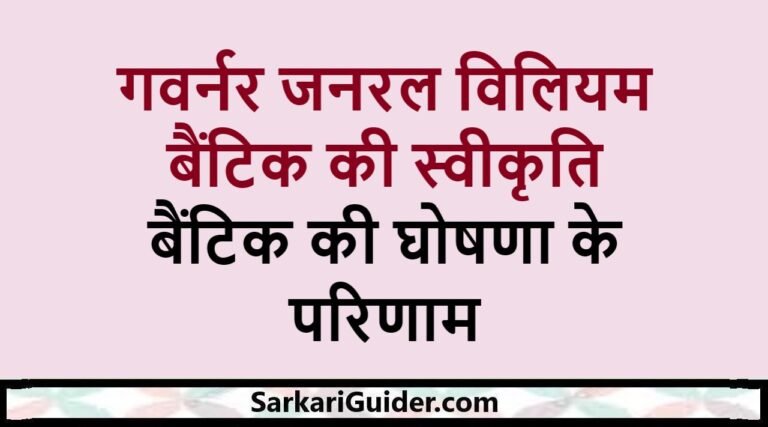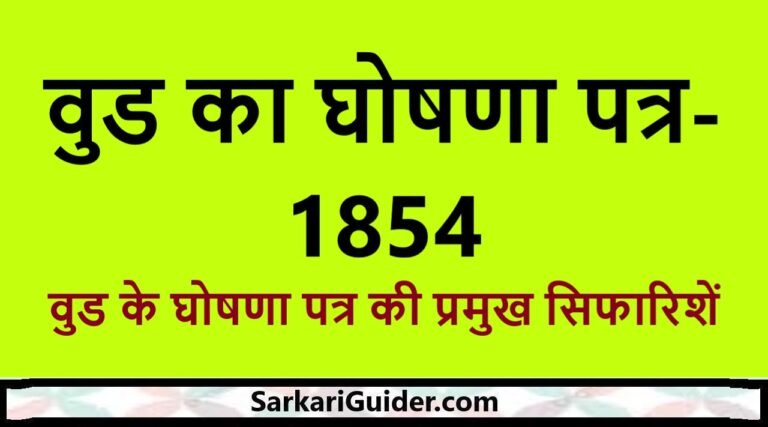माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की धीमी प्रगति के कारण | प्रमुख सिफारिशें

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की धीमी प्रगति के कारण | प्रमुख सिफारिशें
माध्यमिक शिक्षा आयोग के विचार में व्यावसायिक शिक्षा की धीमी प्रगति के कारण
(Causes of the Slow Growth of Vocational Education According to Secondary Education Commission)
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की धीमी प्रगति के निम्निखित कारण दिए हैं-
(1) व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार का केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत आधार पर गभीरतापूर्वक प्रयास नहीं किया गया है।
(2) उद्योग, श्रम तथा शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों में तालमेल (Coordination) तथा सहयोग की सदैव कमी रही है।
(3) व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की सदैव कमी रही है, ऐसे अध्यापक नहीं मिल पाते, जिनमें साधारण ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge) दोनों का सम्मिश्रण हों।
(4) लगभग सभी राज्यों में जन-सम्पर्क विभाग के पास उचित पथ प्रदर्शन सेवा के लिये कोई भी तकनीकी सलाहकार नहीं है, जो कि अपने अनुभव से उन कोर्सी को बुद्धिमता से चला सकें और उनका प्रतिनिधित्व कर सकें।
(5) स्कूलों में आवश्यकतानुसार समान तथा उचित प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक जुटाने के लिए धन की सदैव कमी रही है। उचित प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों तथा आवश्यक भौतिक सुविधाओं की अनुपस्थिति में व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति में बाधा आई है।
व्यावसायीकरण पाठ्यक्रम के पाठ्य विषय (Vocationalisation of Courses)-
कोठारी आयोग, 1966 ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया है। आयोग की रिपोर्ट का नाम शिक्षा और राष्ट्रीय विकास है। इसका अर्थ है कि आयोग ने शिक्षा के विकास की रूपरेखा विकास के संदर्भ में विकसित की है। उसके अनुसार शिक्षा परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण यंत्र है और उत्पादन में सहायक है। आधुनिक प्रगतिशील समाज में शिक्षा का आधार विज्ञान तथा तकनीकी हो। आयोग ने सामान्य शिक्षा में कार्यानुभव (Work Experience) को प्रमुख स्थान देने की सिफारिश की है। शिक्षा हमारी कृषि, उद्योग तथा व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। उसके द्वारा व्यावसायिक, टेक्नीकल तथा प्राविधिक विकास संभव हों। इस प्रकार आयोग हमारे समक्ष शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना प्रस्तुत करता है, जिसका स्पष्ट रूप हमें भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में मिलता है।
प्रमुख सिफारिशें
(Main Recommendations)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 10 तक की सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें 20% व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया गया है। लगभग 14 या 18 विषयों की व्यवस्था की गई है। सभी विषय अनिवार्य रखे गये है। यह शिक्षा का सामान्य बहाव (General stream) होगा इसमें भाषाओं, गणित, व्यावहारिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त कार्य-अनुभव को विशेष महत्त्व दिया गया है। इस सम्बन्ध में ईश्वर भाई पटेल कमेटी, 1977 की सिफारिशें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।
+2 पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा को अन्तिम व महत्त्वपूर्ण सीमा मानते हुए उसमें 50% व्यावसायीकरण की व्यवस्था है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार के कोर्स होंगे। उन्हें साहित्यिक तथा व्यावसायिक में विभक्त किया गया है। दोनों को एक ही विद्यालय के साथ-साथ चलाने की सिफारिश की गई। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को अपने में पूर्ण तथा अन्तिम बनाना है और छात्रों को किसी व्यवसाय के लिये तैयार करना है। व्यावसायिक बहाव (Voational stream) छात्रों को व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा कैसे सीखें (Know-how) प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को ज्ञान की दुनिया में काम की दुनिया (World of work) मे ले जाना है, वे स्वयं कुछ रोजगार पा सके, सृजन, उत्पादन तथा निर्माण में सहायक हो सकें और इस प्रकार वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की व्यवस्था नीली कुर्ती तथा सफेद कुर्ती की दूरी (Gap) को समाप्त करने में समर्थ होगी। इस सब का संबंध कौशल अथवा दक्षता प्राप्त करने से है। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप कार्यवाहक, व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अनुभव प्रदान करना है। देश में बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है।
माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम विद्यालय के पास-पड़ोस का सर्वेक्षण करके उस क्षेत्र की आवश्यकताओं पर पता लगाया जाये। उस क्षेत्र में क्या कार्य करने के अवसर हैं? और क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? साथ ही किस प्रकार सहयोग उपलब्ध है? स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही, व्यावसायिक विषयों का चयन किया जाये और सुविधा प्रदान की जायें। विषयों का स्वरूप कार्यवाहक होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने 1975 में एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- राममूर्ति समीक्षा समिति – 1990 | राममूर्ति समीक्षा समिति की अपनी समीक्षा रिपोर्ट
- जनार्दन रेड्डी समिति – 1992 | जनार्दन रेड्डी समिति के शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव
- संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1992 | शिक्षा प्रबन्ध और नीति 1992 | संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज
- भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रगति | शिक्षक शिक्षा क्या है | Describe in brief the progress of teacher education in India in Hindi
- अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य | N.C.E.R.T. के द्वारा अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य
- माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ | व्यावसायीकरण का विकास | शिक्षा के व्यावसायीकरण में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव
- माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के व्यावसायीकरण की आवश्यकता | शिक्षा के व्यावसायीकरण का महत्त्व
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]