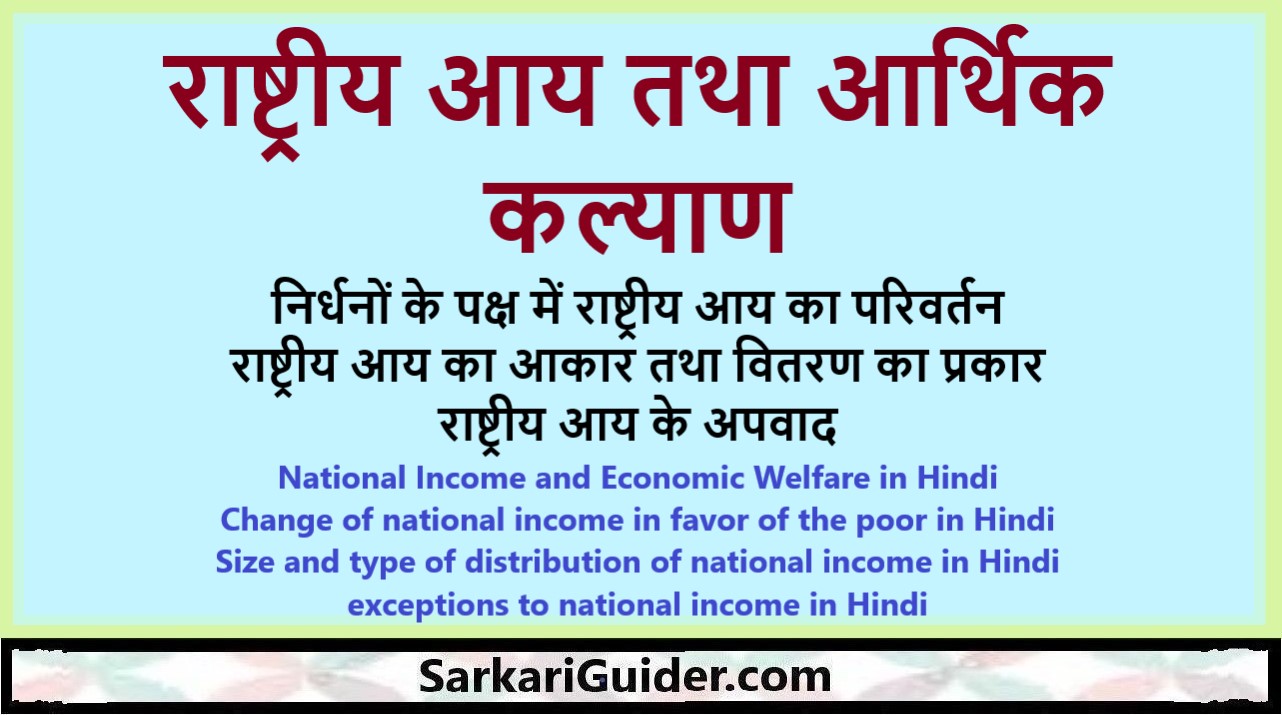राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण | निर्धनों के पक्ष में राष्ट्रीय आय का परिवर्तन | राष्ट्रीय आय का आकार तथा वितरण का प्रकार | राष्ट्रीय आय के अपवाद
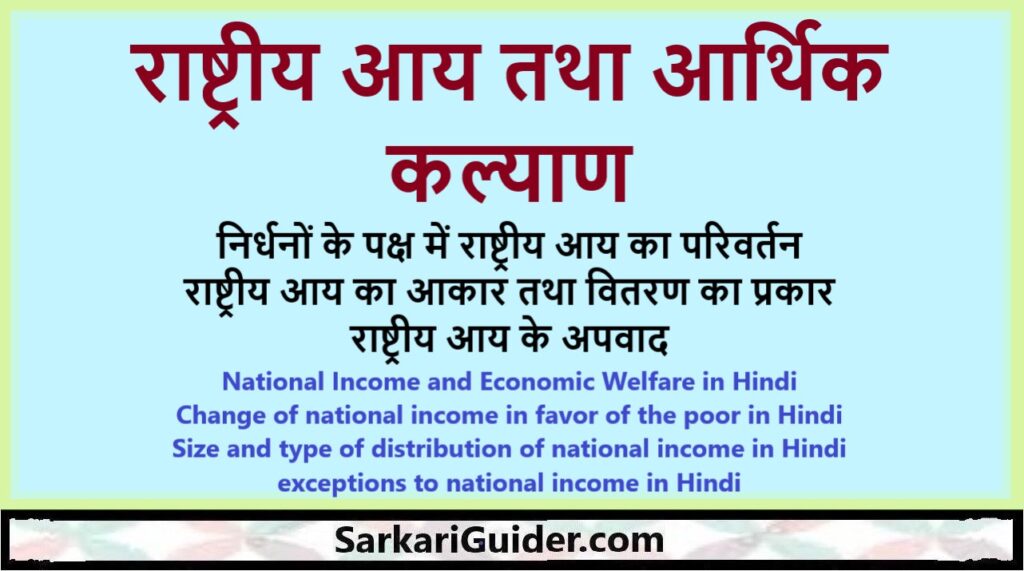
राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण | निर्धनों के पक्ष में राष्ट्रीय आय का परिवर्तन | राष्ट्रीय आय का आकार तथा वितरण का प्रकार | राष्ट्रीय आय के अपवाद | National Income and Economic Welfare in Hindi | Change of national income in favor of the poor in Hindi | Size and type of distribution of national income in Hindi | exceptions to national income in Hindi
राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण-
‘राष्ट्रीय आय’ तथा ‘आर्थिक कल्याण का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हैं। एक में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन को जन्म देता हैं। इसे हम दो भागों में इस प्रकार अध्ययन करते हैं।
- राष्ट्रीय आय की मात्रा में परिवर्तन एवं आर्थिक कल्याण- ‘राष्ट्रीय आय तथा ‘आर्थिक कल्याण’ के मध्य प्रत्यक्ष बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। राष्ट्रीय आय की मात्रा में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में भी स्वतः वृद्धि हो जाती हैं। राष्ट्रीय आय की मात्रा में वृद्धि होने से लोगों के उपभोग के लिए अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ सुलभ हो जाती हैं। इससे आर्थिक कल्याण अधिक हो जाता हैं। इसके प्रतिकूल कमी उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को भी कम कर देती हैं। जिसके फलस्वरूप आर्थिक कल्याण कम हो जाती हैं, परन्तु ऐसा निम्नलिखित दशाओं में लागू होता हैं-
(1) राष्ट्रीय आय की मात्रा में वृद्धि होते समय निर्धन मनुष्यों की आय की मात्रा में कमी पनहीं आनी चाहिए क्योंकि धनी मनुष्यों के लिए वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होने के साथ निर्धन मनुष्यों के लिए वस्तुओं पूर्ति को कमी समाज के आर्थिक कल्याण में कमी उत्पन्न कर देता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती हैं-धनिकों को मिलने वाला लाभ निर्धनों की हानि से बहुत कम होता हैं। इस प्रकार सही सत्यों के प्रतिस्थापना के लिए निर्धनों की आय की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए।
(2) उपभोग में परिवर्तन नवीन रुचियों को जन्म देकर सन्तोष की मात्रा को अधिक बढ़ा देता हैं जिसके फलस्वरूप वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अधिक साधन सुलभ होने के कारण आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाती हैं, जैसे-बचत बैंक निर्धनों द्वारा मितव्ययता से बचत के उत्तम साधन हैं, परन्तु राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप यदि साधारण जनता का झुकाव लॉटरी तथा मदिरालय आदि व्यसनों की ओर हो जाता हैं तो ऐसी देशा में राष्ट्रीय आय तो बढ़गी, परन्तु आर्थिक कल्याण में गिरावट हो जायगी।
(3) यदि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय से प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि अधिक हैं अपेक्षा उसके उत्पादन में त्याग तथा असन्तोष से, तो आर्थिक कल्याण में निश्चिचत ही वृद्धि होगी।
(4) यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ ही जनसंख्या में भी तीव्र दर से वृद्धि हो रही हैं तो प्रति व्यक्ति आय निश्चय ही कम हो जायेगी। अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आर्थिक कल्याण (Economic welfare) में वृद्धि नहीं होगी।
- राष्ट्रीय आय के वितरण परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण- राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन होने से समुदाय को एक वर्ग की आय का हस्तान्तरण दूसरे वर्ग के पक्ष में हो जाता हैं। यह हस्तान्तरण या तो धनिकों के अनुकूल होगा अथवा निर्धनों के अनुकूल होगा। निर्धन वर्ग के पक्ष में होने का आशय हैं उन्हें उपभोग की अधिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हैं। धनिकों के अनुकूल होने पर निर्धनों की आय में कमी और धनी व्यक्तियों की आय में वृद्धि होना होता हैं। इसमें धनीं और धनी तथा निर्धनों की दशा अपेक्षाकृत बहुत खराब हो जाती हैं।
निर्धनों के पक्ष में राष्ट्रीय आय का परिवर्तन
(I) प्रत्यक्ष रीति- इसके अन्तर्गत धनिकों के पास ‘क्रयशक्ति’ पहुँचायी जाती हैं।
(II) अप्रत्यक्ष रीति- इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आय का वितरण अनेक विधियों से निर्धनों के अनुकूल किया जाता हैं-
(क) उत्पादन प्रणाली को ऐसा बनाया जाय कि धनिकों की उपभोग सामग्री महँगी हो जाय और निर्धनों की उपभोग सामग्री सस्ती हो जाय।
(ख) राशनिंग, यथोचित राजस्व नीति अथवा किसी अन्य विधि से धनिकों को उन वस्तुओं के उपभोग पर नियन्त्रण लगाया जा सकता हैं जो निर्धनों के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं और जिनका उत्पादन ह्रासमान नियम के अन्तर्गत हो रहा हैं। इस प्रकार वस्तुओं की माँग कम हो जाने से कीमतें गिर जायेंगी और ये वस्तुएँ निर्धनों को कम कीमतों पर भी प्राप्त हो सकेंगी। इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी।
(ग) एक विशेष सफल उपाय ‘प्रशुल्क नीति’ का भी हैं। धनी व्यक्तियों को शिक्षा, सामाजिक, सेवाओं आदि के रूप में अधिक लाभान्वित किया जा सकता हैं।
उपर्युक्त विधियों में से प्रयोग करते समय एक या अन्य दूसरी विधियों को एक साथ भी राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन हेतु प्रयोग किया जा सकता हैं, परन्तु हर दशा में राष्ट्रीय आय की मात्रा समान रहनी चाहिए।
निर्धनों के पक्ष में राष्ट्रीय आय वितरण का परिवर्तन किस प्रकार से आर्थिक कल्याण को प्रभावित करता है ?
सामान्य लोगों के अनुसार निर्धनों के पक्ष में राष्ट्रीय आय का हस्तान्तरण आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता हैं तथा उनके विपक्ष में परिवर्तन आर्थिक कल्याण को कम करता है। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं-
आर्थिक कल्याण कुल आय पर निर्भर न रहकर उस आय पर निर्भर होता हैं जो वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर व्यय करता हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति के आर्थिक कल्याण और उसकी उपभोग आय की मात्रा में परस्पर सम्बन्ध हैं। एक व्यक्ति जितना अधिक धनी होगा वह अपनी कुल आय का उतना की कम अनुपात उपभोग पर व्यय करेगा, अतः उसकी कुल आय की तुलना में उसका आर्थिक कल्याण कम होगा। इसके अतिरिक्त अधिक आय होने के कारण धनी व्यक्तियों के लिए द्रव्य की ‘सीमान्त उपयोगिता’ कम होती हैं।
इसका सार यह हैं कि धनी व्यक्तियों की आय का कुछ भाग निर्धनों के पक्ष में कर देने से कुल आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी क्योंकि धनी व्यक्तियों की कम महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं के स्थान पर निर्धन व्यक्तियों की अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव होगी।
प्रो० जे.एस. मिल के शब्दों में, “मनुष्य धनी नहीं बनना चाहते हैं वरन् दूसरों से अधिक धनवान होना चाहते हैं। एक लालची व्यक्ति को कितना ही अधिक धन क्यों न दे दिया जाय यदि वह अपने पड़ोसियों तथा देशवासियों में सबसे अधिक धनी हैं तो भी उसे सन्तोष न होगा।”
कुछ लोगों के विचारानुसार निर्धनों के पक्ष में राष्ट्रीय आय वितरण आर्थिक कल्याा में वृद्धि नहीं करता। इसका समर्थन निम्नलिखित तर्कों से होता हैं।
(1) धनी एवं निर्धन स्वभाव से समान नहीं होते हैं। (2) दोनों व्यक्तियों का भिन्न मनोवैज्ञानिक वर्ग होता हैं। (3) धनी व्यक्ति अधिक सन्तुष्टि की क्षमता रखते हैं, निर्धन व्यक्ति की तुलना में। (4) उपर्युक्त दशा में राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन द्वारा कुल आर्थिक कल्याण में वृद्धि सम्भव नहीं होती हैं। (5) धनी लोग अपना पर्यावरण तथा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिससे उनकी प्रकृति आय की निश्चित मात्रा में अधिक सन्तोष प्राप्त करने की बन जाती हैं, परन्तु एक निर्धन व्यक्ति उपर्युक्त दशाओं के अभाव में ऐसा नहीं बन पाता हैं। (6) निर्धनों के आय में वृद्धि होने पर आय को आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर व्यय न कर शराब, जुआ आदि हानिकारक व्यसनों पर व्यय करता हैं, जिससे उसके सन्तोष में कमी आती हैं और फलस्वरूप उसका आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता हैं। कुल कल्याण का अर्थ सभी तरह के कल्याण, जैसे-नैतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक कल्याण से हैं। पीगू के अनुसार, “आर्थिक कल्याण, कुल कल्याण का वह भाग हैं जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्रव्य के मापदण्ड से सम्बन्धित किया जाता हैं।”
राष्ट्रीय आय के अपवाद-
(1) यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि से निर्धन की आय बढ़ने की बजाय कम हो जाय और अमीरों की आय और बढ़ जाय तो राष्ट्रीय आये के बढ़ने पर आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगी।
(2) राष्ट्रीय आय के बढ़ने से लोगों की माँग अधिक होगी, उनकी रुचि में परिवर्तन होगा। यदि रुचि परिवर्तन होगा। अच्छे कामों की ओर होती हैं तो आर्थिक कल्याण होगा, जैसे -पढ़ाई और बचत की रुचि बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बढ़ेगी, लेकिन यदि शराब पीने, जुआ खेलने की रुचि हो तो उन पर व्यय बढ़ाने से आर्थिक कल्याण कम होगा।
(3) यह देखना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ी ? यदि उत्पादन की वृद्धि से, प्रशासन के सुधार से राष्ट्रीय आय की वृद्धि हुई हो तो आर्थिक कल्याण अधिक होगा, लेकिन अगर यह श्रम का शोषण करके किया गया हो तो आर्थिक कल्याण में कमी होगी।
(4) राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ यदि जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से होती हैं तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जायगी और आर्थिक कल्याण अधिक होने की बजाय कम हो सकती हैं।
(5) यदि राष्ट्रीय आय स्थिर रहे और उसका वितरण बदल जाय तो हो सकता हैं कि आर्थिक कल्याण बढ़े या घटे। यदि राष्ट्रीय आय अधिक गरीबों को मिले तो निर्धन व्यक्ति अपनी आर्थिक अवस्था अच्छा बना सकते हैं और आर्थिक कल्याण अधिक होगा, लेकिन धन के वितरण से अमीरों को अधिक प्राप्ति हो और गरीब और गरीब हो जाय तो आर्थिक कल्याण कम हो जायेगा।
यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और उसका एक भाग गरीबों को अनुदान के रूप में दे दिया जाय और फिर राष्ट्रीय आय को बाँटा जाय तो आर्थिक कल्याण होगा।
राष्ट्रीय आय : तिमाही अनुमान, 2020-21
31 अगस्त, 2020 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के लिए स्थिर (2011-12) एवं वर्तमान (Current) दोनों मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान जारी किए गए।
वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में स्थिर (2011-12) मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपये हैं, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 35.35 लाख करोड़ रुपये रहा था।
इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत का संकुचन दिख रहा हैं, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का अनुमान 38.08 लाख करोड़ रुपये हैं, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 49,18 लाख करोड़ रुपये था।
इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 22.6 प्रतिशत का संकुचन दिख रहा हैं, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- विदेशी विनिमय दर निर्धारण माँग एवं पूर्ति सिद्धान्त | विदेशी विनिमय की माँग की लोच | विदेशी विनिमय दर के भुगतान शेष सिद्धान्त
- विनिमय नियंत्रण का अर्थ | विनिमय नियंत्रण के तरीके | बहुल विनिमय दरें | विनिमय नियंत्रण के अप्रत्यक्ष तरीके | विनिमय नियंत्रण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके
- मुक्त या स्वतंत्र व्यापार | स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क | संरक्षण का अर्थ | संरक्षण व्यापार के पक्ष में तर्क | सस्ते श्रम का तर्क | संरक्षित व्यापार के सम्बन्ध में शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या
- स्थिर बनाम लचीली विदेशी विनिमय दरें | परिवर्तनशील विदेशी विनिमय दरें | स्थिर और लोचशील विनिमय दर के गुण और दोषों
- विदेशी विनिमय दर | क्रय शक्ति समता सिद्धान्त का अर्थ एवं परिभाषा | क्रय शक्ति समता सिद्धांत | विनिमय दर निर्धारण के क्रयशक्ति समता सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- अवमूल्यन का अर्थ | अधिमूल्यन | अवमूल्यन के उद्देश्य एवं क्रियाविधि | अवमूल्यन के लोच विधि की सविस्तार व्याख्या
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]