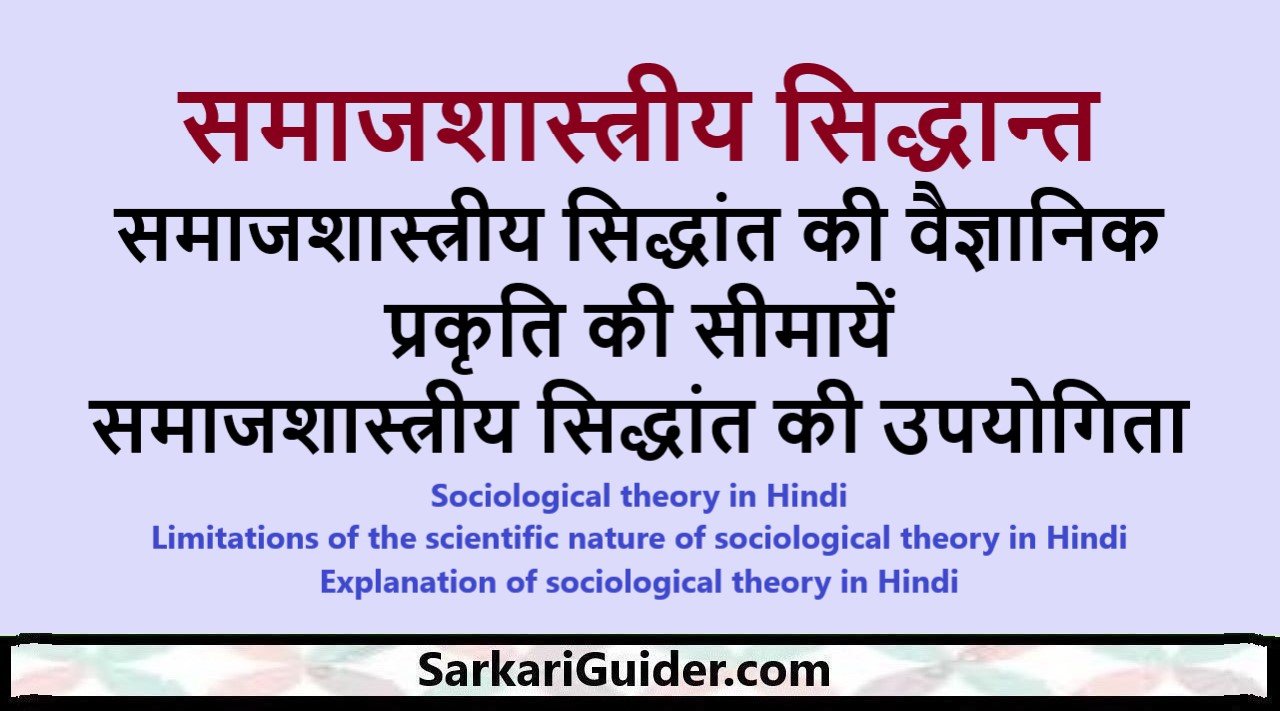समाजशास्त्रीय सिद्धान्त | समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमायें | समाजशास्त्रीय सिद्धांत की उपयोगिता
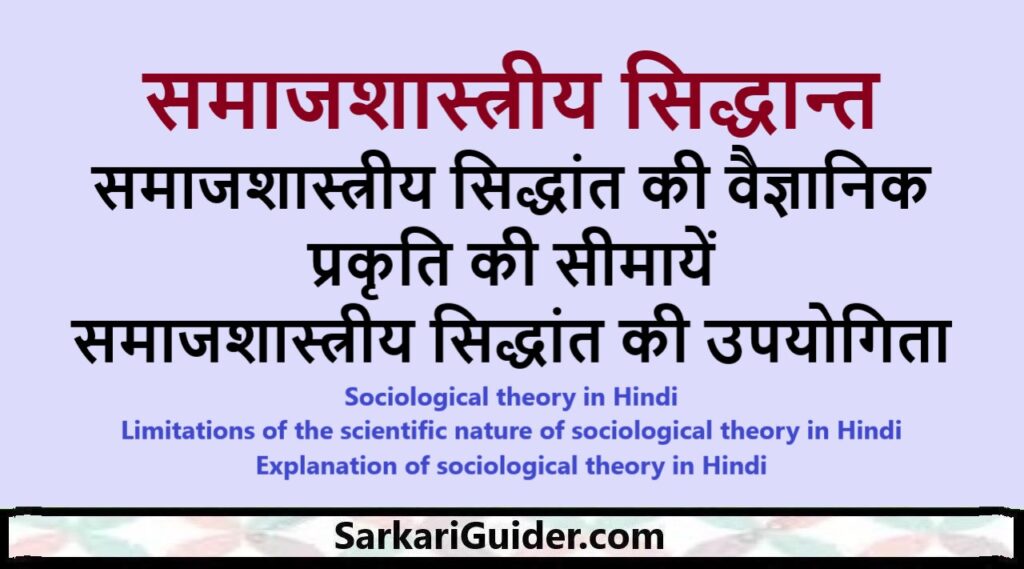
समाजशास्त्रीय सिद्धान्त | समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमायें | समाजशास्त्रीय सिद्धांत की उपयोगिता | Sociological theory in Hindi | Limitations of the scientific nature of sociological theory in Hindi | Explanation of sociological theory in Hindi
समाजशास्त्रीय सिद्धान्त
समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में लोगों के मन में गलत धारणायें भी हो सकती हैं। अतः मर्टन (R. K. Merton) के अनुसार, ‘समाजशास्त्रीय सिद्धांत’ शब्द (Term) समाजशास्त्रीय कहलाने वाले व्यावसायिक समूह के सदस्यों द्वारा किये गये परस्पर संबंधित किंतु स्पष्ट क्रिया-कलापों की उपजों को बतलाने के लिये किया जाता है। परंतु इन क्रिया-कलापों की सभी उपजों को समाजशास्त्रीय सिद्धांत मान लेना उचित न होगा क्योंकि इन क्रिया कलापों का वैज्ञानिक प्रकार्य एक- दूसरे से भिन्न हैं एवं प्रयोग सिद्ध सामाजिक शोध पर उनका प्रभाव भी अलग-अलग ही है। मर्टन ने आगे लिखा है कि प्रायः (1) अध्ययन पद्धति, (2) सामान्य समाजशास्त्रीय अभिविन्यास (3) समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का विश्लेषण (4) तथ्योत्तर समाजशास्त्रीय व्याख्यायें (5) समाजशास्त्र में आनुभाविक या प्रयोगसिद्ध सामान्यीकरण (6) समाजशास्त्रीय सिद्धांत इन छः प्रकार के कार्यों को एक साथ जोड़कर ‘समाजशास्त्रीय सिद्धांत’ (Sociological Theory) बना लिया जाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन में यह सब सहायक आधार हो सकते हैं पर यह सब स्वयं समाजशास्त्रीय सिद्धांत नहीं हैं, न ही अध्ययन पद्धति को समाजशास्त्रीय सिद्धांत कह सकते हैं।
तिमाशेफ (Timasheff) के अनुसार, समाजशास्त्रीय सिद्धांत निम्नलिखित समस्याओं के चारों ओर घूमते रहते हैं जिन्हें कि प्रश्नों के रूप में निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है।
(1) समाज क्या है? और संस्कृति क्या है?
(2) वे कौन-सी मौलिक इकाइयाँ हैं जिनके अंतर्गत समाज और संस्कृति का विश्लेषण किया जाना चाहिये?
(3) समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच अंतसंबंध क्या है?
(4) वे कौन से कारक हैं जो एक समाज या एक संस्कृति की दशा को निर्धारित करते हैं अथवा समाज या संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को निर्धारित करते हैं?
(5) समाजशास्त्र क्या है? और उसकी उपयुक्त पद्धतियाँ क्या हैं? जब किसी एक सिद्धांत को प्रस्तुत करना होता है तो उपर्युक्त समस्याओं (Problems) के अतिरिक्त भी अन्य अनेक समस्यायें एक सी निकल आती हैं जिन्हें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है किंतु इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रायः एक पौधे की भाँति विकसित होता है। इस पौधे की कुछ शाखायें तो अपनी अनेक उपशाखाओं या टहनियों के रूप में शीघ्र ही या कुछ विलम्ब से आगे बढ़ गयी हैं जबकि दूसरी शाखायें या तो पनप नहीं सकीं या फिर गायब ही हो गयी हैं। इतना ही नहीं इन शाखाओं का सहारा लेकर कुछ अन्य प्रकार की शाखायें भी विकसित हो गयीं फिर भी उन सभी में सामाजिक वास्तविकता झलकने के कारण वे सबकी सब पुनः एक दूसरे के निकट भी आ जाती हैं एवं एक-दूसरे के साथ घुल-मिल भी जाती हैं। इसी कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वास्तविक प्रकृति समझना एक कठिन कार्य है।
समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमायें
(Limitations of the Scientific Nature of Sociological Theory)
पी.एस. केहन (P.S. Cahan) के अनुसार, ‘ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से समाजशास्त्रीय सिद्धांत विज्ञान की आदर्श कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। ये कारण अर्थात समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमायें (Limitations) अग्रलिखित हैं-
(1) कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांत विश्लेषणात्मक सिद्धांतों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं और इसलिये उनका आनुभविक परीक्षण संभव नहीं होता। इसी प्रकार एक सिद्धांत यह कहता है कि एक सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंग आवश्यक रूप से अंतः निर्भरशील है। इस सिद्धांत को सच होना भी चाहिये क्योंकि यदि एक सामाजिक व्यवस्था का एक अंग दूसरे किसी भी अंग को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता तो उसे व्यवस्था का अंग नहीं माना जा सकता। इसलिये इतना कह देना कि सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंग अंतः निर्भरशील हैं किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं करता। परंतु यदि उन अवस्थाओं के विषय में बताया जाये जिनके अंतर्गत अंतः निर्भरता की विभिन्न, मात्रायें पायी जायेगी तो वह सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत के अधिक निकट होगा।
(2) बहुत से समाजशास्त्रीय सिद्धांत न तो शुद्ध सार्वभौमिक कथन होते हैं और न ही तथ्य के कथन। उदाहरणार्थ उस सिद्धांत को ही लीजिये जिसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था सामान्य मूल्यों को स्वीकार कर लेने पर आधारित है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाता है कि, ‘कोई भी सामाजिक व्यवस्था सामान्य मूल्यों को स्वीकार किये बिना पनप ही नहीं सकती, तो उस कथन का वास्तव में एक सार्वभौमिक स्वरूप होता है परंतु उपर्युक्त सिद्धांत में तो केवल इतना ही कहा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था सामान्यतया इस बात पर निर्भर करती है कि सामान्य मूल्यों को स्वीकार कर लिया जाये क्योंकि किसी भी व्यवस्था के लिये शक्ति दीर्घकालीन आधार नहीं बन सकता किंतु यदि उस व्यवस्था के संबंध में यह कह सकें कि जिसके अंतर्गत मतैक्य अवस्था को उत्पन्न करता है अथवा वे अवस्थाये जिनके अंतर्गत मूल्य का अभाव अवस्था को उत्पन्न करने में असफल होता है तो यह सिद्धांत सार्वभौमिक हो जायेगा।
(3) बहुत से समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का परीक्षण इसलिये भी कठिन होता है क्योंकि वे कुछ ऐसे अस्पष्ट विधान देते हैं जिनका कि दृढ़ता पूर्वक परीक्षण संभव नहीं होता है। उदाहरणार्थ, उस सिद्धांत को लीजिये जिसके अनुसार, ‘सभी औद्योगिक समाजों में वर्ग संघर्ष होता है।’ स्पष्ट है कि इस सिद्धांत को इतना सामान्य व अस्पष्ट स्वरूप प्रदान किया गया है कि उसका वैज्ञानिक आधार स्वतः ही नष्ट हो जाता है।
समाजशास्त्रीय सिद्धांत की उपयोगिता
उपयोगिता- समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित हैं-
(1) समाजशास्त्रीय सिद्धांत शोध करनेवाले शोधार्थियों का मार्गदर्शन करता है।
(2) यह उपकल्पनाओं के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है।
(3) आनुभाविक को समझने में सिद्धांत विशेष रूप से सहायता करता है।
(4) अवधारणाओं के विश्लेषण में सिद्धांत विशेष योगदान देता है।
(5) यह पैराडिम निर्माण में उपयोगी होता है।
(6) सिद्धांत तथ्य संकलन को उपयोगी बनाते हैं।
(7) समाजशास्त्रीय सिद्धांत न केवल आनुभविक अध्ययनों को निर्देशित करते हैं बल्कि समाजशास्त्र के सैद्धांतिक विकास में अपना योगदान देते हैं।
समाजशास्त्र / Sociology – महत्वपूर्ण लिंक
- आर. के. मर्टन का संदर्भ समूह सिद्धांत | आर. के. मटन के संदर्भ समूह व्यवहार एवं सापेक्षिक अभाव बोध के सिद्धांत की विवेचना
- ईथनो पद्धति में गारफिंकल का योगदान | लोक विधि विज्ञान में हेराल्ड गारफिन्कल का योगदान
- लोक विधि विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएँ | नृजाति-पद्धति-शास्त्र की विशेषताएँ | लोक विधि विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ
- उत्तर संरचनावाद | उत्तर संरचनावाद की विशेषतायें | संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में अन्तर
- एंथोनी गिडिन्स का संरचनावादी परिप्रेक्ष्य | गिडिन्स का संरचनावादी परिप्रेक्ष्य
- सी. लेवी स्ट्रास का संरचनावाद | लेवी-स्ट्राउस के संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन | लेवी-स्ट्राउस का संरचनावादी परिप्रेक्ष्य | लेवी-स्ट्राउस के संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन
- सामाजिक संरचना | सामाजिक संरचना की परिभाषा | सामाजिक संरचना में प्रमुख विचारकों के विचार
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]