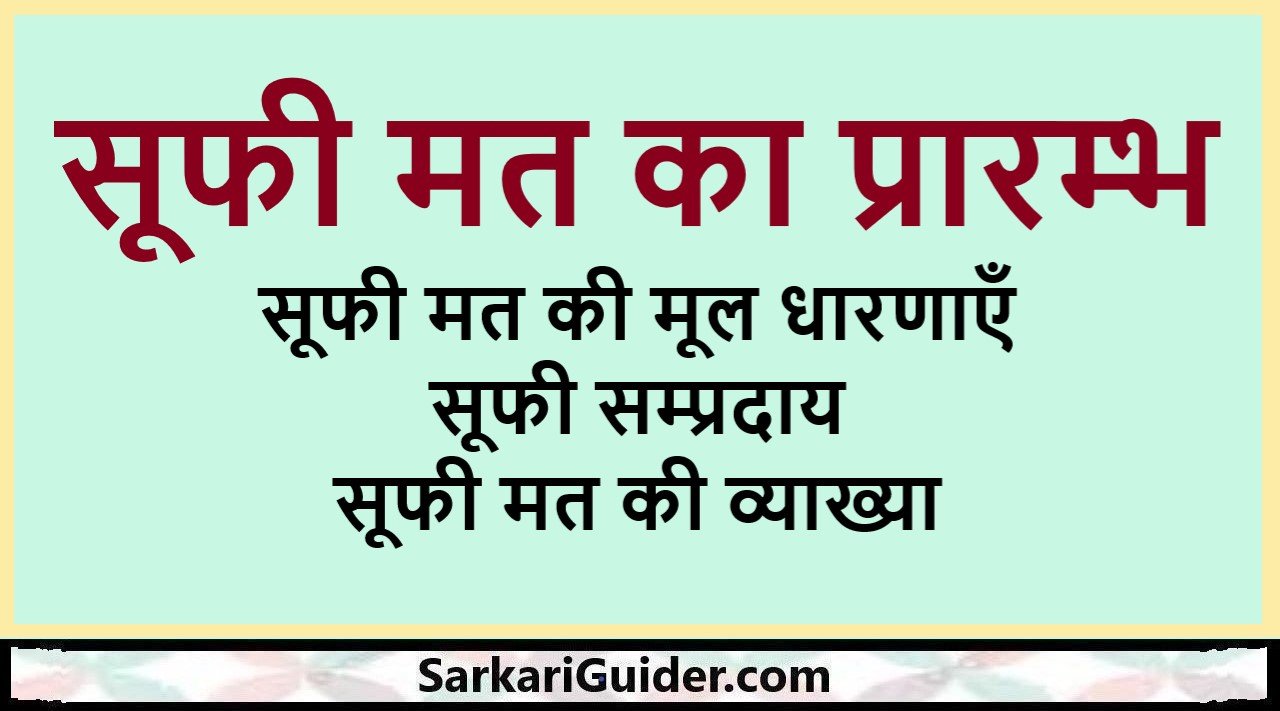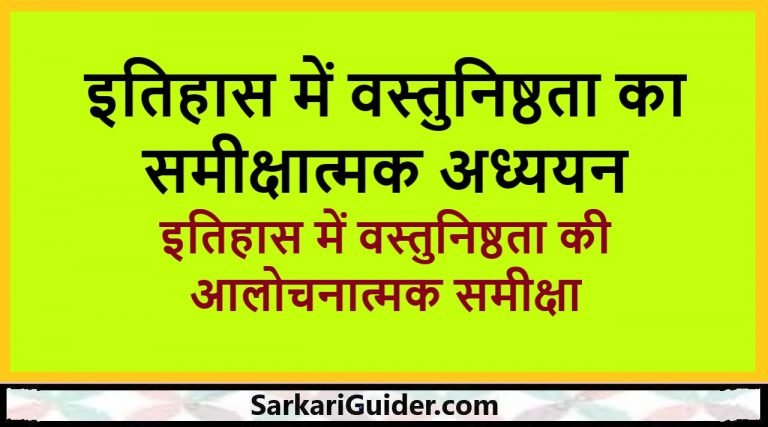सूफी मत का प्रारम्भ | सूफी मत की मूल धारणाएँ | सूफी सम्प्रदाय | सूफी मत की व्याख्या

सूफी मत का प्रारम्भ | सूफी मत की मूल धारणाएँ | सूफी सम्प्रदाय | सूफी मत की व्याख्या
सूफी मत का प्रारम्भ
दर्शन तत्व के पिपासु चिन्तक जो मस्जिदों के सूफों, अर्थात् बरामदों में रहते थे तथा पवित्रता के लिये सूफी (ऊनी) टोपी और लम्बा कुरता पहनते थे-सूफी कहलाने लगे। यद्यपि इस्लाम की आज्ञा थी कि खुदा और रसूल में ईमान रखो, परन्तु ईश्वर में विश्वास रखने वाले अनेक विचारक बन्दे और ख़ुदा (जीव और ब्रह्म) के सम्बन्धों पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करने लगे। कुरान शरीफ में कहा गया है कि अल्लाह-इन्सान से प्यार करता है और इन्सान भी अल्लाह से प्यार करे, परन्तु मुसलमानों ने उस समय में अपनी बल प्रयोग प्रवृत्ति तथा युद्धक स्वभाव के कारण हृदय से ईश्वर प्रेम करने की अपेक्षा खौफे खुदा (ईश्वरीय भय) का प्रतिपादन किया। हजरत मुहम्मद साहब ने यह कहा था कि वे अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं। बल्कि ईश्वर ने उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा दी है। मुहम्मद साहब पर हाल का आलम तारी होता था (अर्थात् वे भावावेश में आते थे) जिसके परिणामस्वरूप उनको ‘इलहाम’ (ईश्वरीय संकल्प) प्राप्त हुआ। सूफीमत के यही लक्षण थे। सूफी सन्तों ने इस्लाम धर्म के वास्तविक रूप को समझा। अपनी प्रेरणा तथा सिद्धान्तों में इस्लाम धर्म स्वयं में महान तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त था। सूफी सन्तों ने उसके वास्तविक रूप को उजागर करके मानवीय प्रेम तथा सहिष्णुता का प्रचार किया।
सूफी मत की मूल धारणाएँ
सूफियों की धारणा है कि समस्त विश्व का स्रोत खुदा है। वह प्रत्येक क्रिया तथा अर्थ में विराजमान है। उसी के द्वारा हृदय में संकल्प उत्पन्न होता है तथा उसकी इच्छा से ही सब कुछ होता है । सूफी मत में खुदा का तस्सवुर या ईश्वर की कल्पना अपने प्रियतम के रूप में की गई है। सूफी सन्त ईश्वर की निस्सीमता के गुण को ‘लाहूत’ कहते हैं। उनके अनुसार खुदा लामहमूद है अर्थात् वह अनन्त है। वह ‘लाइन्हा’ है। बन्दा महमूद है अर्थात् मनुष्य की सीमा है। इसे सूफी ना सूत’ की संज्ञा देते हैं। सूफियों के अनुसार जो रूह’ शरीर में कैद है वह पर कर ही स्वतन्त्र होती है तथा खुदा की हस्ती में वापस मिल जाती है। ऐसी मौत को गले लगाने में ही सन्तुष्टि मिलती है। खुदा की अलौकिकता से प्रेम करने में तर्क बाधा डालता है। सूफियों का विचार है कि तर्क और बुद्धि की अपेक्षा मनुष्य की हार्दिक भावना प्रभु मिलन में अधिक सहायक होती है। दूसरे शब्दों में सूफियों की धारणा यह है कि ‘निजात’ (मुक्ति) की प्राप्ति प्रेम द्वारा होती है। प्रेम सौन्दर्य से उत्पन्न होता है। खुदा सौन्दर्य की पराकाष्ठा है। जब खुदा पूछता है कि ‘क्या तुमने प्यार किया ?’ तो यदि उत्तर ‘न’ में रहे, तो अल्लाह आदेश देते हैं कि जाओ, वापस जाओ। पहले प्यार करो।’ इसी कारण से सूफी ‘इश्क लजाजी’ को ‘इश्क हकीकी’ की पहली सीढ़ी मानते हैं।
प्रेम ही खुदा है तथा वह प्रेम करने वालों से प्रेम करता है। प्रेम और खुदा में कोई अन्तर नहीं है। प्रेमी जन मौला रहते हैं और दिलों में याद करते हैं।
वैसे तो खुदा ने सभी को बराबर-बराबर प्यार दिया है परन्तु विषयानुराग में लिप्त कई बन्दे उसे पहचान नहीं पाते। उनके मन आसक्ति, ममता और अहंकार के पर्दे से ढंके रहते हैं। इस पर्दे को हटाकर, भगवान के प्यार के लिये व्याकुल होना तथा उसी पर निर्भर रहना ही जीवन का आधार तथा उद्देश्य है। पूर्णरूप से समर्पित तथा निष्काम चाह द्वारा ही ‘वस्त’ या प्रभु मिलन हो सकता है। सूफियों के अनुसार जैसे, प्यार किया नहीं, हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम चाह को नहीं जाती, हो जाती है।
सूफी मत के अनुसार प्रेम की चार स्थितियाँ होती हैं-
(1) शरीयत (The Law)- धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करना।
(2) तरीकत (The Way)- अल्लाह के ध्यान में लगे रहना तथा अपने मनोबल की वृद्धि करना।
(3) हक़ीकत (The Truth)- ज्ञान से परिचय पाना । इसके सात सोपान हैं-तौबा, जैहद, सब्र, शुक्र, रिजा, तवुक्कल और रजा।
(4) मारिफत (Merging in the Absolute)- खुदा के अलावा और कुछ नहीं चाहने की अनुभूति तथा उसी में लीन हो जाना। इस वज्द के आलम (प्रेम में मग्न) में मुरीद (साधक) अपना होशोहवास खो बैठता है। यह कोई क्रिया नहीं है, वरन् अपने आप ही ऐसा हो जाता है।
सूफी सम्प्रदाय
सूफी मत इस्लाम धर्म से सम्बन्धित है, तथा इसी के लगभग प्राचीन भी है। इस सम्प्रदाय का भारत में विशेष प्रचार तथा प्रसार हुआ। सूफी सम्प्रदाय की चार प्रमुख शाखाएं हैं-
(1) चिश्तिया सम्प्रदाय- भारत में इस सम्प्रदाय के संस्थापक पीर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (1143-1236 ई०) थे। इनका साधना स्थल अजमेर था। इनकी मजार भी वहीं पर है। अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया इसी चिश्ती परम्परा में हुए थे। बाबा फरीदुद्दीन शक्कर गंज, शेख नासिरुद्दीन, चिराग देहलवी, ख्वाजा सैय्यद मोहम्मद गेसुदराज इसी सम्प्रदाय के सन्त थे। इसी सम्प्रदाय के शेख सलीम चिश्ती की कृपा से अकबर को पुत्ररत्न प्राप्त हुआ था।
(2) सुहरावर्दी सम्प्रदाय- इस सम्प्रदाय के संस्थापक जियाउद्दीन अबुलजीव थे। भारत में इस सम्प्रदाय का प्रचलन शेख बहाउद्दीन जकारिया (1169-1266ई०) ने किया था।
(3) कादरी- शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी ने कादरी सम्प्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद गौस गिलानी, मखदूम जालानी तथा शेख मीर मोहम्मद इसी सम्प्रदाय के अनुयायी थे।
(4) नक्शबंदी- इस सम्प्रदाय का प्रचलन ख्वाजा बहादुद्दीन नक्शबन्दी ने तुर्किस्तान में किया था। भारत में इस सम्प्रदाय का प्रचार सत्रहवीं शती ई० में हुआ।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- वैष्णव धर्म के सिद्धान्त | विष्णु के अवतारों की विवेचना | वैष्णव धर्म के सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए विष्णु के अवतारों की विवेचना
- बौद्ध तथा हिन्दू धर्म का तुलनात्मक अध्ययन | बौद्ध धर्म तथा हिन्दू धर्म की तुलना कीजिए | Compare Buddhism with Hinduism in Hindi
- बौद्ध तथा जैन धर्म का तुलनात्मक विवरण | बौद्ध तथा जैन धर्म की समानताएँ | बौद्ध तथा जैन धर्म की असमानतायें | बौद्ध तथा जैन धर्म की तुलना कीजिये | Compare Buddhism with Jainism in Hindi
- हिन्दू समाज को शंकराचार्य की देन | शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन | शंकराचार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी | हिन्दू समाज के लिए शंकराचार्य का योगदान
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]