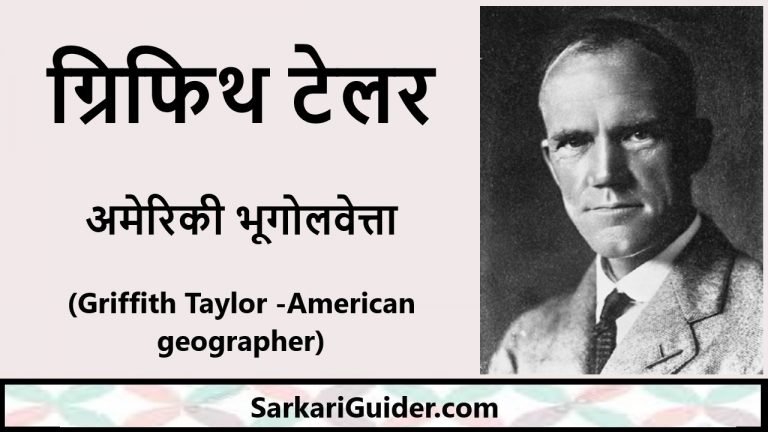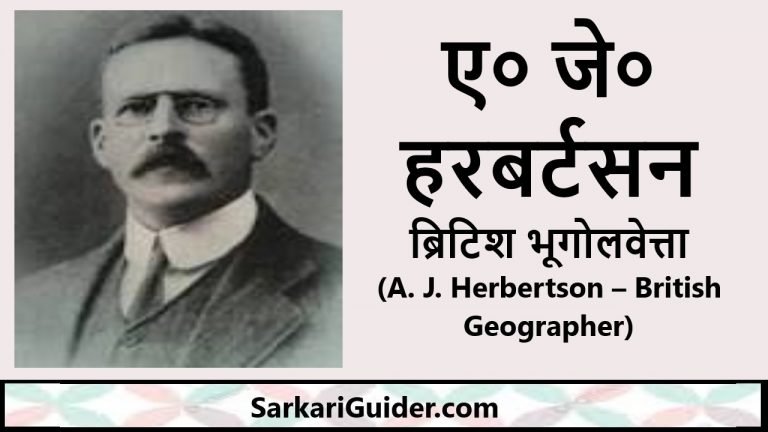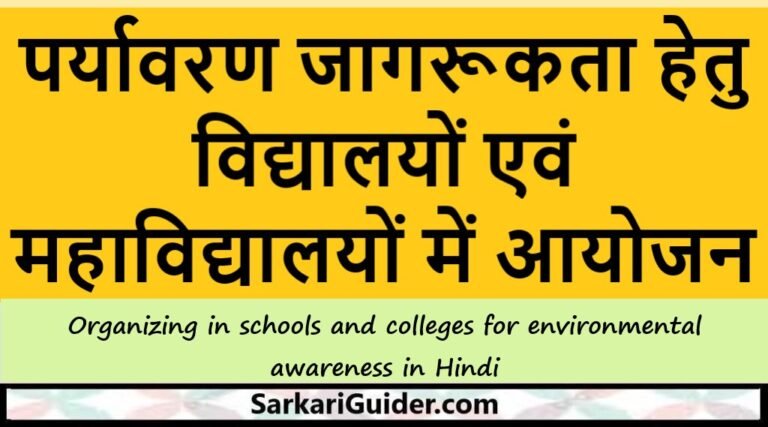थारू जनजाति | थारू जनजाति के आर्थिक तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति का वर्णन
थारू जनजाति | थारू जनजाति के आर्थिक तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति का वर्णन
थारू जनजाति
निवास क्षेत्र (Habitat) –
थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तराई और भाबर की संकीर्ण पट्टी का प्रदेश है, जो कुछ पूर्व के विहार के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यह संकीर्ण पट्टी केवल 25 किमी. चौड़ी है, पर लम्बाई में यह लगभग 600 किमी. है, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के सहारे-एसहारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामगंगा कीछा, शारदा, घाघरा, राप्ती, गण्डक तथा कोसी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलकर मैदान को जाती हुई इस भाबर-तराई की संकरी पेटी को पार करती हैं।
थारू प्रदकश का मुख्य भाग नैनीताल जिले में कीछा, खटीमा, रामपुरा, सितारगंज, नानकमत्ता, बनवासा आदि क्षेत्र हैं। आगे की ओर उत्तर प्रदेश में जिला पीलीभीत, खीरी से लेकर बिहार में जिला मोतीहारी तक के उत्तरी भाग में थारू लोगों की निवास पेटी है।
थारू नाम की उत्पत्ति-
‘थारू’ शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के कई मत है। किन्हीं का मत है कि ये अथर्ववेद से सम्बन्धित हैं, पहले इनका नाम ‘अथरू’ था, बाद में थारू हो गया। ‘थारू’ शब्द का अर्थ है, ठहरे हुए; इस मलेरिया और मच्छरों की भावर-तराई पेटी में भी ये लोग अपने जीविका-निर्वाह और निवास के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए ठहरे रहे हैं; इसलिये इनका नाम थारू हो गया है। मन्दिर को भी ‘थार’ कहते हैं, ये लोग अपने द्वारा तैयार की गयी एक प्रकार की मदिरा (थार) पीते है; इसलिये इनको थारू कहा जाता है। थारू लोगों में विवाह की कई प्रथाएँ है; उनमें एक प्रथा वधू-अपहरण भी है। इस अपहरण प्रथा का नाम ‘थारू’ है, अतः इस कारण भी इन लोगों को थारू नाम दिया जाता है।
भौतिक वातावरण-
शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में भावर की संकीर्ण पेटी है; जो दक्षिण की ओर तराई की पेटी बन जाती है। छोटी-छोटी जल धाराएँ, जो वर्षा काल में शिवालिक पहाड़ियों से बहकर आती हैं, वे भावर पेटी में आकर भूमि के बजरीयुक्त ऊपरी धरातल से नीचे ही बहती हुई तराई की पेटी में पनुः ऊपरी धरातल पर बहती हैं जहाँ भूमि मैदान है। इसी कारण से इस प्रदेश की मिट्टी में तराई अधिक रहती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गण्डक, कोसी आदि नदियों में वर्षाकाल में बातें आती हैं, जिनके कारण तराई की पेटी में बाढ़ के दिनों में जल फैल जाता है। इन बाद क्षेत्रों के बीच-बीच में ऊँची भूमि जहाँ-तहाँ तलछट के टीले हैं। बहुत-सी भूमि दलदली है।
जलवायु मानसूनी है। ग्रीष्मकाल में तापमान 38° सेग्रे से 440 सेये तक रहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा 125 से 150 सेमी तक रहता है, जो अधिकांशतः जुलाई से सितम्बर तक होता है। ऊंचे तापमान, वर्षा और वायुमण्डल में आर्द्रता के ज्यादा होने से इस प्रदेश में मानसूनी वनः जैसे-साल, शीशम, तुन, हल्दू, तेंदू, सैमल, खैर, बरगद आदि के वृक्ष और लम्बी घास उत्पन्न होती है। अधिक तराई ऊँची आर्द्रता और दलदली भूमि के वातावरण में मच्छर उत्पन्न होते हैं, जो मलेरिया फैलाते है।
शीतकाल में तापमान गिरकर लगभग 120 सेग्रे से 150 सेग्रे तक रहता है। शीतकालीन वर्षा केवल 5 सेमी तक होती है। मानसूनी वन और लम्बी घास की प्राकृतिक वनस्पति में चीता, तेंदुआ, भेड़िया, हिरन, सियार, सूअर, लकड़बग्घा आदि जन्तु रहते हैं।
सामान्यतः जलवायु स्वास्थ्य के लिए कुछ हानिकारक है, परन्तु भारत में स्वतन्त्रता के बाद से इस प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। काँस और मूँज जैसी लम्बी घासों को काटकर कृषि के फार्म बनाये जाते हैं, दलदलों के जल को छोटी नहरों में बहाया गया है; काँस और मूँज को कागज बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और मलेरिया पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
भोजन-
थारू लोगों का भोजन चावल का भात, मछली, दाल, भैंस-गाय का दूध-दही और जंगल में आखेट किये हुए जन्तुओं का माँस है। चावल को उबाल कर भात बनाकर खाते हैं और भून कर चबाते भी मक्का की रोटी भी खाते हैं। शाक, मूलीश गाजर तथा आलू भोजन में सम्मिलित हैं। नदियों और तालाबों से मछलियाँ प्राप्त होती हैं, जो भोजन में मुख्यतः सम्मिलित रहती हैं। भोजन के बर्तनों में ताँबे, पीतल और मिट्टी के पात्र तथा लोहे के तवे, कड़ाहियाँ आदि होते हैं।
वस्त्र-
पुरुषों की पोषाक धोती, कुर्ता, टोपी है। कुछ लोग सिर पर बड़े बाल रखते हैं। स्त्रियों की पोशाक धोती और छोटी अंगरखी है। स्त्रियों में चाँदी के आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। हाथों और पैरों में चाँदी के कड़े, भुजाओं पर बाजूबन्द, नाक में नथ और गले में रंगीन मूँगों की मालाएँ तथा गुलूबन्द पहनती हैं। सिर के बालों का जूड़ा नहीं बाँधती, वरन् पीछे लम्बी चोटी की तरह लटकाती हैं।
घर-
थारू लोगों के घर अधिकतर मिट्टी की कच्ची ईटों, बाँस छप्पर के बने होते हैं। मकानों की दीवारों को प्रायः गोबर से लीपते हैं। कुछ लोग लकड़ी जलाकर पकाई हुई ईटों का भी प्रयोग करते हैं। गरीब लोगों के मकानों की दीवारें घास-फूंस की टट्टियों और बांसों की बनाई जाती हैं। ये लोग, भैंस, गाय, पशुओं को प्रायः खललगा है। काँस और मूँज जैसी लम्बी घासों को काटकर कृषि के फार्म बनाये जाते हैं; दलदली के जल को छोटी नहरों में बहाया गया है; काँस और मूंज को कागज बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और मलेरिया पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
घर में सोने-बैठने के कमरे को ही अनाज, अनाज आदि के कोठार की तरह प्रयोग किया जाता है। रसोई के लिए छोटा दालान सा होता है। घर के बाहरी भाग में आँगन होता है। थारू लोग चाहे स्वयं कुछ गन्दे रहें, परन्तु अपने मकानों और गायों के स्थानों को बहुत साफ रखते हैं। प्रायः प्रत्येक घर में एक कमरा बैठक के रूप में ऐसा होता है जिसमें मेहमानों को ठहराते हैं या विवाह, उत्सव, त्यौहार आदि के समय उसका प्रयोग करते हैं।
आर्थिक उद्योग-
मुख्य व्यवसाय स्थायी कृषि है। थारू लोग चावल उत्पादन में बड़े निपुण हैं। यद्यपि अपरदन (erosion) द्वारा मिट्टी कअकर बहती है, फिर भी ये लोग खेतों की मेढ़ें बनाकर अपरदन रोकते हैं और गोबर की खाद से भूमि की उर्वरता को बनाये रखते हैं। खेतों को जोतने का काम पुरुष करते हैं। निराई (weeding), कटाई (harvesting) आदि कार्य स्त्रियाँ करती है। बोने के मौसम में धान की रोपाई के लिए स्त्रियों को जल से भरे खेतों में या कीचड़युक्त खेतों में प्रायः दिन भर रहना पड़ जाता है, जिस कारण से उनके पैरों की अंगुलियाँ गल सह जाती है, हाथों की अंगुलियों के नाखून भी गले हुए से हो जाते हैं।
कृषि की अन्य फसलों में थोड़ी सी मक्का, मूली, गाजर, आलू, शाक-सब्जियाँ आदि हैं। सरसों की खेती भी होती है, जिससे तेल प्राप्त हो जाता है। ये लोग माँस के लिए सूअर और दूध के लिए गाय-भैंस पालते हैं।
नेपाल और गोरखपुर के मध्य भाग में रहने वाले थारू लोग आखेट करते हैं और कृषि भी करते हैं, जिसमें चावल मुख्य उपज है। आखेट द्वारा प्राप्त हुए पशुओं में चर्म, हड्डियाँ, सींग, माँस आदि की बिक्री के लिए नेपाल तथा भारत दोनों देशों में तैयार बाजार रहता है। इस विक्री के बदले में वस्त्र, तम्बाकू, नमक, टार्च, बन्दूकें आदि वस्तुएँ मोल लेते हैं। पश्चिमी कुमाऊँ की तराई में और गढ़वाल की दक्षिणी तराई में रहने वाले वोक्षा (भोकसा) थारू लोग भी आखेटक हैं; वे कृषि के साथ-साथ सूअर पालने और गाय-भैंस पालने का उद्यम भी करते हैं।
रीति-रिवाज-
थारू लोगों के 3 मुख्य वर्ग हैं-
- कुमाऊँ के तराई क्षेत्र में रहने वाले थारू मुख्यतः कृषक हैं।
- नेपाल-भारत की सीमा के क्षेत्र में रहने वाले ‘थारू’ प्रायः चलवासी कृषक और आखेटक हैं।
वर्तमान काल में शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। छोटे उद्यमों और दस्तकारियों की शिक्षा पर वल दिया जा रहा है।
भूगोल – महत्वपूर्ण लिंक
- अधिवास के प्रकार | ग्रामीण अधिवास प्रकार | ग्रामीण अधिवासों के मुख्य लक्षण | विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों की उत्पत्ति और विकास
- ग्रामीण अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास के उत्तरदायी कारक | ग्रामीण अंधिवासों का विश्व वितरण | ग्रामीण अंधिवासों का विश्व वितरण
- बुशमैन जनजाति | ‘बुशमैन’ जनजाति की प्रजातीय विशेषताएँ | बुशमैन के निवास्य क्षेत्र | बुशमैन के अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन
- मसाई जनजाति | मसाई जनजाति का क्षेत्र | मसाई जनजाति के सामाजिक जीवन का वर्णन
- सेमांग जनजाति | सेमांग जनजाति के आवास | सेमांग जनजाति के आर्थिक तथा सामाजिक संगठन
- मानव प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण | विश्व की प्रमुख प्रजातियाँ | कालेशियन प्रजाति की प्रमुख विशेषता
- मध्य गंगा मैदान के अधिवासों के प्रतिरूप | मध्य गंगा मैदान के मकानों के प्रकार | मध्य गंगा मैदान के अधिवासों पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव
- गद्दी जनजाति | गद्दी जनजाति के निवास क्षेत्र तथा अर्थ व्यवस्था का वर्णन | गद्दी जनजाति के समाज का वर्णन
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]